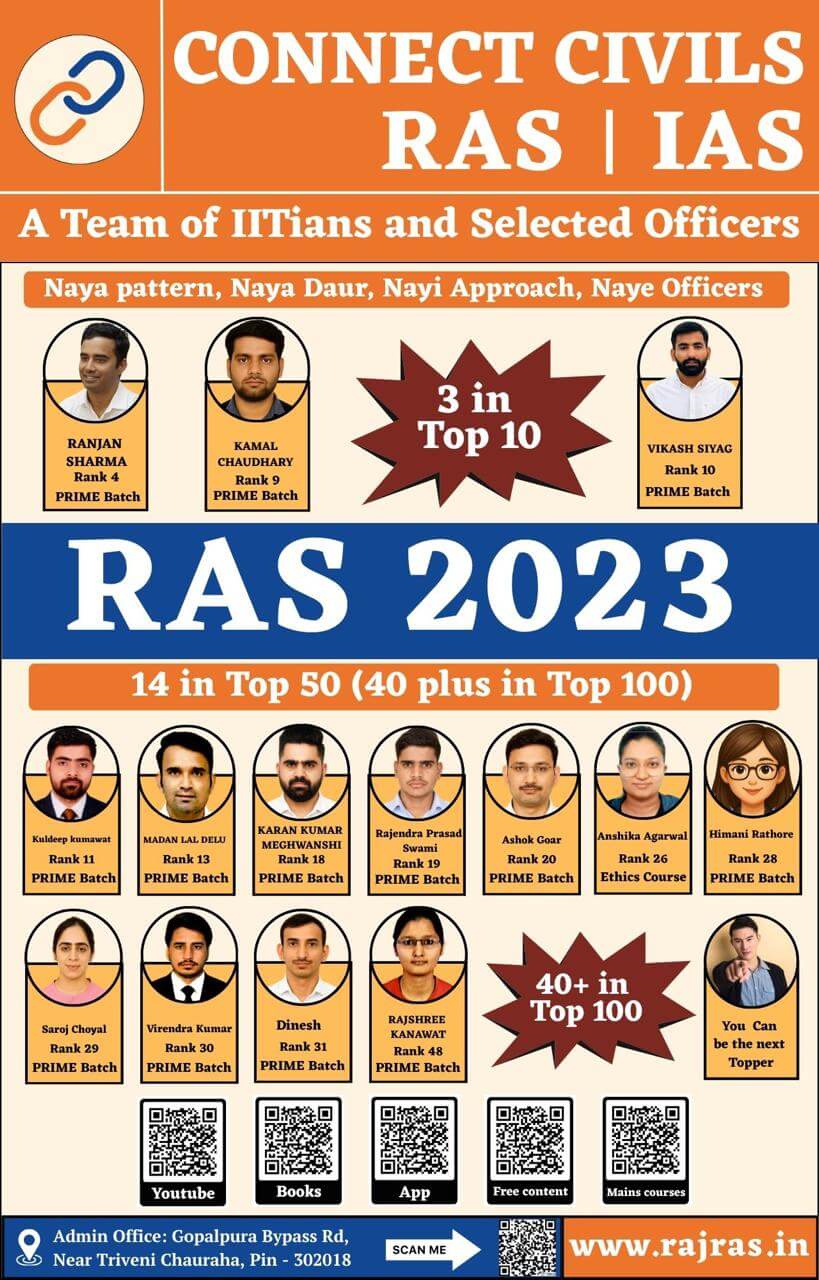एंडेमिक एपिडेमिक पैनडेमिक रोग उनके निदान और नियंत्रण जीवविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलाव के स्तर और उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इन रोगों की पहचान, निदान और नियंत्रण के उपाय समाज को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने में अत्यंत आवश्यक भूमिका निभाते हैं।
स्थानिक रोग (Endemic Diseases)
- परिभाषा: एक स्थानिक रोग वह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या आबादी में लंबे समय तक लगातार मौजूद रहता है। इन रोगों की घटनाओं की दर उस क्षेत्र या आबादी में अपेक्षाकृत स्थिर बनी रहती है।
- घटना: स्थानिक रोग समय के साथ लगातार होते हैं और इनके मामलों की संख्या पूर्वानुमानित व स्थिर होती है।
- उदाहरण: उप-सहारा अफ्रीका में मलेरिया, और चेचक (चिकनपॉक्स) उच्च प्रसार वाले क्षेत्रों में स्थानिक रोगों के उदाहरण हैं।
- रोगजनक प्रकार: स्थानिक रोग पैदा करने वाले रोगजनक अक्सर उस क्षेत्र के स्थानीय जलाशयों या वैक्टर (जैसे मच्छर) में मौजूद रहते हैं।
ये रोग मौसमी या पर्यावरणीय हो सकते हैं, लेकिन पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलाव न होने तक व्यापक प्रकोप नहीं फैलाते। - संचरण: स्थानिक रोग आमतौर पर स्थानीय स्तर पर फैलते हैं और इनमें मलेरिया जैसे रोगों में वैक्टर (मच्छर) शामिल हो सकते हैं।
संचरण आबादी में निरंतर होता है, और समय के साथ आंशिक प्रतिरक्षा विकसित हो सकती है। - मानव प्रतिरक्षा: चूंकि ये रोग आबादी में लगातार मौजूद रहते हैं, स्थानीय लोगों में बार-बार संपर्क के कारण आंशिक प्रतिरक्षा विकसित हो सकती है।
- अवधि: स्थानिक रोग लंबे समय तक मौजूद रहते हैं, जिनमें संक्रमण की दर स्थिर या पूर्वानुमानित होती है।
- भौगोलिक प्रसार: ये रोग रोगजनक के प्राकृतिक जलाशय या वैक्टर के कारण विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं।
उदाहरण: मलेरिया मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। - निदान: स्थानिक रोगों का निदान नैदानिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जिसकी पुष्टि प्रयोगशाला परीक्षणों या दीर्घकालिक महामारी विज्ञान निगरानी से होती है।
- नियंत्रण उपाय: टीकाकरण, वैक्टर नियंत्रण (मलेरिया जैसे रोगों में), स्वच्छता में सुधार, निरंतर जन स्वास्थ्य शिक्षा। अक्सर, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के पास इन रोगों के दीर्घकालिक प्रबंधन की रणनीतियाँ होती हैं।
- प्रभाव: स्थानिक रोगों का प्रभाव महामारियों या महामारियों की तुलना में कम होता है, क्योंकि इनकी घटनाएँ स्थिर होती हैं और नियंत्रण उपाय स्थापित होते हैं।
महामारी रोग (Epidemic Diseases)
- परिभाषा: एक महामारी (Epidemic) किसी विशिष्ट क्षेत्र या आबादी में किसी रोग के मामलों में अचानक और असामान्य वृद्धि को कहते हैं, जो सामान्य अपेक्षा से कहीं अधिक होती है। यह तब होता है जब कोई संक्रामक एजेंट तेजी से फैलता है या उसकी रोग उत्पन्न करने की क्षमता (virulence) बढ़ जाती है।
- घटना: महामारियाँ रोग के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि से पहचानी जाती हैं।
ये अल्पकालिक (कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक) हो सकती हैं, जो रोगजनक और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।
उदाहरण: इन्फ्लुएंजा (फ्लू) के प्रकोप और हैजा (cholera) के प्रकोप महामारी के सामान्य उदाहरण हैं। - रोगजनक प्रकार: महामारियाँ अक्सर रोगजनकों के नए उपभेदों (strains) या उत्परिवर्तनों (mutations) के कारण होती हैं, जिनसे उनकी संक्रामकता या रोग उत्पन्न करने की क्षमता (virulence) बढ़ जाती है।
- संचरण: ये रोग परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में तेजी से फैल सकते हैं।
मानव-से-मानव संचरण खराब स्वच्छता या भीड़भाड़ वाली रहन-सहन की स्थितियों से और बढ़ सकता है। - मानव प्रतिरक्षा: आबादी में नए या उत्परिवर्तित रोगजनक के प्रति कोई या बहुत कम प्रतिरक्षा होती है, जिससे रोग तेजी से फैलता है।
- अवधि: महामारियाँ आमतौर पर महामारियों (pandemics) की तुलना में कम अवधि की होती हैं, लेकिन कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक चल सकती हैं।
- भौगोलिक प्रसार: ये आमतौर पर किसी विशिष्ट देश, राज्य या शहर तक सीमित होती हैं।
उदाहरण: हैजा के प्रकोप अक्सर खराब स्वच्छता या असुरक्षित पेयजल वाले स्थानीय क्षेत्रों में होते हैं। - निदान: लक्षणों (जैसे दस्त, बुखार) के आधार पर शुरुआती निदान किया जाता है।
- प्रयोगशाला परीक्षणों (जैसे मल संवर्धन – हैजा, PCR और सीरोलॉजिकल टेस्ट) से पुष्टि की जाती है।
- नियंत्रण उपाय:
- क्वारंटाइन
- संपर्क अनुरेखण (contact tracing)
- टीकाकरण (इन्फ्लुएंजा जैसे रोकथाम योग्य रोगों के लिए)
- एंटीमाइक्रोबियल उपचार
सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों का त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय फैलाव को सीमित करने के लिए आवश्यक है।
- प्रभाव: रोग की प्रकृति, नियंत्रण उपायों की उपलब्धता और स्वास्थ्य अधिकारियों की प्रतिक्रिया की दक्षता के आधार पर महामारी का प्रभाव मध्यम से उच्च तक हो सकता है।
महामारिक रोग (Pandemic Diseases)
- परिभाषा: एक महामारिक (Pandemic) एक ऐसी बीमारी का प्रकोप है जो वैश्विक स्तर पर होता है और कई देशों या महाद्वीपों की आबादी को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर किसी रोगजनक के नए उपभेद (strain) के कारण होता है, जिसके प्रति अधिकांश आबादी में कोई प्रतिरक्षा नहीं होती।
- घटना: महामारिक तब होते हैं जब कोई बीमारी विश्व स्तर पर फैलती है और बड़ी आबादी को प्रभावित करती है।
ये दुर्लभ होते हैं लेकिन वैश्विक स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डालते हैं।
उदाहरण:- COVID-19 (SARS-CoV-2 वायरस के कारण)
- H1N1 इन्फ्लुएंजा (स्वाइन फ्लू)
- 1918 की स्पैनिश फ्लू
- रोगजनक प्रकार: महामारिक आमतौर पर नए रोगजनकों या वायरसों के उत्परिवर्तित उपभेदों (जैसे COVID-19 के लिए SARS-CoV-2) के कारण होते हैं, जिनके प्रति आबादी में कोई प्रतिरक्षा नहीं होती।
- संचरण: ये रोग तेजी से फैलते हैं, अक्सर मानव-से-मानव संपर्क के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और वैश्वीकरण ने महामारिकों को सीमाओं के पार फैलाने में योगदान दिया है।
- मानव प्रतिरक्षा: चूंकि रोगजनक अक्सर नया या उत्परिवर्तित होता है, लोगों में इसके प्रति कोई प्रतिरक्षा नहीं होती, जिससे व्यापक संचरण होता है। इसके परिणामस्वरूप संक्रमणों की संख्या अधिक हो सकती है और मृत्यु दर भी उच्च हो सकती है।
- अवधि: महामारिक आमतौर पर लंबे समय तक चलते हैं, जो महीनों से लेकर वर्षों तक हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़े क्षेत्रों में फैल सकते हैं और संक्रमण की कई लहरें शामिल हो सकती हैं।
- भौगोलिक प्रसार: एक महामारिक कई देशों या महाद्वीपों को प्रभावित करता है, अक्सर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और आवाजाही के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलता है।
- निदान: नैदानिक मूल्यांकन और प्रयोगशाला परीक्षणों (जैसे SARS-CoV-2 के लिए PCR) द्वारा पुष्टि की जाती है।
WHO जैसी वैश्विक स्वास्थ्य निगरानी प्रणालियाँ महामारिक रोगों के प्रसार को ट्रैक करने में महत्वपूर्ण हैं। - नियंत्रण उपाय:
- अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध
- बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान
- सामाजिक दूरी (social distancing) और मास्क पहनना
- बड़े पैमाने पर परीक्षण
- सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियाँ उपचार और नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती हैं।
- प्रभाव: महामारिक वैश्विक स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं।
स्वास्थ्य प्रणालियाँ अभिभूत हो सकती हैं, जीवन की महत्वपूर्ण हानि हो सकती है, और आर्थिक मंदी व सामाजिक व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं।
रोग निदान एवं जैविक तंत्र
- स्थानिक रोग:
- निदान प्रायः दीर्घकालिक अध्ययनों और निगरानी पर निर्भर करता है ताकि रोग की घटनाओं का पता लगाया जा सके। रक्त स्मीयर (मलेरिया) और मल संवर्धन (टाइफाइड बुखार) जैसे नैदानिक परीक्षण संक्रमण की पुष्टि करने में मदद करते हैं।
- उदाहरण: शिस्टोसोमायसिस, जो Schistosoma जाति के परजीवी कृमियों के कारण होता है, मूत्र या मल में अंडों की पहचान करके निदान किया जा सकता है।
- महामारी रोग:
- मामलों में वृद्धि से रोग के स्रोत, रोगजनक और संचरण मार्गों की पहचान करने के लिए महामारी विज्ञान जांच के प्रयास बढ़ जाते हैं।
- रोगजनक की त्वरित पहचान के लिए अक्सर PCR और सीरोलॉजी का उपयोग किया जाता है (उदाहरण: हैजा प्रकोप में विब्रियो कॉलेरी)।
- महामारिक रोग:
- निदान में वैश्विक स्वास्थ्य निगरानी प्रणालियाँ शामिल हैं, जहां RT-PCR जैसे वास्तविक समय आणविक नैदानिक परीक्षण नए रोगजनकों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं। वैश्विक अनुक्रमण डेटा वायरल उत्परिवर्तन (जैसे SARS-CoV-2 वेरिएंट) को ट्रैक करने में मदद करता है।संक्रमित व्यक्तियों की पहचान और अलगाव के लिए व्यापक संपर्क अनुरेखण का उपयोग किया जाता है।
जैविक सिद्धांतों का उपयोग कर नियंत्रण
- स्थानिक नियंत्रण:
- नियंत्रण उपाय दीर्घकालिक रोकथाम पर केंद्रित होते हैं, जैसे टीकाकरण (उदाहरण: तपेदिक के लिए BCG) या वेक्टर नियंत्रण (उदाहरण: मलेरिया के लिए कीटनाशक-युक्त जाल)। जूनोटिक जोखिमों, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है।
- महामारी नियंत्रण:
- प्राथमिक ध्यान प्रारंभिक पहचान, संपर्क अनुरेखण और प्रभावित व्यक्तियों के संगरोध पर होता है। टीकाकरण अभियान लागू किए जा सकते हैं (उदाहरण: इन्फ्लुएंजा के लिए), और जीवाणुजनित महामारियों (जैसे हैजा) में प्रतिजैविक प्रतिरोध का ध्यान रखा जाता है।
- महामारिक नियंत्रण:
- महामारिक के लिए बहुराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, जिसमें WHO जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन प्रयासों का समन्वय करते हैं। टीकों और एंटीवायरल उपचारों का त्वरित वितरण, साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और PCR एवं एंटीजन परीक्षण सहित परीक्षण आवश्यक उपाय होते हैं।
कोविड-19 महामारी:
कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोनावायरस 2 (SARS-CoV-2) के कारण होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। COVID-19 ने विश्व पर विनाशकारी प्रभाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप विश्व भर में 60 लाख से अधिक मौतें हुई हैं।
वायरस की प्रकृति:
- कोरोनावायरस (CoVs) धनात्मक-सेंस एकल-रज्जुक RNA (+ssRNA) वायरस हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के तहत मुकुट जैसी उपस्थिति होती है, जो उनके आवरण पर स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के कारण होती है।
- SARS-CoV-2 में चार संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं, जिन्हें S (स्पाइक), E (आवरण), M (झिल्ली) और N (न्यूक्लियोकैप्सिड) प्रोटीन के रूप में जाना जाता है।
- ये वायरस प्रजाति अवरोधों को पार कर मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं। SARS-CoV-2 में मानव कोशिकाओं पर एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम 2 (ACE2) रिसेप्टर के लिए पर्याप्त आत्मीयता होती है जिसका उपयोग यह कोशिका प्रवेश के तंत्र के रूप में करता है।
- अन्य RNA वायरस की तरह, SARS-CoV-2 आनुवंशिक विकास और उत्परिवर्तन के साथ अनुकूलन करता है। इसके परिणामस्वरूप उत्परिवर्ती वेरिएंट उत्पन्न होते हैं जिनकी विशेषताएं उनके पैतृक उपभेदों से भिन्न हो सकती हैं।
- SARS-CoV-2 के चिंताजनक वेरिएंट (VOCs):
- अल्फा (B.1.1.7 लिनीज): पहला चिंताजनक वेरिएंट → यूनाइटेड किंगडम (यूके)
- बीटा (B.1.351): पहली बार दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया
- गामा (P.1): पहली बार ब्राजील में रिपोर्ट किया गया
- डेल्टा (B.1.617.2): दिसंबर 2020 में भारत में पहली बार रिपोर्ट किया गया
- ओमिक्रॉन (B.1.1.529): नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार रिपोर्ट किया गया
- (हालांकि SARS-CoV-2 की उत्पत्ति वर्तमान में अज्ञात है, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि इसका जूनोटिक संचरण हुआ है। जीनोमिक विश्लेषण से पता चलता है कि SARS-CoV-2 संभवतः चमगादड़ों में पाए जाने वाले उपभेद से विकसित हुआ। SARS और MERS की तरह, यह परिकल्पना की गई है कि SARS-CoV-2 चमगादड़ों से मध्यवर्ती होस्ट, जैसे पैंगोलिन और मिंक के माध्यम से और फिर मनुष्यों में आया।)
भारत द्वारा अपनाए गए नियंत्रण उपाय
14 मार्च, 2020 को भारत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत महामारी को “अधिसूचित आपदा” घोषित किया।
भारत की 5-सूत्री रणनीति:
- परीक्षण:
- बढ़ाया गया परीक्षण → न्यूनतम 70% RT-PCR परीक्षण
- सघन क्षेत्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग
- अनुरेखण:
- संचरण श्रृंखला तोड़ने हेतु “आरोग्य सेतु” स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया गया
- संक्रमित व्यक्तियों को क्वारंटाइन में रखा गया
- उपचार:
- COVID-19 उपचार AB-PMJAY के तहत शामिल
- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का प्रारंभिक उपयोग
- हल्के से मध्यम मामलों के लिए एंटीवायरल फेविपिराविर
- DRDO द्वारा 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज ⇒ हल्के से गंभीर मामलों के उपचार हेतु
- COVID-उचित व्यवहार: जनता कर्फ्यू
- 24 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा
- तीन क्षेत्रों में विभाजन: ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन
- “2 गज की दूरी“, शारीरिक संपर्क रहित अभिवादन, हमेशा मास्क पहनना, बार-बार हाथ धोना
- टीकाकरण:
- 3 चरणों में टीकाकरण अभियान → 1 अरब से अधिक टीके
- 3 नवंबर को “हर घर दस्तक” COVID-19 टीकाकरण अभियान लॉन्च
- कोविशील्ड से प्रारंभ कर स्वदेशी कोवैक्सिन तक
- बच्चों हेतु: कोर्बेवैक, जाइकोव-डी वैक्सीन
मानवीय नीति प्रतिक्रिया:
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज
- आत्मनिर्भर भारत पैकेज (सकल घरेलू उत्पाद का 10%) के तहत आर्थिक उपाय
- विश्व भर से संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों का “वंदे भारत मिशन” द्वारा विशाल निकासी
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: COWIN पोर्टल का उपयोग
चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत बनाना:
- PPE, ICU, वेंटिलेटर्स
- PM-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के तहत सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना
- PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्वीकृति → PM CARES फंड का उपयोग
COVID-19 महामारी के पुनरुत्थान के खतरे को कम करने के उपाय
- जीनोमिक निगरानी:
- भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक निगरानी कंसोर्टियम (INSACOG) की स्थापना
- SARS-CoV-2 के वेरिएंट उपभेदों के विकास की ट्रैकिंग और जीनोमिक अनुक्रमण हेतु
- भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक निगरानी कंसोर्टियम (INSACOG) की स्थापना
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) दो प्रमुख कार्यक्रमों – राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (एनबीएम) और IND-सीईपीआई मिशन के कार्यान्वयन का समर्थन कर रहा है। इन कार्यक्रमों ने राष्ट्रीय टीका विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में सक्षम बनाया है, ताकि महामारियों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दी जा सके।
- मिशन COVID सुरक्षा:
- आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज के भाग के रूप में लॉन्च, भारतीय COVID-19 टीकों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना
स्थानिक, महामारी और महामारिक रोगों में अंतर
| पहलू | स्थानिक (Endemic) | महामारी (Epidemic) | महामारिक (Pandemic) |
| परिभाषा | एक विशिष्ट क्षेत्र या आबादी में लगातार मौजूद रोग | किसी क्षेत्र में सामान्य से अधिक रोग के मामलों में अचानक वृद्धि | वैश्विक स्तर पर फैला रोग, जो कई देशों/महाद्वीपों को प्रभावित करता है |
| घटना | स्थिर, दीर्घकालिक उपस्थिति | अचानक मामलों में वृद्धि | वैश्विक आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित करता है |
| उदाहरण | मलेरिया, क्षेत्र-विशिष्ट चिकनपॉक्स | इन्फ्लुएंजा प्रकोप, हैजा | COVID-19, H1N1 (स्वाइन फ्लू), स्पैनिश फ्लू |
| रोगजनक प्रकार | स्थानीय जलाशयों/वैक्टरों में मौजूद | नए उत्परिवर्तन या संक्रामक एजेंट का प्रसार | नया/उत्परिवर्तित रोगजनक जो सीमाओं के पार तेजी से फैल सकता है |
| संचरण | स्थानीय, अक्सर वैक्टर-जनित (मच्छर, आदि) | स्थानीय/क्षेत्रीय, नए उपभेदों के कारण | वैश्विक, मानव-से-मानव संचरण |
| मानव प्रतिरक्षा | आंशिक प्रतिरक्षा (दीर्घकालिक संपर्क से) | नए रोगजनक के प्रति कम प्रतिरक्षा | नए रोगजनक के प्रति कोई/नगण्य प्रतिरक्षा |
| अवधि | दीर्घकालिक, स्थिर घटनाएँ | कुछ सप्ताह से महीनों तक | महीनों से वर्षों तक, कई लहरों के साथ |
| भौगोलिक प्रसार | विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित | एक देश/राज्य/शहर तक सीमित | कई महाद्वीपों और देशों में फैला हुआ |
| निदान | नैदानिक लक्षण, दीर्घकालिक निगरानी | PCR, एंटीजन टेस्ट, त्वरित निदान | वैश्विक निगरानी, RT-PCR, जीनोमिक अनुक्रमण |
| नियंत्रण उपाय | टीकाकरण, वेक्टर नियंत्रण, स्वच्छता | संगरोध, संपर्क अनुरेखण, टीकाकरण अभियान | अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, यात्रा प्रतिबंध, सामाजिक दूरी |
| प्रभाव | निम्न-मध्यम (स्थापित नियंत्रण के कारण) | मध्यम-उच्च (रोगजनक और प्रतिक्रिया पर निर्भर) | उच्च, स्वास्थ्य प्रणालियों और अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव |
| रोग उदाहरण | मलेरिया (प्लाज्मोडियम), क्षय रोग (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस) | इन्फ्लुएंजा (इन्फ्लुएंजा वायरस), हैजा (विब्रियो कॉलेरी) | COVID-19 (SARS-CoV-2), H1N1 इन्फ्लुएंजा |
FAQ (Previous year questions)
एंडेमिक एपिडेमिक पैनडेमिक रोग उनके निदान और नियंत्रण / एंडेमिक एपिडेमिक पैनडेमिक रोग उनके निदान और नियंत्रण / एंडेमिक एपिडेमिक पैनडेमिक रोग उनके निदान और नियंत्रण / एंडेमिक एपिडेमिक पैनडेमिक रोग उनके निदान और नियंत्रण / एंडेमिक एपिडेमिक पैनडेमिक रोग उनके निदान और नियंत्रण / एंडेमिक एपिडेमिक पैनडेमिक रोग उनके निदान और नियंत्रण
कोरोनावायरस रोग 2019 (कोविड-19) एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोनावायरस 2 (SARS-CoV-2) के कारण होता है। COVID-19 का दुनिया पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में 6 मिलियन से अधिक मौतें हुई हैं। .
वायरस की प्रकृति:
कोरोना वायरस (सीओवी) पॉजिटिव-सेंस सिंगल-स्ट्रैंडेड आरएनए (+एसएसआरएनए) वायरस हैं, जो सतह पर स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक ताज की तरह दिखते हैं।
SARS-CoV-2 में चार संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं, जिन्हें S (स्पाइक), E (आवरण), M (झिल्ली), और N (न्यूक्लियोकैप्सिड) प्रोटीन के नाम से जाना जाता है।
ये वायरस प्रजातियों की बाधाओं को पार कर सकते हैं और मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकते हैं। SARS‑CoV‑2 में मानव कोशिकाओं पर उपस्थित रिसेप्टर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 (ACE2) से पर्याप्त समानता है जिससे ये उन्हें कोशिका प्रवेश के तंत्र के रूप में उपयोग करता है
अन्य RNA वायरस की तरह, SARS-CoV-2 आनुवंशिक विकास और विकासशील उत्परिवर्तन के साथ अनुकूलित होता है। इसके परिणामस्वरूप ऐसे उत्परिवर्ती रूप सामने आते हैं जिनकी विशेषताएँ उनके पैतृक उपभेदों से भिन्न हो सकती हैं।
SARS-CoV-2 के चिंताजनक स्वरूप (VOCs):
अल्फ़ा (बी.1.1.7 वंश): चिंता का पहला संस्करण → यूनाइटेड किंगडम (यूके)
बीटा (बी.1.351): पहली बार दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया
गामा (पी.1): सबसे पहले ब्राज़ील में रिपोर्ट किया गया
डेल्टा (बी.1.617.2): भारत में पहली बार दिसंबर 2020 में रिपोर्ट किया गया
ओमीक्रॉन (बी.1.1.529): सबसे पहले नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया
भारत द्वारा उठाए गए नियंत्रण उपाय
14 मार्च, 2020 को भारत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत इस महामारी को “अधिसूचित आपदा” घोषित किया।
भारत की 5 गुना रणनीति(5 फोल्ड स्ट्रेटेजी )
परीक्षण: परीक्षण में वृद्धि → न्यूनतम 70% आरटीपीसीआर परीक्षण और घने क्षेत्रों में रैपिड एंटीजन परीक्षण का उपयोग
ट्रेसिंग: ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने के लिए →”संपर्क ट्रेसिंग और प्रसार को नियंत्रित करने” में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु नामक एक स्मार्ट फोन एप्लिकेशन लॉन्च किया गया।
संक्रमित लोगों को क्वारैंटाइन किया गया
इलाज :
AB-PMJAY के अंतर्गत COVID-19 का उपचार शामिल है
शुरुआत में हाई रिस्क एरिया के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल किया गया
हल्के से मध्यम मामलों के लिए एंटीवायरल फेविपिराविर का उपयोग किया जाता है
डीआरडीओ → 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज ⇒ हल्के से गंभीर मामलों का इलाज
कोविड उपयुक्त व्यवहार: जनता कर्फ्यू
24 मार्च को, भारत ने प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी तालाबंदी(लोकडाउन ) की घोषणा की।
सरकार ने पूरे देश को तीन जोन में बांटा- ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन.
लोकप्रियकरण: 2 गज की दूरी, शारीरिक संपर्क के बिना अभिवादन, हर समय पुन: प्रयोज्य हाथ से बना फेस-कवर या मास्क पहनें; बार-बार और अच्छी तरह से हाथ धोएं
टीकाकरण: 3 चरणों में टीकाकरण अभियान → 1 अरब के पार
COVID-19 टीकाकरण अभियान “हर घर दस्तक”, 3 नवंबर को शुरू किया गया
शुरुआत कोविशील्ड और बाद में स्वदेशी कोवैक्सिन से हुई
बच्चों के लिए: कॉर्बेवैक्स, ZyCoV-D टीका
मानवीय नीति प्रतिक्रिया:
गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज:
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आर्थिक उपाय (जीडीपी का 10%)
दुनिया भर से संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों की मेगा निकासी को “वंदे भारत मिशन” कहा गया
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रा: COWIN पोर्टल का उपयोग
चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना :
पीपीई, आईसीयू, वेंटिलेटर
पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना
पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की मंजूरी → पीएम केयर्स फंड का उपयोग किया गया
ओमिक्रॉन वेरिएंट के दौरान:
कोविड पॉजिटिव मामलों के नए समूहों के मामले में तुरंत “कंटेनमेंट जोन”, “बफर जोन” को सूचित करें
अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी के लिए “एयर सुविधा” पोर्टल तक पहुंच का उपयोग करें
यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी आपात स्थिति का जवाब देने के लिए हॉटस्पॉट पर/निकट स्वास्थ्य प्रणालियों की अपेक्षित क्षमता विकसित की गई है, आपातकालीन सीओवीआईडी प्रतिक्रिया पैकेज (ईसीआरपी-द्वितीय) के तहत स्वीकृत धन का उपयोग करें।
कोविड-19 महामारी के दोबारा उभरने के खतरे को कम करने के उपाय
जीनोमिक अनुक्रमण और SARS-CoV-2 के विभिन्न उपभेदों के विकास पर नज़र रखने के लिए एक भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक सर्विलांस कंसोर्टियम (INSACOG) की स्थापना की।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) दो प्रमुख कार्यक्रमों, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (एनबीएम) और इंड-सीईपीआई मिशन के कार्यान्वयन का समर्थन कर रहा है, जिसने राष्ट्रीय टीका विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में सक्षम बनाया है, ताकि महामारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके।
मिशन कोविड सुरक्षा – भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन, भारतीय कोविड-19 टीकों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए तीसरे प्रोत्साहन पैकेज, आत्मनिर्भर भारत 3.0 के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।
पहलू
महामारी
सर्वव्यापी महामारी
परिभाषा
किसी विशिष्ट समुदाय, आबादी या क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी के मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि।
एक महामारी जो कई देशों या महाद्वीपों में फैल गई है, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित
क्षेत्र
किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या समुदाय तक सीमित।
कई देशों या महाद्वीपों में फैलकर विश्व स्तर पर आबादी को प्रभावित करता है।
कारक
वायरल कारक एक उन्नत वाहक के रूप में कार्य करता है, जिससे तेजी से फैलने में सहायता मिलती है।
इसमें आम तौर पर एक नवीन (नई) बीमारी शामिल होती है।
अवधि
रोकथाम के उपायों और बीमारी की गतिशीलता के आधार पर, अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकता है।
यह लंबे समय तक रह सकता है, जिसमें संक्रमण की कई लहरें महीनों या वर्षों तक घटित होती रहती हैं।
उदाहरण
2003 में SARS का प्रकोप
2014 से 2016 तक अफ्रीका में इबोला वायरस का प्रकोप
कोविड-19 महामारी
1918-1919 की स्पैनिश फ़्लू महामारी।