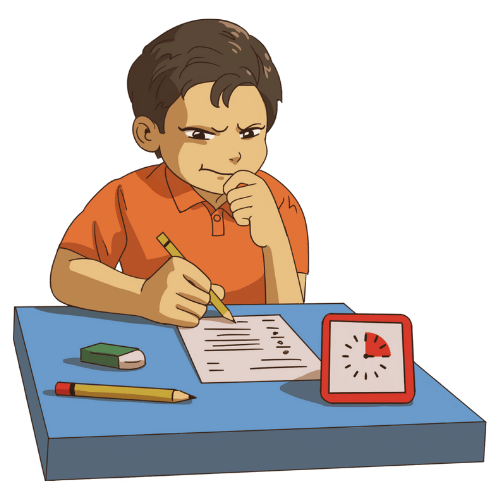This is Day 36 | 90 Days RAS Mains 2025 Answer Writing, We will cover the whole RAS Mains 2025 with this 90-day answer writing program
Click here for the complete 90 days schedule (English Medium)
Click here for complete 90 days schedule (Hindi Medium)
GS Answer Writing – Space technology – Indian space program, Satellites, and their orbits, various launch vehicles; Remote sensing। निबंध लेखन
| आधार | भू-तुल्यकालिक कक्षा | सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा |
| Synchronization | भूस्थिर कक्षा (जीईओ) में उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, जो पृथ्वी की घूर्णन गति से मेल खाते हैं, जिससे वे एक निश्चित स्थान पर स्थिर दिखाई देते हैं। | सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा (एसएसओ) एक ध्रुवीय कक्षा है जहां उपग्रह ध्रुवीय क्षेत्रों में यात्रा करते हैं, सूर्य के साथ सिंक्रनाइज़ रहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वे लगातार एक ही स्थानीय समय पर एक ही स्थान से गुजरें। |
| ऊँचाई | 36000 किमी की ऊंचाई पर. | 500 किमी-800 किमी की ऊंचाई पर. |
| अनुप्रयोग | संचार उपग्रह और मौसम अध्ययन। | पृथ्वी अवलोकन, रिमोट सेंसिंग, जलवायु निगरानी (तूफान की भविष्यवाणी करना और जंगल की आग और बाढ़ की निगरानी करना) |
| Examples | इनसैट सीरीज, जीसैट सीरीज, आईआरएनएसएस/नाविक (INSAT Series, GSAT Series, IRNSS/NavIC) | कार्टोसैट सीरीज, आरआईएसएटी सीरीज, रिसोर्ससैट सीरीज (Cartosat Series, RISAT Series, ResourceSat Series) |
सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष-आधारित वेधशाला, आदित्य-एल1, 2 सितंबर, 2023 को PSLV C 57 रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च की गई थी। हाल ही में, इसे L1 लैग्रेन्जियन बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया । .
- उद्देश्य
- सौर ऊपरी वायुमंडलीय (क्रोमोस्फीयर और कोरोना) की गतिकी का अध्ययन
- कोरोनल हीटिंग तंत्र की भौतिकी और अत्यधिक तापमान के पीछे के कारण समझना ।
- कोरोनल मास इजेक्शन (CME ) की शुरुआत और गतिशीलता को समझना
- सौर कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र और इसके मौसम पर प्रभाव में भूमिका की जांच।
- सोर पवन के उत्पादन को समझने के लिए सूर्य पर कणों के त्वरण की जांच।
- कई परतों (क्रोमोस्फीयर, बेस और विस्तारित कोरोना) पर होने वाली प्रक्रियाओं के अनुक्रम की पहचान जो अंततः सौर विस्फोट की घटनाओं की ओर ले जाती हैं।
सौर घटना को समझना: विद्युत चुम्बकीय और कण डिटेक्टरों का उपयोग करके प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पे-लोड (SUIT, PAPA, HEL1OS, VLEC आदि) हैं।
- सौर परिवर्तनशीलता और पृथ्वी की जलवायु पर इसके प्रभावों को समझने के लिए सौर कोरोना की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है।
- सूर्य की पूर्ण डिस्क छवि कैप्चर करना: विभिन्न सौर वायुमंडल क्षेत्रों से UV विकिरण का अवलोकन ।
- जलवायु परिवर्तन में प्राकृतिक और मानवजनित कारकों की भूमिका को समझना।
- सूर्य का 24X7 अवलोकन: आदित्य-एल1 लगातार बिना किसी ग्रहण या ग्रहण के सूर्य को देखता है, जिससे सौर गतिविधियों का अबाधित अवलोकन संभव हो पाता है।
- अंतरिक्ष मौसम स्टेशन के रूप में कार्य करता है: आदित्य एल1 का डेटा भू-चुंबकीय तूफानों की भविष्यवाणी करने और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करता है, जो उपग्रहों और अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
सौर भौतिकी को आगे बढ़ाना और परमाणु संलयन ऊर्जा अनुसंधान को बढ़ाना
भारत की स्थिति, नेविगेशन और समय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो द्वारा विकसित किया गया ।इसे पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस) के नाम से जाना जाता था।
- संरचना: इसमें 7 उपग्रह और 24 x 7 संचालित ग्राउंड स्टेशनों का एक नेटवर्क शामिल है। तीन उपग्रह भूस्थिर कक्षा में और चार उपग्रह झुकी हुई भू-समकालिक कक्षा में हैं।
- दो प्रकार की सेवाएँ प्रदान करती हैं
- नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए मानक स्थिति सेवा (SPS)।
- रणनीतिक उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित सेवा (RS)।
- कवरेज क्षेत्र: इसमें भारत और भारतीय सीमा से परे 1500 किमी तक का क्षेत्र शामिल है।
भारत के लिए महत्व:
- वैश्विक मान्यता: IMO द्वारा समर्थित, क्षेत्रीय उपग्रह प्रणाली की क्षमता वाला भारत विश्व का चौथा देश बना
- सामरिक स्वायत्तता: जीपीएस पर निर्भरता कम करता है, स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। (कारगिल युद्ध 1999 के दौरान यूएसए द्वारा जीपीएस डेटा शेयरिंग से इंकार )
- सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: आपदा प्रबंधन, वाहन ट्रैकिंग और बेड़े प्रबंधन, सटीक समय, मानचित्रण और जियोडेटिक डेटा कैप्चर आदि के लिए नेविगेशन सक्षम बनाता है।
- सटीकता और विश्वसनीयता: बढ़ी हुई सटीकता के लिए NavIC दोहरी आवृत्तियों (एस और एल बैंड) का उपयोग करता है। यह सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए 5-20 मीटर और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए 0.5-5 मीटर की सटीकता प्रदान करता है।
- नागरिक उड्डयन सहायता: GAGAN प्रणाली विमानन नेविगेशन में सुधार करती है।
- रक्षा संवर्धन: शत्रुता के दौरान सटीक डेटा प्रदान करता है।; आधुनिक हथियार प्रणालियों का समर्थन करता है.
- सुदूर क्षेत्रों में कवरेज: उच्च भू-स्थिर कक्षा उपग्रहों का उपयोग करके दुर्गम क्षेत्रों तक कवरेज बढ़ाता है।
- विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र: जीपीएस की जगह, भारत में सभी मोबाइल फोन में NavIC-सक्षम चिपसेट मानक बन सकता है। इससे मोबाइल दूरसंचार उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
(Extra → सभी स्मार्टफोन के लिए NavIC समर्थन अनिवार्य हो जाएगा: जबकि 5G फोन के लिए 1 जनवरी, 2025 तक NavIC के लिए अनिवार्य समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता होगी, L1 बैंड में काम करने वाले अन्य सभी फोन जो वर्तमान में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) का उपयोग करते हैं, उन्हें अनिवार्य प्रदान करना होगा। दिसंबर 2025 तक NavIC समर्थन)
3. रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन
ये एयरब्रीथिंग जेट इंजन हैं जिनमें कोई चलायमान भाग नहीं है, ये ईंधन को प्रज्ज्वलित करने के लिए कंप्रेसर और टर्बाइन (पारंपरिक जेट विमानों पर पाए जाने वाले टर्बोफैन इंजन में उपयोग किया जाता है) के बजाय इंजन में सुपरसोनिक एयरफ्लो द्वारा बनाए गए भारी दबाव पर निर्भर करते हैं दोनों 100% ईंधन का उपयोग करते हैं और हवा से ऑक्सीकारक प्राप्त करते है
| रैमजेट | स्क्रैमजेट |
| यह एक एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन जेट इंजन है | एक्रोनिम स्क्रैमजेट (SCRAMJET) का मतलब सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट है। |
| एक रैमजेट दहन से पहले हवा को सबसोनिक वेग तक धीमा कर देता है। | स्क्रैमजेट में, दहन सुपरसोनिक वायुप्रवाह में होता है। यह स्क्रैमजेट को पारंपरिक रैमजेट की तुलना में अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। |
| इसमें शॉक कोन (इनलेट कोन) होते हैं जो हवा को धीमा कर देते हैं, जिससे इसकी कुछ ऊर्जा शॉक वेव के रूप में निकल जाती है, लेकिन इससे ईंधन दक्षता कम हो जाती है | स्क्रैमजेट में कोई शॉक कोन नहीं होता है। यह शॉक कोन के स्थान पर अपने प्रज्ज्वलन स्रोत द्वारा उत्पन्न शॉकवेव्स का उपयोग करके वायु प्रवाह को धीमा कर देता है |
| वायु प्रवेश की आवश्यकता है → इस इंजन के काम करने के लिए एक उचित प्रारंभिक बिंदु लगभग मैक 3 है, और वे मैक 6 जितनी तेजी से प्रभावी प्रणोदन बनाए रख सकते हैं। | स्क्रैमजेट इंजन लगभग मैक 6 या उससे अधिक की गति पर कार्य कर सकते हैं। |
| स्क्रैमजेट कम विशिष्ट आवेग उत्पन्न करते हैं। | स्क्रैमजेट उच्च विशिष्ट आवेग उत्पन्न करते हैं। |
| मिसाइलों, विमानों, कुछ प्रायोगिक वाहनों में उपयोग किया जाता है | हाइपरसोनिक वाहन, अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली |
Paper 4 (Comprehension part) – निबंध
एक राष्ट्र, एक चुनाव : चुनौतियाँ व उपाय
भारतीय जन-मानस ने तमाम आशंकाओं को निराधार साबित करते हुए धूम-धाम से लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया तथा परिणाम सबके सामने है। यदि हम आज भारतीय शासन तंत्र पर गर्व कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कुछ कारक मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है-चुनाव प्रणाली। हर प्रणाली में समय-समय पर कुछ बदलावों तथा कुछ सुधारों की गुंजाइश बनी रहती है। उन्हीं सुधारों में से एक है ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ संबंधी अवधारणा, जिसका अभिप्राय है- पूरे देश में एक ही समय पर वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के विपरीत लोकसभा, विधानसभाओं व अन्य स्थानीय स्तर के चुनावों का आयोजन किया जाना। श्री रामनाथ कोविन्द कमिटी की अनुशंशाएँ आने के बाद एक बार फिर इस मुद्दे पर चर्चाएँ बढ़ गई हैं।
एक चुनाव प्रणाली के द्वारा पाँच साल में केवल एक बार चुनाव आयोजित होने से सरकार एक निश्चित समयावधि के लिये चुनाव प्रचारों जैसे कार्यों से मुक्त हो पाएगी तथा शासन व्यवस्था पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएगी, जो विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ध्यातव्य है कि अभी भी भारतीय चुनाव में विकास आधारित एजेंडे की बजाय क्षेत्रीयता को महत्त्व दिया जाता है, किंतु एक साथ सभी स्तरों पर चुनाव होने से लोग प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रीय सरोकारों के आधार पर बड़े उद्देश्यों पर ध्यान दे पाएंगे और उसी के अनुसार अपना मत निर्धारित करने के काबिल हो पाएंगे। साथ ही बार-बार चुनाव आयोजन से होने वाली सुरक्षा संबंधी समस्याओं का निराकरण संभव हो पाएगा। इसके अलावा जनता में उत्साह बढ़ेगा व गवर्नेस संबंधी मानकों में भी सुधार आने की संभावना को बल मिलेगा।
गौरतलब है कि भारत में हर साल किसी-न-किसी राज्य में चुनाव्र होते रहते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर सरकारी व्यय होता है तथा संसाधनों के दोहन में भी तेजी आ जाती है। इसका सीधा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जिसकी भरपाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आम नागरिकों के द्वारा की जाती है। प्रशासन तंत्र का बड़ा भाग चुनाव संपन्न कराने में ही उलझा रहता है। परिणामस्वरूप पहले से बोझ तले दबा हुआ ये तंत्र और गंभीर स्थिति में आ खड़ा होता है व राज्य या देश के उन हिस्सों में, जहाँ चुनाव आयोजित नहीं हो रहे हैं, कानून व प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आ जाती है। चुनावों में अध्यापकों को चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने का जिम्मा सौंपा जाता है, जिससे अध्यापकों की कमी का नकारात्मक प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है।
हालाँकि, ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रणाली अपनाने में भी कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इसकी सबसे बड़ी चुनौती/समस्या इसके सही क्रियान्वयन की है, क्योंकि इसके मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा/रुकावट राजनीतिक पार्टियाँ हैं। जो इस प्रकार की प्रक्रिया की कम समर्थक होती हैं। साथ ही, इस अवधारणा का क्रियान्वयन संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध भी है। वर्तमान समय में अनुच्छेद 172(1) के अंतर्गत जब सरकारों को लगता है कि तात्कालिक परिस्थितियाँ संवैधानिक कार्य के निर्वहन में असमर्थ साबित हो रही हैं, तभी राज्य सरकारें राज्यपालों के आदेश द्वारा नए चुनावों की घोषणा करवा सकती हैं। एक अन्य समस्या ये भी है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के लिये लाखों अधिकारियों व कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जबकि चुनाव आयोग के पास तो अभी तक खुद के पोलिंग बूथ कर्मचारी भी नहीं हैं तथा वह अध्यापकों व अन्य वर्गों से संबंधित कर्मचारियों के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवा पाता है।
इन सारी चुनौतियों के बावजूद ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ अवधारणा को यथार्थ के धरातल पर फलीभूत किया जा सकता है, बशर्ते कुछ सकारात्मक उपाय खोजे जाएँ। सर्वप्रथम इसके लिये दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। सभी राजनीतिक पार्टियों को आपसी मतभेद खत्म कर चुनाव आयोग की क्षमता व शक्तियों में विस्तार करना होगा, ताकि वह इतने बड़े स्तर पर एक साथ चुनावों का आयोजन करवा सके। इस संबंध में केवल निर्वाचन आयोग हेतु समर्पित भर्तियाँ की जानी चाहियें और उन चयनित अधिकारियों की शक्तियाँ भी अन्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के समान होनी चाहियें।
ध्यान रहे चुनावों के समय जिलाधिकारी ही जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका का निर्वहन करता है। साथ ही, तकनीकी अवसंरचना के विस्तार के साथ-साथ अधिक सुदृढ़ स्वरूप प्रदान करना होगा। संवैधानिक अड़चनों से बचने हेतु कुछ प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है।
अतः संपूर्ण परिदृश्य के अवलोकन के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का यह प्रस्ताव बुरा नहीं है। हाँ, इस राह में अभी काफी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिन्हें दूर किये बिना इसे लागू करना दुष्कर है। किंतु, यदि हम राम नाथ कोविंद सिमिती की अनुशंशाओं पर विचार कर इन चुनौतियों को दूर कर पाएँ तो राष्ट्रहित में यह अवधारणा ‘मील का पत्थर’ साबित हो सकती है तथा तमाम संसाधनों के विदोहन को कम करके बेहतर कल का मार्ग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
Day 36 | 90 Days RAS Mains 2025 Answer Writing
Day 36 | 90 Days RAS Mains 2025 Answer Writing