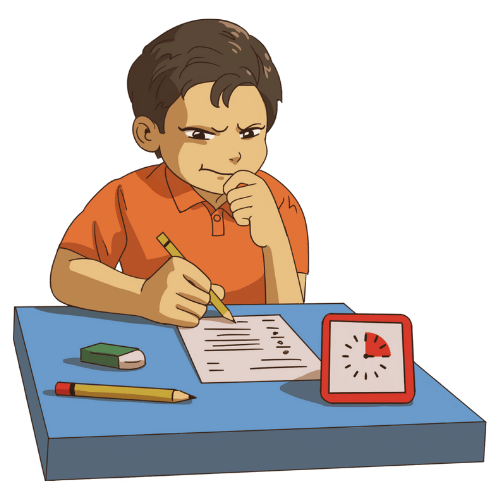This is Day 33 | 90 Days RAS Mains 2025 Answer Writing, We will cover the whole RAS Mains 2025 with this 90-day answer writing program
Click here for the complete 90 days schedule (English Medium)
Click here for complete 90 days schedule (Hindi Medium)
GS Answer Writing – सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में नूतन विकास-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस; बिग डेटा, क्लाउड कप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ अथिंग्स, क्रिप्टोकरेंसी। ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया और उनके प्रभाव; भारत में आईटी उद्योग,डिजिटल इंडिया पहल। निबंध लेखन
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) के अनुसार, बिग डेटा ऐसा डेटा होता है जिसकी मात्रा, विविधता और जटिलता इतनी अधिक होती है कि उसे प्रबंधित करने तथा उसमें से मूल्य और छिपी हुई जानकारी निकालने के लिए नवीन आर्किटक्चर, तकनीकों, एल्गोरिद्म और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, बिग डेटा की पहचान निम्नलिखित विशेषताओं से होती है: वॉल्यूम (मात्रा) – डेटा की अत्यधिक मात्रा, वैरायटी (विविधता) – संरचित और असंरचित दोनों प्रकार का डेटा, वेलॉसिटी (गति) – परिवर्तन की उच्च दर, वैरासिटी (प्रामाणिकता) – डेटा की अनिश्चितता और अपूर्णता
आईटी नियम 2021 ओटीटी प्लेटफार्मों को ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म (ओसीसीपी) के रूप में वर्णित करता है। ओटीटी एक तरह का ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें दर्शकों की मांग के आधार पर फ़िल्म, वेब सीरीज, पॉडकास्ट इत्यादि प्रकार का ऑडियो-विजुअल कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है।
भारत में लोकप्रिय वीडियो-ऑन-डिमांड सेवाओं में डिज़्नी+ हॉटस्टार, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो, सोनी लिव आदि शामिल हैं।
ओटीटी प्लेटफार्मों का उदय:
ऑरमैक्स रिपोर्ट: भारत में 481 मिलियन ओटीटी उपयोगकर्ता (यानी 34% की पहुंच) और 102 मिलियन पेड सब्सक्रिप्शन हैं।
ओटीटी प्लेटफ़ॉर्मों की वृद्धि के कारक
- इंटरनेट की पहुँच और किफायती डेटा योजनाएँ
- नवीन और मौलिक सामग्री, जो अप्रतिम विविधता लिए हुए है
- सुविधाजनक और मांग के अनुसार मनोरंजन की उपलब्धता
- दर्शकों की बदलती हुई देखने की आदतें
- लागत-कुशल सब्सक्रिप्शन योजनाएँ
- कोविड-19 महामारी का प्रभाव
नियामक चुनौतियाँ:
- तीव्र विकास: 2024 में उपयोगकर्ता की पहुंच 45.8% होने का अनुमान है और 2029 तक बढ़कर 54.5% होने की उम्मीद है।
- बाजार प्रभुत्व और अनुचित प्रतिस्पर्धा: नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो और डिज़नी + हॉटस्टार भारत में शीर्ष तीन ओटीटी खिलाड़ी हैं, जिनकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 60-70% है।
- उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा करना और डेटा सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना
- ओटीटी द्वारा ‘विस्तारित रिलीज’, फिल्म उद्योग (सीबीएफसी द्वारा विनियमित) के साथ असमानता को दर्शाता है।
- कमजोर वर्गों की सुरक्षा: 2018 में सुप्रीम कोर्ट और 2020 में राज्यसभा की तदर्थ समिति ने डिजिटल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खतरनाक मुद्दे पर प्रकाश डाला।
- सिविल सोसायटी की मांगें: नागरिक समाज ने यौन रूप से स्पष्ट और किसी भी अन्य सामग्री की निगरानी करने की मांग की, जो “झूठे आख्यानों”, “लव जिहाद” को बढ़ावा देती है और भारत के इतिहास को गलत तरीके से चित्रित करती है।
नियामक चुनौतियों का समाधान:
- 2020: सरकार ने ओटीटी प्लेटफार्मों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की: हाल ही में 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक किया गया
- हाल ही में, टीडीएसएटी ने फैसला सुनाया कि ओटीटी TRAI के अधिकार क्षेत्र से बाहर आते हैं और Meity के तहत सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 द्वारा शासित होते हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021: एक सॉफ्ट-टच स्व-नियामक संरचना → ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए आचार संहिता और त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 का मसौदा जारी किया → प्रसारण, ओटीटी, डिजिटल मीडिया, डीटीएच, आईपीटीवी” के लिए समेकित नियामक के पक्ष में
सोशल मीडिया उन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों और तकनीकों को संदर्भित करता है जो उपयोगकर्ताओं को आभासी समुदायों और नेटवर्क में जानकारी, विचार और सामग्री बनाने, साझा करने, और आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण: फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब और स्नैपचैट।
सूचना के लोकतंत्रीकरण में भूमिका:
- व्यक्तियों को अपने विचारों और राय को स्वतंत्र रूप से साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करके पारंपरिक मीडिया के आधिपत्य का मुकाबला करता है।
- सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अधिक सुलभ, समावेशी हैं और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करते हैं।
- व्यक्तियों को सार्वजनिक चर्चा में भाग लेने, असहमतिपूर्ण विचार व्यक्त करने और सरकारों और संस्थानों को जवाबदेह बनाने के लिए सशक्त माध्यम का काम करता है। उदाहरण के लिए अरब स्प्रिंग के दौरान सोशल मीडिया की भूमिका।
- हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अपने दृष्टिकोण, चिंताओं और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है : मी टू मूवमेंट।
- पुरानी पीढ़ियों सहित लोगो में डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहन।
- सरकारी अधिकारियों, नौकरशाहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्विटर जैसे प्रत्यक्ष संचार चैनलों की सुविधा।
हालाँकि, सूचना का यह लोकतंत्रीकरण आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी चुनौतियाँ पैदा करता है।
| आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ | सामाजिक एकजुटता के लिए चुनौतियाँ |
| कट्टरता: कट्टरपंथी समूह सोशल मीडिया का उपयोग भर्ती, कट्टरपंथ और प्रचार प्रसार के लिए एक उपकरण के रूप में करते हैं।साथ ही आत्म-कट्टरपंथ और लोन वुल्फ हमलों में संभावित भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे: व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर फैली गलत सूचना से प्रेरित मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं।दुष्प्रचार अभियान, विशेषकर सीमावर्ती राज्यों में।विरोधी कारकों द्वारा अपनाई गई साइबर युद्ध रणनीति।असुरक्षित आबादी के खिलाफ अपराध: ऑनलाइन दुर्व्यवहार को बढ़ावा जैसे कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न, पीछा करने जैसी घटनाएँ साइबर अपराध: पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और हैकिंग। | सामाजिक ध्रुवीकरण का बढ़ना: प्रतिध्वनि कक्षों और फिल्टर बुलबुले का निर्माण (फ़िल्टर बबल और इको चैंबर.)। → वैचारिक आधार पर सामाजिक विखंडन। ग़लत सूचना और ग़लत आख्यानों का प्रचार → हिंसा और कलह को भड़काना। साइबर बहिष्करण: डिजिटल स्थानों के भीतर हाशिए पर जाना या भेदभाव। कैंसिल कल्चर का उद्भव: कथित अपराधों पर सार्वजनिक निंदा या बहिष्कार। नकारात्मक सामग्री उपभोग (डूम स्क्रॉलिंग): निराशावादी ऑनलाइन सामग्री में शामिल होने से धीरे-धीरे निराशा पैदा होती है। फ़बिंग घटना: फ़ोन के उपयोग के पक्ष में आमने-सामने की बातचीत की उपेक्षा करना। |
संक्षेप में, जबकि सोशल मीडिया ने सूचना का लोकतंत्रीकरण किया है और व्यक्तियों को सशक्त बनाया है, इसका अनियंत्रित प्रसार और दुरुपयोग आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, सोशल मीडिया प्लेटफार्म को विनियमित करना और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देना शामिल है।
Paper 4 (Comprehension part) – निबंध
समानो मन्त्रः समिति समानो
समानं मनः सह चित्तमेषाम
समानं मंत्राभिः मन्त्रये वः
समानेन वो हविषा जुहोनि !!
लोकतंत्र में समस्त शासन व्यवस्था का स्वरूप जन सहमति पर आधारित मर्यादित सत्ता के आदर्श पर व्यवस्थित होता है। हाल ही में नई दिल्ली में संसद 20 (Parliament-20) शिखर सम्मेलन ने विश्व के सामने भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत और मूल्यों को प्रदर्शित किया। समावेशिता, समानता तथा सद्भाव पर ज़ोर भारतीय लोकतंत्र का केंद्र है। लोकतंत्र केवल शासन के रूप तक ही सीमित नहीं है, वह समाज का एक संगठन भी है। लोकतंत्र वह समाज है जिसमें जाति, धर्म, वर्ण, वंश, धन, लिंग आदि के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं किया जाता है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए विधानमंडलों में आरक्षण व्यवस्था लागू की गयी। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, 1951 में पहले आम चुनाव के दौरान, भारत में 54 राजनीतिक दल थे और अब 2019 के आम चुनाव में यह बढ़कर 464 हो गया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गहराई का प्रमाण है। राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए उसका आर्थिक लोकतंत्र से गठबंधन आवश्यक है। आर्थिक लोकतन्त्र का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने विकास की समान भौतिक सुविधाएँ मिलें। आजादी के समय दो तिहाई जनसंख्या गरीबी से ग्रस्त थी जो अब 20 प्रतिशत के आसपास है। साथ ही, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर 1990 के दशक के आर्थिक संकट से निपटने तक लोकतांत्रिक मूल्यों का विशेष ख्याल रखा गया और इसी दायरे में रहते हुए एक क्षेत्रीय शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना इसका प्रमाण है। एक ओर घोर निर्धनता तथा दूसरी ओर विपुल संपन्नता के वातावरण में लोकतंत्रात्मक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है।
भारतीय लोकतंत्र समृद्ध है, अनूठा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है; परन्तु अब भारत जिसने हर संकट की घड़ी में बिना धैर्य खोये हर मुसीबत का सामना किया, अनेकों बुराइयों से जकड़ गया; मसलन आतंकवाद, भ्रष्टाचार, आर्थिक विषमता, जातिवाद, सत्ता लोलुपता के लिए सस्ती राजनीति करना जो कि कभी कभी सामाजिक वैमनस्य के साथ साथ देश की एकता को ही संकट में डाल देता है, राजनीति में वंशवाद व भाई-भतीजावाद, न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब आदि-आदि। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग ने सिविल और न्यायिक प्रशासन के बारे में कहा है कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, उदासीनता और अक्षमता ने गैर-कानूनी प्रणालियों, समानांतर अर्थ-व्यवस्थाओं और सामानांतर सरकारों तक को जन्म दिया है। इस कुशासन की वजह से लोगों का अब लोकतंत्र की संस्थाओं में अविश्वास और मोहभंग हो गया है। अनुच्छेद 311 ने सिविल सेवाओं को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की है, बेईमान अधिकारी अपने गलत कामों के परिणामों से बचने के लिए इस अनुच्छेद की आड़ लेते हैं। संविधान द्वारा स्थापित लोकतंत्रात्मक राज्य-व्यवस्था पर भारी दबाव है। राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण, बाहुबल, धनबल, और माफिया शक्ति के बढ़ते हुए महत्त्व, राजनीतिक जीवन में जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा भ्रष्टाचार के प्रभाव ने राजनीतिक परिदृश्य को विषाक्त कर दिया है। 17वीं लोकसभा में 50% सदस्य आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। भारत में आजादी के इतने वर्ष बाद अभी भी गरीब और अशिक्षित है जो कि एक कलंक के समान है। खंडित समाज में राष्ट्र की एकता, राष्ट्रीय अखंडता या भारतीय अस्मिता राजनीतिक मंचों से बोले जाने वाले नारे-मात्र सिद्ध हुए हैं। देश के लिए गर्व का ये मुहावरा “विविधता में एकता” जो भारत के लिए प्रयोग किया जाता है, राजनीतिज्ञों के दु-राजनीति करने का हथियार बन चुका है।
डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत पर flawed democracy का टैग लगाना और वी डेम रिपोर्ट द्वारा इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की संज्ञा देना सोचनीय है। राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के व्यापारियों वोटों के लिए धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश आदि के नाम पर फूट डालकर एकता को खंडित करते हैं। उनके लिए विकास, जनसेवा अथवा राष्ट्र-निर्माण की बात करना बेईमानी है। पद लोलुपता और शक्ति का केंद्र बनने की लालसा के चलते आंशिक बहुमत और गठबंधन सरकारें विकासात्मक मुद्दों के बजाय “रिजॉर्ट डेमोक्रेसी” तक सीमित हो गई हैं जहां राजनेताओं की बाड़ेबंदी और नवीन सरकार गठन की तरकीबों के पीछे समय जाया किया जाता है। यद्यपि भारत ने आजादी के 75 वर्षों के सफर में उल्लेखनीय प्रगति की हैं, अनेक समस्याओं का समाधान किया है, परंतु चुनौतियाँ खत्म नहीं हुई हैं। यदि हर स्तर पर सामूहिक कोशिश की जाए तो अनेक समस्याओं से और इन चुनौतियों से निजात पायी जा सकती है।
उपरोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु नवाचारों की जरूरत है। हाल ही में सांसद शशि थरूर जी ने संसद में सप्ताह में एक दिन “अपोजिशन डे” के रूप में घोषित करने की मांग की जो ब्रिटिश संसदीय नवाचार है। यह नवाचार मजबूत लोकतंत्र हेतु मजबूत विपक्ष की धारणा को बलवती बनाएगा। आलोचनाओं का स्वागत करने की परंपरा, सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द, धर्म और जाति पर राजनीति के बजाय मुद्दा आधारित राजनीति पर बल दिया जाए। इस हेतु चुनाव आयोग को पहल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी न्यायिक सक्रियतावाद के तहत नज़ीर पेश करनी चाहिए। सुधारों का एक विकल्प गांधी जी का मॉडल है जिसके अंतर्गत राजनीति को जनता की सेवा का साधन समझा जाता है, सत्ता का निम्न स्तर तक विकेंद्रीकरण होता है; साधारण व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है और शासन-कार्यों में भाग लेता है। शासन की इकाई गाँव होता है, सत्ता का रूख नीचे से ऊपर की ओर होता है, समूचा शासन पारदर्शी होता है। उपरोक्त समाधान और नवाचारों को अपनाते हुए अमृत काल के अंत (2047) तक हमें सही मायने में सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति करनी होगी।
विश्व भारत को लोकतंत्र की जननी (mother of democracy) के रूप में जनता है, पर अब देश के सामने जो चारित्रिक संकट है जो व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी। हर कर्तव्यपरायण नागरिक को विशेषकर युवाओं को व्यवस्था में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आगे आकर अपना विरोध जताना चाहिए; उनमें सुधार का प्रयास करना चाहिए। भारत युवाओं का देश हैं, युवा ही देश का भविष्य है। अब उन्हें ही समस्याओं तथा चुनौतियों के मूल तक जाना होगा और समझ कर उसका निदान ढूँढना होगा। युवाओं को अब स्वामी विवेकानंद जैसे चिंतको के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का समय आ गया है, उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा है कि-
“उत्तिष्ठत जाग्रत,
प्राप्यवरान्निबोधत !
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या
दुर्ग पथस्तत कवर्योवदन्ति !!”
Day 33 | 90 Days RAS Mains 2025 Answer Writing