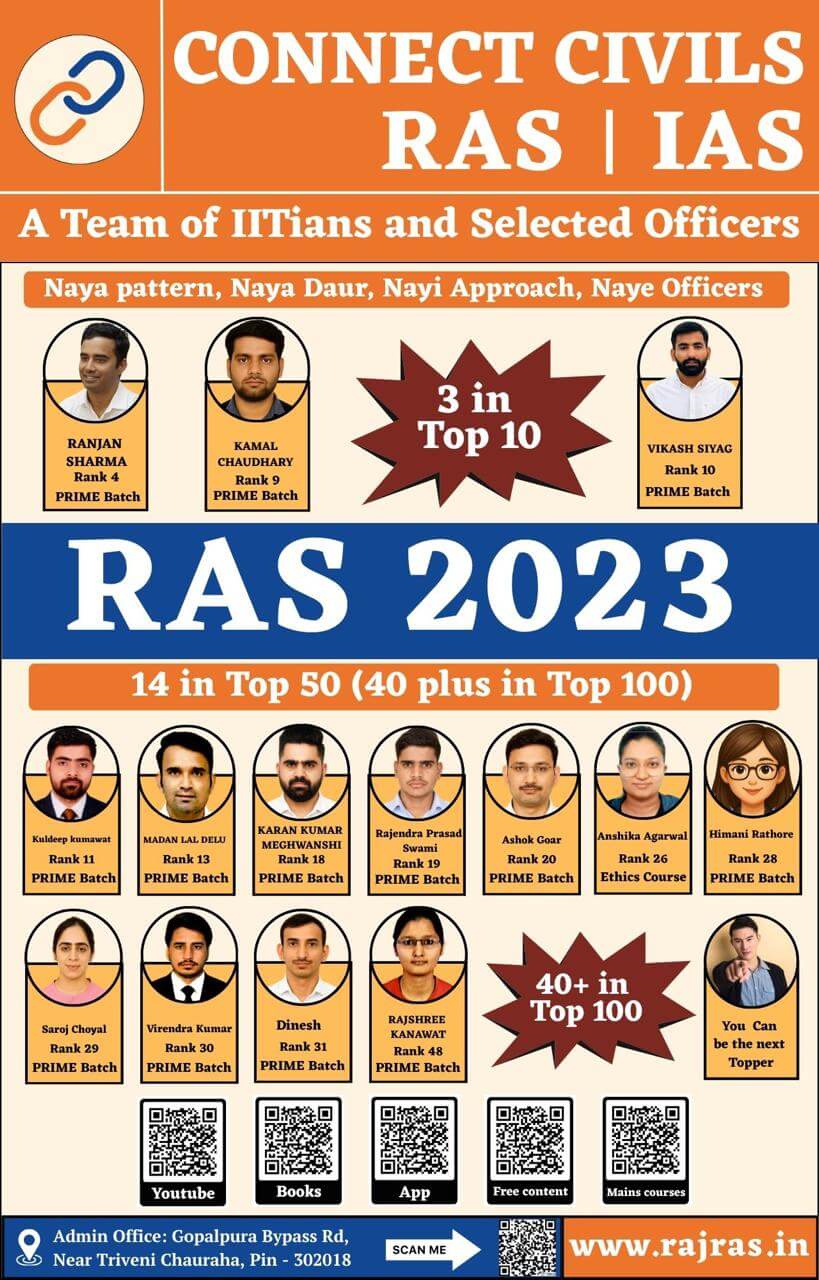सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार, सामाजिक न्याय और मानवीय चिन्ता नैतिकशास्त्र के अंतर्गत सत्यनिष्ठा न केवल व्यक्तिगत चरित्र की आधारशिला है, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदनाओं की भी मूल भावना को दर्शाती है। इस विषय के माध्यम से हम सत्य, न्याय और मानव कल्याण से जुड़ी दार्शनिक अवधारणाओं को गहराई से समझ सकते हैं।
विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न
सामाजिक न्याय, मानवीय चिन्ता
| वर्ष | प्रश्न | अंक |
| 2013 | समाज में निर्बल वर्गों के प्रति लोक सेवकों को अधिक करुणामय बनाने हेतु तीन सुझाव दें। | 5M |
| 2018 | अतिवाद घातक है । हम इससे कैसे बच सकते हैं ? | 5M |
सत्यनिष्ठा
- सत्यनिष्ठा शब्द लैटिन शब्द ‘इन-टैंगरे’ से आया है, जिसका अर्थ है अछूता [इसलिए वह सिद्धांत जिनसे कोई समझौता न किया जा सके ]
- स्थान, समय और संदर्भ की परवाह किए बिना नैतिक सिद्धांतों का कड़ाई से पालन (समझौता करने से पूर्ण इनकार)
- ज्ञान सही मार्ग को जानना है, सत्यनिष्ठा उस पर चलना है
- सत्यनिष्ठा नैतिक सिद्धांतों की सुदृढ़ता है।
- सिविल सेवा आचरण नियम ‘पूर्ण सत्यनिष्ठा’ की मांग करते है। सत्यनिष्ठा आपको किसी भी राजनीतिक दबाव से बचाती है, यदि आप एक ईमानदार अधिकारी हैं, जिसने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, तो राजनेता यह जानते हैं, अतः उनमें आपके कार्यालय में आकर अनुचित मांग करने का साहस कभी नहीं होगा। लेकिन अगर उन्हें पहले से ही पता है कि अधिकारी अनुचित तरीकों से पैसा बनाता है, तो वे आपसे संपर्क करेंगे। और उस स्थिति में, अधिकारी उनकी भ्रष्ट मांगों पर विचार न करने का नैतिक अधिकार खो देता है।
- एक ईमानदार अधिकारी कभी भी वरिष्ठ अधिकारियों, रिश्तेदारों या परिवार के किसी सदस्य के दबाव के आगे नहीं झुकेगा, भले ही उसे उस समय निजी रिश्तों से समझौता करना पड़े। वह सही काम केवल इसलिए करेगा क्योंकि वह सही है।
- कार्यबल में सत्यनिष्ठा से संगठन की कार्यक्षमता बढ़ती है।
- यह विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ाता है।
- दुविधा की स्थिति में सबसे उचित निर्णय लेने में मदद करता है। हितों के टकराव जैसी स्थितियों से बचाव होता है .
- महात्मा गांधी – चोरा चोरी कांड→ मन, कर्म और वचन में सामंजस्य।
- वह द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के लिए तैयार थे क्योंकि उस समय अंग्रेजों की कमजोरी का फायदा उठाना उनके नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ था। साथ ही साम्राज्य के एक हिस्से के रूप में, उन्होंने सोचा कि स्वतंत्रता की मांग को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए उस समय अंग्रेजों की मदद करना भारत का नैतिक कर्तव्य था।
नोट – ज्ञान के बिना सत्यनिष्ठा कमजोर और बेकार है, और सत्यनिष्ठा के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक है।
सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार
| आधार | अवधारणाएँ जो सत्यनिष्ठा की ओर ले जाती हैं |
| आंतरिक दृढ़ विश्वास | अंतरात्मा की आवाज (गांधी)आध्यात्मिक ज्ञान (बुद्ध)अंतर्निहित नैतिक मूल्य (करुणा जैसे मूल्य आनुवंशिक हो सकते हैं)मेयो क्लिनिक के शोध के अनुसार 30-60% दयालुता आनुवंशिक रूप से निर्धारित होती है। |
| प्राचीन भारतीय दर्शन | वेद – ऋग्वेद (ऋत और रिन)उपनिषद, गीता, स्मृतियाँ, संहिताएँपुरुषार्थ – धर्म, अर्थ, काम और मोक्षसत्यमेव जयते – मुण्डक उपनिषदमाँ गृध् कसास्यविद्नाम् – ईसावास्योपनिषद्चाण्क्य का अर्थशास्त्र |
| आधुनिक भारतीय दर्शन | विवेकानन्द, गाँधी, संविधान, प्रस्तावना आदि |
| पश्चिमी दर्शन | सुकरात – ज्ञान सर्वोच्च हैप्लेटो- सामंजस्यपूर्ण कार्यप्रणाली (मन, शरीर और आत्मा)अरस्तू – स्वर्णिम मध्य का सिद्धांतजॉन रावल – अज्ञानता का पर्दा (निष्पक्षता)कान्ट- कर्तव्य सर्वोपरि हैरूढ़िवाद – कष्ट के बिना, जीवन कायम नहीं रह सकताजेरेमी बेंथम – आपके काम से अधिकतम लोगों को लाभ होना चाहिएमैक्स वेबर – शक्ति के दुरुपयोग से बचने के लिए अवैयक्तिक।विश्व बैंक द्वारा सुशासन का आंदोलन 1992 (प्रशासन में सत्यनिष्ठा पर विशेष जोर) |
सामाजिक न्याय
- सामाजिक न्याय का तात्पर्य समाज में संसाधनों, अवसरों और विशेषाधिकारों के उचित विभाजन और समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण (ROPE) से है।
- विश्व सामाजिक न्याय दिवस – 20 फरवरी
सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों है?
- शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के लिए
- मानव जाति की गरिमा को बढ़ावा देना (कान्ट)
- धरती माता के संसाधनों का कुशल उपयोग (उपयोगितावाद)
- समाज में ख़ुशी को अधिकतम करना (अरस्तू का समम बोनम)
- जॉन रॉल्स का सामाजिक न्याय का सिद्धांत
- राज्य का कर्तव्य [कर्तव्यशास्त्र, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत]
- 1. अनुच्छेद 38– एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था करना जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल हो
- 2.अनुच्छेद 39– समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम हित की पूर्ति हो सक
- लोकसंग्रह (समाज का कल्याण – गीता)
- सर्वोदय और अंत्योदय, तलिस्मान (गांधी)
उदाहरण
- 1950 और 60 के दशक का अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन
- संवैधानिक प्रावधान – अनुच्छेद 14, 15, 16, 17
- आरक्षण की मांग (सकारात्मक भेदभाव)
- 1970 के दशक का दलित आंदोलन
- गरीबों और वंचितों के लिए सरकारी योजनाएं
- अन्ना हजारे आंदोलन (भ्रष्टाचार के खिलाफ)
- आदिवासी आंदोलन – ओडिशा में नियामगिरि सुरक्षा समिति
- LGBTQ+ अधिकार आंदोलन, तीसरे लिंग को मान्यता
- मनोवृत्ति में परिवर्तन-अपंग की जगह दिव्याँग
मानवीय चिंता
ऐसी घटना या घटनाओं की श्रृंखला, जो व्यापक रूप से मानवता के लिए खतरा उत्पन्न करती है, मानवीय चिंता कहलाती है।
मानवीय चिंता एवं प्रशासन से संबंधित उनके उदाहरण
प्राकृतिक आपदाएँ (भूकंप, सुनामी, बाढ़)
- नेपाल भूकंप 2015 – भारतीय प्रशासनिक मशीनरी ने भोजन, दवा, पानी, प्राथमिक चिकित्सा आदि की आपूर्ति करके ऑपरेशन मैत्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- 2018 में केरल में बाढ़ – आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने घर गए बिना 8 दिनों तक लगातार काम किया और एक अन्य आईएएस अधिकारी एमजी राजमाणिक्यम ने अपने कंधे पर चावल की बोरियां उठाईं
- सुनामी 2004 – भारत सरकार ने श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित सुनामी से प्रभावित अन्य देशों को राहत सहायता प्रदान की।
- सीरिया भूकंप 2023 – ऑपरेशन दोस्त
महामारियाँ एवं महामारियाँ-कोविड 19
- भीलवाड़ा मॉडल (आईएएस राजेंद्र भट्ट और टीना डाबी)
- सख्त लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन ने की मदद
- ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री (100 से अधिक देशों को कोविड वैक्सीन)
सीमा पार संकट
- यूक्रेन (ऑपरेशन गंगा), सीरिया, अफगानिस्तान और सूडान (ऑपरेशन कावेरी) से भारतीयों की निकासी
जलवायु परिवर्तन
- सौर ऊर्जा नीति, जैव ईंधन नीति, नवीकरणीय ऊर्जा पर काम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच आदि सक्षम भारतीय प्रशासन द्वारा डिजाइन, कार्यान्वित और समन्वित किए गए हैं।
- जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत शीर्ष 10 में।
आतंक
- भारत संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ी शांति सेना वाले देशों में से एक है।
गरीबी
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मनरेगा, पीएम किसान जैसी विभिन्न योजनाएं
राजनीतिक शरणार्थी संकट
- सीएए का कार्यान्वयन – प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को बचाना।
- भारत ने 1950 के दशक से तिब्बती शरणार्थियों की मेजबानी की है, उन्हें आश्रय, शिक्षा और आजीविका के अवसर प्रदान किए हैं।
- भारत ने म्यांमार में हिंसा से भाग रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दी है।
सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार
FAQ (Previous year questions)
हाल ही में, गोपालगंज (बिहार) के जिला मजिस्ट्रेट ने सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ते हुए एक निम्न जाति की विधवा द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के लिए बनाए गए भोजन को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, जिससे अस्पृश्यता के खिलाफ एक मजबूत संदेश गया। यह इस बात का प्रतिबिंब है कि नैतिक, मूल्य-प्रेरित प्रशासनिक कार्रवाई जमीनी स्तर पर सामाजिक सुधार को बढ़ावा दे सकती है।
सामाजिक सुधार में प्रशासन की भूमिका –
सामाजिक सुधार
प्रशासन की भूमिका
गरीबी उन्मूलन
गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है – महात्मा गांधी।सर्वोदय और लोक संग्रह के सिद्धांतों का पालन करना।सरकारी योजनाओं जैसे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, डीबीटी योजनाएँ, पेंशन योजनाएँ, मुद्रा योजना आदि का प्रभावी कार्यान्वयन।सहकारी आंदोलन [उदाहरण – वर्गीज कुरियन]।
महिला सशक्तिकरण
“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता”।प्रत्येक मानव एक साध्य है और इसलिए समान व्यवहार का हकदार है – कांट।विशाखा दिशानिर्देश, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1961 आदि का अनुपालन सुनिश्चित करना।बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PCPNDT अधिनियम, उज्ज्वला योजना आदि योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।
भ्रष्टाचार से मुकाबला (व्हिसलब्लोइंग)
“मा गृधः कस्यस्विद्धनम्” – किसी के धन का लालच न करें (ईशा उपनिषद)।लोकपाल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से।उदाहरण – दुर्गा शक्ति नागपाल, सत्येंद्र दुबे, अशोक खेमका आदि।
धार्मिक सद्भाव
विश्व बंधुत्व के सिद्धांत का सम्मान [वसुधैव कुटुंबकम]।संवैधानिक मूल्यों जैसे धर्मनिरपेक्षता, समानता, और बंधुत्व को बनाए रखना।अनुच्छेद 25-28 [धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार]।हेट न्यूज़, धार्मिक असहिष्णुता, कट्टरवाद आदि के खिलाफ कार्रवाई।
शैक्षणिक सुधार
NEP 2020 का कार्यान्वयन।बच्चों में सहानुभूति, करुणा, और साहस जैसे मूल्यों का समावेश।बच्चों में नैतिक तर्क का विकास (सुकरात)।उदाहरण – प्रभाकर रेड्डी (IAS, आंध्र प्रदेश), जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया → उदाहरण के माध्यम से नेतृत्व।
स्वास्थ्य सुधार
“सर्वं भवन्तु सुखिनः, सर्वं सन्तु निरामयाः” – सभी सुखी हों, सभी रोगमुक्त हों।प्रशासकों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित निरीक्षण।पीएम जन औषधि केंद्र, आयुष्मान भारत योजना आदि योजनाओं का कार्यान्वयन।
युवा सशक्तिकरण
युवाओं में कौशल विकास।उदाहरण – “कलेक्टर ब्रॉ” नाम से प्रसिद्ध एन. प्रशांत (IAS, केरल कैडर) – युवाओं के साथ सोशल मीडिया पर सक्रिय सहभागिता के लिए लोकप्रिय
जैसा कि गांधी जी ने कहा, “विश्व में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं, उसे स्वयं बनें”, प्रशासकों को उन मूल्यों को अपनाना चाहिए जिन्हें वे समाज में बढ़ावा देना चाहते हैं।
अतिवाद एक ऐसी स्थिति या गुण है जिसमें व्यक्ति राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या वैचारिक दृष्टिकोणों में अति पर चला जाता है। इसका मुख्य कारण असहिष्णुता, एकांगी सोच, और समालोचनात्मक विचारों की कमी होती है।
अतिवाद घातक है क्योंकि –
हिंसा या युद्ध को जन्म देता है – हिटलर के अतिवादी विचारों ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया।
सामाजिक सद्भाव को नष्ट करता है – यह किसी विशेष विचार, वर्ग, धर्म, या समुदाय के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है [यहूदी समुदाय के लिए खतरा]।
यह आतंकवाद का प्रजनन स्थल है [उदाहरण – धार्मिक कट्टरवाद]।
सामूहिक कल्याण (लोक संग्रह) में बाधा डालता है – अतिवादी कृत्य संकीर्ण और स्वार्थी होते हैं, जो समाज के व्यापक हित को नुकसान पहुंचाते हैं।
वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के विरुद्ध है – क्योंकि यह समभाव और सार्वभौमिक भाईचारे के विचार को नकारता है।
इससे कैसे बचा जा सकता है?
समालोचनात्मक सोच विकसित करके – सुकरात ने “Know Thyself” (स्वयं को जानो) पर बल दिया और अंधविश्वासों को तर्क के माध्यम से चुनौती दी। उनका मानना था कि अज्ञान ही अतिवाद जैसे बुराइयों की जड़ है।
प्लेटो के अनुसार न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करके – शासक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हों जो अतिवादी विचारों का प्रचार न करें।
स्वर्णिम मध्यमार्ग के सिद्धांत (Golden Mean) का पालन – उग्रवाद विश्वास, व्यवहार या भावना की अति को दर्शाता है। वाणी, विचार और कर्म में संतुलन इस प्रवृत्ति से बचने में मदद करता है।
गांधीजी का संयम और अहिंसा – किसी को भी विचार, वचन या कर्म से हानि नहीं पहुँचाना चाहिए।
ईशावास्यम इदं सर्वम् – क्योंकि सब कुछ ईश्वर का अंश है और इसलिए प्रत्येक प्राणी करुणा का पात्र है।
स्वामी विवेकानंद का सार्वभौमिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक एकता – विवेकानंद ने सभी प्राणियों की दिव्यता, धार्मिक बहुलता और निःस्वार्थ सेवा पर बल दिया, जिससे अतिवाद से बचा जा सकता है।
गीता का लोक संग्रह सिद्धांत – अतिवाद स्व-केंद्रित या समूह-केंद्रित सोच से उत्पन्न होता है। निष्काम भाव से समाज के कल्याण के लिए कार्य करना सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है।
उपयोगितावाद (Utilitarianism) – अतिवादी कृत्य अल्पकालिक लाभ तो दे सकते हैं, परंतु दीर्घकालिक हानि पहुंचाते हैं। इसलिए “सर्वाधिक लोगों के लिए सर्वाधिक कल्याण” का सिद्धांत अपनाना चाहिए।
सत्य, न्याय, सहानुभूति, सहिष्णुता और संतुलन जैसे मूल्यों को अपनाकर।