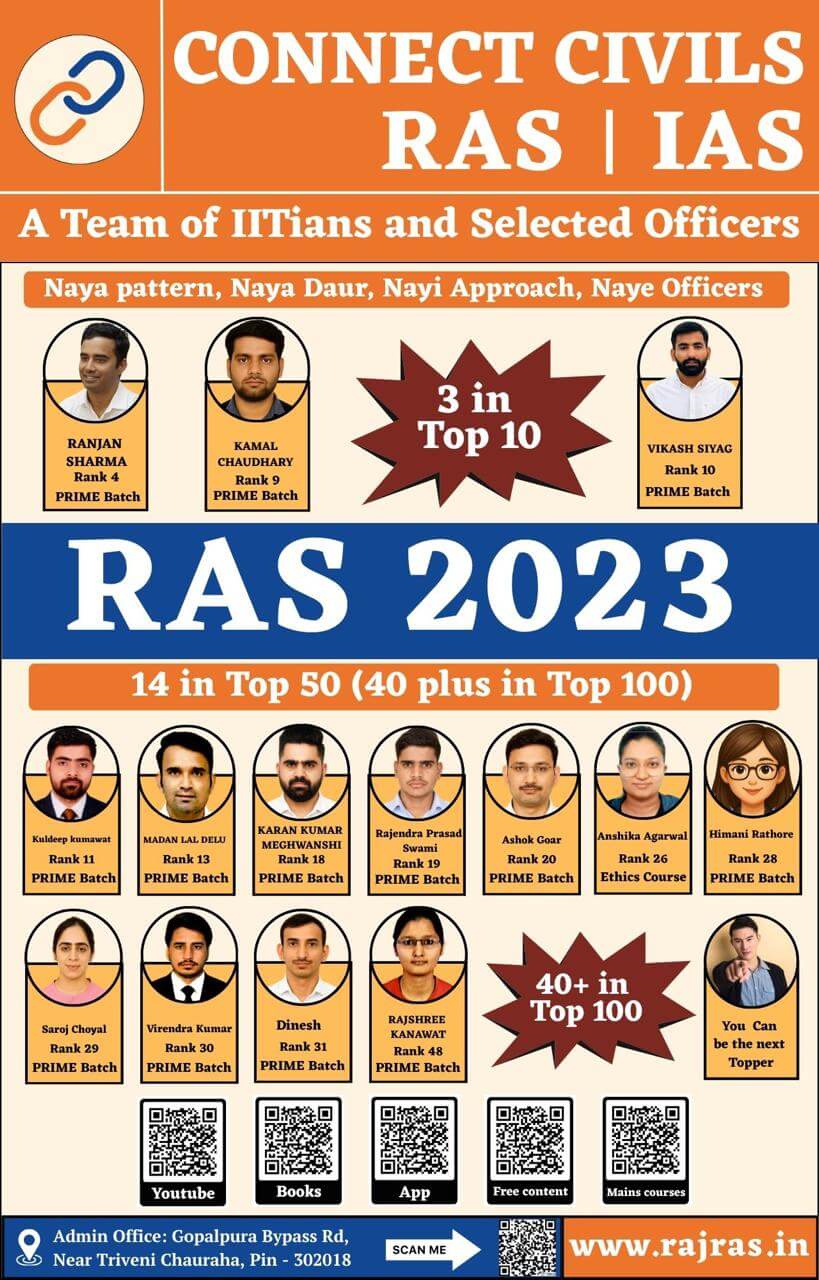राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय
राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय राजस्थान इतिहास & संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, जिन्होंने समाज में आध्यात्मिक जागरण और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। इन संतों और उनके संप्रदायों ने भक्ति, सेवा और समानता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाया, जिससे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और भी समृद्ध हुई।
विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न
| वर्ष | प्रश्न | अंक |
| 2012 | दादू संप्रदाय की राजस्थान में चार शाखाएँ | 2M |
| 2008 | पुष्टिमार्ग | 2M |
| 2008 | संत राना बाई | 2M |
| 2007 | पाशुपत संप्रदाय | 2M |
| 1985 | दादूपंथियों के प्रमुख तीर्थ स्थल | 2M |
| 2000 | निरंजनी संप्रदाय | 5M |
| 1997, 1994 | संत जाम्भोजी | 5M |
| 1994 | सुंदरदास जी के उपदेशों का वर्णन। | 5M |
| 2010 | मध्यकालीन राजस्थान के भक्ति संत और लोक देवताओं का वर्णन करें। | 10M |
| 2007 | धार्मिक मान्यताएँ एवं संप्रदाय तथा प्रमुख संतों एवं उनके पंथों की विवेचना कीजिए। | 10M |
| 1991 | भक्ति आंदोलन क्या था? इसके प्रमुख संतों की शिक्षाओं का वर्णन करें। | 10M |
राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय
राजस्थान एक ऐसा भूमि है जो विविध धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं से समृद्ध है, जहाँ विभिन्न संतों और संप्रदायों ने इसकी सांस्कृतिक धरोहर को आकार दिया है। आराधना की विधियों के आधार पर, राजस्थान की आध्यात्मिक परंपराओं को दो प्रमुख संप्रदायों में बाँटा जा सकता है: सगुण और निर्गुण।
- सगुण संप्रदाय:
- यह संप्रदाय रूप, गुण और मूर्तियों के साथ भगवान की पूजा करता है, जिसमें प्रमुख रूप से राम और कृष्ण जैसे देवताओं की पूजा की जाती है।
- सगुण संप्रदाय की कुछ प्रमुख शाखाएँ: रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, पशुपत संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय।
- निर्गुण संप्रदाय:
- यह संप्रदाय निराकार, गुणविहीन भगवान की पूजा करता है, जिसमें आंतरिक भक्ति और आत्मिक अनुभव को महत्व दिया जाता है।
- निर्गुण संप्रदाय की कुछ प्रमुख शाखाएँ : विश्नोई संप्रदाय, जाम्बोजी संप्रदाय, दादू संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, कबीरपंथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय
वैष्णव संप्रदाय
वे लोग जो भगवान विष्णु और उनके दस अवतारों की पूजा करते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। इस संप्रदाय में भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति, कीर्तन, नृत्य आदि को प्राथमिकता दी जाती थी। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के घोसुंडी अभिलेख में मिलता है । राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रमुख संप्रदाय निम्नलिखित हैं ।
रामानंदी संप्रदाय :
- यह वैष्णव संप्रदाय की सबसे पुरानी शाखा है।
- यह संप्रदाय रामानंद जी द्वारा स्थापित किया गया, जो रामानुज के पाँचवें शिष्य थे और जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया।
- राम की पूजा इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र है।
- रामानंदी संप्रदाय में 12 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें धन्ना जी, पीपा जी, कबीर, और अनंतानंद जी शामिल थे।
- राजस्थान में इस संप्रदाय की स्थापना श्री कृष्णदास जी पयहारी ने की थी, जो अनंतानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने 1503 ई. में गालता जी (उत्तर तोताद्रि), जयपुर में इस संप्रदाय की मुख्य शाखा स्थापित की।
- रामानंदी संत जनेऊ और तुलसी की माला पहनते हैं, साथ ही उनके माथे पर गोपीचंदन से खड़ा तिलक किया जाता है।
- रासिक संप्रदाय की स्थापना आग्रदास जी ने की थी, जो पयहारी जी के शिष्य थे। इस संप्रदाय में राम को ‘रासिक नायक’ के रूप में पूजा जाता है।
- लश्करी शाखा: जयपुर के शासक सवाई मानसिंह जी इस संप्रदाय के एक नागा संत बालानंद जी से प्रभावित होकर जयपुर में उनका एक बड़ा स्थल बनवाया जो की लश्करी शाखा के नाम से जाना गया।
- बालानंद जी ने जयपुर के शासकों को मराठा आक्रमणों से बचाया और 1760 में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ भारतपुर के शासक की मदद की।
- उपदेश:
- राम के प्रति भक्ति: राम को सर्वोच्च देवता मानकर पूर्ण भक्ति का महत्व।
- भक्ति में समानता: सभी जातियों और पृष्ठभूमियों के लोगों को भक्ति में समान स्थान।
- सरल जीवन: त्याग, विनम्रता, और साधारण जीवन की प्रधानता।
- गुरु-शिष्य परंपरा: आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए गुरु का महत्व।
- भक्ति आंदोलन का प्रसार: प्रेम, भक्ति और सेवा का संदेश फैलाने की प्रेरणा।
- हिंदी का प्रचार: संस्कृत की बजाय हिंदी का प्रयोग, ताकि आम जन तक आध्यात्मिक शिक्षाएँ पहुँच सकें।
वल्लभ संप्रदाय :
- संस्थापक: वल्लभाचार्य जी
- राजस्थान में मुख्य शाखा: नाथद्वारा (राजसमंद)
- गोस्वामी दामोदरदास जी और गोविंद जी ने श्रीनाथ जी की मूर्ति को औरंगजेब से छिपते-छिपाते ब्रज क्षेत्र से सिहाड़ गाँव में स्थानांतरित किया वहाँ महाराणा राजसिंह जी ने श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की और सिहाड़ गाँव को नाथद्वारा के नाम से जाना जाने लगा।
- यह संप्रदाय कृष्ण के बाल रूप की पूजा करता है और ‘सेवा’ के माध्यम से कृष्ण के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करता है।
- संप्रदाय की शाखाएँ:
- द्वारकाधीश जी – कंकरोली (राजसमंद)
- मथुरेश जी – कोटा
- गोपालचंद जी – क़ामाँ (भरतपुर)
- मदन मोहन जी – क़ामाँ (भरतपुर)
- विठलनाथ जी – नाथद्वारा (राजसमंद)
- गोवर्धननाथ जी – गोवर्धन (उत्तर प्रदेश)
- बालकृष्ण जी – सूरत (गुजरात)
- किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह ने इस संप्रदाय को अपनाया, अपना राज्य त्याग दिया और वृंदावन में जाकर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए एवं अपना नाम नागरीदास रख लिया।
- उपदेश:
- कृष्ण के प्रति भक्ति: कृष्ण को सर्वोच्च देवता मानकर पूर्ण समर्पण और भक्ति का पालन।
- पुष्टिमार्ग: इस मार्ग में भगवान की कृपा को मुक्ति का मार्ग माना जाता है।
- सेवा: कृष्ण की मूर्ति की प्रतिदिन पूजा और सेवा का महत्व।
- भक्ति और गृहस्थ जीवन: गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का पालन करना, त्याग की बजाय भक्ति को प्राथमिकता देना।
- भक्ति में समानता: सभी जातियों और समुदायों के भक्तों का स्वागत।
रामस्नेही संप्रदाय :
रामस्नेही संप्रदाय एक निर्गुण संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति रामानंदी परंपरा से हुई है। राजस्थान में इसकी चार शाखाएँ हैं।
शाहपुरा शाखा :
- संस्थापक: रामचरन जी (शाहपुरा, भीलवाड़ा)।
- प्रथाएँ:
- निर्गुण भक्ति का पालन।
- मूर्ति पूजा का निषेध।
- केवल फूलडोल उत्सव का आयोजन।
- ग्रंथ: शिक्षाएँ अनवैभावनी में संकलित।
- शिक्षाएँ:
- मोक्ष प्राप्ति के लिए “राम” नाम की महिमा।
- जाति व्यवस्था का विरोध।
- नैतिकता, ईमानदारी, और धार्मिक अनुशासन पर जोर।
- अच्छी संगति और सत्य के प्रति भक्ति का महत्व।
रैन शाखा :
- संस्थापक: दरियाव जी (रैन, मेड़ता)।
- शिक्षाएँ:
- मोक्ष के लिए गुरु की भूमिका पर जोर।
- गुरु की भक्ति से ही मुक्ति संभव।
- “राम” नाम जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग।
सिंहथल शाखा :
- संस्थापक: हरिरामदास जी (बीकानेर)।
- शिक्षाएँ:
- गुरु को भगवान के बाद दूसरा स्थान।
- हिंदू और मुस्लिम के बीच भेदभाव का विरोध।
खेड़ापा शाखा :
- संस्थापक: रामदास जी (खेड़ापा, जोधपुर)।
रामस्नेही संप्रदाय की शिक्षाएँ:
- राम भक्ति: मोक्ष प्राप्ति के लिए “राम” नाम की महिमा पर जोर।
- समानता: जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव का सख्त विरोध।
- गुरु की भूमिका: गुरु को ईश्वर के बाद दूसरा स्थान, मोक्ष के लिए अनिवार्य।
- नैतिकता और सत्य: सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने पर जोर।
- निर्गुण भक्ति: निर्गुण ईश्वर की आराधना, मूर्ति पूजा और अनावश्यक कर्मकांडों से परहेज।
- सरल जीवन: साधारण जीवन जीने की शिक्षा, फूलडोल जैसे उत्सव मनाने की परंपरा।
- अच्छी संगति: आध्यात्मिक प्रगति के लिए सत्संग और अच्छे लोगों की संगति का महत्व।
- सार्वभौमिक भाईचारा: सभी धर्मों और समुदायों में एकता को बढ़ावा, मानवता को प्राथमिकता।
- अनुशासन: आत्म-नियंत्रण और धार्मिक अनुशासन पर बल।
- सेवा भाव: सेवा को ईश्वर से जुड़ने का माध्यम मानना।
निम्बार्क संप्रदाय :
- संस्थापक: आचार्य निम्बार्क द्वारा स्थापित।
- दर्शन: द्वैताद्वैत (द्वैत-अद्वैत) नामक नया दर्शन प्रस्तुत किया।
- इसे हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है।
- यह संप्रदाय राधा-कृष्ण के युगल स्वरूप (युगल स्वरूप) की पूजा, जिसमें राधा को श्रीकृष्ण की परिणीता माना जाता है।
- इस संप्रदाय को राजस्थान में परशुराम जी ने स्थापित किया।
- स्थापना स्थान: सलेमाबाद, किशनगढ़ (अजमेर)।
- परशुराम जी ने ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी में ‘परशुराम सागर’ नामक काव्य की रचना की।
- शिक्षाएँ :
- द्वैताद्वैत दर्शन: द्वैत और अद्वैत का सामंजस्य।
- राधा-कृष्ण पूजा: राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा।
- गुरु भक्ति: आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु का महत्व।
- निस्वार्थ सेवा: ईश्वर की निस्वार्थ सेवा और भक्ति पर जोर।
- समानता: सभी प्राणियों में समानता की शिक्षा, जाति भेद का विरोध।
- भक्ति: मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति योग पर जोर।
- नैतिक जीवन: सत्य, ईमानदारी और धर्म के पालन का महत्व।
गौड़ीय संप्रदाय :
- संस्थापक: इस संप्रदाय के प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभू थे।
- आराध्य देव: भगवान विष्णु की सच्चिदानंद (सत, चित, आनंद) रूप में पूजा।
- जयपुर के राजा मानसिंह जी ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया।
- सवाई जयसिंह जी ने जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया।
- जयपुर के शासकों ने गोविंद देव जी को जयपुर का राजा घोषित किया और ख़ुद को उनका दीवान।
- करौली का मदन मोहन जी का मंदिर भी इसी संप्रदाय से संबंधित है।
विश्नोई संप्रदाय :
- 1485 ईस्वी में, जांभोजी ने समराथल में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की।
- जांभोजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, और उनके अनुयायियों को विश्नोई कहा जाता है।
- जांभोजी ने अपने अनुयायियों के लिए 29 सिद्धांत दिए, जो पशु कल्याण और वृक्षों की रक्षा पर जोर देते हैं।
- संप्रदाय का एक मुख्य सिद्धांत यह है कि पशुओं और पर्यावरण के कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
- प्रकृति के प्रति गहरे लगाव के कारण जांभोजी को पर्यावरणविद् भी माना जाता है।
- जांभोजी के अनुसार, “सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान”, जिसका तात्पर्य है कि वृक्ष की रक्षा के लिए यदि किसी को अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़े, तो यह एक महान और मूल्यवान बलिदान है।
- जांभोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ
- जांभ संहिता
- जांभ सागर शब्दावली
- विश्नोई धर्मप्रकाश
- जांभसागर
- महत्वपूर्ण स्थल:
- मुकाम (नोक़ा, बीकानेर): यह वह स्थान माना जाता है जहां जांभोजी ने समाधि प्राप्त की थी।
- समराथल (बीकानेर): जांभोजी ने जीवन के सामंजस्यपूर्ण मार्ग के लिए 29 उपदेशों के रूप में अपनी शिक्षाएं दीं।
- जांभोजी नगरी (पीपासर): यह गुरु जांभोजी का जन्मस्थान है, जो राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है।
- जांभोजी की शिक्षाएं :
- भगवान विष्णु की पूजा: भगवान विष्णु को परम देवता मानते हुए पूर्ण भक्ति पर बल।
- समानता और सामाजिक सुधार: जाति प्रथा का विरोध और सभी व्यक्तियों के बीच समानता का प्रचार।
- धार्मिक कट्टरता का विरोध: हिंदू और इस्लाम दोनों में कठोर धार्मिक प्रथाओं की आलोचना करते हुए समावेशी आध्यात्मिकता को बढ़ावा।
- पर्यावरण संरक्षण: पशुओं और वृक्षों की रक्षा का समर्थन, और प्रकृति के संरक्षण को प्राथमिकता देने की प्रेरणा (जैसे “सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान”)।
- निःस्वार्थ सेवा: दूसरों और प्रकृति के कल्याण पर केंद्रित, सेवा, बलिदान और सादगीपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा।
आधुनिक समय में जांभोजी की शिक्षाओं की प्रासंगिकता
- पर्यावरण संरक्षण: “सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान” जैसे सिद्धांत जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के समाधान के लिए प्रेरणा देते हैं।
- सामाजिक समानता और समरसता: जाति-आधारित भेदभाव और सांप्रदायिक संघर्षों को समाप्त करने के प्रयासों में उनकी शिक्षाएं प्रेरणादायक हैं।
- आध्यात्मिकता और समावेशिता: धर्म के नाम पर विभाजन और हिंसा के समय में उनकी समावेशी आध्यात्मिकता शांति और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देती है।
- निःस्वार्थ सेवा और सरल जीवन: सादगी और सेवा पर उनका जोर उपभोक्तावाद और भौतिकवाद से जूझ रहे आधुनिक समाज के लिए एक शक्तिशाली संदेश है।
- प्राकृतिक आपदाओं और जल संकट के समाधान: जल संरक्षण, वृक्षारोपण और भूमि संरक्षण जैसे उनके नियम आज के जल संकट और प्राकृतिक आपदाओं का व्यावहारिक समाधान प्रदान करते हैं।
- वैश्विक पर्यावरणीय आंदोलनों में योगदान: उनकी “प्रकृति ही जीवन है” की विचारधारा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से गहराई से जुड़ी हुई है।
जसनाथी संप्रदाय :
- जसनाथजी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर (बीकानेर) में हुआ था। उनके गुरु गोरखनाथ थे। एक प्रसिद्ध किवदंती के अनुसार, उन्होंने गोरखमलिया (बीकानेर) में बारह वर्षों तक कठोर तपस्या की और सभी प्राणियों के प्रति करुणा का संदेश दिया।
- इस संप्रदाय के लोग 36 नियमों का पालन करते है, एवं गले में काली ऊन का धागा पहनते है एवं अग्नि नृत्य कृति हैं।
- जसनाथजी ने एक तांत्रिक लोह पांगल के घमंड को तोड़ा और उसे पराजित किया।
- उन्होंने राव लूणकर्ण को बीकानेर का शासक बनने का आशीर्वाद भी दिया।
- उनकी चमत्कारी शक्तियों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुलतान सिकंदर लोदी ने उन्हें कतरियासर के पास भूमि दान दी।
- 1500 ईस्वी में जसनाथजी और जांभोजी की मुलाकात हुई।
- 1506 ईस्वी में आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन मात्र चौबीस वर्ष की आयु में जसनाथजी ने कतरियासर में समाधि ली।
- उनकी शिक्षाएं सिंभुधडा और कोंडो ग्रंथों में संगृहीत हैं।
- लालदासजी, चोखनाथजी एवं सवाईदास जी इसी संप्रदाय से संबंधित थे ।
- जसनाथजी की शिक्षाएं
- करुणा और अहिंसा: जसनाथजी ने सभी प्राणियों के प्रति करुणा और अहिंसा का प्रचार किया। उनका संदेश था कि जीवन में सबके साथ प्रेम और दया से पेश आना चाहिए।
- तंत्र-मंत्र के सिद्धांतों का विरोध: उन्होंने तंत्र-मंत्र के अंधविश्वास और रूढ़िवादी पद्धतियों का विरोध किया।
- ईश्वर की भक्ति: जसनाथजी ने जीवन में ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण की बात की।
- सामाजिक समानता: उन्होंने समाज में असमानता को दूर करने और सभी को समान सम्मान देने की शिक्षा दी।
- आध्यात्मिक साधना: तपस्या और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति पर जोर दिया।
लालदासी संप्रदाय:
- प्रवर्तक: लालदासजी
- जन्मस्थान: धोलिदूब गाँव, अलवर
- इन्होंने तिजारा के गदन चिस्ती से दीक्षा ली एवं लालदासी संप्रदाय का प्रारंभ कर निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया।
- लालदासजी के उपदेश ‘लालदास की चेतावणी’ में संग्रहित है।
- इनका देहांत 108 वर्ष की आयु में नगला (भरतपुर) में हुआ।
- लालदासजी के अनुसार इस पंथ में अकर्मण्यता को कोई स्थान नहीं है, और उन्होंने जीवन में परिश्रम और सच्चे आचरण की महत्वपूर्णता पर जोर दिया।
- उनका प्रसिद्ध कथन था: “लालजी साधु ऐसा चाहिए, धन कमाकर खाय। हिर्दे हर की चाकरी, पर घर कभु ना जाए।“
- यह उपदेश संतों के जीवन की दिशा को दर्शाता है कि एक सच्चे साधु को कभी भी भिक्षा या चाकरी के लिए दूसरों के घर नहीं जाना चाहिए। उसे अपने परिश्रम से जीविकोपार्जन करना चाहिए और अपने हृदय में केवल हरि (राम) के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए।
- लालदासजी, कबीर, दादू आदि संतों की तरह निराकार, सर्वव्यापक, और सत्यस्वरूप हरि की अनन्य भक्ति पर विश्वास रखते थे। वे सत्य आचरण और सरल, पवित्र जीवन जीने के पक्षधर थे।
अलखिया संप्रदाय:
- अलखिया संप्रदाय के संस्थापक साधु ‘लालगिरी’ का जन्म चुरू जिले में हुआ था।
- उन्होंने बचपन में ही नागा साधु बनने का संकल्प लिया और बीकानेर किले के सामने 12 वर्षों तक तपस्या की। आज भी उनकी याद में वहां एक लाल पत्थर स्थापित किया गया है, जहां इस संप्रदाय के लोग नारियल चढ़ाने आते हैं।
- वह जाति से मोची थे, लेकिन उनके शिष्य सभी जातियों से थे। इस संप्रदाय के लोग जातिवाद और ऊँच-नीच में विश्वास नहीं करते हैं।
शैव धर्म
राजस्थान में भगवान शिव की पूजा विभिन्न नामों से की जाती है, जैसे- एकलिंग, गिरिपति, समाधिश्वर, चंद्रचूड़मणि, भवानीपति, अचलेश्वर, शंभु, पिनाकी, और स्वयंभू। 7वीं-8वीं शताबदी के पुरातात्विक प्रमाण, जैसे- शिव के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन, अभानेरी और ओसियां जैसे स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जो शिव की पूजा की प्राचीनता को दर्शाते हैं।
शैव धर्म का राजस्थान की कई राजवंशों पर गहरा प्रभाव था, विशेष रूप से मेवाड़ और मारवाड़ के राजतंत्रों पर। मेवाड़ में, लकुलिश पंथ का प्रमुख प्रभाव था, जबकि मारवाड़ में, नाथ पंथ ने शैव विश्वासों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
लकुलिश पंथ (पशुपत) :
- प्रवर्तक: लकुलिश, जिन्हें पशुपत पंथ के अनुयायी शिव के 28वें और अंतिम अवतार के रूप में मानते हैं।
- मेवाड़ में लकुलिश पंथ के संत हरित ऋषि थे। उदयपुर के राजपरिवार इन्ही का सदस्य था।
- उदयपुर स्थित एकलिंग (शिव) मंदिर लकुलिश पंथ का प्रमुख मंदिर है, जिसे बापा ने बनवाया।
- उदयपुर के महाराणाओं ने भगवान एकलिंग को उदयपुर के राजा के रूप में माना और खुद को उनका दीवान माना।
- लकुलिश पंथ का राजस्थान में महत्वपूर्ण प्रभाव था, और कई मंदिरों में, जैसे- जालोर जिले के सुगंधा (सुंडा) माता मंदिर में आज भी लाकुलीश परंपरा के शिव प्रतिमाएं स्थापित हैं।
नाथ पंथ :
- मुख्य प्रचारक: मत्स्येन्द्रनाथ जी
- राजस्थान में नाथ पंथ की दो प्रमुख शाखाएं प्रसिद्ध हैं:
- बैरागी पंथ: इसका पहला प्रचारक भार्तृहरी को माना जाता है, और इसका मुख्य केंद्र ‘रताड़ूँगा’ (पुष्कर के पास) में स्थित है।
- माननाथी पंथ: इसका मुख्य केंद्र जोधपुर में स्थित महामंदिर में है, जिसे जोधपुर के राजा मानसिंह ने स्थापित किया था।
- 852 ईस्वी में, योगी रतननाथ ने भाटी राजा देवराज को लोद्रवा (जैसलमेर) का राजा बनाया और उन्हें ‘रावल’ की उपाधि दी, जिनका मठ जैसलमेर के बाहर स्थित था।
- नाथ पंथ के अनुयायीयों की राजस्थान में अनेक क़िस्में है: नाथ, मसाणिया, कालबेलिया, ओघड़, अघोरी, रावल।
निरंजनी पंथ :
- प्रवर्तक: हरिदास जी
- हरिदास जी का जन्म 1452 ईस्वी में कपड़ोद गाँव, डीडवाना में हुआ था।
- वे संखला क्षत्रिय थे और अपना जीवन यापन करने के लिए डकैती करते थे। बाद में, एक महात्मा की शिक्षा से वे साधु बन गए।
- उनके अनुयायियों का परिवार ‘निरंजनी पंथ’ के रूप में जाना जाता था।
- इस पंथ के अनुयायी ‘निरंजन’ के शब्द की पूजा करते हैं।
इस पंथ के दो प्रकार के अनुयायी होते हैं: निहंग और घरबारी। - निहंग अपने गले में खाकी रंग का कपड़ा पहनते हैं और भिक्षाटन से जीवन यापन करते हैं, जबकि घरबारी वे होते हैं जो इस पंथ को गृहस्थ रहते हुए मानते हैं।
- हरिदास जी की शिक्षाएं ‘मंत्रराजप्रकाश’ और ‘श्री हरिपुरुष जी की वाणी’ में संग्रहित हैं।
- हरिदास जी का निधन गाढ़ा (नागौर) में हुआ।
शाक्त धर्म :
शक्ति धर्म, जो देवी शक्ति की पूजा पर आधारित है, राजस्थान में विशेष रूप से शासकों, सेनापतियों और सैनिकों के बीच शक्ति और बल की प्राप्ति के लिए प्रचलित रहा है। समय के साथ, यह धर्म विभिन्न पंथों में बंट गया। प्रत्येक राजवंश ने अपनी कुलदेवी (परिवार देवी) का निर्धारण किया, जैसे:
- जोधपुर: नागणेची
- आमेर: शिलादेवी
- जैसलमेर: स्वांगिया देवी
- बीकानेर: करणी माता
राजस्थान में दुर्गा की पूजा विभिन्न स्वरूपों में की जाती है, जैसे – मातृदेवी, महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा, पार्वती, काली और कात्यायनी। यहाँ शाक्त धर्म के प्रति गहरी आस्था को प्रमाणित करने वाले कई शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
- भ्रमर माता (490 ई.) – अजमेर
- पीपलाज माता (959 ई.) – उदयपुर
- अंबिका माता (960 ई.) – उदयपुर
यह शिलालेख न केवल देवी-पूजा की प्राचीन परंपरा को उजागर करते हैं, बल्कि राजस्थान में शक्ति साधना के व्यापक स्वरूप को भी दर्शाते हैं।
अन्य संप्रदाय :
दादू संप्रदाय :
- दादूदयाल, जिन्हें राजस्थान के कबीर के रूप में जाना जाता है, का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था।
- वे संत वृद्धानंद से दीक्षा लेकर 1568 ईस्वी में सांभर आए और यहां पर कढ़ाई का काम करने लगे। उन्होंने यहीं से
- उपदेश देना शुरू किया। बाद में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर आए और अगले 14 वर्षों तक यहीं रहे।
- उनके प्रमुख शिष्य ग़रीबदास, मिस्किंसदास, सुंदरदास बख़नाजी, राजजब, माधोदास आदि थे।
- 1585 में वे मुग़ल सम्राट अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी भी गए। इसके बाद उन्होंने ढूँढाड़ और मारवाड़ के राज्यों में यात्रा की और वहां उपदेश दिए।
- 1602 में वे नरैना आए और 1603 में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को अपने शरीर का त्याग किया।
- दादू के शरीर को उनके निर्देशानुसार भेराना पहाड़ी के पास दादू खोल नामक स्थान पर रखा गया, जो दादूपंथियों के लिए एक पवित्र स्थल है।
- अलख दरीबा – दादू पंथ के सत्संग स्थल
- दादूजी की मृत्यु के बाद दादुपंथियों की 6 शाखाएँ बनी।
- खालसा
- खाकी
- विरक्त
- उत्तरादे
- नागा
- निहंग
- दादूजी की शिक्षाएँ ‘दादूजी की वाणी‘ और ‘दादू रा दूहा‘ जैसे ग्रंथों में पाई जाती हैं, जिनमें ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष के बारे में उपदेश दिए गए।।
- शिक्षाएँ :
- दादूजी, कबीर की तरह एक सुधारक थे, जिन्होंने आचार-व्यवहार को महत्वपूर्ण माना और परम सत्य की खोज की।
- उन्होंने कर्मकांड, जातिवाद, मूर्तिपूजा और पंथपरक कट्टरता का कड़ा विरोध किया।
- दादू का संदेश था कि व्यक्ति को अपने आचार-व्यवहार में शुद्धता और सरलता रखनी चाहिए और केवल भगवान की सच्ची भक्ति से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।
- दादू ने कहा की ईश्वर एक है जिसके दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है।
- इन्होंने स्थानीय भाषा ढूँढाड़ी में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया ।
नवल संप्रदाय :
- प्रवर्तक – नागौर के हस्सोलाब गाँव में जन्मे नवलदास ज़ी
- मुख्य मंदिर – जोधपुर
- इनके उपदेश नवलेश्वर अनुभववाणी में संग्रहित है।
राजस्थान के प्रमुख संत
संत पीपा :
- पीपा खींची राजपूत थे, जिनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ। वे गागरोन (झालावाड़) के शासक थे।
- पीपा ने अपना राज्य त्यागकर पत्नी सीता के साथ रामानंद का साथ दिया।
- बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपाजी का भव्य मंदिर है, जहाँ चैत्र शुक्ल पूर्णिमा पर दर्जी समाज का वार्षिक बड़ा आयोजन होता है।
- शिक्षाएँ:
- भक्ति (भगवान के नाम का जप) को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन बताया।
- मूर्तिपूजा और जातिगत भेदभाव का विरोध किया।
- सभी प्राणियों को समान मानने पर जोर दिया।
- ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु के मार्गदर्शन को आवश्यक बताया।
- साहित्यिक योगदान:
- पीपा की कथा, पीपा-पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ और पद जैसे ग्रंथों की रचना।
- चितावनी(17वीं सदी) नामक ग्रंथ भी रचा।
संत धन्ना :
- संत धन्ना का जन्म 1415 ई. में टोंक जिले के धुवा गांव में एक जाट परिवार में हुआ।
- बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले, काशी में आचार्य रामानंद के शिष्य बने और निर्गुण ब्रह्म की साधना की।
- उनके चार पद ‘आदि ग्रंथ’ में शामिल हैं।
- उपदेश :
- गृहस्थ जीवन जीते हुए भक्ति का प्रचार किया।
- आचरण की पवित्रता पर जोर दिया।
- गुरु भक्ति और ईश्वर के नाम जाप को जीवन का उद्देश्य माना।
- आडंबरपूर्ण कर्मकांडों का कड़ा विरोध किया।
संत मीराबाई :
- मीराबाई, जिन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है, 16वीं सदी की प्रसिद्ध संत, कवयित्री और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थीं।
- जन्म लगभग 1498 ई. में कुड़की (पाली) के राठौड़ परिवार में हुआ।
- बचपन से ही कृष्ण को अपना जीवनसाथी माना।
- 1516 ई. में मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से विवाह हुआ।
- विधवा होने के बाद कृष्ण भक्ति में लीन हो गईं और द्वारका के रणछोड़ मंदिर में 1547 ई. में कृष्ण में विलीन हो गईं।
- कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति पर केंद्रित जीवन।
- अंतिम समय गुजरात के द्वारका में रणछोड़ मंदिर में बिताया और 1547 ई. में कृष्ण में लीन हो गईं।
- साहित्यिक योगदान:
- ‘टीका राग गोविंद’, ‘रुक्मिणी मंगल’, ‘नरसी मेहता की हुंडी’, और ‘नरसी जी रो मायरो'(रत्ना खाती द्वारा)।
संत रणाबाई :
- जन्म 1504 ई. वैशाख शुक्ल तृतीया को हरनावा गाँव (मकराना के पास, मारवाड़) में।
- पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या।
- एकांत में भक्ति की और दिव्य व्यवस्था से जीविका प्राप्त की।
- चुटकी आटा भिक्षा (अल्प भोजन) के सिद्धांत का पालन किया।
- मथुरा और वृंदावन की यात्रा कर गुप्तिनाथ और राधा की मूर्तियाँ हरनावा लाईं और उनकी दैनिक पूजा शुरू की।
- 1570 ई. फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को हरनावा गाँव में 66 वर्ष की आयु में जीवन समाधि प्राप्त की।
- जोधपुर महाराजा अभय सिंह के अहमदाबाद पर हमले के दौरान बोरवड़ के ठाकुर राज सिंह को आशीर्वाद दिया।
- मीरा बाई की तरह अडिग कृष्ण भक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं।
संत मावजी :
- 1714 ई. में साबला गाँव में जन्म।
- 12 वर्ष की आयु में माही और सोम नदियों के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने के लिए घर छोड़ दिया।
- संवत 1784, माघ शुक्ल एकादशी को ज्ञान प्राप्त किया और उसी दिन बेणेश्वर (वेणा वृंदावन) की स्थापना की।
- अनुयायी मावजी को विष्णु के दसवें अवतार कल्कि मानते हैं।
- उपदेश:
- निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों को स्वीकार किया।
- निष्कलंक संप्रदाय (पवित्र और पापरहित) की स्थापना की।
- जातिगत भेदभाव के बिना धर्म का प्रचार किया और सभी समुदायों के शिष्यों को स्वीकार किया।
- विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया।
- जनजातियों को अंधविश्वासों से बचने के लिए जागरूक किया।
- जाति प्रथा समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया।
- साहित्यिक योगदान :
- चोपड़ा :
- पाँच बड़े हस्तलिखित ग्रंथ, जिनमें 72 लाख 96 हजार श्लोक हैं, वाद-विवाद की शैली में लिखे गए, जो केवल दीवाली पर प्रकट किए जाते हैं।
विषय: - आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान कृष्ण की लीलाएँ, रासलीला और भविष्य की झलक प्रस्तुत करने वाली भविष्यवाणियाँ।
- पाँच बड़े हस्तलिखित ग्रंथ, जिनमें 72 लाख 96 हजार श्लोक हैं, वाद-विवाद की शैली में लिखे गए, जो केवल दीवाली पर प्रकट किए जाते हैं।
- चोपड़ा :
सांगलिया धूनी :
- 1649 ई. में लक्खड़दास महाराज द्वारा स्थापित।
- मुख्य केंद्र सांगलिया गाँव, धोद तहसील, सीकर जिला।
- मूल विश्वास :
- जातिगत भेदभाव का विरोध।
- अंधविश्वासों और ताबीज के उपयोग का खंडन।
- सदाचारी जीवन जीने का प्रचार।
संत सुंदरदास जी :
- 1653 ई. में दौसा, राजस्थान में खंडेलवाल वैश्य परिवार में जन्म।
- दादू जी से दीक्षा ली और उनके प्रमुख शिष्य बने।
- निर्गुण भक्ति का प्रचार किया और इसे काव्य और साहित्यिक उत्कृष्टता से समृद्ध किया।
- साहित्यिक कृतियाँ:
- 42 पुस्तकों की रचना की, जो निर्गुण भक्ति साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है।
- प्रमुख रचनाएँ: ज्ञान समुद्र, बावनी, सुंदर विलास, बर्ह अष्टक, और सुंदर सार।
- काव्य को धार्मिक शिक्षाओं के साथ जोड़ा।
- दादू संप्रदाय में नागा साधु वर्ग की स्थापना की।
- प्रमुख शिष्य: दयालदास, श्यामदास, दामोदरदास, निर्मलदास, और नारायणदास। इन्हें पाँच स्तंभ माना जाता है।
संत रज्जब जी :
- 1624 ई. में सांगानेर, जयपुर में जन्म।
- विवाह के दौरान दादू जी की शिक्षाएँ सुनीं और उनसे प्रेरित होकर उनके शिष्य बन गए।
- जीवनभर दूल्हे के रूप में ही रहकर दादू जी की शिक्षाओं का प्रचार किया ।
- साहित्यिक योगदान:
- रज्जबवाणी और सर्वांगी की रचना की, जो दादू संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हैं।
राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय / राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय/ राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय/ राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय /राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय/ राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय/ राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय