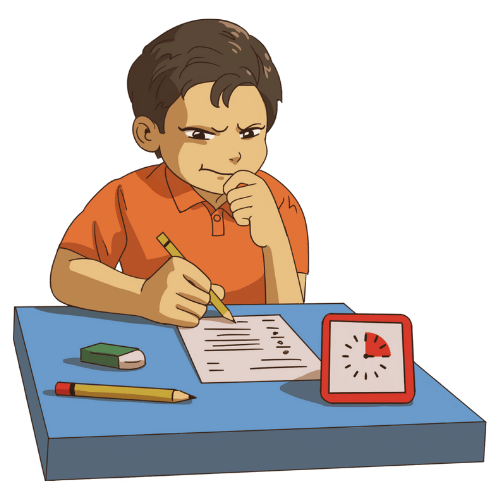This is Day 35 | 90 Days RAS Mains 2025 Answer Writing, We will cover the whole RAS Mains 2025 with this 90-day answer writing program
Click here for the complete 90 days schedule (English Medium)
Click here for complete 90 days schedule (Hindi Medium)
GS Answer Writing – विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान । राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। विज्ञान और प्रौद्यौगिकी से संबंधित सरकार की नीतियाँ। । निबंध लेखन
सी. वी. रमन एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जो प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे।
| रमन प्रभाव की खोज वर्ष 1928 में हुई थी। | यह प्रकाश के अरेखीय प्रकीर्णन (inelastic scattering) की खोज थी, जो गैसों, द्रवों या ठोस पदार्थों के अणुओं द्वारा किया जाता है। यह अणुओं के दोलनी (vibrational) एवं घूर्णन (rotational) प्रकार्यों के विश्लेषण के लिए एक शक्तिशाली तकनीक प्रदान करता है। |
| संगीतीय ध्वनि | रमन ने वायलिन जैसे धनुषधारी वाद्ययंत्रों की अनुप्रस्थ कंपन (transverse vibration) के सिद्धांत को गति के अध्यारोपण (superposition of velocities) के आधार पर स्पष्ट किया। |
| समुद्र का नीला रंग: | रमन ने यह प्रदर्शित किया कि समुद्र का नीला रंग आकाशीय प्रकाश पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह अणुगत विवर्तन (molecular diffraction) के कारण होता है। |
एमएस स्वामीनाथन:
एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें अक्सर “भारत में हरित क्रांति का जनक” कहा जाता है, ने कृषि विज्ञान, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल ही में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
मुख्य कार्य:
| खाद्य सुरक्षा | हरित क्रांति: 1960 और 1970 के दशक में भारत में उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों (High-Yielding Variety Seeds) की शुरुआत का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन, विशेषकर गेहूँ और चावल, में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। |
| किसानों को समर्थन: | फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक निर्धारित करने की वकालत की। |
| कृषि अनुसंधान और विकास में योगदान: | एम. एस. स्वामीनाथन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की।पौध आनुवंशिकी और प्रजनन के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया, जिससे अधिक सहनशील (resilient) और उत्पादक फसल किस्मों का विकास संभव हुआ।भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) तथा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में नेतृत्व के पदों पर कार्य किया। |
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपाय करता है।
DST, राजस्थान द्वारा उठाए गए कदम:
- बौद्धिक संपदा अधिकारों पर राजस्थान राज्य नीति 2021-2026
- जैवप्रौद्योगिकी प्रभाग: राजस्थान जैवप्रौद्योगिकी नीति 2015
- उद्यमिता विकास प्रभाग
- पेटेंट सूचना केंद्र: बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) पर जागरूकता पैदा करने और क्षेत्र से पेटेंट भरने की सुविधा प्रदान करने के लिए
- अनुसंधान और विकास प्रभाग: अनुप्रयोग उन्मुख अनुसंधान को बढ़ावा देना
- महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
स्कूलों और कॉलेजों में
- किशोरी शैक्षणिक मेला
- राष्ट्रीय आविष्कार योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रदर्शनी
- 5,000 सरकारी स्कूलों में विज्ञान क्लबों को 10,000 रुपये का समर्थन
- बूटकैंप और स्कूल स्टार्टअप कार्यक्रम
डिजिटल युग कौशल:
- राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड लर्निंग, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट (जोधपुर), जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी
- कोटा, जयपुर में आईटी पार्क
- SATCOM सुविधाओं का उपयोग करके STEMM विषयों के लिए मुफ्त कोचिंग भी
नीतियां और योजनाएं
- राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022
- iStart योजना
- KARYA योजना: विज्ञान विषयों के लिए फ़ेलोशिप प्रदान करने के लिए 2018 में शुरू की गई थी।
युवाओं में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना
- डीएसटी, राजस्थान: विज्ञान संचार और लोकप्रियकरण प्रभाग →बाल विज्ञान कांग्रेस, विज्ञान केंद्र और जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में विज्ञान पार्क
- जोधपुर, कोटा और उदयपुर में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से ताराघर (प्लेनेटेरियम) का निर्माण किया जाएगा।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सुधार और अभिविन्यास के लिए राजस्थान स्टेट फेकल्टी डेवलपमेंट एकेडेमी (RSFDA) की स्थापना को मंजूरी दी गई → इस मंजूरी से कॉलेज जाने वाले छात्रों और ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण मिलेगा
हाल के वर्षों में, 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ भारत में डिजिटलीकरण तेजी से बढ़ा है। हालाँकि, बढ़ते डिजिटल पदचिह्न के साथ साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और तकनीकी नवाचार से संबंधित कई चुनौतियाँ आती हैं।
इन चुनौतियों के जवाब में, भारत सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधायी कार्यवाहियाँ की हैं:
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023
- व्यक्तिगत डेटा को किसी व्यक्ति की सहमति पर केवल वैध उद्देश्य के लिए संसाधित किया जा सकता है।
- डेटा फ़िडुशियरीज़ डेटा की सटीकता बनाए रखने, डेटा को सुरक्षित रखने और अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद डेटा को हटाने के लिए बाध्य होंगे।
- व्यक्तियों को जानकारी प्राप्त करने, सुधार और मिटाने का अधिकार और शिकायत निवारण का अधिकार प्रदान करता है।
- सीमा पार डेटा प्रवाह को आसान बनाने के लिए ब्लैकलिस्टिंग तंत्र का प्रस्ताव।
- गैर-अनुपालन पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करेगी
- जुर्माना: डेटा उल्लंघनों को रोकने में विफलता के लिए 250 करोड़ रुपये।
- सोशल मीडिया कंपनियों पर प्रभाव: उपयोगकर्ता का सत्यापन तंत्र विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा फ़िडुशियरीज़ प्रयास करेंगे । गुमनामी, ट्रोलिंग, फर्जी समाचार और साइबरबुलिंग को कम होने की उम्मीद है।
2. प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 (डीआईए) देश के बढ़ते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भविष्य के लिए तैयार कानूनी ढांचा स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
- दो दशक पुराने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (आईटी अधिनियम) को बदलने के उद्देश्य डीआईए
- ऑनलाइन सुरक्षा और विश्वास: डिजिटल क्षेत्र में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर।
- प्रौद्योगिकी का जिम्मेदार उपयोग।
- विनियमन के साथ नवाचार को बढ़ावा देना: नैतिक AI , ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों में डेटा गोपनीयता और इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग में जवाबदेही के लिए तंत्र को बढ़ावा देना।
- वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में भारत को एक जिम्मेदार देश के रूप में स्थापित करना।
- खुले इंटरनेट को कायम रखना: व्यवस्था बनाए रखने और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पहुंच और आवश्यक नियमों के बीच संतुलन। पहनने योग्य उपकरणों के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) आवश्यकताओं को सख्त करना अनिवार्य है
- ऑनलाइन जवाबदेही मानकों की समीक्षा: ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए “सेफ हार्बर” सिद्धांत की समीक्षा पर विचार करता है।
3. भारतीय न्याय संहिता की धारा 111(1) बीएनएस 2023 में संगठित अपराध पर विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं, जो साइबर अपराध को शामिल करता हैं।
4. सार्वजनिक वस्तु के रूप में डेटा⇒ शिक्षा जगत और स्टार्ट-अप को अनाम डेटा(अनोनीमाईज़ड) प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस नीति (एनजीडीपी) का गठन। इस नीति का उद्देश्य डेटा-संचालित शासन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के साथ-साथ डेटा विज्ञान, एनालिटिक्स और एआई के पारिस्थितिकी तंत्र को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए बढ़ावा देना है।
5. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021
6. दूरसंचार अधिनियम 2023: यह सरकार को साइबर सुरक्षा और डेटा एन्क्रिप्शन सहित विभिन्न पहलुओं के लिए अनुरूपता मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है।
निष्कर्षतः, भारत के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए की गई हालिया विधायी कार्रवाइयां साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा की उभरती चुनौतियों से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक हैं।
Paper 4 (Comprehension part) – निबंध
“नहीं नदी नाला अटै, नहीं अरवर सरराय एक आसरो बादली, मरू सूखी मत जाय।”
प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने ‘राजस्थान’ में जल की आवश्यकता तथा महल को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। “जलस्य जीवनम्’ की धारणा के अनुकरण में ‘नीला सोना’ (जल) को सहेजने तथा भविष्य के लिए संरक्षित करने की परम्परा हमारे यहाँ बहुआयामी उपयोग करते हुए ‘जल है तो कल है का पाठ पढाया हैं।
राजस्थान देश में सर्वाधिक भू-आकार को धारण करता है, उसी अनुपात में जल की उपलब्धता बहुत ही कम है। राज्य का आधा भाग ‘थार का सागर’ जो अरावली पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्रों में स्थित होने के कारण वर्षा नहीं प्राप्त करता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ नदियों भी कम है और वर्षा ऋतु में ही प्रभावित होती है। वनों की कमी, भू-जल स्तर का निम्न स्तर आदि सम्मिलित कारक है, जो राजस्थान में जल की कम मात्रा हेतु उत्तरदायी है।
राजस्थान में प्राचीन समय से ही राजा-महाराजाओं, सामंतों तथा शासकों ने जल संरक्षण हेतु अनेक तालाबों, कुँओं, बावड़ियों, झालरा, टोबा, खडीन का निर्माण करवाया। रहीमदास जी ने पानी की महता को इस प्रकार व्यक्त किया है:-
“रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून
पानी गये ना ऊबरे, मोती मानस चून।”
हमारे यहाँ वर्षा जल ही मुख्य जल स्त्रोत है, अतः इसका संरक्षण करने हेतु राजस्थान में अनेक झीलों का निर्माण किया गया-राजसमंद, जयसमंद, फतेहसागर, आनासागर, स्वरूप सागर, सांभर, नवलखा, गरदड़ा, बालसमंद, कांकनेय आदि झीलें आज भी जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
ध्यातव्य है कि बाँध बनाकर नदी जल को रोककर उसका उपयोग भी जल संरक्षण का प्रभावी उपाय है इसी क्रम में माही बजाज सागर, सूकड़ी बाँध जसवंतसागर बाँध, रामगढ़ बाँध, बीसलपुर बाँध का निर्माण किया गया जो पेयजल मय सिंचाई सुविधा प्रदान करते हैं, यह प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का ही अग्रगामी रूप है।
राजस्थानी संस्कृति में जल को सहेजना मधुक्खियों के शहद बनाने की प्रक्रिया से सीखा गया है। इस संबंध में प्रचलित “राजस्थानी सींठना इस प्रकार:-
“मौमख्याँ फूला स्यूं रस को कण कण चुग ‘र शहद रो ढेर लगा सकै है, तो के म्हाँ माणस बादले रा बरसते रस ने नी सहेज सका हां।”
विचारणीय पक्ष यह है कि प्राचीन समृद्ध संरक्षण परम्परा को आज भी उतना ही महत्त्व दिया जा रहा है, या नहीं? क्या जल का संरक्षण आज भी हमारी जीवनशैली का हिस्सा है?
इन प्रश्नों पर गौर करें तो, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति की होड में, विकास की अंधी दौड़ में, वैश्विक तापन तथा जलवायु परिवर्तन की भीषण समस्या ने इन पारंपरिक पद्धतियों को खण्डित किया हैं। औद्योगिक, नगरीकरण, बढ़ती आबादी, कृषि पर बढ़ता भार, वनों की अधाधुंध कटाई आदि ने जल संरक्षण की आवश्यकता को और अधिक बढ़ा दिया हैं। पश्चिमी राजस्थान में जल को घी से भी ज्यादा मूल्यवान बताकर इसके संरक्षण के प्रयास जारी हैं:-
“घी ढुल्याँ म्हारो कई नी जासी
पानी ढुल्याँ म्हारो जियो जल जाय।”
राजस्थान में वर्तमान में जल को संरक्षित करने की दिशा में व्यक्तिगत, सामूहिक तथा संस्थागत स्तर पर प्रयास जारी हैं। चाहे राजस्थान के ‘वाटर मैन’ ‘राजेन्द्र सिंह’ हो जिन्होंने पूर्वी राजस्थान में जल क्रांति से कायाकल्प किया हो या पश्चिमी राजस्थान में ‘इंदिरा गाँधी नहर’ को लाने का भागीरथी प्रयास जिसने मरूधरा हो हराभरा कर लोगों को जीवनदान दिया हो।
सरकारी प्रयासों के तहत ‘मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान’ हो जिसने पारंपरिक जल स्त्रोतों का पुनरुद्धार कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित की है, या ‘जल नीति’ जो जल की प्राथमिकता के साथ जल सरंक्षण को बढ़ावा दे रही है निजी प्रयासों के तहत ‘तरूण भारत संघ एनजीओ हो या ‘जलधारा संस्थान’ सभी जल संरक्षण की दिशा में प्रयासरत है।
सार यह है, कि जल ही वह अमूल्य थाती है, जो हम अपनी अगली पीढ़ी के अस्तित्व के लिए संरक्षित कर प्रकृति का अमूल्य उपहार, जिसे प्रकृति ने हमें दिया है, हम संजीदगी से उसका उपयोग करते हुए इसे समावेशी और सतत् रूप से आगे बढ़ा सकें अथवा मनुष्य का अस्तित्व तो संकट में पड़ेगा ही साथ ही सृष्टि का भी विनाश निश्चित ही है इस दिशा में सकारात्मक, सुनियोजित, समावेशी, सुदीर्घ रणनीति बनाकर जल संसाधनों का सदुपयोग करके ही भावी जीवन की सफलता का आधार तैयार कर सकते है।
अंत में:-
“उद्भव सृष्टि का जल से, जल ही प्रलय घन है पानी बिन सब सून जगत में, यह अनुपम धन है। त्राहि-त्राहि करता फिरता, कितना मूरख मन है।”
Day 35 | 90 Days RAS Mains 2025 Answer Writing
Day 35 | 90 Days RAS Mains 2025 Answer Writing