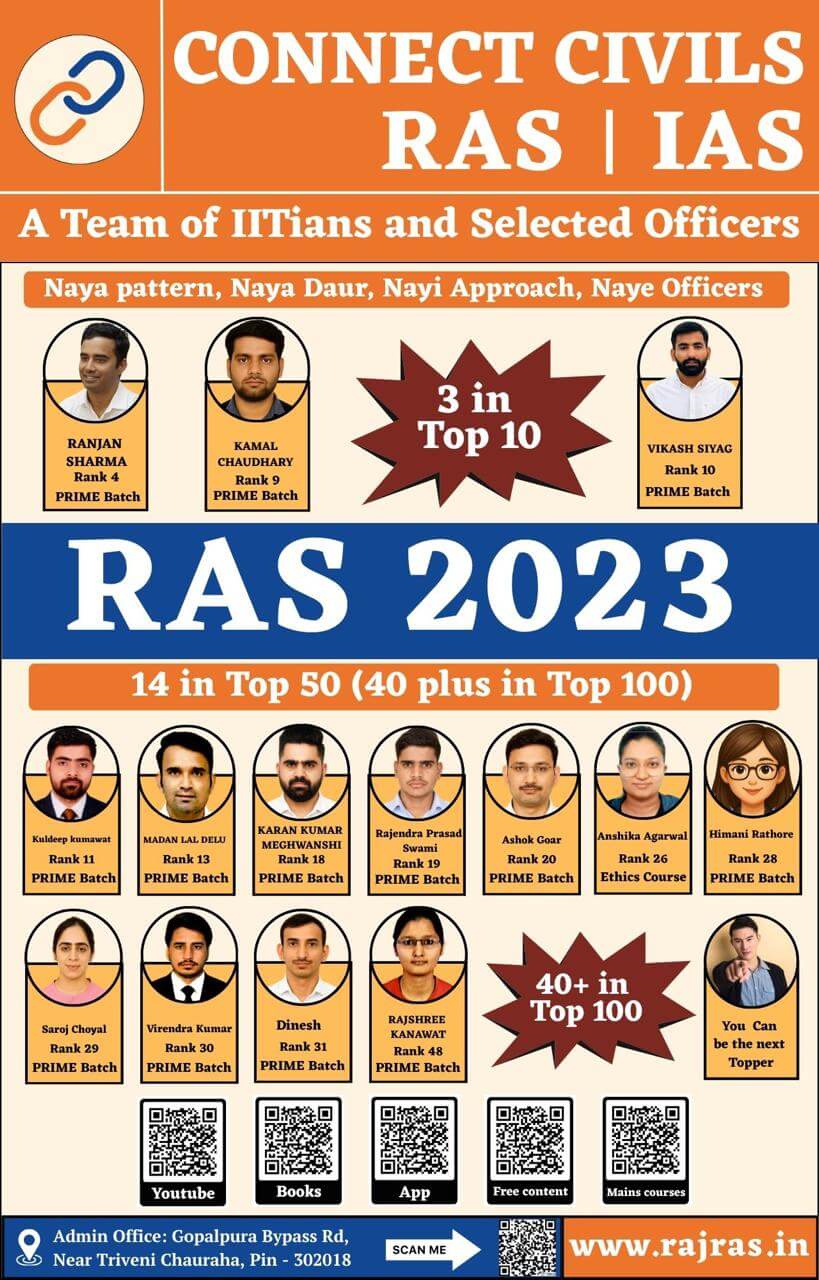राजस्थान में 1857 की क्रांति राजस्थान इतिहास & संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के योगदान को दर्शाता है। यद्यपि यह क्रांति राजस्थान में व्यापक रूप से सफल नहीं हो सकी, फिर भी नसीराबाद, कोटा, भरतपुर और एरिनपुरा जैसे केन्द्रों पर सैनिकों, स्थानीय शासकों और क्रांतिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। तात्या टोपे के प्रयासों और देशभक्त साहित्यकारों के योगदान ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजागृति फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
राजस्थान में 1857 का विद्रोह :
1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। यह विद्रोह शीघ्र ही पटना के आसपास के क्षेत्र से लेकर राजस्थान की सीमा तक फैल गया। इस विद्रोह के मुख्य केंद्र कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार में आरा थे। राजस्थान उन राज्यों में से एक था जिसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। लेकिन, दुर्भाग्यवश, राजस्थान के अधिकांश शासकों ने राष्ट्रीय शक्तियों की मदद करने के बजाय इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया।

- 1832 में, अजमेर में एजीजी (एजेंट टू गवर्नर जनरल) मुख्यालय की स्थापना की गई। राजस्थान के पहले एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। 1845 में, यह मुख्यालय माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया।
- 1857 के विद्रोह के दौरान जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजीजी थे। उस समय राजस्थान को छह ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था:
| नसीराबाद | अजमेर |
| देवली | टोंक |
| एरिनपुरा | पाली |
| नीमच | कोटा |
| खेरवाड़ा | उदयपुर |
| ब्यावर | अजमेर |
- अजमेर और ब्यावर की छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया।
| शहर | पोलिटिकल एजेंट | शासक (1857) |
| भरतपुर | मॉरिसन | महाराजा जसवंत सिंह I |
| जयपुर | विलियम ईडन | महाराजा राम सिंह II |
| जोधपुर | मैक मैसन | महाराजा तख़्त सिंह |
| कोटा | मेजर बर्टन | महराव राम सिंह |
| उदयपुर | कैप्टन बर्ट | महाराणा स्वरूप सिंह |
नसीराबाद का विद्रोह:
- राजस्थान में 1857 का विद्रोह सबसे पहले नसीराबाद में 28 मई को शुरू हुआ।
- मेरठ विद्रोह की खबर एजीजी जॉर्ज लॉरेंस तक पहुंची, और उन्होंने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री, जो अजमेर में थी, को नसीराबाद भेजा क्योकि हाल ही ये मेरठ से आई थी, इससे सैनिकों में असंतोष फैल गया।
- 28 मई 1857 को नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फैंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 30वीं नेटिव इन्फैंट्री के सैनिक भी इसमें शामिल हो गए। छावनी पर कब्जा कर सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ गए।
नीमच का विद्रोह:
- नसीराबाद के विद्रोह की खबर नीमच के सैन्य अधिकारी कर्नल एबॉट तक पहुंची। 2 जून 1857 को उन्होंने सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाने का प्रयास किया।
- इस दौरान घुड़सवार अली बेग ने कहा, “अंग्रेजों ने अवध के साथ अपनी शपथ नहीं निभाई, इसलिए भारतीयों पर भी इसका पालन करने का कोई दायित्व नहीं है।” 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया।
- परिणामस्वरूप 3 जून, 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। छावनी को जलाने के बाद वे चित्तौड़, हम्मनगढ़, बनेड़ा और शाहपुरा होते हुए दिल्ली के लिए चल पड़े और वहां क्रांतिकारियों से मिल गए तथा ब्रिटिश सेना पर भीषण हमला बोल दिया।
- कैप्टन शॉवर्स मेवाड़ की सेना लेकर नीमच पहुंचे तथा ए.जी.जी. लारेंस ने कोटा और बूंदी की सेना को नीमच भेजा। 8 जून, 1857 को अंग्रेजों ने पुनः नीमच पर अधिकार कर लिया।
एरिनपुरा का विद्रोह:
- एरिनपुरा छावनी में 21 अगस्त 1857 को भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया। उन्होंने “चलो दिल्ली, मारो फिरंगी” का नारा लगाया।
- रास्ते में आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने नेतृत्व संभाला। उन्होंने विद्रोही सैनिकों को संगठित किया और अंग्रेजी सेना के खिलाफ सफल युद्ध लड़ा।
- 21 अगस्त 1857 को जोधपुर सेना ने सैन्य तख्तापलट करके विद्रोह कर दिया। चूंकि कुशाल सिंह अंग्रेजों के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने इन विद्रोहियों को अपने साथ मिला लिया। संयुक्त सेना ने जोधपुर राज्य की सेना को आउवा के पास हरा दिया (8 सितम्बर 1857- बिठोडा का युद्ध) और लेफ्टिनेंट हीथकोट को पीछे हटना पड़ा।
- घटना के बाद ए.जी.जी. लॉरेंस आउवा पहुंचे और भीषण युद्ध हुआ (18 सितम्बर 1857- चेलावास का युद्ध)। जनरल लॉरेंस की सेनाएं पराजित हुईं और विद्रोही सेना ने राजनीतिक एजेंट मैक मैसन को मार डाला।
- आउवा की हार का बदला लेने के लिए ए.जी.जी. जॉर्ज लॉरेंस डिसा और ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना को आउवा भेजा गया। इसके बाद एक और भीषण युद्ध हुआ लेकिन इस बार कुशाल सिंह को सलूंबर की ओर भागने पर मजबूर होना पड़ा।
- अंग्रेजों ने आउवा को लूटा और सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले गए। ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
- बाद में मेजर टेलर जांच आयोग ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया और 1864 में उदयपुर में उनकी मृत्यु हो गई। आउवा के युद्ध को राजस्थान के लोकगीतों में “काले और गोरों की लड़ाई” कहा गया है।
कोटा का विद्रोह :
- कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खान और जयदयाल कायस्थ के नेतृत्व में हुआ।
- उन्होंने 15 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन, उनके दो बेटों और एक डॉक्टर की हत्या कर दी। 3 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने करौली महारावल मदनपाल की मदद से कोटा में विद्रोह को कुचल दिया।
- इस विद्रोह के बाद मेहराब खान और जयदयाल कायस्थ को फांसी दे दी गई। यह सबसे तीव्र और व्यापक विद्रोह था, जिसमें क्रांतिकारियों ने छह महीने तक कोटा पर नियंत्रण रखा।
भरतपुर का विद्रोह :
- भरतपुर में गोसाइयों और मेवातियों ने विद्रोह में भाग लिया।
- 31 मई 1857 को भरतपुर सेना ने विद्रोह कर दिया, जिससे मेजर मॉरिसन को आगरा भागना पड़ा।
धौलपुर का विद्रोह:
- अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर के विद्रोही सैनिक धौलपुर पहुंचे और स्थानीय विद्रोहियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ दबाव बनाया।
- राव रामचन्द्र और हीरालाल के नेतृत्व में लगभग 1000 विद्रोही महाराणा धौलपुर की तोपों के साथ आगरा भाग गये।
- अंततः धौलपुर के महाराजा की सहायता से अंग्रेजी शासन पुनः स्थापित किया गया।
1857 के विद्रोह में राजस्थान के क्रांतिकारी
डूंगजी-जवारजी (सीकर) :
- डूंगजी, जो शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार थे, अपनी नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और “धावड़िया” बन गए।
- उन्होंने स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए धनी लोगों से धन संग्रह किया और मना करने पर लूटपाट का सहारा लिया।
- घारसीसर (बीकानेर) में, वे ब्रिटिश सेना और बीकानेर एवं जोधपुर की संयुक्त सेनाओं से घिर गए।
- जवारजी खैरखट्टा भाग गए, लेकिन डूंगजी को जोधपुर की सेना ने छलपूर्वक पकड़ लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया।
- डूंगजी की मृत्यु जोधपुर के किले में हुई।
अभय सिंह और चिमन सिंह (खोंखरी) :
- खोंखरी के जागीरदार इन भाइयों ने ब्रिटिशों को डाक सेवाओं और खजाने को लूटकर परेशान किया।
- उन्होंने डूंगजी-जवारजी के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में भाग लिया।
- उनकी वीरता और साहस का वर्णन आधा जादूराम और आसीया बुढ़जी के गीतों में किया गया है।
रावत केसरी सिंह (सलूम्बर) :
- मेवाड़ के सलूम्बर के रावत ने विद्रोहियों को हथियार, रसद और सैनिक प्रदान कर समर्थन दिया।
- उन्होंने मेवाड़ के महाराणा को चेतावनी दी कि वे पारंपरिक अधिकारों को आठ दिनों के भीतर बहाल करें, अन्यथा वे चित्तौड़ में एक प्रतिद्वंद्वी महाराणा स्थापित करेंगे।
- उन्होंने तात्या टोपे और कुशल सिंह को हथियार और रसद देकर सहायता की और आऊवा के पतन के बाद कुशल सिंह को शरण दी।
अमरचंद बाठिया (दूसरे भामाशाह) :
- बाँठिया का जन्म 1797 में बीकानेर में हुआ था। ये व्यापार के सिलसिले में ग्वालियर बस गये थे।
- अमरचंद ने स्वतंत्रता संग्राम को बनाए रखने के लिए तात्या टोपे को अपनी संपूर्ण संपत्ति समर्पित कर दी।
- उनके इस बलिदान के कारण उन्हें फांसी दी गई, जिससे वे 1857 के विद्रोह में फांसी पर चढ़ने वाले पहले राजस्थानी बने।
मीर आलम खान (टोंक) :
- टोंक के नवाब वज़ीर-उद-दौला के मामा मीर आलम खान ने खुले तौर पर ब्रिटिशों का विरोध किया और विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया।
- नवाब ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया और उनके खिलाफ शाही सेना भेजी। मीर आलम खान लड़ते हुए शहीद हो गए।
रावत जोध सिंह (कोठारिया) :
- कोठारिया के रावत ने विद्रोह के दौरान विद्रोहियों का समर्थन किया और तात्या टोपे और कुशल सिंह को सहायता दी।
- कहा जाता है कि उन्होंने नाना साहेब को शरण दी और हर संभव मदद की।
तांत्या टोपे और राजस्थान में उनका योगदान
- तांत्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, नाना साहेब के निष्ठावान समर्थक थे और उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया।
- वे ग्वालियर के विद्रोहियों के साथ राजस्थान में प्रवेश किए। टोंक के नवाब की सेना, वज़ीर खान के नेतृत्व में, ने भी तांत्या टोपे को ब्रिटिशों के खिलाफ समर्थन दिया।
- तांत्या टोपे ने बांसवाड़ा और मेवाड़ के रास्ते जयपुर की ओर प्रस्थान किया, जहां उनकी मुलाकात शहजादे फिरोज से हुई।
- 1 मार्च 1858 को विद्रोहियों ने ब्रिटिशों के घेरे को तोड़ दिया और अलवर के रास्ते सीकर पहुंचे, लेकिन कर्नल होम्स की सेना से हार गए।
- इसके बाद तांत्या टोपे बूंदी के रास्ते मेवाड़ पहुंचे, लेकिन जनरल अब्राहम रॉबर्ट्स ने भीलवाड़ा के पास उन्हें पराजित कर दिया।
- 11 दिसंबर 1858 को तांत्या टोपे फिर से बांसवाड़ा पहुंचे। महारावल लक्ष्मण सिंह जंगलों में भाग गए, लेकिन तांत्या टोपे के साथी मान सिंह रुक्का ने ब्रिटिशों की मदद की और उन्हें नरवर के जंगलों में पकड़वा दिया।
- तांत्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में फांसी दी गई।
साहित्यकारों की भूमिका
राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता फैलाने और लोगों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी प्रभावशाली कविताओं के माध्यम से उन्होंने जनता में उत्साह और एकता का संचार किया। इनमें से कुछ प्रमुख कवि हैं
सूर्यमल मिश्रण :
- बूंंदी के दरबारी कवि होते हुए भी मिश्रण ने क्रांतिकारी कवि की भूमिका निभाई।
- उनकी कविताएं विद्रोह में शामिल होने और देश के लिए बलिदान देने के लिए जनता को प्रेरित करती थीं।
बांकीदास :
- उन्होंने राजपूतों की विलासितापूर्ण जीवनशैली की आलोचना की और उन्हें ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
- अपनी कविताओं में उन्होंने बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह जैसे शासकों की निंदा की, जिन्होंने ब्रिटिशों का समर्थन किया।
- उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी तांत्या टोपे की प्रशंसा की।
- उनकी प्रसिद्ध पंक्ति “आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर” ने लोगों को ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित किया।
शंकरदान सामौर :
- उन्होंने ब्रिटिशों को “मुल्क रा मीठा ठग” (देश के मीठे चोर) कहकर संबोधित किया।
- उन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करने का सुनहरा अवसर माना।
हुलासी :
- हुलासी ब्रिटिशों के खिलाफ कविताएं लिखने वाले शुरुआती कवियों में से एक थे।
- उनकी रचनाएं वीरता और देशभक्ति से भरी थीं, जो जनता को संघर्ष जारी रखने का आह्वान करती थीं।
दलजी कवि (डूंगरपुर) :
- दलजी कवि ने ब्रिटिश विरोधी भावना को बढ़ावा देने के लिए व्यंग्य और तीखी आलोचना का सहारा लिया।
- उनकी कविताएं शासकों की निष्क्रियता और जनता की उदासीनता पर प्रहार करती थीं।
चारण कवि :
- उन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह (आऊवा) और ठाकुर सावंतसिंह (निंबाज) जैसे स्थानीय नायकों के बारे में वीरगाथाएं लिखीं।
- इन कविताओं ने इन नेताओं की वीरता की प्रशंसा की और जनता को ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
इन कवियों ने अपनी प्रेरणादायक रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बीज बोए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध की भावना को प्रज्वलित किया। उन्होंने जो देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की, उसे बाद के स्वतंत्रता सेनानियों ने सहेजा, जिससे अंततः 1947 में स्वतंत्रता संग्राम की सफलता सुनिश्चित हुई।
राजस्थान में क्रांति के कारण :
- विशेषाधिकारों में कटौती: शासकों और सामंतों के विशेषाधिकारों में कटौती और अंग्रेजों द्वारा राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप से शासक, सामंत और जनसामान्य अंग्रेजों के विरोधी बन गए।
- उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप: अंग्रेजों ने देशी राज्यों के उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप किया, जैसे अलवर और भरतपुर के उत्तराधिकार मामले।
- आर्थिक शोषण: अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों, नमक और अफीम पर एकाधिकार, रेलवे का विस्तार, भूमि बंदोबस्त और अंग्रेजी माल के प्रसार ने ग्रामीण किसानों और व्यापारियों की दशा को शोचनीय बना दिया।
- धार्मिक और सामाजिक सुधार: अंग्रेजों के धार्मिक और सामाजिक सुधारों ने जनमानस को अंग्रेजों के प्रति विरोधी बना दिया।
- प्रशासनिक हस्तक्षेप में वृद्धि: देशी रियासतों के प्रशासनिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा।
- समकालीन साहित्य की भूमिका: तत्कालीन साहित्य ने अंग्रेज विरोधी वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1857 के विद्रोह के परिणाम राजस्थान में :
- क्रांतिकारियों के सहयोगियों को दंड : जिन लोगों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कठोर दंड दिया। उदा: बीकानेर के अमरचंद बाठिया को विद्रोह में भागीदारी के लिए फांसी दे दी गई।
- जमींदारी प्रणाली पर प्रहार : विद्रोह के प्रमुख नेता सामंती जमींदार थे। विद्रोह के बाद, ब्रिटिशों ने सामंती व्यवस्था की शक्ति को समाप्त करने के लिए कई कठोर उपाय अपनाए।
- देशी शासकों के सम्मान में वृद्धि : विद्रोह के दौरान ब्रिटिशों का साथ देने वाले देशी शासकों को पुरस्कार और खिताब दिए गए। उदा: जयपुर के महाराजा राम सिंह प्रथम को “सितार-ए-हिंद” की उपाधि और कोटपूतली परगना प्रदान किया गया।
- संचार के मध्यमों का विकास : विद्रोह के दौरान सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में ब्रिटिशों को गंभीर कठिनाई हुई। 1865 में विद्रोह के बाद जयपुर से अजमेर और नसीराबाद से नीमच होते हुए चित्तौड़गढ़ तक सड़कें बनाई गईं।
- सामाजिक संरचना में परिवर्तन : विद्रोह के बाद राजस्थान की पारंपरिक सामाजिक संरचना में बदलाव आया। आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ और अंग्रेजी कानून सभी रियासतों में लागू हुए। इसके परिणामस्वरूप, ब्राह्मणों का सामाजिक महत्व कम हो गया।
- जन चेतना का उदय : इस विद्रोह ने आम जनता में एक नई चेतना और जागरूकता उत्पन्न की। श्री नाथूराम खरगावत के अनुसार, “सामान्य जनता ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया।”
1857 के विद्रोह की राजस्थान में असफलता के कारण
- देशी शासकों की दूरदृष्टि की कमी : देशी शासक ब्रिटिशों के प्रति निष्ठावान थे और उन्होंने विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया।
- नेतृत्व और संगठन का अभाव : विद्रोहियों का कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं था और उनमें एकता तथा संगठन की कमी थी।
- युद्ध कौशल में कमी : विद्रोही युद्ध के मैदान में ब्रिटिश सेना की तुलना में कम कुशल थे।
- अजमेर पर कब्जा न होना : विद्रोही अजमेर पर कब्जा नहीं कर सके, जिससे उन्हें राजस्थान के शासकों का समर्थन नहीं मिला। (प्रिचर्ड ने अपनी पुस्तक द म्युटिनी इन राजस्थान में लिखा है
- विद्रोह का सीमित प्रभाव : 1857 का विद्रोह राजस्थान के केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा।
- देशी रियासतों का ब्रिटिश समर्थन : अधिकांश रियासतों ने ब्रिटिशों का समर्थन किया। लॉर्ड कैनिंग ने कहा, “राजाओं ने तूफान के दौरान लहरों के खिलाफ अवरोधक की तरह काम किया, नहीं तो हमारी नाव डूब जाती।”
राजस्थान में 1857 की क्रांति का स्वरूप :
राजस्थान में 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्थानीय और राष्ट्रीय प्रतिरोध का मिश्रण था, जो व्यापक असंतोष और ब्रिटिश विरोधी भावना से प्रेरित था। नसीराबाद, नीमच और एरिनपुरा की घटनाएँ जहां देशव्यापी विद्रोह का हिस्सा थीं, वहीं कोटा और आउवा के विद्रोह स्थानीय समस्याओं के कारण उत्पन्न हुए थे। आउवा की जनता ने सैन्य सहायता के बिना भी निरंतर संघर्ष किया, और भरतपुर, कोटा और टोंक के शासकों ने जनदबाव में ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध किया।
अंत में कहा जा सकता है कि राजस्थान की जनता ब्रिटिशों को “फिरंगी” कहती थी और अपने धर्म की रक्षा के लिए उनसे मुक्ति चाहती थी। इस प्रकार, 1857 का यह विद्रोह विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने का पहला महत्वपूर्ण प्रयास माना जा सकता है।
ब्रिटिश काल में राजस्थान में सामाजिक सुधार
राजपूताना का समाज पारंपरिक रूप से संरचित था, लेकिन जब शासक कंपनी शासन के संपर्क में आए, तो इसका प्रभाव न केवल आर्थिक, प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्रों में देखा गया, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी महसूस किया गया। ब्रिटिश प्रभाव के कारण कई मध्यकालीन प्रथाओं और रीतियों का अंत होने लगा, जिससे प्रगतिशील विचारों की एक नई पीढ़ी का उदय हुआ। इस परिवर्तन का विस्तार से अध्ययन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है।
1. सामाजिक सुधार :
ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्थान में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। सती प्रथा को सबसे पहले 1822 में बूँदी के राव विष्णु सिंह द्वारा अवैध घोषित किया गया, और कोटा के महाराव राम सिंह ने 1833 में कन्या वध को प्रतिबंधित किया। जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने 1841 में त्याग प्रथा को समाप्त किया, जबकि उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने जे.सी. बुकर, मेवाड़ भील कॉर्प्स के कमांडर, के प्रयासों से 1853 में डाकन प्रथा को समाप्त किया। 1831 में कोटा में मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया, और 1844 में जयपुर के राजनीतिक एजेंट लुडलो के प्रयासों से जयपुर में समाधि प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए प्रयास 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम में परिणत हुए, जबकि 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। महिला शिक्षा की शुरुआत भी स्कूलों जैसे हुसैन गर्ल्स स्कूल (जोधपुर), सवित्री गर्ल्स स्कूल और सोफिया गर्ल्स स्कूल (अजमेर), और महारानी सुदर्शन इंटरमीडिएट कॉलेज (बीकानेर) से हुई। वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा के प्रयास राजपूत समाज से सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में अत्यंत सराहनीय थे।
विभिन्न मध्यकालीन प्रथाएँ
- सती प्रथा : इस प्रथा में विधवाएँ अपने पति के अंतिम संस्कार की चिता पर आत्मदाह कर लेती थीं।
- त्याग प्रथा: राजपूत समुदाय में विवाह के अवसर पर कुछ जातियों द्वारा कन्या पक्ष से उनकी माँग के अनुसार दान या दक्षिणा लेने का हठ किया जाता था। इसे “त्याग” कहा जाता था।
- डाकन प्रथा: निम्न जातियों की महिलाओं पर जादू-टोने (डाकन) का आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था और मार दिया जाता था। यह प्रथा जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित थी।
- समाधि प्रथा: इस प्रथा में कोई पुरुष या साधु स्वेच्छा से मृत्यु को अपनाने के लिए जल समाधि (तालाब में पानी में बैठकर जान देना) या भू समाधि (गड्ढा खोदकर उसमें बैठकर उसे मिट्टी से भर देना) ले लेता था।
- सागड़ी प्रथा (बंधुआ मजदूरी): सागड़ी प्रथा में जमींदार या साहूकार गरीब या जनजातीय व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को उधार दी गई राशि के बदले घरेलू नौकर के रूप में रख लेते थे। इन्हें बहुत कम या बिल्कुल वेतन नहीं दिया जाता था और कर्ज बढ़ता रहता था। ये व्यक्ति जीवन भर उनके खेतों या घरों में काम करने के लिए बाध्य होते थे। इन्हें हाली या चाकर कहा जाता था।शारदा अधिनियम: यह 1929 में हरिविलास शारदा (अजमेर) के प्रयासों से पारित बाल विवाह निषेध अधिनियम था, जिसमें लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई।
2. न्यायिक सुधार :
1817-18 में संधियों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करने के बाद, ब्रिटिशों ने न्यायिक प्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। इन सुधारों का उद्देश्य न्यायिक प्रशासन को संगठित करना और आधुनिक कानूनी ढांचे को लागू करना था। इनमें से कुछ सुधार इस प्रकार हैं:
- जयपुर राज्य: 1839 में राजनीतिक एजेंट थॉरसबि ने न्यायपालिका को प्रशासनिक विभाग से अलग किया और सिविल और आपराधिक न्यायालयों की स्थापना की।
- जोधपुर राज्य: 1839 में एक शासन समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजनीतिक एजेंट द्वारा की जाती थी, जिसने सिविल और आपराधिक न्यायालयों की स्थापना की।
- मेवाड़ राज्य: महाराणा शंभु सिंह ने ‘महकमा खास‘ की स्थापना की, जबकि महाराणा सज्जन सिंह ने ‘इजलाज खास‘ की स्थापना की ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके। स्थानीय अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ अपील उदयपुर के न्यायालयों में की जा सकती थी।
- बीकानेर राज्य: 1910 में महाराजा गंगा सिंह ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया, जो इंग्लैंड में उस समय की सामान्य प्रथा थी।
इन सुधारों ने कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित की, जाति, धर्म, वंश, रैंक या स्थिति के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया। अंग्रेजी कानूनों को धीरे-धीरे देशी राज्यों में लागू किया गया, जिससे एक आधुनिक न्यायिक प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन सुधारों ने न केवल कानूनी ढांचे को मजबूत किया, बल्कि प्रभावी प्रशासनिक शासन की नींव भी रखी।
3. औद्योगिक सुधार :
1850 के बाद, राजस्थान में कई उद्योगों की स्थापना हुई, जो मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक और सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए थे। इन उद्योगों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
- Ist – स्थानीय जरूरतों और विलासिता की वस्तुओं के लिए उद्योग: जैसे कांच, चमड़ा, सोडा वॉटर उद्योग।
- IInd – कृषि उत्पादों को निर्यात योग्य कच्चे माल में बदलने वाले उद्योग: जैसे कपास, चीनी मिलें।
औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण विकास
- 1889 : कृष्णा कॉटन मिल (ब्यावर)।
- 1906 : एडवर्ड कॉटन मिल (ब्यावर) – आधुनिक तकनीक आधारित।
- 1913 : सीमेंट कारख़ाना (लाखेरी), 1930 में एक और सीमेंट कारख़ाना सवाई माधोपुर में।
- 1932 : पहला चीनी मिल (भूपाल सागर)।
- 1943 : मेवाड़ तेल मिल।
- बिजली : राजस्थान में बिजली का पहला उपयोग बीकानेर में हुआ था।
ये औद्योगिक विकास न केवल स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए थे, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के व्यापक हितों की पूर्ति के लिए भी थे, जिन्होंने राजस्थान की आर्थिक रूपांतरण में योगदान दिया।
4. राजस्थान में परिवहन और संचार
1865 और 1875 के बीच, ब्रिटिशों ने प्रमुख शहरों जैसे आगरा, भरतपुर, जयपुर और जोधपुर को जोड़ने वाले सड़क निर्माण की शुरुआत की, जो दीसा तक विस्तारित थीं। सैन्य जरूरतों के लिए उदयपुर-खैरवाड़ा सड़क बनाई गई। जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़ राज्य ने परिवहन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के तौर पर, जयपुर ने जयपुर से सांभर झील तक बगड़ू होते हुए सड़क बनाई।
1873 में रेलवे का परिचय हुआ, जिसने बंदीकुई, अजमेर और नसीराबाद को दिल्ली और आगरा से जोड़ा। 1899 में, मेवाड़ के महाराणा ने उदयपुर-चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन की स्थापना का समर्थन किया।
ब्रिटिशों ने संचार प्रणालियों का भी विस्तार किया। 1839 में जोधपुर में पहला ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस स्थापित हुआ। 1866-67 तक, जयपुर में 18 पोस्ट ऑफिस थे, और 1872 तक बीकानेर में चुरू, रतनगढ़ और सुजानगढ़ में पोस्ट ऑफिस खोले गए। इसके अतिरिक्त, 1864 में आगरा और अजमेर के बीच टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई।
हालाँकि, ये विकास साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए थे, लेकिन इन्होंने राजस्थान के भीतर शहरों और बाजारों को जोड़ने का कार्य भी किया, जिससे व्यापार, रोजगार और आवश्यक आपूर्ति तक पहुंच में वृद्धि हुई, खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में।
FAQ (Previous year questions)
पृष्ठभूमि: डूंगजी और जवाहरजी शेखावाटी ब्रिगेड के पूर्व रेसलदार थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और “धावड़िया” बन गए।
गतिविधियाँ: उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए धनराशि एकत्र की, और यदि धन देने से इनकार किया जाता तो लूटपाट का सहारा लिया। वे अपने प्रयासों में बैतोत पटेड़ा के ठाकुरों के समर्थन से समर्थ थे।
घरसिसर की मुठभेड़ : घरसिसर (बीकानेर) में, डूंगजी और जवाहरजी को ब्रिटिश सेना और बीकानेर व जोधपुर की सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से घेर लिया गया।
गिरफ्तारी और भाग्य: जवाहरजी खैरखट्टा भागने में सफल रहे, लेकिन डूंगजी को धोखे से जोधपुर की सेनाओं ने पकड़ लिया और ब्रिटिश सेना को सौंप दिया। बाद में, वह जोधपुर किले में ब्रिटिश गिरफ्त में मृत्यु को प्राप्त हुए।
राजस्थान में 1857 की क्रांति / राजस्थान में 1857 की क्रांति / राजस्थान में 1857 की क्रांति / राजस्थान में 1857 की क्रांति / राजस्थान में 1857 की क्रांति / राजस्थान में 1857 की क्रांति