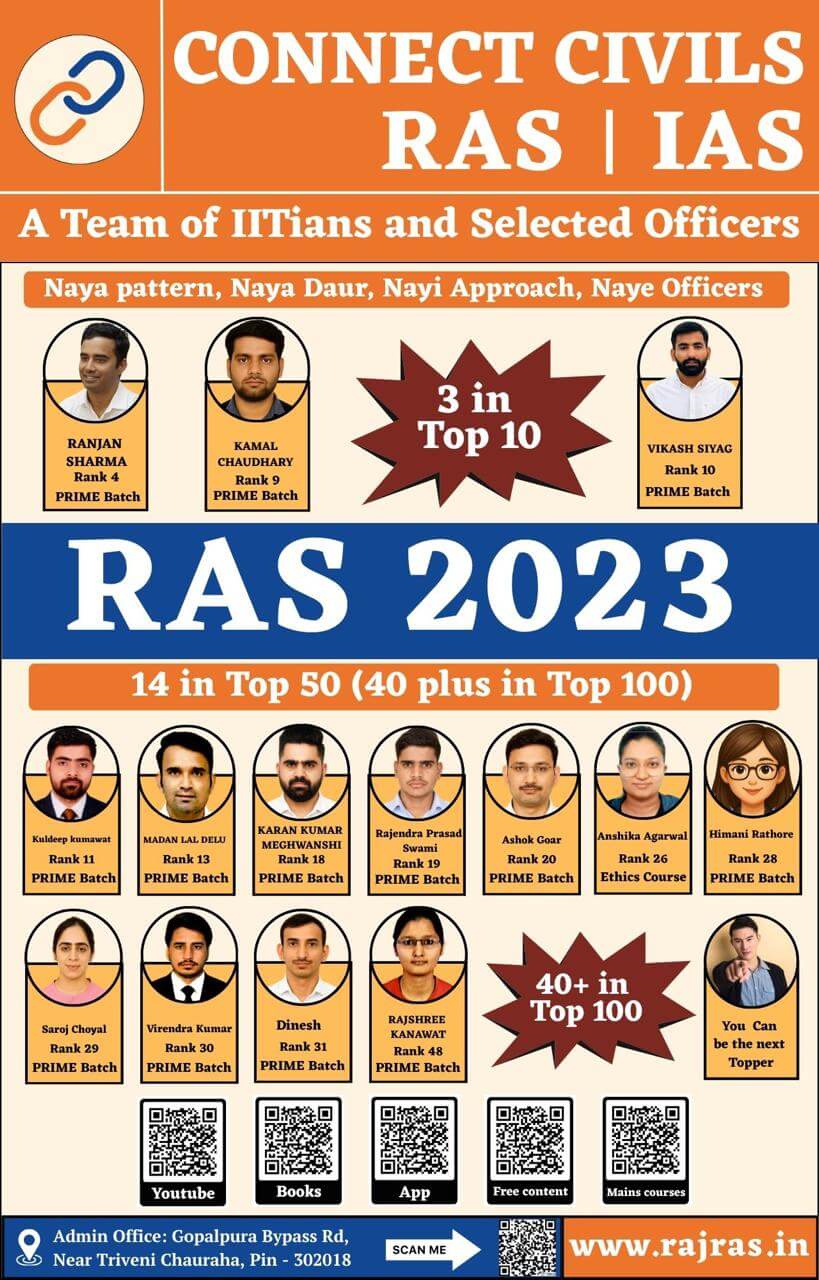राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान इतिहास & संस्कृति विषय के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक आंदोलन था, जिसने जनता को रियासतों के शासकों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य जनतांत्रिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रताओं और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था।
राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का उदभव एवं विकास
राष्ट्रीय चेतना का विकास और स्वतंत्रता आंदोलन का उभरना राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। 19वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियों के बाद, राजस्थान का ब्रिटिशों के साथ रिश्ता बदल गया। 1857-58 के विद्रोह ने रियासतों के शासकों और आम जनता के ब्रिटिशों के प्रति अलग-अलग रवैये को उजागर किया। जहां शासक वर्ग ने ज्यादातर ब्रिटिशों का साथ दिया, वहीं जनता ने ब्रिटिश शासन पर सवाल उठाने शुरू किए। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में लोगों में सामंती व्यवस्था के जुल्म और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के दबाव से आजादी की चाहत बढ़ी। कई कारकों ने इस राजनीतिक जागृति को बढ़ावा दिया जो की निम्नलिखित हैं।
राजनीतिक जागृति के कारण : –
कृषक असंतोष :
सामंती व्यवस्था में भारी कर, लाग-बाग (अनधिकृत शुल्क), और बेगार (जबरन श्रम) ने किसानों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। बिजोलिया किसान आंदोलन (1905) इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसका नेतृत्व वी.एस. पाठिक और माणिक्य लाल वर्मा ने किया, जिन्होंने स्थानीय जागीरदारों के अन्याय का विरोध किया।
सामाजिक सुधार आंदोलन – आर्य समाज :
स्वामी दयानंद सरस्वती की 19वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान यात्रा और आर्य समाज की विचारधारा ने स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी, और स्वभाषा पर केंद्रित सुधारों को बढ़ावा दिया। अजमेर में वैदिक यंत्रालय प्रेस और उदयपुर में परोपकारिणी सभा (1883) ने राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित कर राजनीतिक जागृति को बल दिया।
शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय :
अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से वकीलों, शिक्षकों और पत्रकारों का मध्यम वर्ग उभरा। योग्य होने के बावजूद प्रशासन में उच्च पदों से वंचित इस वर्ग ने राजनीतिक सुधारों की मांग की और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा। जय नारायण व्यास और मास्टर भोलानाथ जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
समाचार पत्रों की भूमिका :
राजस्थान केसरी (1920) और नवीन राजस्थान (1922) जैसे प्रकाशनों ने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन समाचार पत्रों ने राजनीतिक विमर्श को मंच प्रदान किया और स्वतंत्रता की मांग को तेज किया।
परिवहन की भूमिका :
रेलवे और सड़कों के विकास ने कनेक्टिविटी में सुधार किया, जिससे राष्ट्रवादी विचारों और राजनीतिक जुटान का प्रसार राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में हुआ।
सामाजिक संस्थाएँ और सुधार :
सेवा समितियों और हितकारिणी सभाओं जैसी संस्थाओं ने सामंती शोषण प्रभावित क्षेत्रों में सुधार और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया, जिससे एकता और भागीदारी को बल मिला।
उग्रवादी आंदोलनों की असफलता :
रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरित शुरुआती उग्रवादी आंदोलन दीर्घकालिक नहीं रहे। गांधीवादी अहिंसक दृष्टिकोण ने व्यापक समर्थन प्राप्त किया, जिससे स्वतंत्रता के लिए जन-आंदोलन को बल मिला।
अन्य कारण
स्वदेशी आंदोलन ने राजस्थानियों को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया और स्वतंत्रता की मांग को बढ़ावा दिया। प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) की आर्थिक कठिनाइयों ने ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ असंतोष को बढ़ाया। इसके अलावा, शहरी केंद्रों में प्रगतिशील विचारों से अवगत व्यापारिक समुदाय ने स्वतंत्र भारत के लिए सक्रिय रूप से समर्थन किया।
प्रजामंडल आंदोलन
राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों की शुरुआत रियासती राज्यों में लोकतांत्रिक शासन की बढ़ती मांग से हुई। 1927 में बंबई में आयोजित अखिल भारतीय राज्य प्रजाजनों के सम्मेलन ने रियासती राज्यों के लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की अनुमति दी। उसी वर्ष, विजय सिंह पथिक की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद और राजस्थान में राजपूताना देसी लोक परिषद की स्थापना हुई, जिसने इन आंदोलनों की नींव रखी। 1935 तक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने रियासती राज्यों के निवासियों के स्वशासन के अधिकार का समर्थन किया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि संघर्ष का नेतृत्व स्थानीय स्तर पर ही होना चाहिए। हालांकि, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में आईएनसी ने रियासती राज्यों को भारत का अभिन्न हिस्सा घोषित कर दिया और उत्तरदायी शासन तथा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। इससे राजस्थान के प्रजामंडलों को लोकतांत्रिक सुधारों के लिए और अधिक प्रेरणा मिली
स्वभाव
- सामंती और उपनिवेशी विरोधी रुख: यह आंदोलन रियासती राज्यों की दमनकारी सामंती व्यवस्थाओं और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन दोनों का विरोध और आम जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता था।
- उत्तरदायी शासन की माँग :प्रजामंडल आंदोलन का लक्ष्य राजा-महाराजाओं को प्रजा के प्रति जवाबदेह बनाना था। यह शाही शोषण के खिलाफ था और संवैधानिक शासन की स्थापना का प्रस्ताव रखता था, जिसमें जनता को प्रशासन में भागीदारी मिले। शाहपुरा में गोकुल लाल असावा द्वारा स्थापित प्रथम उत्तरदायी शासन इसका प्रमुख उदाहरण है।
- राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा :प्रजामंडल आंदोलन ने रियासती शासन के निरंकुश नियंत्रण के खिलाफ आवाज उठाई, लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों की मांग की, और लोगों को उनके राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया।
- राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एकीकरण: प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने अपने रियासती राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों को लागू किया, जैसे स्कूल स्थापित करना, खादी का प्रचार करना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, और अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में जन जागरूकता: इस आंदोलन ने व्यापक ग्रामीण क्षेत्र में जन जागरूकता फैलाई। नेताओं ने दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों और गांवों का दौरा किया, किसानों और आदिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में शिक्षित किया और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
- क्षेत्रीय संगठनों का गठन: विभिन्न रियासती राज्यों में प्रजामंडल की स्थापना हुई, जो नागरिक अधिकार आंदोलनों और प्रशासनिक सुधारों के लिए एक संगठित मंच प्रदान करते थे। 1946 में, इन क्षेत्रीय संगठनों का विलय राजपूताना प्रांतीय सभा में हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में समन्वय और सामूहिक कार्रवाई को बल मिला।
- स्थानीय नेतृत्व का सशक्तिकरण : इन आंदोलनों ने स्थानीय नेतृत्व को सशक्त किया जिससे की नेतृत्व की दूसरी पंक्ति तैयार हुई जैसे कि हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, जिसने बाद में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- सामाजिक सुधार : आंदोलन ने समाज में व्याप्त कुप्रथाओं और असमानताओं को खत्म करने की कोशिश की। इसमें जातिवाद, महिलाओं के अधिकार, और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की पहल की गई।
गतिविधियाँ
- इन आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों को अपने रियासती राज्यों में लागू किया। उन्होंने स्कूलों की स्थापना की, खादी का उपयोग बढ़ाया, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया, और अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन शुरू किया।
मेवाड़ प्रजामंडल :
बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रभाव से मेवाड़ के अन्य वर्गों में जागृति आई, जिससे लोग नागरिक अधिकारों और राज्य की नीतियों के खिलाफ संगठित हुए। 1932-1938 के बीच कई प्रदर्शन हुए, लेकिन नेतृत्व की कमी के कारण वे सफल नहीं हो सके। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने ‘मेवाड़ प्रजामंडल’ की स्थापना की, जो जल्दी ही लोकप्रिय हो गया।
राज्य ने प्रजामंडल को अवैध घोषित कर माणिक्यलाल वर्मा और अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया। इसके बावजूद, प्रजामंडल ने जनजागृति के प्रयास जारी रखे और सत्याग्रह किया। 1941 में प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटाया गया, लेकिन आंदोलन जारी रहा। 1942 के ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के दौरान, प्रजामंडल ने ‘राजाओ अंग्रेजों का साथ छोड़ो’ का नारा दिया, जिससे फिर से गिरफ्तारियां हुईं।
1946 में, मेवाड़ महाराणा ने संविधान निर्मात्री समिति बनाई, लेकिन उसकी सिफारिशों को नहीं माना गया। 1947 में के.एम. मुंशी द्वारा बनाया गया संविधान लागू हुआ। 1948 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें प्रजामंडल को सफलता मिली, लेकिन मंत्रिमंडल गठन को लेकर विवाद हुआ। 5 अप्रैल, 1948 को दो छात्रों की मौत के बाद महाराणा ने मेवाड़ को राजस्थान संघ में मिलाने का निर्णय लिया।
जयपुर प्रजामण्डल :
प्रारंभिक प्रयास (1907-1931)
- अर्जुनलाल सेठी ने 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना कर जयपुर में जन-जागृति का पहला संगठित प्रयास किया, जो क्रांतिकारी गतिविधियों का केन्द्र बना।
- जयपुर हितकारिणी सभा और आर्य समाज जैसी संस्थाएँ भी युवाओं में राष्ट्रीय भावना जागृत करने में सक्रिय रहीं।
- 1922 में हिंदी को राज्य की राजभाषा बनाने के लिए ठाकुर कल्याणसिंह और श्यामलाल वर्मा ने आंदोलन चलाया, और जमनालाल बजाज द्वारा 1927 में स्थापित चरखा संघ ने खादी और जन-जागृति के प्रयास किए।
प्रजामण्डल की स्थापना (1931-1938)
- 1931 में श्री कपूरचन्द पाटनी और जमनालाल बजाज द्वारा जयपुर प्रजामण्डल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य महाराजा के संरक्षण में उत्तरदायी शासन और नागरिक अधिकारों की स्थापना करना था।
- इस दौरान प्रजामण्डल ने उत्तरदायी शासन, नागरिक अधिकारों और धारा सभा की स्थापना की माँग की।
- 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद, प्रजामण्डल का पुनर्गठन किया गया, जिसमें जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री और चिरंजीलाल मिश्र प्रमुख रूप से शामिल हुए।
सत्याग्रह और अधिकारों के लिए संघर्ष (1938-1942)
- 1938 में राज्य सरकार ने प्रजामण्डल की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून लागू किए, जिससे सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई।
- जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने इस आंदोलन में भाग लिया और हजारों लोगों ने गिरफ्तारियाँ दीं। 1939 में गांधीजी की सलाह पर सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया।
- 1942 में जमनालाल बजाज के निधन के बावजूद प्रजामण्डल ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राज्य में उत्तरदायी शासन की माँग की।
भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रति जयपुर प्रजामंण्डल का दृष्टिकोण
जयपुर प्रजामण्डल का भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण शुरुआत में सक्रिय था, लेकिन बाद में यह नर्म पड़ा। 1942 में, हीरालाल शास्त्री ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के साथ एक ‘जेन्टिलमेन्स एग्रीमेण्ट’ किया।
इस समझौते के बाद, शास्त्री ने आंदोलन की घोषणा नहीं की, और उनकी नीति पर कड़ी आलोचना हुई। प्रजामण्डल के कुछ नेताओं ने, जैसे कि बाबा हरिश्चन्द्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भण्डारी, और हंस डी. राय, ने ‘आजाद मोर्चा’ बनाकर आंदोलन को जारी रखा। इस गुट को सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। शास्त्री के समझौते के अनुसार, इन नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, जो शास्त्री की नीति के खिलाफ था।आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए यह कहा जा सकता है कि शास्त्री की नीति ने आंदोलन को कमजोर कर दिया। शास्त्री के समझौते ने भारत छोड़ो आंदोलन की मूल भावना का उल्लंघन किया, जिससे जयपुर का योगदान केवल प्रतीकात्मक रह गया। विरोधी गुट ने शास्त्री की नीति को धोखाधड़ी के रूप में देखा और इस विभाजन के कारण जयपुर प्रजामण्डल की प्रभावशीलता कम हो गई।
राजनीतिक मान्यता (1946-1947)
- स्वतंत्रता के बाद भी प्रजामण्डल ने उत्तरदायी शासन की माँग जारी रखी और 1946 के चुनावों में भाग लिया।
- 1947 में एक नया मंत्रिमण्डल गठित हुआ, जिसमें प्रजामण्डल के नेताओं जैसे हीरालाल शास्त्री, देवेशंकर तिवाड़ी और दौलतमल भण्डारी को महत्वपूर्ण पद मिले।
- प्रजामण्डल के संघर्ष ने जयपुर राज्य के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को आकार दिया और अंततः यह राजस्थान राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मारवाड़ सेवा संघ :
प्रारंभिक संघर्ष और चेतना जागरण (1920-1931)
- मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई, जिसका उद्देश्य खादी प्रचार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, और मादा पशुओं की निकासी पर प्रतिबंध के खिलाफ संघर्ष था।
- मारवाड़ हितकारिणी सभा और जयनारायण व्यास ने 1927 में उत्तरदायी शासन की माँग की और समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रतिबंध और किसानों पर अत्याचार का विरोध किया।
- 1929 में जयनारायण व्यास ने ‘मारवाड़ की अवस्था’ और ‘पोपाबाई की पोल’ जैसी पुस्तिकाएँ लिखकर राज्य शासन की कटु आलोचना की।
मारवाड़ प्रजामण्डल का गठन और दमनकारी नीति (1931-1936)
- 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई, जिसमें खादी प्रचार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, और नागरिक अधिकारों की माँग की गई।
- 1932 में राज्य सरकार ने मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश जारी कर सभी आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाया।
- 1934 में मारवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना हुई और राज्य द्वारा कृष्णा मामले में उदासीनता को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए। 1936 में प्रजामण्डल को अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन राज्य में जागरूकता बढ़ी।
लोक परिषद् की स्थापना और संघर्ष (1938-1940)
- 1938 में मारवाड़ लोक परिषद् की स्थापना हुई, जिसमें उत्तरदायी शासन और जागीरदारी प्रथा के विरोध में आंदोलन किया गया।
- 1939 में जयनारायण व्यास का निष्कासन रद्द होने पर आंदोलन को और बल मिला।
- 1940 में लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित करते हुए पुलिस ने जुलूस पर लाठीचार्ज किया, फिर भी आंदोलन जारी रहा।
स्वतंत्रता संग्राम और अंतिम चरण (1941-1948)
- भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में लोक परिषद् ने संघर्ष जारी रखा।
- 1944 में लोक परिषद को नगरपालिका चुनावों में बहुमत मिला, और जयनारायण व्यास को नगरपालिका अध्यक्ष चुना गया।
- 1947 में डाबड़ा काण्ड (किसान सम्मेलन पर अत्याचार) ने राज्य के सामंती अत्याचारों को उजागर किया।
- स्वतंत्रता के बाद मारवाड़ लोक परिषद का संघर्ष समाप्त हुआ और जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया।
बीकानेर प्रजामंडल :
प्रारंभिक आंदोलन और राजनीतिक जागरूकता
- बीकानेर राज्य में जनता को जागरूक करने का पहला प्रयास 1907 में स्वामी गोपालदास ने चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना करके किया। इस सभा के माध्यम से उन्होंने लोगों को उनके अधिकारों और ब्रिटिश शासन के दोषों के बारे में जागरूक किया।
- 1930 में महंत गणपतिदास और चन्दमल बहड़ जैसे नेताओं ने चूरू में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया।
- 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान बीकानेर प्रशासन नामक पर्चा वितरित किया गया, जिससे राज्य प्रशासन की आलोचना की गई। इस घटना के कारण कई नेताओं को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया गया।
प्रजामंडल की स्थापना
- 1936 में बाबू मुक्ताप्रसाद और अन्य नेताओं ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। राज्य सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए प्रजामंडल के नेताओं को निर्वासित कर दिया।
- 1937 में, प्रजामंडल को कोलकाता में पुनः स्थापित किया गया।
- 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बीकानेर में व्यापक गतिविधियाँ नहीं हो सकीं क्योंकि राज्य सरकार ने कड़ा दमन किया, लेकिन झंडा फहराने जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास जारी रहे।
राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष
- बीकानेर प्रजा परिषद ने किसानों के अधिकारों का समर्थन किया और जागीरदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की आलोचना की।
- रायसिंह नगर में तिरंगा जुलूस के दौरान पुलिस फायरिंग में बीरबल सिंह की मौत हो गई, जिससे राज्य के दमनकारी रवैये की सर्वत्र निंदा हुई।
- कर प्रणाली के खिलाफ हड़ताल और अन्य विरोध गतिविधियों से जनता के बीच राज्य के प्रति असंतोष बढ़ता गया।
उत्तरदायी शासन की ओर बढ़त और बीकानेर का विलय
- 1946 में महाराजा शार्दूल सिंह ने उत्तरदायी शासन का वादा किया, लेकिन इसे लागू करने में देरी हुई, जिससे फिर से आंदोलन शुरू हो गया।
- बीकानेर एक्ट 1947 के माध्यम से प्रशासनिक ढांचे में सुधार किए गए, लेकिन इन प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया।
- 1948 में एक मिश्रित मंत्रिमंडल का गठन किया गया, लेकिन मतभेदों के कारण प्रजा परिषद के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। अंततः, 1949 में बीकानेर वृहद राजस्थान संघ में शामिल हो गया, जिससे राज्य की स्वतंत्रता समाप्त हो गई।
जैसलमेर प्रजामंडल
प्रारंभिक संघर्ष
- जैसलमेर में महारावल की निरंकुशता के खिलाफ आवाज सबसे पहले सागरमल गोपा और नारायणदास भाटी ने उठाई।
- गोपा ने एक वाचनालय की स्थापना कर राष्ट्रीय साहित्य को जनता तक पहुँचाने और राज्य में मिडिल तक की शिक्षा व्यवस्था की माँग की।
- शासन सुधारों की माँग करने पर गोपा, रघुनाथसिंह मेहता, और आईदान को जेल भेजा गया।
प्रजामंडल का गठन
- 1932 में रघुनाथसिंह ने ‘माहेश्वरी नवयुवक मंडल’ की स्थापना की, जिससे उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा।
- गोपा ने महारावल की निरंकुशता को उजागर करने के लिए ‘रघुनाथसिंह का मुकदमा’ और ‘जैसलमेर का गुंडाराज’ जैसी पुस्तकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, जिसके कारण उन्हें जैसलमेर छोड़कर नागपुर में प्रजामंडल की स्थापना करनी पड़ी।
प्रजा परिषद
- 1939 में शिवशंकर गोपा ने जैसलमेर में प्रजा परिषद की स्थापना की, लेकिन उन्हें जैसलमेर से निर्वासित कर दिया गया। लालचंद जोशी और जीवनलाल को कठोर कारावास मिला।
- 1941 में, सागरमल गोपा अपने पिता की मृत्यु के बाद जैसलमेर लौटे, लेकिन उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया, जहाँ 1946 में अत्याचारों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।
- गोपा की शहादत ने प्रजामंडल के आंदोलन में नई ऊर्जा भरी।
वृहद राजस्थान में विलय
- 1946 में मीठालाल व्यास ने जयनारायण व्यास और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जैसलमेर में तिरंगा फहराया और उत्तरदायी शासन की माँग की।
- 1947 में गाँधी जयंती के जुलूस पर पुलिस लाठीचार्ज हुआ।
- जैसलमेर के सामंती तत्वों ने ‘जैसलमेर राज्य लोक परिषद’ का गठन किया, लेकिन यह सक्रिय नहीं रह सका।
- अंततः, 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का वृहद राजस्थान में विलय हो गया, जिससे पाकिस्तान में विलय का विचार त्यागना पड़ा।
कोटा प्रजामण्डल
प्रारंभिक प्रयास
- कोटा राज्य में जन जागरूकता लाने का श्रेय पंडित नयनूराम शर्मा को जाता है।
- 1918 में उन्होंने कोटा में ‘प्रजा प्रतिनिधि सभा’ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जनता की शिकायतों को महाराव और प्रशासन तक पहुँचाना था।
- अक्टूबर 1921 में, इस सभा ने अनाज पर कर वृद्धि के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिससे राज्य को कर घटाना पड़ा।
- असहयोग आंदोलन के दौरान इस सभा ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और खादी के प्रचार का काम किया।
हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना
- 1934 में पंडित नयनूराम शर्मा ने कोटा में ‘हाड़ौती प्रजामंडल’ की स्थापना की, और हाजी फैज मोहम्मद इसके पहले अध्यक्ष बने।
- प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और मैकडोनाल्ड पंचाट का विरोध कर जन जागरूकता फैलाने का काम किया।
कोटा प्रजामंडल की स्थापना
- 1939 में पंडित नयनूराम शर्मा और अभिन्न हरि ने ‘कोटा राज्य प्रजामंडल’ की स्थापना की।
- प्रजामंडल का पहला अधिवेशन मांगरोल में हुआ, जहाँ उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
- 26 जनवरी 1941 को प्रजामंडल ने स्वतंत्रता दिवस मनाया और उत्तरदायी शासन की माँग को दोहराया।
भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका
- 1942 में ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के दौरान, कोटा के हर्बर्ट कॉलेज और सिटी स्कूल के छात्रों ने महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल की और जुलूस निकाला।
- 13 अगस्त को अभिन्न हरि, शंभूदयाल सक्सेना और बेनी माधव प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया।
- 14 अगस्त को छात्रों और जनता ने तिरंगे के साथ जुलूस निकाला और प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस ने गोलीबारी की।
- जनता ने कोतवाली को घेर कर उस पर तिरंगा फहराया, और सरकार को समझौता करके गिरफ्तार नेताओं को रिहा करना पड़ा।
संघ में विलय
- प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की माँग को जारी रखा।
- मार्च 1946 में, कोटा महाराव ने श्री हिरण्या के नेतृत्व में एक समिति बनाई, जिसने एक निर्वाचित प्रतिनिधि सभा की स्थापना की सिफारिश की।
- 1948 में, महाराव भीमसिंह द्वितीय ने अभिन्न हरि के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनाने का निर्णय लिया, लेकिन राजस्थान संघ के निर्माण के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका।
बूंदी प्रजामंडल
प्रारंभिक दौर
- 1926 में राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में किसानों का बेगार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ।
- 1927 में पुलिस द्वारा पुरोहित रामनाथ कुदाल की हत्या के बाद जनता में रोष पैदा हुआ।
- बूंदी के दीवान वेब के दमनात्मक रवैये ने लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।
बूंदी प्रजामंडल की स्थापना
- 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई।
- इसके प्रमुख सदस्यों में कांतिलाल, ऋषिदत्त मेहता, नित्यानंद नागर, गोपाल कोटिया, और अन्य शामिल थे।
- प्रजामंडल ने प्रभात फेरियां निकालीं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, और शराब की दुकानों पर धरना देकर जनता को जागरूक किया।
- उन्होंने उत्तरदायी शासन और नागरिक अधिकारों की मांग की।
प्रजामंडल की गतिविधियाँ और संघर्ष
- 1937 में प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को बूँदी से निर्वासित कर दिया गया, जिससे आंदोलन कमजोर हुआ।
- 1939 में पशु निकासी और जकात को लेकर प्रजामंडल ने फिर से आंदोलन शुरू किया।
- 1940 में ऋषिदत्त मेहता बूँदी लौटे और सरकार के संविधान प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया।
लोक परिषद का गठन और संघ में विलय
- भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नित्यानंद नागर, ऋषिदत्त मेहता, और बृजसुंदर शर्मा ने सभाओं और प्रदर्शनों का नेतृत्व किया।
- सरकार ने प्रजामंडल के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया।
- 1944 में जेल से रिहा होने के बाद ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया।
- 1945 में पुलिस की गोलीबारी में वकील रामकल्याण की मृत्यु हो गई, जिससे आंदोलन और तेज हो गया।
- भयभीत होकर बूंदी महाराव बहादुर सिंह ने लोक परिषद की उत्तरदायी शासन की मांग मान ली।
- 25 मार्च 1948 को बूंदी का राजस्थान संघ में विलय हो गया।
भरतपुर प्रजामंडल
आर्य समाज के माध्यम से प्रारंभिक जागरूकता:
भरतपुर में जन चेतना की शुरुआत आर्य समाज के प्रयासों से हुई, जिसने भरतपुर, डीग, कुम्हेर, बयाना और अन्य स्थानों में शाखाएँ स्थापित कीं। आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और स्वतंत्रता के प्रचार के लिए काम किया। 1912 में, जगन्नाथ अधिकारी ने ‘हिंदी साहित्य समिति’ की स्थापना की और ‘वैभव’ पत्रिका प्रकाशित की ताकि जन जागरूकता बढ़ाई जा सके, जिसके लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। 1924 से 1927 के बीच ठाकुर देशराज ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा के लिए कई सभाओं का आयोजन किया। जागरूकता के बावजूद, सरकार उदासीन बनी रही।
भरतपुर राज्य प्रजा संघ का गठन (1928):
दीवान डंकन मैकेंजी की कठोर नीतियों के बाद, जिन्होंने सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया और अधिकारों को सीमित कर दिया, नवंबर 1928 में ‘भरतपुर राज्य प्रजा संघ’ का गठन किया गया। गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष बने और ठाकुर देशराज सचिव। प्रजा संघ ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए संघर्ष किया।
भारत छोड़ो आंदोलन और प्रजामंडल:
इस बार विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। नेताओं (नित्यनंद नगर, ऋषिदत्त मेहता, बृज सुंदर शर्मा, राजेश्वरी देवी और धर्मवती) को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। आंदोलन को शांत करने के लिए महाराजा ने ‘बृज जय प्रतिनिधि सभा’ का गठन किया। हालांकि, सभा को सीमित शक्तियाँ दी गईं, जिससे असंतोष हुआ और 1945 में प्रजा परिषद के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया।
उत्तरदायी शासन की मांग:
प्रजामंडल ने जबरन श्रम प्रणाली को समाप्त करने और उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग जारी रखी। इस संघर्ष में बलिदान भी हुए, जैसे 1947 में विरोध के दौरान रमेश स्वामी की मौत।
विलय:
स्वतंत्रता के बाद, भरतपुर प्रजामंडल के नेता, जैसे गोपीलाल यादव और मास्टर आदित्येंद्र, मंत्री नियुक्त हुए। अंततः यह क्षेत्र भरतपुर मत्स्य संघ का हिस्सा बन गया।
प्रजामण्डल आंदोलनों के प्रभाव
सामाजिक-आर्थिक प्रभाव :
प्रजामण्डल आंदोलन ने निम्नलिखित सामाजिक और आर्थिक सुधारों के जरिए जनमानस में जागरूकता बढ़ाई।
महिलाओं को आंदोलन से जोड़ना:
प्रजामण्डल आंदोलन ने महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल किया। राजस्थान की कई महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया और बड़े स्तर पर गिरफ्तारियाँ दीं। उदाहरण के तौर पर, बाँसवाड़ा की श्रीमती जिया बहिन, मारवाड़ की महिमा देवी किंकर, जयपुर की दुर्गादेवी शर्मा और मेवाड़ की नारायणी देवी जैसी महिलाएँ इस आंदोलन में शामिल हुईं। इसने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा किया।
दलित उत्थान का कार्य:
प्रजामण्डल आंदोलन ने दलितों को मुख्यधारा में लाने का कार्य किया। दलितों के लिए कई संगठन स्थापित किए गए, जैसे पं. हरिनारायण का ‘अस्पृश्यता निवारण संघ’ और गोकुल भाई भट्ट का ‘हरिजन सेवा संघ’। इन संगठनों ने मद्य निषेध, शिक्षा, मंदिर प्रवेश, गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यों के जरिए समाज में भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया।
आदिवासी उत्थान:
प्रजामण्डल आंदोलन ने दक्षिण अरावली क्षेत्र में आदिवासियों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए। ठक्कर बापा और अमष्टतलाल पाठक जैसे नेताओं ने जनजातियों में जागरूकता फैलाने और उनके लिए विशेष कानून बनाने का कार्य किया। इसके अलावा, आदिवासी छात्रावासों की स्थापना, शराबबंदी और सागड़ी प्रथा की रोकथाम के लिए भी अभियान चलाए गए।
शिक्षा प्रसार:
प्रजामण्डल आंदोलन ने शिक्षा के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रजामण्डल ने गांव-गांव और शहर-शहर में पाठशालाएँ, रात्रि पाठशालाएँ, और ‘कबीर पाठशालाएँ’ खोलीं। महिला शिक्षा के क्षेत्र में हीरालाल शास्त्री द्वारा ‘वनस्थली विद्यापीठ’ और हरिभाई किंकर द्वारा ‘महिला शिक्षा सदन’ की स्थापना की गई।
बेगार और बलेठ प्रथा उन्मूलन:
प्रजामण्डल आंदोलन ने बेगार और बलेठ प्रथाओं के खिलाफ अभियान चलाया और इसके खिलाफ कानून बनवाए। जयनारायण व्यास, पं. नयनूराम शर्मा, भोगीलाल पण्ड्या जैसे नेताओं ने इन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। इसके परिणामस्वरूप, कृषक और आदिवासी क्षेत्रों में बड़े आंदोलन हुए।
सामाजिक सौहार्द और एकता की स्थापना:
प्रजामण्डल आंदोलन ने जातीय और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने का कार्य किया। यह आंदोलन हिन्दू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामाजिक समानता और भाईचारे का संदेश देता था। आंदोलन में विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग एक साथ शामिल हुए, क्योंकि उनकी एक समान समस्या थी – निरंकुश सामन्तशाही।
सामाजिक सुधार कार्य:
प्रजामण्डल ने कई कुरीतियों का विरोध किया, जैसे बाल विवाह, कन्या वध, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, दहेज प्रथा, डाकन प्रथा, छुआछूत, ऊँच-नीच का भेदभाव। इसके साथ ही विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, और विवाह की आयु बढ़ाने जैसे मुद्दों का समर्थन किया। आंदोलन ने जनजागृति पैदा करने के लिए व्यापक अभियान चलाए। इसके अलावा, शराबबंदी, नशीली वस्तुओं का प्रचार रोकने, और मजदूरों के अधिकारों के लिए कानून बनाने के लिए भी आंदोलन ने कार्य किए।
आर्थिक सुधार:
इन आंदोलनों ने खादी के प्रयोग और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हुए और ब्रिटिश वस्त्रों पर निर्भरता कम हुई। इसके साथ ही बाढ़ और अकाल राहत कार्यों में जनसहयोग को भी बढ़ावा दिया गया, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता मिल सके।
निष्कर्ष:
प्रजामण्डल आंदोलन ने न केवल राजनीतिक अधिकारों की बहाली की, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों के जरिए समाज में जागरूकता, समानता, और एकता की भावना का संचार किया। इसने रियासतों में व्याप्त अत्याचारों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आंदोलन खड़ा किया और आम जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए।
राजनीतिक महत्त्व
प्रजामण्डल आंदोलनों ने राजस्थान में राजनीतिक जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन आंदोलनों के राजनीतिक महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत समझा जा सकता है:
राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना:
राजस्थान की जनता पहले राजशाही और सामन्ती शोषण के तहत उदासीन थी। प्रजामण्डल आंदोलनों के माध्यम से जन चेतना का संचार हुआ, जिससे जनता शोषण और अत्याचारों के खिलाफ संगठित रूप से खड़ी हुई तथा अपने मौलिक, राजनीतिक अधिकारों और शासन में भागीदारी की मांग के प्रति जागरूक हुई।
उत्तरदायी शासन की स्थापना:
1938 के हरिपुरा अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने प्रत्येक राज्य में जन आंदोलनों का उत्तरदायित्व स्थानीय नेतृत्व पर डाला। प्रजामण्डल आंदोलनों ने सीमित साधनों के बावजूद निरंकुश राजशाही और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और उत्तरदायी शासन की दिशा में सफलता प्राप्त की।
युवाओं की भागीदारी और राष्ट्रीय जागरूकता:
इन आंदोलनों ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल किया। शिक्षा, समुदाय संगठनों और प्रदर्शनों के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय जागरूकता और समानता के विचारों से परिचित कराया।
राष्ट्रीय आंदोलन को बल देना:
1938 तक रियासतों में जनता अपने स्तर पर आंदोलन कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने इन आंदोलनों को सहयोग देना शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये स्थानीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गए। इससे राजशाही की सत्ता कमजोर हुई और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ एक मजबूत जन आंदोलन खड़ा हुआ।
राजनीतिक एकता के सूत्र में देश को बांधना:
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, प्रजामण्डल आंदोलनों के दबाव में कई राजाओं ने भारतीय संघ में मिलने का निर्णय लिया। आंदोलन से उत्पन्न भारी जनमत ने इन राजाओं को पाकिस्तान में मिलाने से रोका, जिससे देश की राजनीतिक एकता को बल मिला।
महिलाओं को राजनीतिक आंदोलनों से जोड़ना:
प्रजामण्डल आंदोलन ने महिलाओं को सक्रिय रूप से राजनीतिक आंदोलन से जोड़ा। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भाग लीं, जो इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
सामाजिक सुधार एवं रचनात्मक कार्यों द्वारा जनसंवाद स्थापित करना:
प्रजामण्डल आंदोलनों ने दलित, आदिवासी, और समाज के अन्य वर्गों के उत्थान के लिए कई सामाजिक सुधार कार्य किए। इन आंदोलनों ने शराबबंदी, नशीली वस्तुओं के प्रचार का विरोध, शिक्षा का प्रसार, चर्खा और खादी उत्पादन केंद्रों की स्थापना, और सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत आदि के खिलाफ संघर्ष किया, जिससे सामान्य जनता आंदोलन से जुड़ी।
ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता:
प्रजामण्डल आंदोलनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। यह ग्रामीण शिल्प, कृषि और आर्थिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, स्थानीय स्तर पर शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों का निर्माण किया।
कानूनी और प्रशासनिक सुधार:
प्रजामण्डल नेताओं ने स्वतंत्रता के बाद कानूनी और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कार्य किया, जो लोकतांत्रिक और पारदर्शी शासन की स्थापना में सहायक रहे।
प्रजामंडल आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका
प्रजामंडल आंदोलनों में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई, जो उनके साहस और नेतृत्व को दर्शाती है। विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं के योगदान को इस प्रकार समझा जा सकता है:
जयपुर प्रजामंडल आंदोलन
जयपुर में कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं को संगठित कर राजनीतिक जागरूकता फैलाई। उन्होंने नथमल जी के कटले में महिलाओं को संबोधित किया और उन्हें आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। रमादेवी देशपांडे, शारदा देवी, सुशीला गोयल, और इंद्र देवी जैसी महिलाओं ने सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई। रतन देवी, वनस्थली विद्यापीठ की संचालिका, ने छात्राओं को आंदोलन में भाग लेने की स्वतंत्रता दी, जिससे शांति देवी ने सभा को संबोधित किया।
शेखावाटी अंचल में, महिलाओं ने ठाकुर मानसिंह के अत्याचारों के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाई। किशोरी देवी और उत्तमा देवी के नेतृत्व में कटराथल में आयोजित महिला सम्मेलन (24 अप्रैल 1934) में महिलाओं ने धारा-144 का उल्लंघन कर अपने संकल्प का प्रदर्शन किया। जानकी देवी, सावित्री देवी, अंजना देवी, और रामदेवी जोशी ने गांव-गांव जाकर महिलाओं को शिक्षित और जागरूक किया। वे बिजोलिया और बेगू आंदोलन में भी महिलाओं का नेतृत्व करती रहीं।
जोधपुर की महिलाएं
जोधपुर में महिमा देवी किंकर ने सत्याग्रह कर महिलाओं के साहस को उजागर किया। रामदेवी, कृष्ण कुमारी, और दयावती ने ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए आम सभाओं को संबोधित किया। इस आंदोलन में गोरजा देवी जोशी, सावित्री देवी भाटी, सिरेकंवल व्यास, और राजकौर व्यास ने अपनी गिरफ्तारी दी।
बीकानेर में महिलाएं
लक्ष्मीदेवी आचार्य ने कोलकाता से बीकानेर राज्य प्रजामंडल का नेतृत्व कर महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता को बढ़ावा दिया।
मेवाड़ की महिलाओं का संघर्ष
नारायणी देवी और उनकी बेटियां स्नेहलता और भगवती देवी ने मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया। नारायणी देवी अपने छह माह के पुत्र को साथ लेकर जेल गईं। अकाल के समय इन्होंने ‘अकाल सहायता समिति’ की स्थापना की। उन्होंने महिलाओं को स्वदेशी और स्त्री शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया। कालीबाई, भील समुदाय की एक महिला, रास्तापाल सत्याग्रह में भाग लेते हुए 1947 में शहीद हुईं।
भरतपुर और कोटा की महिलाएं
भरतपुर में भगवती देवी और कृष्णा ने ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन में भाग लिया, जबकि सरस्वती बोहरा के नेतृत्व में महिलाओं ने जुलूसों में सक्रिय भूमिका निभाई। वे नमक कानून के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुईं।
कोटा की महिलाएं
‘भारत छोड़ों’ आंदोलनके समय राजकीय महाविद्यालय और सिटी स्कूल के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल कर दी। इसमें कृष्णगोपाल गुप्ता और छात्रा कुसुम गुप्ता का योगदान उल्लेखनीय रहा। यहाँ पर तो छात्राओं ने पुलिस कोतवाली रामपुरा पर तक अधिकार कर लिया था।
सिरोही में महिलाओं की सहभागिता
सिरोही में प्रजामंडल की पहली जयन्ती के दौरान 800 महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने प्रजामंडल के जुलूस में हिस्सा लेकर अपने साहस का परिचय दिया। इन आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी ने यह साबित कर दिया कि वे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में केवल सहायक भूमिका में नहीं थीं, बल्कि उन्होंने नेतृत्व करके समाज में बदलाव की दिशा तय की। उनके बलिदान और साहस ने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया।
FAQ (Previous year questions)
भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक चरण 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। जयपुर जैसे देशी रियासतों तथा विशेष रूप से जयपुर प्रजामंडल जैसी संस्थाओं की प्रतिक्रिया जटिल और मिश्रित थी।
कार्यवाहियाँ एवं समझौता:
प्रारंभ में, हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की मंशा प्रकट की।
किन्तु बाद में, शास्त्री ने जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल के साथ एक ‘जेन्टलमैन एग्रीमेंट’ (1942) किया, जिसके प्रमुख बिंदु थे:
जयपुर राज्य द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोई आर्थिक सहायता न देना,
प्रजामंडल की शांतिपूर्ण गतिविधियों की अनुमति देना,
‘उत्तरदायी शासन’ की दिशा में कदम उठाना,
महाराजा के प्रत्यक्ष विरोध से बचना।
इस समझौते के परिणामस्वरूप शास्त्री ने जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ नहीं किया, जिससे उन्हें आंतरिक आलोचना का सामना करना पड़ा।
आलोचना (आंतरिक असहमति एवं कमजोरियाँ):
बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी तथा हंस डी. राय जैसे नेताओं ने समझौते की अवहेलना करते हुए ‘आज़ाद मोर्चा’ का गठन किया और आंदोलन को जारी रखा।
इनकी गिरफ्तारी ने समझौते की भावना का उल्लंघन किया तथा शास्त्री की रणनीति की कमियों को उजागर किया।
जयपुर में आंदोलन निष्क्रिय और प्रतीकात्मक बनकर रह गया, जिससे देशी रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन की तीव्रता कम हो गई।
प्रजामंडल के भीतर उत्पन्न आंतरिक विभाजन ने उसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को क्षति पहुँचाई।
निष्कर्ष:
शास्त्री के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल की यह सतर्क नीति टकराव से बचने की कोशिश तो थी, परंतु इसने भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांतिकारी भावना से समझौता कर लिया। आंतरिक असहमति ने मध्यमार्गी और उग्र रणनीतियों के बीच तनाव को उजागर किया, जिससे जयपुर का योगदान ऐतिहासिक रूप से सीमित, परंतु राजनीतिक दृष्टि से विचारणीय बन गया।
राजस्थान में प्रजामण्डल आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में रियासतों में प्रचलित निरंकुश शासन के खिलाफ एक सशक्त जन जागृति के रूप में उभरा। इसके मूलभूत विशेषताएँ थी।
उत्तरदायी शासन की माँग : प्रजामंडल आंदोलन का लक्ष्य राजा-महाराजाओं को प्रजा के प्रति जवाबदेह बनाना था। यह शाही शोषण के खिलाफ था और संवैधानिक शासन की स्थापना का प्रस्ताव रखता था, जिसमें जनता को प्रशासन में भागीदारी मिले। शाहपुरा में गोकुल लाल असावा द्वारा स्थापित प्रथम उत्तरदायी शासन इसका प्रमुख उदाहरण है।
राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा : प्रजामंडल आंदोलन ने रियासती शासन के निरंकुश नियंत्रण के खिलाफ आवाज उठाई, लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों की मांग की, और लोगों को उनके राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया।
सामंती और उपनिवेशी विरोधी रुख : यह आंदोलन रियासती राज्यों की दमनकारी सामंती व्यवस्थाओं और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन दोनों के खिलाफ था। इसका उद्देश्य आम जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना था।
स्थानीय नेतृत्व का सशक्तिकरण : इन आंदोलनों ने स्थानीय नेतृत्व को सशक्त किया जिससे की नेतृत्व की दूसरी पंक्ति तैयार हुई जैसे कि हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, जिसने बाद में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना : प्रजामंडल ने राजस्थान के गांव-गांव में जागरूकता फैलाने के लिए गांवों-शहर में संगठन बनाए और हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया। आंदोलन ने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और संवाद को बढ़ावा दिया।
सामाजिक सुधार : आंदोलन ने समाज में व्याप्त कुप्रथाओं और असमानताओं को खत्म करने की कोशिश की। इसमें जातिवाद, महिलाओं के अधिकार, और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की पहल की गई।
राष्ट्रीय आंदोलन के साथ समन्वय : प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों को अपने रियासती राज्यों में लागू किया। इसमें स्कूलों की स्थापना, खादी का प्रचार, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन शामिल थे।
प्रजामंडल आंदोलन ने राजस्थान में निरंकुश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आंदोलन ने लोकतांत्रिक अधिकारों, सामाजिक समानता और राष्ट्रीय चेतना की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए।
राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन / राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन/ राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन/ राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन/ राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन/ राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन/ राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन / राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन