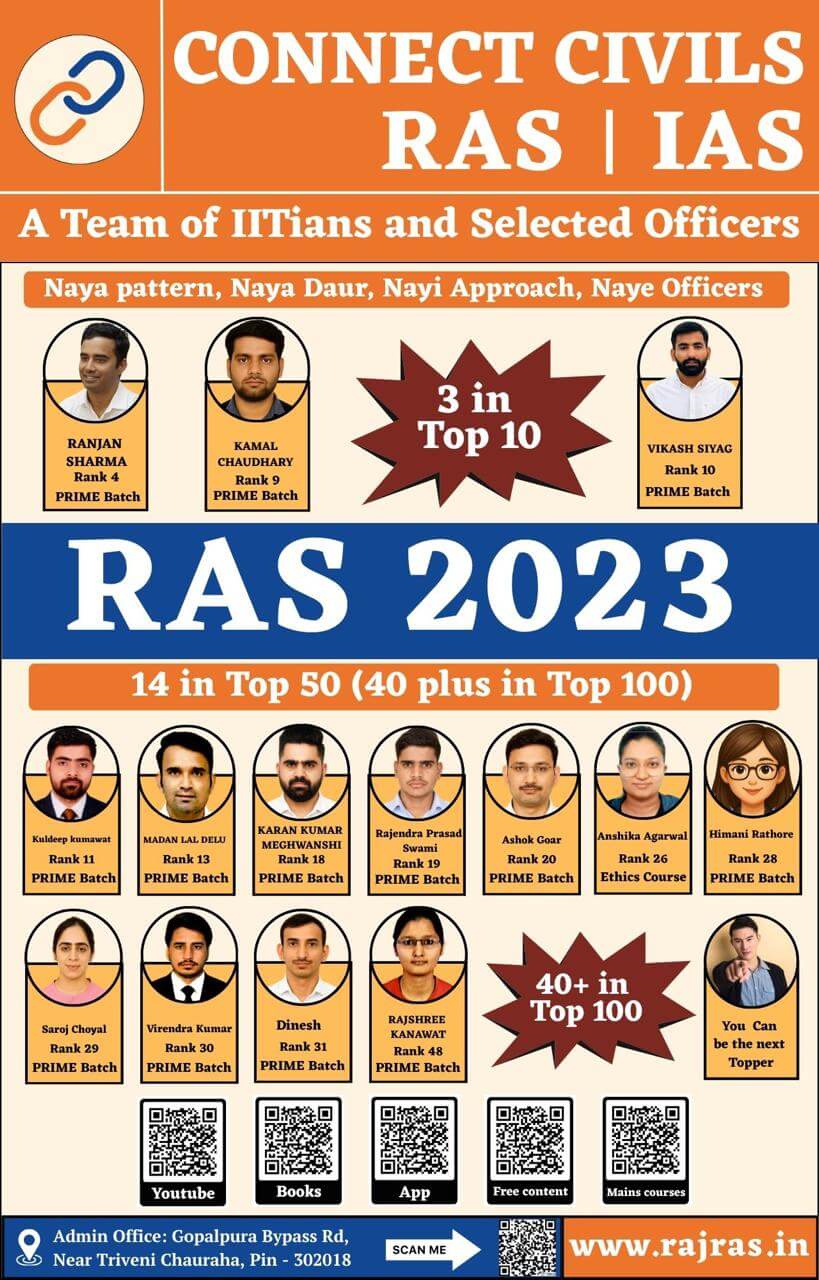राजस्थान की राजनीति के निर्धारक तत्त्व व लक्षण राज्य की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों से गहराई से जुड़े हुए हैं। इन तत्त्वों के माध्यम से राजस्थान की राजनीतिक संरचना, नेतृत्व शैली और मतदाता व्यवहार को समझा जा सकता है।
राजस्थान की राजनीति के निर्धारक तत्त्व व लक्षण
प्रजामंडल और किसान आंदोलन
- प्रजामंडल का उद्देश्य – रियासतों के कुशासन को समाप्त करना और नागरिकों को मौलिक अधिकार दिलाना।
- योगदान – देशी रियासतों में राजनीतिक जागरूकता और रचनात्मक गतिविधियों की शुरुआत।
- किसान आंदोलनों का प्रभाव – बिजौलिया, बेगूं, नीमूचना और मेव किसान आंदोलनों ने जनजागरण किया और रियासती दमन के विरुद्ध संघर्ष को प्रेरित किया।
जाति की भूमिका
- स्वतंत्रता के बाद राजस्थान की राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण कारक बनी।
- 1950-1970 तक जाट और राजपूत प्रमुख जातीय समूह रहे।
- जातिगत संघर्ष –
- जाट और कृषक जातियाँ कांग्रेस के पक्ष में रहीं।
- राजपूत जातियाँ रामराज्य परिषद और स्वतंत्र पार्टी का समर्थन करती थीं।
- जातीय संतुलन – कांग्रेस में लंबे समय तक जाट या राजपूत मुख्यमंत्री नहीं बन पाए।
- जातिगत निष्ठा ने दलीय निष्ठा को कमजोर किया और गुटबाजी को बढ़ावा दिया।
- 1990 के बाद मीणा, मेघवाल, गुर्जर, सैनी, यादव जैसी जातियाँ भी संगठित हुईं।
- रिचर्ड सिसॉन (The Congress Party in Rajasthan, 1971) –
- जाटों की शिक्षा, नौकरियों और भूमि स्वामित्व में वृद्धि से उनकी राजनीतिक चेतना बढ़ी।
- राजपूतों ने राम राज्य परिषद, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ और भाजपा का समर्थन किया।
सामंती पृष्ठभूमि और औद्योगिकीकरण का अभाव
- राजस्थान की राजनीति पर सामंती संस्कृति का प्रभाव रहा।
- 1950-1970 – सामंतों, राजाओं और जागीरदारों का प्रभाव रहा।
- स्वतंत्र पार्टी और राम राज्य परिषद् सामंती तत्वों के नियंत्रण में थीं।
- महत्वपूर्ण सामंती नेता –
- जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह
- डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह
- जयपुर की महारानी गायत्री देवी
- भैरोंसिंह शेखावत – राजपूत होते हुए भी सामंतवाद के विरोधी थे।
- वसुंधरा सरकार – “महारानी सरकार” कहे जाने से सामंती मानसिकता का संकेत।
- औद्योगिकीकरण की कमी और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने राजनीतिक ढांचे को प्रभावित किया।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और बढ़ती राजनीतिक चेतना
- शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि से नए राजनीतिक समूहों का उदय हुआ।
- इससे राजनीति बहुलवादी और प्रतिस्पर्धी बनी।
सांप्रदायिक राजनीति की सीमित भूमिका
- सामान्यतः राजस्थान की राजनीति सांप्रदायिक प्रभाव से मुक्त रही।
- 1992 – राम मंदिर आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ा।
- 2014 के बाद – हिन्दुत्व राजनीति का प्रभाव बढ़ा।
एकदलीय से द्विदलीय प्रणाली का विकास
- 1977 तक – कांग्रेस का वर्चस्व (एकदलीय प्रभुत्व प्रणाली)।
- 1977-1980 – जनता पार्टी का उभार, द्विदलीय प्रणाली की शुरुआत।
- 1980-1993 – बहुदलीय प्रणाली (कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, अन्य क्षेत्रीय दल)।
- 1993 से वर्तमान – भाजपा और कांग्रेस के बीच द्विदलीय मुकाबला।
गुटबाजी की प्रधानता
- कांग्रेस – हमेशा गुटबाजी से प्रभावित (सुखाड़िया का दौर अपवाद)।
- वर्तमान कांग्रेस – अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट गुट।
- भाजपा –
- भैरोंसिंह शेखावत के खिलाफ हरिशंकर भाभड़ा और ललित किशोर चतुर्वेदी का ब्राह्मण गुट।
- वसुंधरा राजे बनाम अन्य गुट।
दल-बदल और जोड़-तोड़ की राजनीति
- 1950 – जयनारायण व्यास ने सामंती विधायकों को कांग्रेस में मिलाकर राजनीति की।
- 1967 – मोहनलाल सुखाड़िया ने समर्थन जुटाने के लिए विधायकों का दल-बदल करवाया।
- 1990 और 1993 – भैरोंसिंह शेखावत ने जोड़-तोड़ से सरकार बनाई।
- 2008 और 2018 – अशोक गहलोत ने निर्दलीयों और छोटे दलों के समर्थन से सरकार बनाई।
क्षेत्रीयता से प्रभावित राजनीति
- प्रारंभ में – राजनीति ढूंढाड़ (जयपुर), मारवाड़ (जोधपुर), मेवाड़ (उदयपुर) के प्रभाव में रही।
- आज भी – क्षेत्रीय संतुलन राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करता है।
निर्दलीयों की निर्णायक भूमिका
- 1952 – 39 निर्दलीय विधायक जीते (27% वोट)।
- 1967, 1993, 2008, 2018 – निर्दलीयों ने सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- 2018 विधानसभा चुनाव – 13 निर्दलीय विधायक जीते, 9.5% वोट प्राप्त।
बाहरी नेताओं का प्रभाव
- राजस्थान की राजनीति में प्रभावशाली बाहरी नेता –
- बूटा सिंह (जालौर)
- राजेश पायलट (दौसा)
- बलराम जाखड़ (सीकर)
- चौधरी देवीलाल (हरियाणा, प्रभाव सीकर में)
विपक्ष की भूमिका
- विपक्ष संख्यात्मक रूप से कमजोर लेकिन प्रभावशाली रहा।
- 1977, 1993, 2003, 2013 – विपक्ष ने सत्ता परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बढ़ती जनभागीदारी और समावेशी राजनीति
- 1952 – मतदान प्रतिशत 37.42% था।
- 2018 – मतदान प्रतिशत बढ़कर 74.72% हो गया।
- राजनीतिक समावेशिता –
- पहले जाट, राजपूत और ब्राह्मण प्रभावी थे।
- अब ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
- राजनीतिक चेतना – हाशिए पर रहे समुदाय अब अपने अधिकारों को पहचानने लगे हैं।
निष्कर्ष
- राजस्थान की राजनीति जाति, क्षेत्रीयता, गुटबाजी, दल-बदल और निर्दलीय विधायकों की भूमिका से प्रभावित रही है। प्रारंभ में सामंती प्रभाव प्रमुख था, लेकिन लोकतांत्रिक चेतना बढ़ने के साथ राजनीति अधिक प्रतिस्पर्धी और समावेशी बन गई है। कांग्रेस और भाजपा के बीच द्विदलीय व्यवस्था मजबूत हुई है, जबकि जातीय और सामाजिक समीकरण भी राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रहे हैं।
राजस्थान की राजनीति पर महत्त्वपूर्ण पुस्तकें
- रिचर्ड सिसॉन (कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, अमेरिका) ने अपनी पुस्तक “The Congress Party in Rajasthan” में कांग्रेस पार्टी के विस्तार का अध्ययन किया।
- प्रो. के. एल. कमल (पूर्व कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय) ने “Party Politics in an Indian State” में सभी राजनीतिक दलों और जातीय प्रभाव का विश्लेषण किया।
- रूडोल्फ एंड रूडोल्फ – “Essays on Rajasthan: Reflections on History, Culture and Administration” (1984)
- के. एल. कोचर – “रियासती राजपूताना से जनतांत्रिक राजस्थान”
- विजय भंडारी – “राजस्थान की राजनीति: सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में”
राजस्थान की राजनीति में जाति
राजस्थान की राजनीतिक प्रणाली का आधारभूत तत्व सामाजिक संरचना एवं राजनीतिक पद्धति के मध्य अन्तर्सम्बन्ध है। ऐतिहासिक वंशों के लिए जाति राजनीतिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण सीढ़ी है। राजस्थान जैसे राज्य में जहां बहुत कम आधुनिकीकरण हुआ है, जातिगत झुकाव ही इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, राजनीतिक नेतृत्व द्वारा प्रभावशाली व स्थायी राजनीतिक पद्धति के लिए जातिगत संरचना का उपयोग किया जाता है।
प्रारंभिक राजनीति और जातीय प्रभाव (1952-1977)
1952 का पहला विधानसभा चुनाव
- कुल 160 सीटों में से 54 राजपूत, 22 ब्राह्मण, 12 जाट, 15 वैश्य, 10 अनुसूचित जाति, 6 जनजाति, 2 मुस्लिम और 39 अन्य जातियों के विधायक निर्वाचित हुए।
- राजपूतों ने सामंती शक्ति के साथ सत्ता प्राप्ति की कोशिश की।
- कांग्रेस को मुख्य चुनौती सामंतों और राजपूतों से मिली।
1957-1967: जातीय ध्रुवीकरण की दो धाराएँ
- कांग्रेस समर्थक जातियाँ: जाट, ब्राह्मण, वैश्य, मुस्लिम, अनुसूचित जाति एवं जनजाति।
- राजपूतों का झुकाव सामंतवाद की ओर: स्वतंत्र पार्टी और अन्य गुटों में सक्रिय भूमिका।
- जयनारायण व्यास ने 22 राजपूत जागीरदार विधायकों को कांग्रेस में लाने की कोशिश की, जिससे जाट नेताओं में असंतोष बढ़ा।
- मोहनलाल सुखाड़िया ने जाटों को संतुलित करने की नीति अपनाई, जिससे जाटों का प्रभाव बढ़ा।
- 1966 में जाट नेता कुम्भाराम आर्य और राजपूत नेता हरिश्चंद्र सिंह कांग्रेस से अलग हुए और जाट राजनीति का केंद्रबिंदु बन गए।
1962-1977: स्वतंत्र पार्टी और सामंतवादी राजनीति
- 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई, जिसने राजपूत सामंतों और उद्योगपतियों का समर्थन प्राप्त किया।
- गायत्री देवी (जयपुर महारानी) ने स्वतंत्र पार्टी को ताकत दी, जिससे राजपूतों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा।
- 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स खत्म किए, जिससे सामंतशाही कमजोर हुई।
- 1977 के बाद जातीय राजनीति अधिक प्रभावी हुई, क्योंकि पिछड़ी जातियों की भागीदारी बढ़ने लगी।
मंडल आयोग, जातीय उभार और सामाजिक विभाजन (1977-1999)
मंडल आयोग और जातीय ध्रुवीकरण (1978-1992)
- 1978 में केंद्र सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया।
- 1990 में वी.पी. सिंह सरकार ने पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की सिफारिश लागू की।
- सवर्ण जातियों में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हुआ, कई युवाओं ने आत्मदाह किए।
- राजस्थान में जयपुर, अजमेर, कोटा जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए।
1990: भाजपा-जनता दल (जद) गठबंधन और जातीय समीकरण
- भाजपा और जनता दल ने मिलकर सरकार बनाई, जिसका आधार जाट-राजपूत गठबंधन था।
- विधानसभा चुनावों में 32 जाट और 19 राजपूत विधायक निर्वाचित हुए।
- केंद्र में नाथूराम मिर्धा (जाट नेता) मंत्री बने, और चौधरी देवीलाल उपप्रधानमंत्री बने।
1996-1999: भाजपा में जाटों का प्रभाव बढ़ा
- 1996 में नाथूराम मिर्धा की मृत्यु के बाद भाजपा ने जाटों को आकर्षित किया।
- 1997 के नागौर उपचुनाव में भाजपा ने रामनिवास मिर्धा को हराया।
- 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जाटों को OBC में शामिल करने की घोषणा की, जिससे भाजपा को बड़ा राजनीतिक लाभ हुआ।
- जाटों के भाजपा की ओर झुकाव से राजपूतों में असंतोष बढ़ा, जिससे सामाजिक न्याय मंच नामक संगठन का गठन हुआ।
21वीं सदी की जातीय राजनीति (2003-2023)
2003: भाजपा और गुर्जर-ST आरक्षण वादा
- गुर्जर समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल करने का वादा किया गया।
- भाजपा को 2003 के चुनाव में भारी बहुमत मिला।
- वादा पूरा न करने के कारण 2007 में गुर्जर आंदोलन भड़का, जिससे राजस्थान में गुर्जर-मीणा जातीय संघर्ष हुआ।
2007-2008: गुर्जर आंदोलन और जातीय हिंसा
- गुर्जर समुदाय ने आंदोलन तेज किया, पुलिस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी मारे गए।
- मीणा समुदाय ने विरोध किया कि गुर्जर ST श्रेणी में नहीं आते।
- भाजपा सरकार ने समस्या को केंद्र सरकार पर टाल दिया, जिससे गुर्जरों में नाराजगी और भाजपा को राजनीतिक नुकसान हुआ।
2018-2023: जातिगत ध्रुवीकरण और कांग्रेस-भाजपा की रणनीति
- राजपूतों की भाजपा से नाराजगी बढ़ी, जिससे 2018 में कांग्रेस को समर्थन मिला।
- गुर्जर, मीणा और अन्य जातियों ने आरक्षण की मांग जारी रखी।
- 2023 चुनाव में भाजपा ने फिर से जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की।
निष्कर्ष
- राजस्थान की राजनीति में जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं।
- 1950-70 के दशक में सामंतशाही और राजपूत प्रभाव प्रमुख था, लेकिन 1977 के बाद पिछड़ी जातियां राजनीति में मजबूत हुईं।
- 1990 के दशक में जाट और राजपूतों के समीकरण ने भाजपा को सत्ता में पहुंचाया।
- 1999 में जाटों को ओबीसी में शामिल करने से भाजपा को बड़ा लाभ हुआ, लेकिन इससे राजपूत समाज में असंतोष बढ़ा।
- 2003 के चुनावों में भाजपा ने गुर्जरों को ST का दर्जा देने का वादा किया, लेकिन इसे पूरा न करने पर गुर्जर आंदोलन हुआ।
- जातिगत संघर्षों और आरक्षण संबंधी आंदोलनों ने राजस्थान की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है।
- 2023 तक जातिगत ध्रुवीकरण जारी रहा, और सभी प्रमुख दल जातीय संतुलन बनाने में लगे रहे।
राजस्थान की राजनीति में जातिवाद, आरक्षण आंदोलन और राजनीतिक समीकरणों का प्रभाव लगातार बना रहा है, और भविष्य में भी यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है।
राजनीतिक जनांकिकी
राजनीतिक जनांकिकी और उसका प्रभाव
- राजनीतिक जनांकिकी (Political Demographics) का अर्थ है, जनसंख्या के ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू जो राजनीतिक व्यवहार और परिणामों को प्रभावित करते हैं। यह समाज की जनसांख्यिकीय संरचना को देखते हुए चुनावी परिणामों, मतदान की प्रवृत्तियों, राजनीतिक पार्टियों की रणनीतियों, और विभिन्न जनसमूहों की राजनीतिक भागीदारी को समझने में मदद करता है।
- राजनीतिक जनांकिकी एक जटिल और विकासशील क्षेत्र है। विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न जनांकिकी समूहों का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- चुनाव परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल विविध आबादी को सफलतापूर्वक एकजुट कर सकता है और उनसे अपील करता है।
- राजस्थान में कई जनसांख्यिकीय विशेषताएँ हैं, जो राज्य की राजनीति और चुनावी व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इन प्रमुख कारकों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है:
- जनसंख्या आकार:
- राजस्थान का जनसंख्या आकार देश में आठवें स्थान पर है, जो इसे चुनावों के दौरान एक महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्र बनाता है।
- आयु वितरण:
- राज्य की अधिकांश आबादी युवा है, और युवा मतदाताओं की राजनीतिक प्राथमिकताएँ पुरानी पीढ़ी से भिन्न होती हैं।
- जाति और समुदाय:
- विभिन्न जातियों और समुदायों का राजनीतिक प्रभाव अलग-अलग स्तर का होता है। विभिन्न दल इन समुदायों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
- धार्मिक विविधता:
- धार्मिक पहचान और साम्प्रदायिक राजनीति मतदान व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- लिंग जनसांख्यिकी:
- महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी राजनीतिक जनांकिकी का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।
- शहरी और ग्रामीण विभाजन:
- राजस्थान की अधिकांश आबादी ग्रामीण है, लेकिन शहरीकरण का विस्तार हो रहा है। शहरी और ग्रामीण निवासियों की चिंताएँ अलग-अलग होती हैं, जो राजनीतिक मुद्दों और मतदान पैटर्न को प्रभावित करती हैं।
- शिक्षा और साक्षरता:
- शिक्षित जनसंख्या राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी को प्रभावित करती है।
- आर्थिक स्थिति:
- राज्य की जनसंख्या कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न है, जो राजनीतिक प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं।
- प्रवासन:
- आंतरिक और बाहरी प्रवासन पैटर्न राज्य की जनांकिकी और राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है।
राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव (1952) में राजनीतिक जनांकिकी
जनसांख्यिकीय स्थिति:
- 1951 की जनसंख्या गणना के अनुसार, राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 1.6 करोड़ थी।
- साक्षरता दर केवल 8% थी, जिससे चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक भागीदारी प्रभावित हुई थी।
कुल मतदाता और चुनावी आंकड़े:
- कुल मतदाता: 92.68 लाख।
- कुल मतदान उपस्थिति: 35.19%।
- कुल सीटें: 160 (जिसमें 140 सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और 1 जनजातीय समुदाय हेतु आरक्षित था)।
- 11 राजनीतिक दलों ने चुनाव में भाग लिया, जिनमें 10 राष्ट्रीय दल और किसान जनता संयुक्त पार्टी शामिल थे।
निर्दलीय उम्मीदवार:
- कुल 35 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें से कई ने जीत हासिल की।
महिला उम्मीदवारों की स्थिति:
- 4 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन सभी हार गईं।
- इसके बाद 17 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें पहली महिला विधायक यशोदा देवी (बांसवाडा) और दूसरी महिला विधायक कमला बेनीवाल विजयी हुईं।
मुस्लिम उम्मीदवारों की स्थिति:
- इस चुनाव में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की।
जातिगत राजनीति:
- जाट-राजपूत संघर्ष की राजनीति इस चुनाव में प्रमुख रही, जो राजस्थान की राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन गई।
लोकसभा और राज्यसभा चुनाव:
- राजस्थान में पहले लोकसभा चुनाव के समय 22 लोकसभा सीटें निर्धारित की गई थीं।
- राज्यसभा की सीटें भी निर्धारित थीं।
- प्रथम लोकसभा चुनाव में 2 महिला प्रत्याशियों ने भाग लिया, लेकिन वे दोनों हार गईं।
- राज्यसभा की पहली महिला सांसद श्रीमती शारदा भार्गव थीं।
राजस्थान के 16वें विधानसभा चुनाव (2023) में राजनीतिक जनांकिकी
1. मतदान एवं मतगणना
- राजस्थान में 16वीं विधानसभा के लिए 25 नवंबर 2023 को चुनाव संपन्न हुए।
- 3 दिसंबर 2023 को मतगणना हुई।
- कुल मतदान प्रतिशत: 75.45% (2018 के 74.71% से 0.73% अधिक)।
- पोस्टल बैलेट से मतदान: 0.83%।
- ईवीएम से मतदान: 74.62%।
- पुरुष मतदाता: 74.53%
- महिला मतदाता: 74.72%
2. निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत
- सबसे अधिक मतदान:
- कुशलगढ़ (88.13%) – 2018 में 86.13% था।
- पोकरण (87.79%) – 2018 में 87.50% था।
- तिजारा (86.11%) – 2018 में 82.08% था।
- सबसे कम मतदान:
- आहोर (61.24%) – 2018 में 61.53% था।
- मारवाड़ जंक्शन (61.29%) – 2018 में 60.42% था।
- सुमेरपुर (61.44%) – 2018 में 60.89% था।
- महिला मतदाता अधिक:
- पोकरण (88.23%), कुशलगढ़ (87.54%), तिजारा (85.45%)।
- महिला मतदाता कम:
- जोधपुर (62.97%), टोडाभीम (63.22%), बामनवास (63.63%)।
3. मतदान में वृद्धि और गिरावट
- सबसे अधिक वृद्धि:
- बसेड़ी (+9.6%), तारानगर (+7.65%), आसपुर (+7.01%)।
- सबसे अधिक गिरावट:
- फलौदी (-7.15%), हिंडौन (-6.10%), जैसलमेर (-4.79%)।
4. कुल मतदान संख्याएँ
- ईवीएम से कुल वोट पड़े: 3,92,11,399।
- महिला वोट: 1,88,27,294।
- पुरुष वोट: 2,03,83,757।
- थर्ड जेंडर वोट: 348।
- वैध वोट: 3,98,30,823 (99.89%)।
- अमान्य वोट: 43,783 (0.11%)।
- कुल डाले गए वोट: 3,98,74,606 (75.33%)।
- पंजीकृत मतदाता: 5,29,31,152।
5. राजनीतिक दलों का प्रदर्शन
- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा): 115 सीटें (बहुमत)।
- कांग्रेस: 69 सीटें।
- अन्य दल एवं निर्दलीय: 15 सीटें।
6. राजनीतिक रुझान एवं सामाजिक जनांकिकी
- जातीय समीकरण:
- जाट, गुर्जर, ओबीसी और एसटी मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर बढ़ा।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति मतदाता पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई।
- महिला मतदाता:
- भाजपा की महिला केंद्रित योजनाओं ने महिलाओं का समर्थन आकर्षित किया।
- युवा मतदाता:
- भाजपा की रोजगार और विकास नीतियों का असर दिखा।
राजस्थान की राजनीति के निर्धारक तत्त्व व लक्षण / राजस्थान की राजनीति के निर्धारक तत्त्व व लक्षण