राजपूतों का उत्पत्ति राजस्थान इतिहास व संस्कृति का एक प्रमुख विषय है, जो गुर्जर-प्रतिहार, राठौड़, चौहान, कछवाहा और गुहिल (मेवाड़ के सिसोदिया) जैसी शक्तिशाली राजवंशों के उदय से जुड़ा हुआ है। ये वंश अपनी वीरता और शाही विरासत के लिए प्रसिद्ध हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुल, ऐतिहासिक, पौराणिक और विदेशी सिद्धांत उनके जटिल और विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, जो मध्यकालीन राजस्थान के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं।
राजपूतों का उत्पत्ति
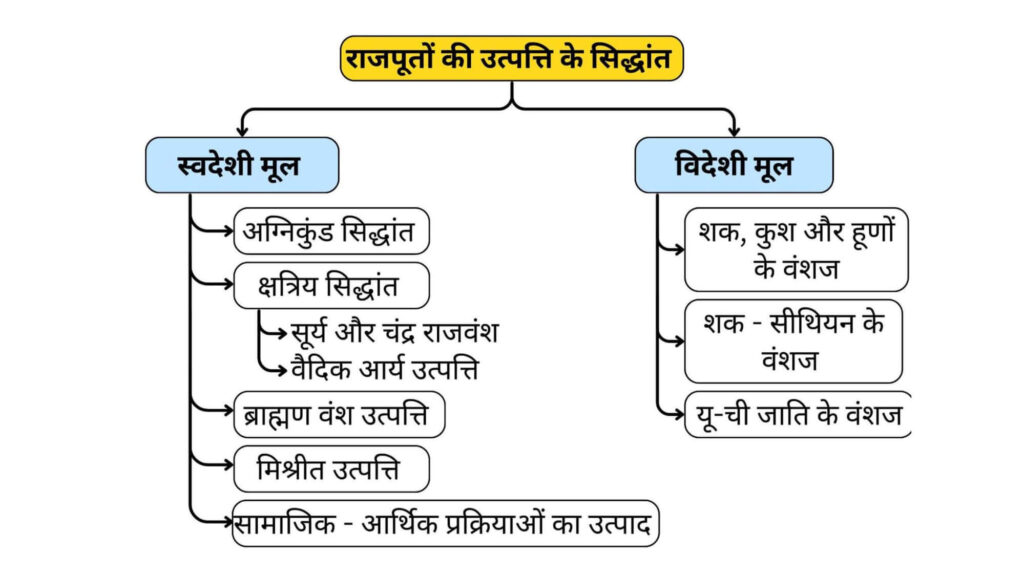
राजपूत शब्द का उपयोग 6वीं शताब्दी ईस्वी से होने लगा था। राजपूतों की उत्पत्ति एक विवादित विषय है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में दो प्रमुख विचारधाराएँ हैं:
विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत:
- शक, कुषाण, और हुणों के वंशज –
- राजपूत शको, कुषाणों, हुणों जैसी जातियों के वंशज हैं।
- समर्थक: डॉ. वी.ए. स्मिथ, कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रूक्स
- आधार: राजपूतों और शक जाति के बीच समानता, जैसे – सती प्रथा, सूर्य पूजा, अस्तबल पूजा, अश्वमेध यज्ञ, राज्याभिषेक, अग्नि पूजा, मद्यपान आदि।
- शक-सीथियन वंशज –
- समर्थक: कर्नल जेम्स टॉड
- यू-ची (कुषाण) जाति के वंशज –
- समर्थक: कन्निंघम
- आधार: ब्रॉचगुर्जर ताम्र पत्र
स्वदेशी उत्पत्ति सिद्धांत:
अग्निकुंड सिद्धांत –
- राजपूतों का उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, जिसे ऋषि वशिष्ठ ने गुरु शिखर, माउंट आबू में यज्ञ करके उत्पन्न किया था। अग्निकुंड से चार प्रमुख राजपूत वंशों का जन्म हुआ – चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार।
- समर्थक: मुहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण
- आधार: पृथ्वीराज रासो, चंदरबरदाई
क्षत्रिय सिद्धांत –
- राजपूत विदेशी उत्पत्ति के नहीं हैं, वे पौराणिक क्षत्रिय नायकों जैसे कि राम के वंशज हैं।
- इस सिद्धांत में राजपूतों को उनके वंश के आधार पर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में बांटा गया है।
- सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उत्पत्ति
- समर्थक: डॉ. गौरीशंकर ओझा, दशरथ शर्मा
- आधार: शृंगि ऋषि शिलालेख (गुहिल सूर्यकुल के वंशज), हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय (चौहान सूर्यवंशी क्षत्रिय), ग्वालियर प्रशस्ति (प्रतिहार सूर्यवंशी वंश से हैं)
- भाटी (जैसलमेर) अपनी उत्पत्ति चंद्रवंश से मानते हैं।
- वैदिक आर्य वंशज –
- समर्थक: सी.वी. वैद्य
ब्राह्मणिक उत्पत्ति –
- समर्थक: डॉ. भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा
- आधार: बिजोलिया शिलालेख (चौहान वत्स गोत्र ब्राह्मण हैं), अचलेश्वर शिलालेख (गुहिल नागर ब्राह्मण हैं)
मिश्रित उत्पत्ति –
- समर्थक: डॉ. डी. पी. चट्टर्जी
- राजपूत एक मिश्रित जाति है, जिनमें से कुछ आर्यवंशी थे जबकि अन्य विदेशी जातियों जैसे हुण, शक आदि से थे
गुर्जर-प्रतिहार
प्रतिहार वंश, जो अग्निकुल के सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक है, ऐतिहासिक रूप से गुर्जर-प्रतिहार के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका संबंध गुर्जर समुदाय से है। गुर्जरों का प्रथम उल्लेख बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के ‘ऐहोल अभिलेख’ में मिलता है। इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार, गुर्जर-प्रतिहारों ने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक उत्तर-पश्चिम भारत पर शासन किया और अरब आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक दीवार के रूप में कार्य किया। उनकी उत्पत्ति को लेकर विभिन्न सिद्धांत मौजूद हैं, परंतु मुहणोत नैणसी ने गुर्जर-प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें मंडोर, जालोर, राजगढ़, कन्नौज, उज्जैन और भड़ौच की शाखाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
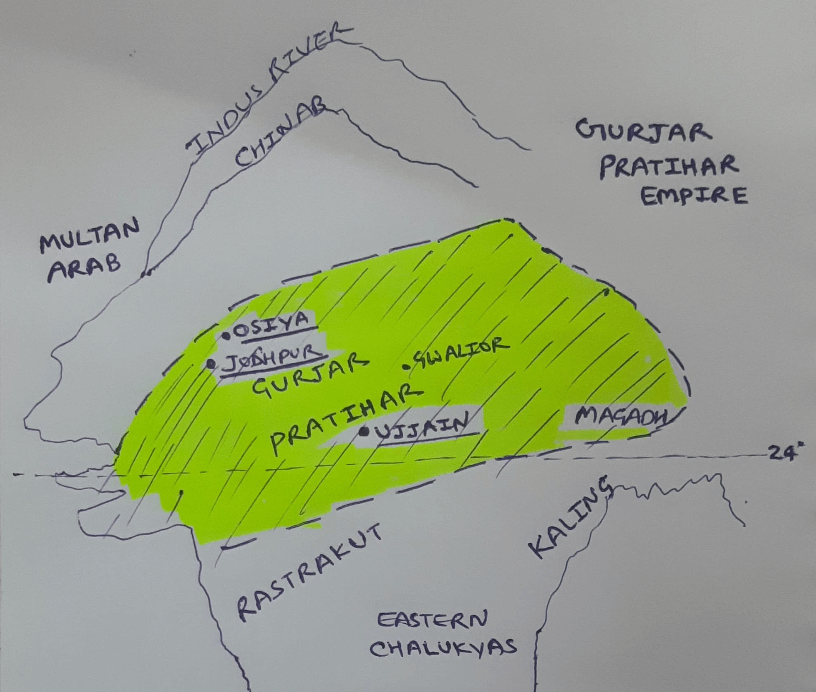
मंडोर के प्रतिहार
मंडोर एक प्राचीन नगर है और यह मंडव्यपुर के प्रतिहारों का मुख्य स्थान था, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र पर शासन किया। इस वंश की उत्पत्ति का वर्णन दो शिलालेखों में मिलता है:
- 837 ईस्वी का जोधपुर का बाउका शिलालेख
- 861 ईस्वी का घंटियाला (या घाटियाला) शिलालेख, जो कक्कुक का है।
रुडोल्फ होर्नले ने प्रत्येक पीढ़ी के लिए 20 वर्षों की अवधि मानते हुए, इस वंश के संस्थापक हरिचंद्र को लगभग 640 ईस्वी में रखा। बैजनाथ पुरी ने हरिचंद्र को लगभग 600 ईस्वी में रखा। वहीं, आर. सी. मजूमदार ने प्रत्येक पीढ़ी के लिए 25 वर्षों की अवधि मानते हुए उन्हें लगभग 550 ईस्वी में रखा। वंश के शासकों और उनके शासनकाल की सूची, 25 वर्षों की अवधि मानते हुए, इस प्रकार है:
गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद, प्रतिहारों की एक शाखा मंडोर में शासन करती रही। 1395 ईस्वी में, इस शाखा की एक राजकुमारी का विवाह राठौर कुल के राव चूंडा से हुआ। इसके परिणामस्वरूप, राव चूंडा को मंडोर का जूनागढ़ किला दहेज में मिला और उन्होंने अपनी राजधानी वहीं स्थानांतरित कर ली। यह नगर 1459 ईस्वी तक राठौड़ो की राजधानी बना रहा, जब राव जोधा ने नई नगर जोधपुर की स्थापना करके अपनी राजधानी वहां स्थानांतरित कर दी।
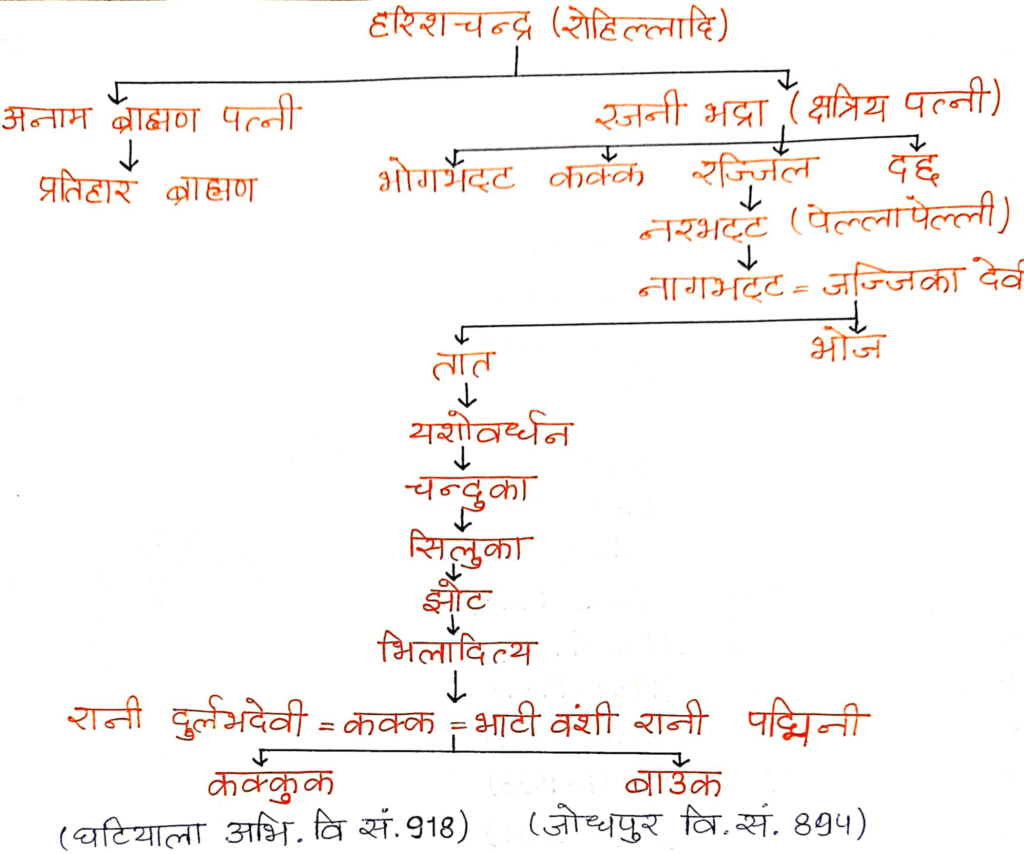
जालौर (भीनमाल) के प्रतिहार
जालौर, उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहार मंडोर के प्रतिहारों से निकटता से जुड़े थे। हरिश्चंद्र के समय से, उनके वंशज अलग-अलग क्षेत्रों जैसे कन्नौज, मालवा, गुजरात और राजस्थान में बसने लगे, और धीरे-धीरे अपने साम्राज्य स्थापित किए। उज्जैन के प्रतिहारों का उदय नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में हुआ, जिन्हें उज्जैन, कन्नौज और जालौर में प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है।
नागभट्ट प्रथम (730-760 ईस्वी)
गुर्जर-प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम का शासनकाल प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। उनकी नेतृत्व क्षमता ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की और भारत को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा।
राजनीतिक उपलब्धियाँ:
- अरब आक्रमणकारियों पर विजय:
- नागभट्ट प्रथम ने सिंध के बाद पश्चिमी भारत में अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश कर रहे अरब आक्रमणकारियों को हराया। ग्वालियर के शिलालेख में उन्हें “नारायण” और “म्लेच्छ-नाशक” (विदेशियों का नाश करने वाला) कहा गया है।
- शक्ति का समेकन:
- नागभट्ट प्रथम ने गुजरात, राजस्थान और मध्य भारत के छोटे-छोटे राज्यों को एकीकृत किया और गुर्जर-प्रतिहार वंश के लिए एक मजबूत राजनीतिक नींव रखी।
प्रशासनिक योगदान:
- नागभट्ट प्रथम ने प्रशासनिक स्थिरता और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित किया। उन्होंने नगरों की सुरक्षा और व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया, जिससे वाणिज्य और समृद्धि को बढ़ावा मिला।
सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण:
- नागभट्ट प्रथम ने हिंदू धर्म का समर्थन किया और मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहित किया, जिससे भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का पुनरुत्थान हुआ।
वत्सराज (783-795 ईस्वी)
वत्सराज के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, जो लगभग 150 वर्षों तक चला। यह संघर्ष कन्नौज पर नियंत्रण के लिए गुर्जर-प्रतिहार (उत्तर-पश्चिम), राष्ट्रकूट (दक्षिण) और पाल (बंगाल) के बीच था।
साहित्यिक योगदान:
- उद्योतनसुरी ने जालौर में ‘कुवलयमाला’ की रचना की और आचार्य जिनसेन ने ‘हरिवंश पुराण’ लिखा।
धार्मिक और स्थापत्य योगदान:
- उनके शासनकाल में ओसियां में महावीर जैन मंदिर का निर्माण हुआ, जो पश्चिमी राजस्थान के सबसे पुराने जैन मंदिरों में से एक है।
मिहिर भोज (836-885 ईस्वी)
मिहिर भोज गुर्जर-प्रतिहार वंश के महानतम शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल में गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य अपने राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक उत्कर्ष पर था।
राजनीतिक उपलब्धियाँ:
- राजपूताना पर नियंत्रण: मिहिर भोज ने मंडोर के प्रतिहार शासक बाउक को हराकर राजपूताना पर नियंत्रण स्थापित किया। जोधपुर और चाटसू के शिलालेख उनके शासनकाल के विस्तार को दर्शाते हैं।
- त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय: उन्होंने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण III को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, जो उनके साम्राज्य की राजधानी बन गई।
- अरब विस्तार के खिलाफ प्रतिरोध: मिहिर भोज ने अरबों के विस्तार को प्रभावी ढंग से रोका। अरब यात्री सुलेमान ने उन्हें “इस्लाम का दुश्मन” कहा और उनके शासनकाल की स्थिरता और समृद्धि की प्रशंसा की।
प्रशासनिक सुधार:
मिहिर भोज ने कर संग्रह प्रणाली को मजबूत किया और व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उनके शासनकाल में कृषि और सिंचाई प्रणालियों में सुधार हुआ, जिससे किसानों की समृद्धि बढ़ी।
सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान:
मिहिर भोज वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और मंदिर निर्माण तथा धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उनके वैष्णव धर्म के प्रति समर्पण को ग्वालियर शिलालेख में उनके “आदिवराह” शीर्षक से व्यक्त किया गया है।
महेंद्रपाल प्रथम (885-910 ईस्वी)
मिहिर भोज के बाद उनके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम ने गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य का सिंहासन संभाला। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और संस्कृति का अत्यधिक विकास हुआ।
- राजशेखर की साहित्यिक रचनाएँ:
- कर्पूरमंजरी: प्राकृत में लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक।
- काव्यमीमांसा: काव्य के सिद्धांत और अभ्यास पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ।
- विद्धशालभंजिका: एक नाटक, जो उनकी साहित्यिक प्रतिभा को दर्शाता है।
- बालभारत और बालरामायण: रामायण और महाभारत की कहानियों पर आधारित नाटक।
- हरविलास: एक काव्य रचना।
- प्रचंड पांडव: पांडवों पर एक कथा।
- भुवनकोश: एक भौगोलिक ग्रंथ।
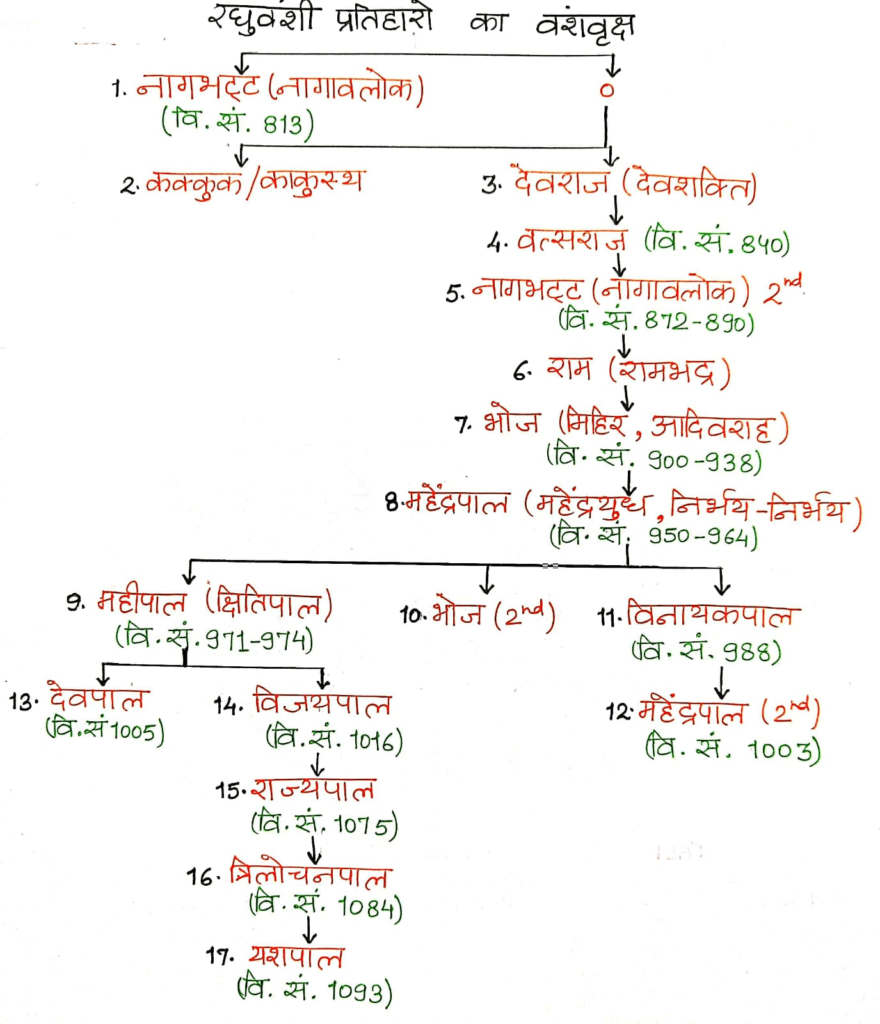
त्रिपक्षीय संघर्ष (750-900 ईस्वी):
त्रिपक्षीय संघर्ष (8वीं–12वीं शताब्दी) उत्तरी भारत में पाल, प्रतिहार, और राष्ट्रकूट वंशों के बीच युद्धों की एक श्रृंखला थी। ये संघर्ष गंगा के मैदानों में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुआ।
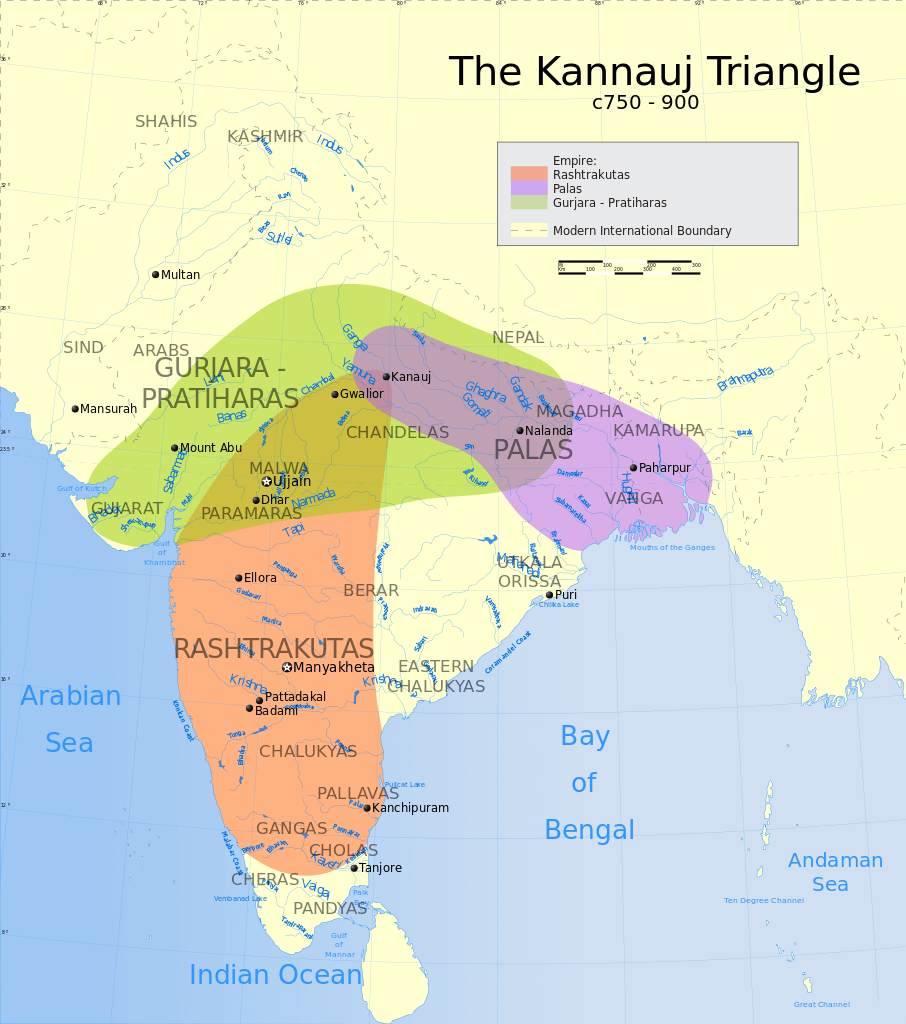
|
चरण |
घटनाक्रम और विवरण |
|
पहला चरण |
|
|
दूसरा चरण |
|
|
तीसरा चरण |
|
|
चौथा चरण |
|
यशपाल (1027-1036 ईस्वी)
यशपाल गुर्जर-प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे। उनके बाद, 1093 ईस्वी में, गहड़वाल राजा चंद्रदेव ने प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया और प्रतिहारों की स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता का अंत कर दिया। इसके बाद प्रतिहार गहड़वालों, राठौड़ो और चौहानों के केवल जागीरदार बनकर रह गए।
- तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद, मोहम्मद गोरी ने जयचंद पर आक्रमण किया।
- 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। जल्द ही गहड़वाल साम्राज्य नष्ट हो गया।
- कन्नौज के जयचंद के पोते राव सीहाजी अपने द्वारका तीर्थयात्रा के दौरान मारवाड़ आए।
- उनके पुत्र, राव आस्थान ने पाली और खेड़ (पश्चिमी मारवाड़ में) पर कब्जा कर लिया, लेकिन अंततः दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के हाथों युद्ध में मारे गए।
- राव चूंडा/चंद्रजी, सीहा की दसवीं पीढ़ी, ने अंततः मारवाड़ पर गुर्जर प्रतिहारों से नियंत्रण छीन लिया और मारवाड़ में राठौड़ों का शासन स्थापित किया। जोधपुर राठौड़ों का मुख्य राज्य थी, लेकिन विभिन्न राज्यों (बीकानेर, किशनगढ़ आदि) में भी राठौड़ों ने अपना शासन स्थापित किया ।
- प्रतिहारों के पतन के बाद, उनकी राजधानी कन्नौज पर गहड़वालों (राठौड़ों) ने क़ब्ज़ा कर लिया। चंद्रदेव, जो राठौर क़बीले से संबंधित थे, ने गोपाला को पराजित किया और गहड़वाला वंश की स्थापना की।
गुर्जर-प्रतिहारों का मूल्यांकन:
गुर्जर-प्रतिहारों ने उत्तर भारत के राजनीतिक, सैन्य, और सांस्कृतिक इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकारित किया। पुष्यभूति वंश के पतन के बाद, इन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, विदेशी आक्रमणों का विरोध किया और कला तथा वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उपलब्धियाँ:
- मजबूत साम्राज्य: गुर्जर-प्रतिहारों ने हर्ष के निधन के बाद उत्तर भारत में पहला बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, जो लगभग 150 वर्षों तक कायम रहा।
मिहिर भोज के शासनकाल को इनका सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है, जब बागरामा अभिलेख में उन्हें “सम्पूर्ण पृथ्वी के विजेता” के रूप में वर्णित किया गया। - पश्चिमी सीमा के रक्षक: नागभट्ट I ने सिंध के निकट अरबी आक्रमणकारियों को निर्णायक रूप से पराजित किया, उसे ग्वालियर अभिलेख में “नारायण” और “म्लेच्छ-नाशक” कहा गया। मिहिर भोज ने अरब आक्रमणों को विफल कर दिया, जिसकी सुलेमान ने मिहिर भोज को “इस्लाम का दुश्मन” कहकर प्रशंसा की।
- सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण: गुर्जर-प्रतिहार कला और साहित्य के महान संरक्षक थे, और महेन्द्रपाल I के दरबार में संस्कृत कवि राजशेखर का स्वागत हुआ। गुर्जर-प्रतिहार शैली ने भारतीय मंदिर वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे जटिल उकेराई और विस्तृत शिखरों के लिए जाना जाता है, जैसे कि ओसियां सूर्य मंदिर।
- सैन्य और राजनीतिक उपलब्धियाँ: लंबे समय तक चले त्रिपक्षीय संघर्ष के बावजूद, इन्होंने इस क्षेत्र में अपनी प्रमुखता बनाए रखी।
नागभट्ट II ने कन्नौज को पुनः प्राप्त किया, जबकि मिहिर भोज के अभियानों ने साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे उत्तर भारत में इसकी श्रेष्ठता स्थापित हुई।
गुर्जर-प्रतिहारों का पतन:
- विदेशी आक्रमण: महमूद गज़नी के आक्रमणों, विशेष रूप से कन्नौज की लूट, ने साम्राज्य के पतन को तेज किया।
- आंतरिक संघर्ष: कुटुंबीय विवादों और शक्ति संघर्षों ने साम्राज्य को कमजोर किया।
- जमींदारों का उदय: कमजोर केंद्रीय नेतृत्व ने जमींदारों को स्वतंत्रता की ओर प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप साम्राज्य का विखंडन हुआ।
- त्रैतीयक युद्ध का प्रभाव: कन्नौज पर एक सदी तक चले संघर्ष ने उन्हें बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील बना दिया।
मारवाड़ के राठौड़

राठौड़ वंश के संस्थापक सीहा थे, जिन्हें कन्नौज के जयचंद गढ़वाल का वंशज माना जाता है। वे हरिश्चंद्र [जयचंद के पुत्र] के पोते और सेंतराम के बेटे थे। सिहाजी के पश्चात अस्तान, दूहड़, राव चड़ा और अंत में राव चुंडा का शासन हुआ।
राव चूड़ा (1394-1423 ई.)
- चंद्रजी ने मारवाड़ राज्य की स्थापना की और युद्ध में मारे गए।
- राव चंदा की मृत्यु के बाद, उनके पुत्र कान्हा को अपने भाई राव रणमल से राजा बनने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
- अंततः रणमल सफल हुआ। यह वही रणमल है जिसने अपनी बहन हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा से करवाई।
राव जोधा (1438-1489 ई.)
- रणमल के पुत्र राव जोधा जोधपुर के पहले स्वतंत्र शासक बने। 1459 में उन्होंने जोधपुर नगर की नींव रखी।
- 1453 ई. में राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच ‘आवल-बावल’ संधि हुई, जिसके अनुसार राव जोधा को मेवाड़ के सिसोदिया शासकों से मंडोर प्राप्त हुआ। जोधपुर किलें का निर्माण भी शुरू किया।
- राव जोधा के पुत्र राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना की।
1453 ईस्वी में, आवल-बावल की संधि राव जोधा और महाराणा कुम्भा के बीच हुई। इसके तहत उन्हें मेवाड़ के सिसोदिया से मंडोर प्राप्त हुआ। मेहरानगढ़ किले का निर्माण शुरू किया। यह संधि मेवाड़ और मारवाड़ के सीमा विवाद को सुलझाने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए थी। इस संधि की मध्यस्थता हंसाबाई ने की थी। इस संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा निर्धारित की गई, जिसमें सोजत को केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में लिया गया। इस संधि में राव जोधा की बेटी शृंगार देवी की शादी कुम्भा के बेटे रायमल से हुई, जिससे गठजोड़ और मजबूत हुआ।
राव सातल (1489-1492)
- नागौर/पीपाड की युद्ध [कोषाणा के युद्ध] 1492 – राव सातल देव ने अजमेर के घुडले खान को हराया, जो सूबेदार मल्लू खान का सेनापति था।
- मारवाड़ के प्रसिद्ध ‘घुडला महोत्सव’ की शुरुआत इसी विजय की याद में की गई, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है।
राव मालदेव (1532-1562)
- राव मालदेव ने अपने शासनकाल में 52 युद्ध लड़े और 58 परगने को जीत लिया। उनका पहला सैन्य अभियान भाद्राजून (1532 ई) का था, जहाँ उन्होंने वीर सैन्धल को हराया और नियंत्रण स्थापित किया।
पाहोबा / साहेबा का युद्ध (1542 ईस्वी) :
- राव मालदेव ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से कुम्पा के नेतृत्व में बीकानेर की ओर एक बड़ी सेना भेजी। बीकानेर के राव जैतसी ने शेर शाह सूरि से मदद मांगी, लेकिन साहेबा में राव मालदेव की शक्तिशाली सेनाओं का सामना किया। हमला सहन न कर पाने के कारण जैतसी युद्ध में मारे गए, और मालदेव ने जांगल देश पर नियंत्रण स्थापित किया।
गिरी / सुमेल का युद्ध (1544 ईस्वी) :
यह युद्ध शेरशाह सूरी की अफगान सेनाओं और राव मालदेव राठौड़ द्वारा नेतृत्व किए गए राजपूतों के बीच लड़ी गई थी। राजपूत सेनाएं (12,000 राजपूत बनाम 80,000 अफगान) संख्या में बहुत कम होने के बावजूद, सेनापति जैता, कुम्पा और पचैन ने अद्वितीय साहस दिखाया।
- शेर शाह ने धोखाधड़ी का सहारा लिया, जाली पत्र भेजकर मालदेव के कैंप में अविश्वास फैलाया, जिससे राजा को जोधपुर की ओर पलायन करना पड़ा। हालांकि, जैता और कुम्पा ने अपनी निष्ठा साबित की और शेर शाह के कैंप पर तीव्र हमले किए, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। दोनों जैता और कुम्पा युद्ध में मारे गए, लेकिन उनके साहस ने शेर शाह को चकित कर दिया, और उसने प्रसिद्ध टिप्पणी की: “मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता।”
- हालाँकि शेर शाह विजयी हुआ, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके जनरल ख्वास खान ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया और अजमेर से लेकर माउंट आबू तक के मारवाड़ को आक्रमण कर लिया। राव मालदेव ने जुलाई 1555 ईस्वी तक इन क्षेत्रों को फिर से कब्जा कर लिया।
- इस युद्ध का महत्व : सुमेल की युद्ध राजपूत इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इससे पहले, पृथ्वीराज चौहान, हम्मीर चौहान, महाराणा कुम्भा, महाराणा संघा और राव मालदेव जैसे शासक राजपूत वंश की गौरव, स्वतंत्रता और शक्ति का प्रतीक थे। वे अपने साहस और आत्मनिर्भर शासन के लिए प्रसिद्ध थे।
- हालाँकि, सुमेल के युद्ध के बाद राजपूत शक्ति और स्वतंत्रता का युग समाप्त हो गया। इसके बाद का काल उपनिवेशीकरण का था, जिसमें राजपूत शासक बड़े साम्राज्यों जैसे मुगलों पर निर्भर हो गए। इस नए युग में वीरम, कल्याणमल, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, और अजित सिंह जैसे नेता शामिल थे, जिन्होंने अक्सर बड़े साम्राज्यों के सहयोगी या अधीनस्थ के रूप में कार्य किया, न कि स्वतंत्र रूप से शासन किया।
हरमाडा के युद्ध (1557 ईस्वी) :
- राव मालदेव और हाजी खान सूर की संयुक्त सेनाओं ने राणा उदयसिंह (मेवाड़) को हराया।
- पृष्ठभूमि : सुमेल के युद्ध (1544) में राव मालदेव को हराने के बाद, शेर शाह सूरि ने चित्तौड़ की ओर बढ़ने का प्रयास किया। राणा उदयसिंह, किले का बचाव करने में असमर्थ, बिना प्रतिरोध के समर्पण कर दिया और अपनी सीमाओं पर नियंत्रण बनाए रखा। सुमेल में हार के बावजूद, राव मालदेव ने 1555 तक अपने खोए हुए क्षेत्र फिर से प्राप्त कर लिए थे। 1556 में, हाजी खान सूर ने राणा उदयसिंह और राव सूरजन (बूंदी) के सहयोग से अजमेर और नागौर पर आक्रमण किया। राणा उदयसिंह के भुगतान की मांगों और एक नर्तकी (रंगरे) को लेकर विवाद हुआ, जिससे एक झगड़ा हुआ (संदर्भ: मंहुट नैनसी रा ख्यात)। हाजी खान ने राव मालदेव से संधि की, और दोनों ने मिलकर 1557 में मेवाड़ पर हमला किया। इस काल में राजपूतों और अफगानों के बीच बदलती संधियाँ देखी गईं।
मालदेव का योगदान :
- नागौर, सिवाणा, सोजत और अन्य नगरों को सुदृढ़ करके मारवाड़ को मजबूत किया।
- जोधपुर के रणिसर कोट, शहरपन्ह (शहर की दीवारें) का निर्माण किया और नागौर की किलाबंदी की मरम्मत की।
- अजमेर के तारागढ़ किले में जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए जलाशयों का निर्माण किया और पानी की आपूर्ति के लिए फारसी पहिए लगाए।
- उनकी रानी झाली स्वरूपदे ने स्वरूप सागर झील का निर्माण किया, जिसे बहुजी रो तालाब भी कहा जाता है।
- उन्होंने कला के संरक्षण की शुरुआत की, जिसमें चोखेलाव महल और उत्तराध्यान सूत्र में प्रारंभिक कार्य शामिल हैं।
मालदेव के हुमायूँ व शेरशाह के साथ संबंध
हुमायूं से संबंध – सतर्कता के साथ गठबंधन:
- 1541 में शेरशाह से हारकर भाग रहे हुमायूं को मारवाड़ के राव मालदेव ने 20,000 सैनिकों के साथ सैन्य और राजनीतिक सहायता दी।
- यह मदद केवल सहानुभूति नहीं थी, बल्कि मालदेव ने इसे हुमायूं को सत्ता में लौटाकर एक शक्तिशाली सहयोगी पाने और मारवाड़ की प्रतिष्ठा को राणा सांगा की तरह ऊँचा उठाने के अवसर के रूप में देखा।
- लेकिन 1542 में हुमायूं की देरी और शेरशाह की उत्तरी भारत में मज़बूत स्थिति के कारण यह गठबंधन असफल रहा।
- जोखिम को भाँपकर मालदेव ने समर्थन वापस ले लिया—कुछ इतिहासकार इसे विश्वासघात कहते हैं, पर यह वास्तव में एक रणनीतिक कदम था।
शेरशाह से संबंध – तनाव एवं रणनीतिक टकराव:
- मारवाड़ में राव मालदेव की बढ़ती ताकत शेरशाह के पश्चिमी विस्तार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई।
- हालाँकि मालदेव शुरू में तटस्थ रहे, लेकिन शेरशाह ने उन्हें खतरे के रूप में देखा और 1544 में मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी, जिसके परिणामस्वरूप सैमल (गिरी-सुमेल) का युद्ध हुआ।
- शेरशाह ने मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाई और मालदेव के शिविर में भ्रम फैलाने के लिए जाली पत्र भेजे। इस कारण मालदेव को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उनके सेनानायकों जैता और कूंपा ने अद्भुत वीरता दिखाई। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर शेरशाह ने कहा, “मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता”
समालोचनात्मक मूल्यांकन:
- आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थवाद: मालदेव के निर्णय शक्ति-संतुलन की व्यावहारिक वास्तविकताओं पर आधारित थे। हुमायूं से समर्थन वापसी विश्वासघात नहीं, बल्कि उदीयमान शेरशाह से टकराव टालने हेतु रणनीतिक विवेक था।
- दीर्घकालिक दृष्टिकोण की कमी: मालदेव कोई स्थायी विदेश नीति नहीं बना पाए। उनके असमंजस ने उनकी सौदेबाजी की शक्ति को कम किया और वे हुमायूं एवं शेरशाह दोनों से दूर हो गए।
- क्षेत्रीयता की प्राथमिकता, साम्राज्यिक दृष्टिकोण की उपेक्षा: मालदेव ने सम्राटों से गठबंधन की दीर्घकालिक रणनीति के बजाय क्षेत्रीय स्वायत्तता को प्राथमिकता दी—जिससे मारवाड़ का अखिल-भारतीय राजनीति में योगदान सीमित रह गया।
- आलोचनात्मक विवेचना : मालदेव ने सम्राटों से गठबंधन की दीर्घकालिक रणनीति के बजाय क्षेत्रीय स्वायत्तता को प्राथमिकता दी—जिससे मारवाड़ का अखिल-भारतीय राजनीति में योगदान सीमित रह गया।
मालदेव और हुमायूँ के संबंधों को समझते हुए यह कहा जा सकता है कि उनका व्यवहार कूटनीतिक और राजनीतिक विवेक से प्रेरित था। जबकि शुरुआत में उन्होंने हुमायूँ का समर्थन किया, बाद में शेर शाह के बढ़ते प्रभाव और बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के कारण उनका रुख बदल गया। यह निर्णय विश्वासघात नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और राज्यहितों की रक्षा करने के लिए लिया गया था।
राव मालदेव की व्यक्तित्व मूल्यांकन
- राव मालदेव एक बहुआयामी नेता थे, जो अपने सैन्य कौशल और प्रशासनिक दूरदृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। मारवाड़ का विस्तार, 52 युद्धों में विजय प्राप्त करने और 58 परगनों का अधिग्रहण, उनके साहस और रणनीतिक विशेषज्ञता को प्रदर्शित करता है। उनके कूटनीतिक कौशल का उदाहरण उनकी हुमायूं के साथ सतर्क बातचीत से मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा को नैतिक दायित्वों से अधिक प्राथमिकता दी। उन्हें फारसी इतिहासकारों द्वारा “हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक” के रूप में सराहा गया, और डॉ. भार्गव ने उन्हें “एक भगवान द्वारा उपहार में दिया गया सैनिक और कुशल कूटनीतिज्ञ” के रूप में वर्णित किया।
- मालदेव ने सुमेल की युद्ध में अद्वितीय साहस दिखाया, जहाँ उनके कमांडरों ने शेर शाह सूरि के खिलाफ अतुलनीय साहस दिखाया।
- मालदेव का किलाबंदी, जल प्रबंधन और अवसंरचना में योगदान उनके मजबूत और आत्मनिर्भर मारवाड़ के लिए दृष्टि का प्रतीक है। हालांकि, अपने सक्षम बेटे राम के बजाय चंद्रसेन को नियुक्त करने का उनका निर्णय, जो उनकी दूसरी रानी के प्रभाव में था, एक दुर्लभ निर्णय त्रुटि साबित हुआ, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। यही द्वैत मालदेव को एक निर्भीक योद्धा, दूरदर्शी शासक और कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में परिभाषित करता है, हालांकि वे कभी-कभी व्यक्तिगत प्रभावों से प्रभावित होते थे।
राव चंद्रसेन (1562-1565) :
- राव मालदेव, अपने बड़े बेटे राम से असंतुष्ट होकर, चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज नियुक्त किया।
- उनके छोटे बेटे, उदयसिंह को उनकी माँ, रानी स्वरूपदे (चंद्रसेन की माँ) द्वारा सिंहासन से वंचित कर दिया गया।
राम, उदयसिंह, और चंद्रसेन के बीच संघर्ष छिड़ गया, जिसमें चंद्रसेन विजयी हुए। - आखिरकार, राम सिंह ने अकबर के साथ शरण ली, जिसने 1570 में हुसैन कुली खान के नेतृत्व में सेना भेजकर मारवाड़ पर नियंत्रण स्थापित किया। अकबर ने विजय के बाद राम को मारवाड़ का शासक नियुक्त किया।
- नागौर दरबार (1570) :
- अकबर ने 1570 में राजपूत शासकों की वफादारी परखने के लिए नागौर दरबार का आयोजन किया।
- चंद्रसेन दरबार में जोधपुर प्राप्त करने की आशा लेकर पहुंचे। अकबर की अपने भाइयों, राम और उदयसिंह के प्रति झुकाव को देख चंद्रसेन दरबार से चले गए।
चंद्रसेन के व्यक्तित्व का मूल्यांकन
राव चंद्रसेन मुगल युग के दौरान राजस्थान के सबसे बहादुर और स्वतंत्र शासकों में से एक थे। अक्सर “मारवाड़ के भूले-बिसरे नायक” के रूप में संदर्भित, उनका योगदान ऐतिहासिक कथाओं में कम सराहा गया है। हालाँकि, डॉ. भार्गव के अनुसार, वह एक ऐसे नेता थे, जो अपनी मातृभूमि को मुगल शासन से मुक्त रखने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थे। अकबर की सेनाओं का सामना करने के लिए उनकी अटूट दृढ़ता और देशभक्ति की भावना उनके अविश्वसनीय संकल्प को प्रदर्शित करती है।
चंद्रसेन की सैन्य रणनीति में उनकी रणनीतिक सूझबूझ स्पष्ट थी। वह पहले राजपूत राजा थे जिन्होंने पारंपरिक किलों की तुलना में जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों की रक्षा को प्राथमिकता दी। छापामार युद्ध को अपनाकर उन्होंने अन्य शासकों से खुद को अलग कर लिया और यह रणनीति बाद में महाराणा प्रताप द्वारा अपनाई गई। यह दृष्टिकोण उनकी अनुकूलन क्षमता, संसाधनशीलता और दूरदर्शिता को दर्शाता है; गुण जो उन्हें सीमित संसाधनों के बावजूद शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती देने की अनुमति देते थे।
अकबर के सामने झुकने से इंकार करने और 19 वर्षों तक स्वतंत्रता के लिए उनकी अनवरत युद्ध ने उनके गर्व और बहादुरी का प्रतीक बना दिया। उन्हें महाराणा प्रताप के लिए “मार्गदर्शक” के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने उन्हें मुगल अत्याचार के खिलाफ युद्ध में मार्गदर्शन किया। इस कारण, चंद्रसेन को अक्सर “मारवाड़ का प्रताप” कहा जाता है। वह विद्रोह का प्रतीक बन गए, अपने लोगों की स्वतंत्रता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसित। एक कवि ने एक बार कहा था, “अनडगिया तुरी उजला… चंद्रसेन प्रवित।” यह दर्शाता है कि चंद्रसेन और महाराणा प्रताप, दोनों ने अपने साझा प्रतिरोध में, मुगल उत्पीड़न के खिलाफ अडिग रहे, कभी भी अपने सम्मान से समझौता नहीं किया।
चंद्रसेन का व्यक्तित्व उनके साहस, नेतृत्व और आत्म-बलिदान से परिभाषित था। प्रताप की तरह, वह केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी भी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता और गर्व के मूल्य को समझा। उनकी अटल भावना, हार स्वीकार करने से इनकार, और अपने लोगों की स्वायत्तता को प्राथमिकता देना उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में परिभाषित करता है जिन्होंने संघर्ष के मार्ग को चुना न कि समर्पण को।
राजा उदय सिंह (मोटा राजा) (1583-1595)
- 1583 में, अकबर ने उदय सिंह को जोधपुर (मारवाड़) का शासक नियुक्त किया, जिससे वे मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले पहले मारवाड़ शासक बने।
- मुगल-मारवाड़ वैवाहिक संधि – 1587 में, उदय सिंह ने अपनी बेटी, जोधा बाई (जगत गुसाईं), का विवाह जहांगीर से करवाया।
- जोधा बाई, जिन्हें मनमती या मानीबाई भी कहा जाता था, खुर्रम (शाहजहाँ) की माता थीं, जो जहांगीर के पुत्र।
- 1609 में, उदय सिंह के पुत्र, किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की, जिससे यह राठौड़ शक्ति का तीसरा केंद्र बन गया।
महाराजा जसवंत सिंह (1638-1678)
शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध (1658-59 ईस्वी) के दौरान, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने धरमत के युद्ध (अप्रैल 1658 ईस्वी) में औरंगजेब के खिलाफ दारा शिकोह का समर्थन किया। हालांकि, कासिम खान के विश्वासघात के कारण दारा को हार का सामना करना पड़ा, जिससे जसवंत सिंह और उनके सहयोगियों को जोधपुर वापस लौटना पड़ा।
जोधपुर लौटने पर, उनकी पत्नी, महारानी जसवंत दे, जिन्हें “उदयपुरी रानी” कहा जाता था, ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने संदेश भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या युद्धक्षेत्र में अपने जीवन का बलिदान देते हैं। उन्होंने घोषणा की कि पराजित राजा वापस नहीं आ सकता, और उन्होंने सती की तैयारी शुरू कर दी। अंततः, रानी माँ द्वारा मनाए जाने और जसवंत सिंह द्वारा हार का बदला लेने के वादे पर, किले के द्वार खोल दिए गए।
कला, साहित्य और वास्तुशिल्प योगदान
- कला – उनके शासनकाल के दौरान जोधपुर स्कूल की चित्रकला कृष्ण कथाओं और मुगल कला से प्रभावित हुई। कुछ प्रसिद्ध चित्रकार थे – करीम, नाथो नारायण, नागो आदि।
- साहित्यिक योगदान
- महाराजा जसवंत सिंह ज्ञान के संरक्षक और स्वयं एक विद्वान थे।
उन्होंने “भाषा-भूषण” जैसी महत्वपूर्ण कृतियाँ लिखीं, जो अलंकार और सौंदर्यशास्त्र पर आधारित हैं, और “अपरोक्ष सिद्धांत,” “अनुभव प्रकाश,” “आनंद विलास,” “सिद्धांत सार,” और “सिद्धांत बोध” जैसे दार्शनिक ग्रंथ लिखे। - जसवंत सिंह ने श्रीमद भागवत पर एक टीका लिखी और संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी में “चंद्रप्रबोध” नाम से अनुवाद किया।
- उनके दरबार में सुरत मिश्रा, दलपति मिश्रा, नरहरिदास बारहठ, नवीन कवि, और बनारसीदास जैसे प्रसिद्ध विद्वान थे। उनके दीवान और चारण, मुहनोत नैणसी, ने राजस्थान का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ “नैणसी री ख्यात” और गजेटियर “मारवाड़ रा परगना री विगत” लिखा।
- महाराजा जसवंत सिंह ज्ञान के संरक्षक और स्वयं एक विद्वान थे।
वास्तुकला में योगदान
- महाराजा जसवंत सिंह ने कई जलाशयों, उद्यानों और उत्कृष्ट इमारतों का निर्माण करवाया।
- उन्होंने औरंगाबाद में “जसवंतपुरा” की स्थापना की और आगरा के पास मुगल-राजपूत वास्तुकला शैली में “कचहरी भवन” बनवाया।
- उनकी रानी, रानी अतीरंगदे, ने “जन सागर तालाब” का निर्माण करवाया, जिसे “शेखावतजी का तालाब” भी कहा जाता है।
- एक अन्य रानी, रानी जसवंते, ने “राई का बाग,” “उसका कोट,” और “कल्याण सागर तालाब” का निर्माण करवाया, जो “राता नाडा” नामक क्षेत्र में स्थित है।
- “रूपा बावड़ी” नामक एक बावड़ी मेडती गेट के भीतर महाराजा की देखभालकर्ता, रूपा धाय के सम्मान में बनवाई गई थी।
महाराजा अजीत सिंह (1679-1724)
- जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, उनके कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं थे, लेकिन उनकी दो पत्नियाँ गर्भवती थीं। बाद में अजीत सिंह का जन्म हुआ। हालाँकि, औरंगजेब ने इंद्र सिंह को शासक नियुक्त कर दिया।
- दुर्गादास ने औरंगजेब से अजीत सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने की मांग की, लेकिन औरंगजेब ने अजीत सिंह के इस्लाम में धर्मांतरण की शर्त रखी, जिसे दुर्गादास ने अस्वीकार कर दिया।
- अगले 20 वर्षों तक मारवाड़ सीधे मुगल शासन के अधीन रहा, जबकि दुर्गादास संघर्ष करते रहे।
- 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, दुर्गादास ने मौके का फायदा उठाया और अजीत सिंह ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया।
वास्तुकला में योगदान :
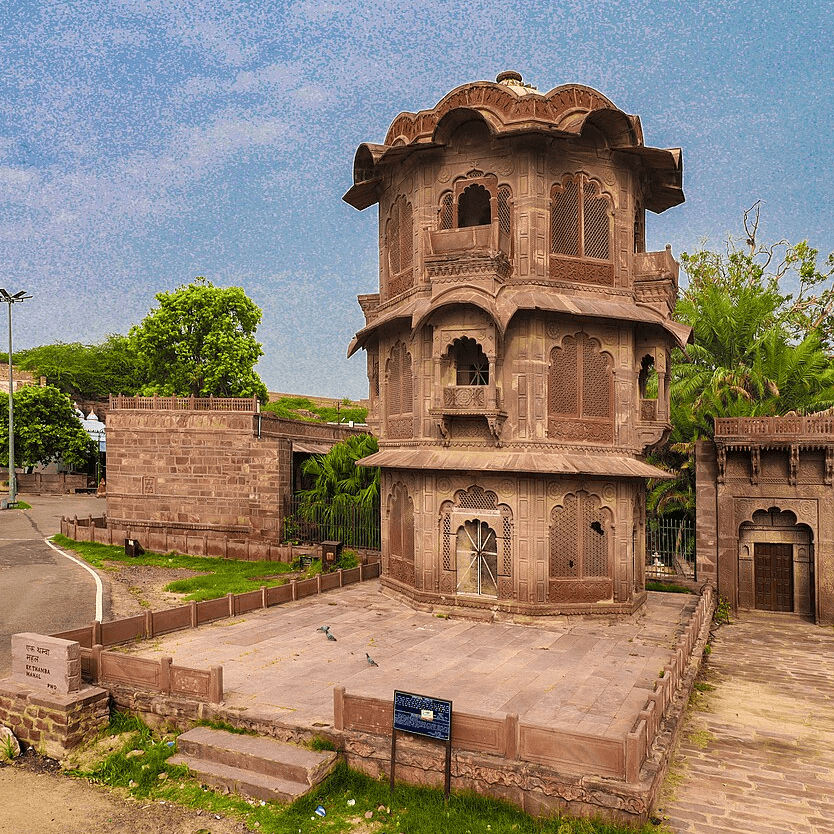
महाराजा अजीत सिंह ने अपनी निर्माण कृतियों में हिंदू-मुगल वास्तुकला शैलियों का कुशलता से मिश्रण किया।
- एक थंबा महल: उन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में मंडोर में एक सात फुट ऊंचे मंच पर तीन मंजिला छतरी (देवल) का निर्माण करवाया। इसे “एक थंबा महल” भी कहा जाता है और यह हिंदू-मुस्लिम वास्तुकला के मिश्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- फतेह महल और दौलतखाना राज महल: जोधपुर किले में बनाए गए।
- मंडोर में जसवंत सिंह की स्मृति में एक स्मारक।
- जोधपुर शहर में घनश्यामजी मंदिर और मूलनायक मंदिर।
- रानी रणावती ने बावड़ी (झालरा) के पास शिखरचंद मंदिर बनवाया।
कला और साहित्य में योगदान :
महाराजा अजीत सिंह एक धर्मपरायण शासक थे, जिन्होंने साहित्य और कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ‘गुणसागर,’ ‘दुर्गापथ भाषा,’ ‘निर्वाण दूहा,’ ‘अजीत सिंह रा कह्या दोहा,’ और ‘गज उद्धार’ जैसी रचनाएँ कीं, जो भागवत पुराण पर आधारित थीं। उनके भक्ति गीत जैसे ‘दुहा श्री ठाकुरा रा’ और ‘महाराजा अजीत सिंह रा गीत’ सराहे गए। उनके शासनकाल में जोधपुर चित्रकला शैली पर सामंती संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट था।
अजीत सिंह ने जगजीवन भट्ट, जिन्होंने ‘अजीतोदय’ लिखा, पंडित बालकृष्ण शर्मा, जिन्होंने संस्कृत ‘अजीत चरित्र’ की रचना की, और पंडित श्यामराम, जिन्होंने ‘ब्रह्मांड वर्णन’ की रचना की, जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। ये योगदान मारवाड़ की सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
व्यक्तित्व मूल्यांकन
महाराजा अजीत सिंह ने उल्लेखनीय प्रशासनिक कौशल और वास्तुकला में गहरी रुचि दिखाई। उनके शासनकाल को हिंदू और मुगल वास्तुकला शैलियों के सम्मिश्रण के लिए याद किया जाता है, जो फतेह महल, दौलतखाना राज महल, और मंडोर में “एक थंबा महल” जैसी उत्कृष्ट कृतियों में दिखाई देते हैं। मंदिर निर्माण और शहरी विकास में उनके योगदान से उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण की प्रतिबद्धता भी स्पष्ट होती है।
हालांकि, उनका व्यक्तित्व कई कमजोरियों से ग्रस्त था। इतिहासकारों जैसे डॉ. गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उन्हें घमंडी, कान का कच्चा (आसानी से प्रभावित होने वाला) और प्रतिशोधी बताया है। मुगल आक्रमणों के खिलाफ मारवाड़ की प्रभावी रक्षा करने में उनकी अक्षमता और प्रतिकूल शर्तों को स्वीकार करने की तत्परता ने उनकी साहसिकता और मानसिक दृढ़ता की कमी को उजागर किया। इसके अलावा, उनका सबसे बड़ा दोष उनके वफादार समर्थक दुर्गादास राठौड़ के प्रति कृतघ्नता थी, जिन्हें उन्होंने दुर्भावनापूर्ण सलाहकारों के प्रभाव में निर्वासित कर दिया। यह विश्वासघात उनके शासन पर एक स्थायी दाग लगा गया, जो अन्यथा उल्लेखनीय था।
वीर दुर्गादास राठौड़

वीर दुर्गादास, वफादारी और वीरता के प्रतीक, का जन्म 13 अगस्त 1638 को सालवा गांव में हुआ था। उनके पिता आसकरण महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। दुर्गादास ने जसवंत सिंह की सेना में सेवा की और महाराजा की मृत्यु के बाद मारवाड़ के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने जीवन को अजीत सिंह, जोधपुर के वैध उत्तराधिकारी, को मुगल सम्राट औरंगजेब से सुरक्षित रखने के लिए समर्पित कर दिया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक राठौड़- सिसोदिया गठबंधन का नेतृत्व किया।
उनकी सहिष्णुता और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण तब देखा गया जब उन्होंने, एक कट्टर हिंदू होने के बावजूद, राजकुमार अकबर के बच्चों बुलंद अख्तर और सफियातुन्निसा को उचित इस्लामी शिक्षा दिलाने का प्रबंध किया। उनके सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के इस कार्य ने उनके व्यक्तिगत या धार्मिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाया।हालांकि, जीवन के अंतिम समय में अजीत सिंह के साथ मतभेद के कारण, दुर्गादास मेवाड़ चले गए, जहां उन्होंने स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत किया। उनका निधन 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में हुआ। दुर्गादास मारवाड़ में अपनी वीरता और वफादारी के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने हुए हैं, जिन्हें “माँ रैद ऐसा पूत जन, जैसा दुर्गादास” कहावत के साथ याद किया जाता है। इतिहासकार जेम्स टॉड ने उन्हें “राठौड़ों के यूलिसिस” के रूप में संदर्भित किया।
महाराजा अभय सिंह (1724-1749)
- महाराजा अभय सिंह को कविता और साहित्य से गहरा लगाव था। उनके संरक्षण में चारण कवि कर्णीदान ने सूरजप्रकाश की रचना की। इसके अलावा, सरबुलंद खान के साथ उनकी युद्ध से प्रेरित होकर, उन्होंने एक छंदबद्ध रचना विरुद्ध श्रृंगार (जिसे बिद्रा श्रृंगार भी कहा जाता है) की रचना की। उनकी इस कृति से प्रसन्न होकर, महाराजा ने उन्हें अलावास गाँव लाकपासव के रूप में प्रदान किया, कविराज की उपाधि दी, और मंडोर से उन्हें हाथी पर बिठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर उनके घर तक छोड़कर असाधारण सम्मान दिया।
- उनके संरक्षण में कई अन्य कवि, जैसे कि रसचंद, सेवक, प्रयाग, मैदास, सावंतसिंह और पृथ्वीराज, भी फले-फूले। इनमें से, संडू वंश के चारण कवि पृथ्वीराज ने अभय विलास नामक एक लोकभाषा में साहित्यिक रचना की।
- अन्य साहित्यिक कृतियाँ:
- अभयोदय (संस्कृत में) – भट्ट जगजीवन द्वारा।
- राजरूपक – रतनू वीरभान द्वारा।
- कवित्त श्री माता रा – रसपुंज द्वारा।
चिपको आंदोलन

खेजड़ी पेड़ की रक्षा के लिए पहला चिपको आंदोलन 28 अगस्त 1730 को अमृता देवी के बलिदान के साथ शुरू हुआ। अमृता देवी, जो रामोजी विश्नोई की पत्नी थीं, ने जोधपुर के खेजड़ली गाँव में 363 अन्य लोगों के साथ अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशमी के पवित्र दिन पर खेजड़ी के पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगाया। गिरीधर दास, स्थानीय अधिकारी, के आदेश पर इस आंदोलन के दौरान 363 लोगों की हत्या कर दी गई। इस पर्यावरणीय आंदोलन की उपलक्ष्य में, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार स्थापित किया, और राजस्थान सरकार ने अमृता देवी विश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार की शुरुआत की।
महाराजा मान सिंह (1803-1843)
- महाराजा मान सिंह का शासन जोधपुर पेंटिंग स्कूल के सुनहरे युग के रूप में माना जाता है।
- इस अवधि में कलाकारों ने शिव पुराण, दुर्गा पुराण, अजीत सिंह के शिकार अभियानों और नाथ चरित्र की कहानियों को चित्रित किया।
- इस युग के प्रमुख चित्रकारों में दाना भाटी, अमरदास भाटी, और शिवदास शामिल थे, जिनके योगदानों ने जोधपुर की कलात्मक धरोहर को समृद्ध किया।
कला:
- The reign of Maharaja Man Singh is considered the golden era of the Jodhpur School of Painting.
- During this period, artists created exquisite works depicting scenes from the Shiv Puran, Durga Puran, Ajit Singh hunting expeditions, and narratives of Nath Charitra.
- The prominent painters of this era included Dana Bhati, Amardas Bhati, and Shivdas, whose contributions significantly enriched the artistic heritage of Jodhpur.
साहित्य:
- उनकी कला और साहित्य के प्रति रुचि के कारण जोधपुर किले में ‘पुस्तक प्रकाश’ पुस्तकालय की स्थापना की गई, जहाँ उन्होंने पुस्तकें और चित्र संग्रहित किए।
- उन्होंने प्रेम, भक्ति, और आध्यात्मिकता के विषयों पर कविता लिखी, और राजस्थानी में श्रीमद्भागवतम पर टिप्पणी की। वे ‘चौरासी पदार्थ नामावली,’ ‘कृष्ण विलास’ जैसे कार्यों के लेखक भी थे, जो श्रीमद्भागवतम का काव्यात्मक रूपांतर था।
- महाराजा की भाटियानी रानी, रानी प्रताप कुंवरी, एक कवयित्री और विदुषी थीं। उनके प्रमुख कार्यों में ‘ज्ञान सागर,’ ‘प्रताप पच्चीसी,’ ‘प्रेम सागर,’ और ‘रघुबर स्नेहलिला’ शामिल हैं।
धार्मिक आस्था:
- वे नाथ सम्प्रदाय के प्रति गहरे समर्पित थे और इसके सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए कई रचनाएँ कीं, जैसे ‘जलंधर नाथ जी रो चरित्र’ और ‘नाथचरित्र’। नाथ परंपरा की मान्यता में, उन्होंने जोधपुर में महामंदिर की स्थापना की, जो इस सम्प्रदाय की महत्वपूर्ण शाखा बन गया।
महाराजा सर तखत सिंह (1843-1873)
- महाराजा तक़त सिंह के शासनकाल में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएँ और सार्वजनिक कल्याण सुधार हुए। 1857 के विद्रोह के दौरान उनका समय था, और उन्होंने ब्रिटिशों का पूरा समर्थन किया।
- 1857 का विद्रोह:
- महाराजा तक़त सिंह ने अपने सैनिकों को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा।
- 8 सितंबर 1857 को उनकी कमांडर ओनैद सिंह ‘बिथोड़ा की लड़ाई’ में मारे गए।
- उनके समर्थन की मान्यता में, ब्रिटिशों ने 1862 में जोधपुर दरबार को गोद लेने का अधिकार दिया।
- सार्वजनिक कल्याण कार्य:
- उन्होंने मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना के लिए ₹1 लाख का योगदान दिया।
- उन्होंने सती प्रथा, संन्यासियों के समाधि प्रथा, और राजपूतों में कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाया।
- जोधपुर में ‘मारवाड़ राज्य प्रेस’ की स्थापना की, जिसने “मरुधर भीत” (बाद में मारवाड़ गजट) प्रकाशित किया।
- दर्बार स्कूल की स्थापना की।
- रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की।
- कला, साहित्य और विद्वतापूर्ण प्रयास:
- उनके समय में कला में सोने के रंगों का अधिक प्रयोग और सजावट बढ़ी, और कंपनी की शैली का प्रभाव देखा गया।
- कवि शेष ने तख़्त विलास’ नामक चंपू काव्य रचा।
- रानी प्रताप कुनवारी ने ‘हरिपदावली’ और ‘रामपदावली’ लिखी, जो बाद में ‘प्रतापकुनवारी-पद रत्नावली’ के नाम से प्रकाशित हुईं।
- निर्माण कार्य:
- जोधपुर किले में चामुंडा माता मंदिर का नवीनीकरण किया।
- मंडोर में मान सिंह की छतरी और तक़त सागर का निर्माण कराया।
- मेहरानगढ़ किले में श्रृंगार चौकी और कयलाना पहाड़ियों में बिजोलाई महल का निर्माण कराया।
महाराजा सर जसवंत सिंह II (1873-1895)
उन्होंने 1883 में स्वामी दयानंद का स्वागत किया, और आर्य समाज के सिद्धांतों का समर्थन किया। उन्होंने आर्य समाज को प्रोत्साहित किया और शिक्षा और सुधार को बढ़ावा दिया।
- प्रशासनिक सुधार:
- अप्रैल 1873 में महकमाखास की स्थापना की, ताकि प्रशासनिक कार्यों में दक्षता सुनिश्चित हो।
- 1882 में ‘अदालत पटदर्शन’ और ‘कोर्ट-सरदारन’ जैसे नए न्यायालयों की स्थापना की।
- साहित्यिक योगदान:
- दरबार कवि बारहठ मुरारीदान ने ‘जसवंत रसो भूषण’ नामक काव्य रचना की।
- महाराजा ने मुरारीदान को ‘कवि राजा’ का खिताब और लाख पासव दिया।
- 1888 में मारवाड़ के इतिहास को दस्तावेजित करने के लिए ‘तवारीख का महकमा’ की स्थापना की।
- सैन्य विकास:
- 1889 में 600 सैनिकों के साथ ‘सरदार रिसाला’ (घुड़सवार पलटन) का गठन किया और 1891 में इसका विस्तार किया।
- सामाजिक कार्य: 1885 में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया।
महाराजा सर सरदार सिंह (1895-1911)
महाराजा सदार सिंह ने अपने पिता, जसवंत सिंह II, की याद में जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की तलहटी में जसवंत थड़ा का निर्माण कराया। इसे राजस्थान का ‘ताज महल’ कहा जाता है, यह संगमरमर का स्मारक वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक है।
- महत्वपूर्ण योगदान:
- जसवंत महिला अस्पताल (मातृ अस्पताल) की स्थापना की।
- एल्गिन राजपूत स्कूल (विक्टोरियाई वायसरॉय, लॉर्ड एल्गिन के जोधपुर आगमन के दौरान) की स्थापना की।
- 1910 में ‘एडवर्ड रिलीफ फंड’ की स्थापना की, जिसमें जोधपुर शहर के गरीब निवासियों को पेंशन देने के लिए ₹29,000 वार्षिक आवंटित किए गए।
- चीन में बॉक्सर्स विद्रोह: महाराजा सदार सिंह ने ब्रिटिशों की मदद करने के लिए मारवाड़ी सेना भेजी। सम्मान के रूप में “चाइना 1900” को मारवाड़ ध्वज पर अंकित किया गया।
महाराजा सर उम्मेद सिंह (1918-1947)
- महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल राहत प्रयासों के हिस्से के रूप में उम्मेद पैलेस, जिसे छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, के निर्माण का आदेश दिया था।
महाराजा सर हनुवंत सिंह (1947-47)
- महाराजा उम्मेद सिंह की मृत्यु के बाद, उनके पुत्र हनवंत सिंह को 21 जून 1947 को जोधपुर के महाराजा के रूप में सिंहासनारूढ़ किया गया। उनके शासनकाल के दौरान ही भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की।
- महाराजा हनवंत सिंह ने प्रारंभ में जोधपुर को पाकिस्तान के साथ संरेखित करने में रुचि दिखाई और यहाँ तक कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए, उस समय के बीकानेर के महाराजा के साथ, पाकिस्तान की यात्रा भी की।
- हालांकि, वी.पी. मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन और सरदार वल्लभभाई पटेल के निरंतर प्रयासों और समझाने के बाद, महाराजा हनवंत सिंह अनिच्छापूर्वक भारतीय संघ में विलय करने के लिए सहमत हो गए।
बीकानेर के राठौड

15वीं शताब्दी में, जब राव बीका, राव जोधा के पुत्र, बीकानेर पहुंचे, उस समय यह क्षेत्र सात जाट कबीलों द्वारा नियंत्रित था, जिनके नाम थे: सीहाग, ढाका, पूनिया, गोडारा, सारण, बेनीवाल, जोहिया और कस्वां। राव बीका ने जाट कबीले के बीच मौजूद आपसी प्रतिद्वंद्विता का उपयोग कर अपने राज्य के लिए जगह बनाई। जेम्स टॉड के अनुसार, जिस स्थान को बीका ने अपनी राजधानी के लिए चुना, वह नेहरा जाट का पैतृक अधिकार था, जो केवल इस शर्त पर इसे छोड़ने के लिए तैयार हुआ कि उसका नाम हमेशा के लिए इस जगह के साथ जोड़ा जाएगा। नायरा, या नेरा, उस मालिक का नाम था, जिसे बीका ने अपने नाम के साथ जोड़ दिया, इस प्रकार भविष्य की राजधानी का नाम ‘बीकानेर’ बना।
राव बीका (1465-1504)
- राव जोधा द्वारा राव सातल देव को राजा नियुक्त किए जाने के कारण, बीका अपने चाचा कान्धल और छोटे भाई बीदा के साथ जोधपुर छोड़कर चले गए।
- 1465 ईस्वी में, करणी माता के आशीर्वाद से, बीका ने जांगलदेश क्षेत्र में राठौड़ राज्य की स्थापना की।
- 1488 ईस्वी (वैशाख शुक्ल द्वितीया, संवत 1545) में, बीका ने आधिकारिक रूप से बीकानेर शहर की स्थापना की।
राव लूणकरण (1505-26)
- उन्होंने 1526 ईस्वी में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अबी मीरा के साथ लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की।
- बीठा सूजा ने अपनी पुस्तक ‘राव जैतसी रो छंद’ में उन्हें ‘कलियुग का कर्ण’ कहा है। जयसोम ने अपनी पुस्तक ‘कर्मचंद्रवंशोत्कीर्तनक काव्यम’ में भी उनकी उदारता की तुलना कर्ण से की है। उन्होंने ‘लूणकरणसर झील’ का निर्माण करवाया।
राव जैत सिंह (1526-42)
- 1534 ईस्वी में, बीकानेर के राव जैतसी ने काबुल के मुगल शासक और हुमायूं के भाई कामरान को हराया। इस विजय का वर्णन कवि बीठू सूजा द्वारा लिखित ‘राव जैतसी रो छंद’ में किया गया है।
- पाहेबा / साहेबा युद्ध (1541-42 ईस्वी): यह युद्ध बीकानेर के राव जैतसी और मारवाड़ के मालदेव के बीच हुआ। इस युद्ध में राव जैतसी मारे गए और मालदेव द्वारा बीकानेर के प्रशासक के रूप में कम्पा को नियुक्त किया गया।
- परिणाम:
- राव जैतसी के पुत्र कल्याणमल ने शेर शाह सूरी के साथ शरण ली, जिससे शेर शाह को मारवाड़ पर हमला करने का बहाना मिल गया।
- यह अंततः 1544 ईस्वी में सुमेल के युद्ध की ओर ले गया, जिसमें शेर शाह ने मालदेव को हराकर जोधपुर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया।
राव कल्याण सिंह (1542-71)
- मालदेव की हार के बाद वे बीकानेर के शासक बने।
- वह पहले राठौड़ थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की।
पृथ्वीराज राठौड़

बीकानेर के राव कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ एक बहादुर योद्धा और कुशल कवि थे। राजस्थानी साहित्य में “पीथल” के नाम से जाने जाने वाले पृथ्वीराज संस्कृत और डिंगल के विद्वान थे। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ “वेली कृष्ण रुक्मणी री” अत्यधिक सम्मानित है और इसे दुरसा आढ़ा ने “पांचवां वेद” कहा है। अन्य प्रमुख कृतियों में “दशम भागवत रा दुहा”, “ठाकुर जी रा दुहा” और “गंगा लहरी” शामिल हैं। वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्हें गागरोन का किला दिया गया था। कर्नल टॉड और एल.पी. टेसिटोरी ने उन्हें महान योद्धा और कवि के रूप में सराहा, उन्हें “डिंगल का नायक” कहा।
राजा राय सिंह I (1571-1611)
वास्तुकला उपलब्धियां:
- मंत्री करमचंद की देखरेख में 1589-1594 के बीच जूनागढ़ किले (पूर्व में चिंतामणि किला) का निर्माण किया।
- किले के भीतर राय सिंह प्रशस्ति अंकित की।
कला और साहित्य विकास:
- लिखित कार्य जैसे राय सिंह महोत्सव (चिकित्सा से संबंधित)
वैधक वंशावली, बाल बोधिनी, और ज्योतिष रत्नमाला पर टिप्पणी। - जयसोम द्वारा लिखित करमचंद वंशोत्कीर्तनकाव्य में ‘राजेन्द्र’ के रूप में प्रशंसा की गई।
- बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत की, जिसमें सबसे पुराना ज्ञात पांडुलिपि भागवत पुराण है, जो उनके शासनकाल में बनाई गई।
- मुगल प्रभाव वाले कलाकारों जैसे उस्ता अली रजा, उस्ता हमीद रुकनुद्दीन को क्षेत्र की कलात्मक परंपराओं को समृद्ध करने के लिए आमंत्रित किया।
अकाल राहत प्रयास:
- अपने शासन के दौरान गंभीर अकाल का सामना करते हुए, खाद्य वितरण के लिए सदाव्रत खोले और जानवरों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था की।
- इतिहासकार देवी प्रसाद ने उनकी उदारता और करुणा के लिए उन्हें ‘राजपूताना के कर्ण’ के रूप में सराहा।
राव कर्ण सिंह जंगलपत बादशाह (1631-67)
- घटना – मतीरे-री-राड (तरबूज विवाद)
महाराजा राव अनुप सिंह (1669-1698)
- औरंगज़ेब द्वारा ‘महाराजा’ की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति।
- 1672 में सालेहर में, 1675 में बीजापुर में, और 1687 में गोलकुंडा की घेराबंदी में दक्कन अभियान में भाग लिया।
- 1677-1678 में औरंगाबाद के प्रशासक रहे।
योगदान और उपलब्धियां:
साहित्यिक योगदान
- महाराजा अनुप सिंह का शासन बीकानेर में “साहित्य का स्वर्ण युग” माना जाता है। एक अत्यंत विद्वान और ज्ञान के संरक्षक के रूप में, उन्होंने संस्कृत में उल्लेखनीय कार्यों जैसे ‘अनुप विवेक’ (तंत्र शास्त्र), ‘कामप्रबोध’ (काम शास्त्र), ‘श्रद्धाप्रयोग चिंतामणि’ और गीत गोविंद पर ‘अनुपोदय टीका’ की रचना की।
- उन्होंने अनुप संस्कृत पुस्तकालय की स्थापना की, जहाँ उन्होंने दक्षिण भारत से प्राप्त कई दुर्लभ पांडुलिपियों और साहित्यिक खजानों को संरक्षित किया।
- महाराजा अनुप सिंह को विद्वानों के समर्थन के लिए “विद्वानों के उत्पत्ति कारक” की उपाधि दी गई। उनके दरबार में भव भट्ट, अनंत भट्ट, मणिराम, वैद्यनाथ जैसे प्रमुख विद्वान सुशोभित थे, जिन्होंने संस्कृत साहित्य को ‘ज्योत्पत्तिसार’ (ज्योतिष), ‘अनुप व्यवहार सागर’ (ज्योतिष), ‘अनुप विलास,’ ‘धर्मांबुधि’ (धर्म शास्त्र), और ‘तीर्थरत्नाकर’ जैसे कार्यों से समृद्ध किया।
- देशीय साहित्य
अनूप सिंह जी को भाषाओं में गहरी रुचि थी, इसलिए उन्होंने कई पुस्तकों का संस्कृत और राजस्थानी में अनुवाद कराया। इन पुस्तकों में ‘सुकसारिका’ (72 कहानियों का संग्रह) को राजस्थानी और संस्कृत में अनुवादित किया गया, और श्रीधर की भगवद गीता पर टीका का मारवाड़ी में अनुवाद करवाया, जो उनके देशीय साहित्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है।
संगीत में योगदान
- महाराजा अनुप सिंह संगीत के बड़े प्रेमी थे। उनके दरबारी संगीतकार भव भट्ट ने ‘संगीतानुपंकुश,’ ‘अनुपसंगीतविलास,’ ‘अनुपसंगीतरत्नाकर,’ और ‘नष्टोद्दिशत प्रबोध कंठोपद टीका’ जैसे कई संगीतशास्त्रीय ग्रंथों की रचना की।
- ये कार्य उनके शास्त्रीय भारतीय संगीत और उसके सैद्धांतिक आधारों में गहरे जुड़ाव को उजागर करते हैं।
कलात्मक विकास
- महाराजा अनुप सिंह का शासन बीकानेर पेंटिंग के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उनके शासन में दक्षिण भारतीय शैलियों का प्रभाव प्रमुख हो गया, और मथेरनण और उस्ता कलाकारों ने पारंपरिक बीकानेर कला रूप को नवाचार दिया।
महाराजा राव सूरत सिंह (1787-1828)
- 9 मार्च 1818 को सहायक संधि के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संरक्षण में आए।
- उनका शासनकाल “अंग्रेजों के उदय” का प्रतीक था। वह अपनी वीरता, सद्गुण और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। वह अन्याय को सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी कि वह “कान के कच्चे” राजा थे।
महाराजा राव रतन सिंह (1828-51)
- रतन सिंह ने महिला भ्रूण हत्या रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने राजपूत शासकों से गया में अपनी बेटियों को न मारने की शपथ दिलवाई।
- उनके पुत्र, महाराजा सरदार सिंह ने 1854 ई. में अपने राज्य में सती प्रथा और जीवित दफनाने की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा पत्र जारी किया।
- 1857 के विद्रोह के दौरान, सरदार सिंह ने ब्रिटिशों का समर्थन किया और क्रांतिकारियों को सक्रिय रूप से दबाया।
महाराजा राव डूंगर सिंह (1872-1887)
- राजस्थान में बिजली लाने वाले पहले व्यक्ति।
- उन्होंने पुलिस बल, डाक प्रणाली, एक अस्पताल और एक आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की।
- उनके शासनकाल में प्रसिद्ध ‘बीकानेरी भुजिया’ की शुरुआत हुई। उन्होंने बीकानेर किले का पुनर्निर्माण कराया।
महाराजा सर राव गंगा सिंह (1887-1943)
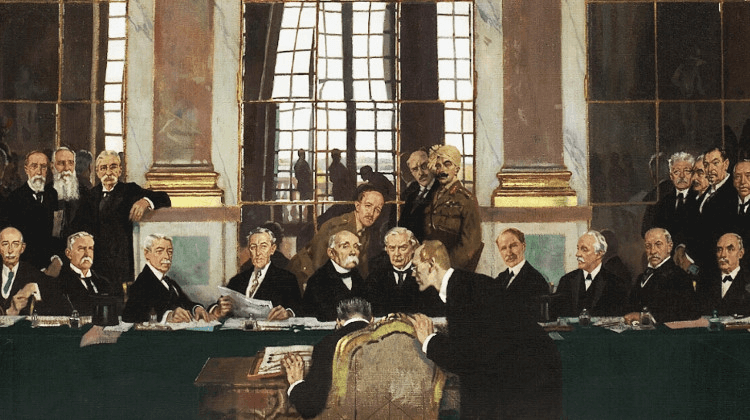
- बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, जिन्हें अक्सर “आधुनिक बीकानेर के वास्तुकार” और “आधुनिक भारत के भागीरथ” के रूप में सराहा जाता है, ने निम्नलिखित परिवर्तनीय पहल की:
राजनीतिक योगदान:
- 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, जो राजस्थान में एक विधायी निकाय की दिशा में पहला कदम था।
- नगरपालिकाओं के चुनावों के साथ आंशिक आंतरिक लोकतंत्र की शुरुआत की।
- उनकी “रोम नोट” ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की वकालत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- उन्होंने 1921 में नरेन्द्र मंडल (राजाओं की सभा) के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके पहले अध्यक्ष (1921-1925) के रूप में कार्य किया।
- 1927 में बटलर कमेटी के समक्ष रियासतों की स्वायत्तता की वकालत की।
- तीन गोलमेज सम्मेलनों (1930, 1931, 1932) और लीग ऑफ नेशन्स (5वें सत्र) में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान इंपीरियल वॉर कैबिनेट में भाग लिया, जिसमें वे एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि थे।
- चीन के बॉक्सर विद्रोह में ब्रिटिशों की सहायता की और चीन युद्ध पदक प्राप्त किया।
रोम नोट (1917)
महाराजा गंगा सिंह ने 15 मई 1917 को रोम में एक ऐतिहासिक नोट लिखा, जिसे “रोम नोट” के रूप में प्रसिद्ध किया गया। यह नोट ऑस्टिन चेम्बरलेन को संबोधित किया गया था और इसमें भारतीयों और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच संबंधों को उदार और सहानुभूतिपूर्ण उपायों से मजबूत करने की सिफारिशें शामिल थीं।
मुख्य बिंदु:
- ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए स्वशासन स्थापित करना।
- भारत में ब्रिटिश प्रशासन को अधिक समावेशी और दयालु बनाना।
- भारतीयों के लिए अधिक अधिकार और भागीदारी सुनिश्चित करना।
- भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का एक मजबूत हिस्सा बनाने के लिए व्यापक और उदार उपाय लागू करना।
1918 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों को आंशिक रूप से रोम नोट में उल्लिखित विचारों से प्रभावित माना जाता है। ये सुधार भारत में स्वशासन प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं।
सामाजिक योगदान:
- अकाल से निपटने और जीवन स्तर में सुधार के लिए सुधारों को लागू किया।
- कैदी सुधारों को लागू किया; कैदियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाने वाले कालीनों को बनाया।
- करणी माता मंदिर, देशनोक के लिए चांदी के दरवाजे दान किए।
- सिख समुदायों के बीच सिंचाई और पुनर्वास की वकालत की।
- इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सख्ती से नियंत्रित किया, जो बीकानेर साजिश मामले में देखा गया।
शैक्षिक योगदान:
- महिलाओं के लिए संस्थानों सहित कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए।
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संरक्षक के रूप में समर्थन किया।
- राज्य में शैक्षणिक सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया ताकि व्यापक पाठ्यक्रम शामिल हो सके।
वास्तुकला योगदान:
- अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में प्रतिष्ठित लालगढ़ पैलेस का निर्माण किया।
- करनी माता मंदिर और रामदेवरा मंदिर का नवीनीकरण और सुधार किया।
- रेलवे, बिजली नेटवर्क, और सिंचाई प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे का विकास किया।
सैन्य प्रयास:
- गंगा रिसाला (ऊंट कोर) का गठन किया, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में सेवा की। स्वतंत्रता के बाद, इसने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की नींव रखी और बीएसएफ के भीतर बीकानेर ऊंट कोर के रूप में अस्तित्व में है।
- ब्रिटिश संबंधों के प्रबंधन और उनके सैन्य प्रयासों में योगदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- राज्य के भीतर आंतरिक रक्षा तंत्र को मजबूत किया।
आर्थिक और भूमि सुधार:
- गंग नहर (1925-1927) का निर्माण किया, जिससे सतलुज के पानी को बीकानेर के शुष्क क्षेत्र में लाया गया, जो इसे उपजाऊ क्षेत्र में बदल दिया।
- Founded and developed Sri Ganganagar, known as the “Grain Bowl of Rajasthan.”
- श्री गंगानगर की स्थापना और विकास किया, जिसे “राजस्थान का अन्न भंडार” कहा जाता है।
- आर्थिक उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों और कृषकों को आकर्षित किया।
व्यक्तित्व मूल्यांकन:
महाराजा गंगा सिंह एक दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने बीकानेर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे गंगा नहर परियोजना और शिक्षा और बुनियादी ढांचे में प्रगति। उनके कूटनीतिक प्रयास, जैसे “रोम नोट,” 7 अगस्त 1947 को भारत के अधिराज्य में सम्मिलन पर हस्ताक्षर किए। ने भारत के भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाया। हालाँकि, उनके भी दोष थे, जैसे कि उनका अधिनायकवादी स्वभाव (बीकानेर साजिश मामला) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना। बावजूद इसके, उनके सुधार और नेतृत्व आधुनिक बीकानेर के निर्माण में महत्वपूर्ण थे। कुल मिलाकर, गंगा सिंह के योगदान राज्य के विकास में निर्णायक थे।
महाराजा सर राव सादुल सिंह (1943-1950)
- उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का समर्थन किया।
- उन्होंने बीकानेर से के. एम. पणिकर को संविधान सभा के लिए नामांकित किया।
- 7 अगस्त 1947 को भारत के अधिराज्य में सम्मिलन पर हस्ताक्षर किए।
- 30 मार्च 1949 को अपने राज्य को राजस्थान के वर्तमान राज्य में विलय कर दिया।
- उन्होंने अपने राज्य में ‘नोटा’ (शादी के निमंत्रण) और ‘तख्तनशीनी की भाषा’ (उत्तराधिकार कर) जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया।
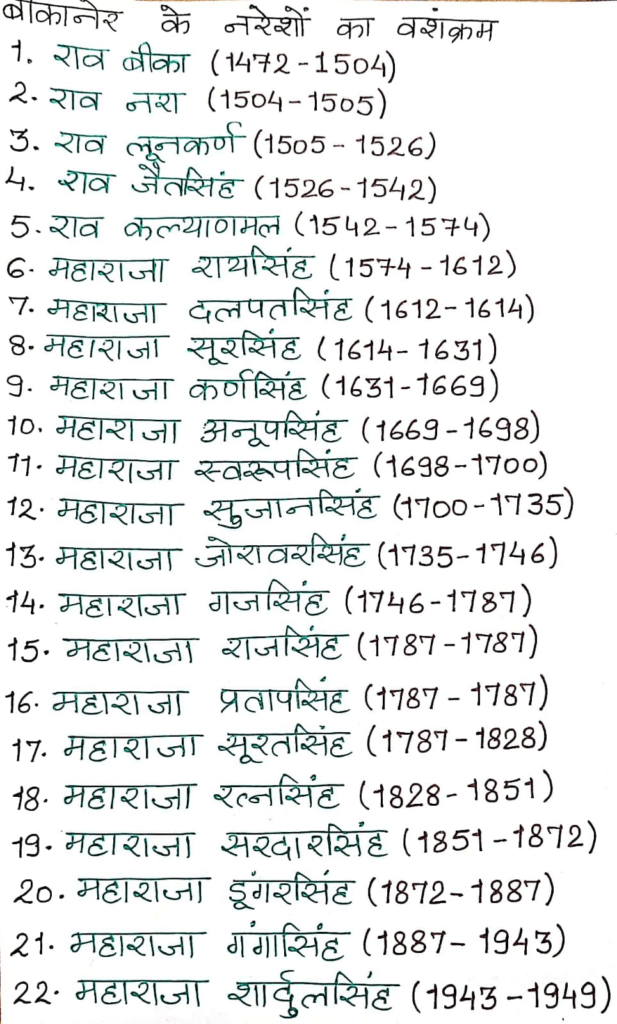
चौहान वंश
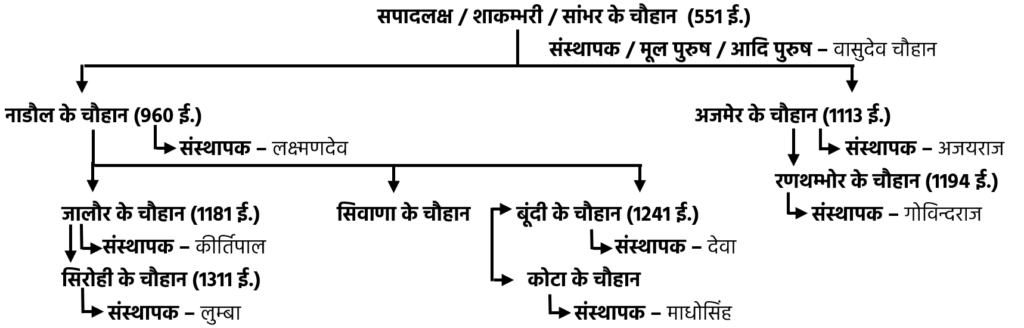
- चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासो के प्रारंभिक संस्करणों में चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं बताया गया है, जबकि बाद के संस्करणों में इस बात का उल्लेख मिलता है।
- 15वीं शताब्दी की हम्मीर महाकाव्य (नयचंद्र सूरी) और जयनीक की पृथ्वीराज विजय चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं।
- पंडित गौरीशंकर ओझा भी इस मत का समर्थन करते हैं।
- बिजोलिया शिलालेख (1170 ईस्वी) के आधार पर डॉ. दशरथ शर्मा मानते हैं कि चौहान वंश के प्रारंभिक पूर्वज का जन्म अहिच्छत्रपुर में वत्स गोत्र में हुआ था। अहिच्छत्रपुर को आधुनिक नागौर के रूप में पहचाना जा सकता है।
- ऐसा माना जाता है कि चौहान वंश के प्रारंभिक शासक अहिच्छत्रपुर के छोटे राजा थे। जैसे-जैसे चौहान वंश का क्षेत्रीय विस्तार हुआ, उनके अधीनस्थ सम्पूर्ण क्षेत्र को सपादलक्ष कहा जाने लगा।
- समय के साथ चौहानों ने विभिन्न स्थानों पर राजवंश स्थापित किए। मुख्य चौहान राजवंशों में शामिल हैं:
- शकंभरी के चौहान
- रणथंभौर के चौहान
- जालोर के चौहान
- हाड़ौती के हाड़ा (जो चौहान वंशज होने का दावा करते हैं)
शाकंभरी के चौहान
वासुदेव (6वीं शताब्दी ईस्वी):
- शकंभरी शाखा के संस्थापक, लगभग 551 ईस्वी में।
- प्रारंभिक राजधानी: अहिच्छत्रपुर।
- पृथ्वीराज विजय के एक मिथकीय कथानक के अनुसार, उन्हें सांभर झील एक विद्याधर से उपहार में मिली थी।
गोविंद-राज प्रथम (809-836 ईस्वी):
- गुवक प्रथम के नाम से भी जाने जाते हैं।
- प्रतिहार शासक नागभट्ट के सामंत थे।
- उन्होंने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया।
अजय-राज द्वितीय (1110-1135 ईस्वी):
- 1113 ईस्वी में अजयमेरु (अजमेर) शहर और अजयमेरु किले की स्थापना की।
- राजधानी को अजयमेरु (अजमेर) स्थानांतरित किया।
- ग़ज़नवी आक्रमण को विफल किया और परमार राजा नरवर्मन को हराया।
- वे शैव मत के अनुयायी थे, लेकिन जैन और वैष्णव अनुयायियों के प्रति भी सम्मान रखते थे।
अर्णोराज (1135-1150 ईस्वी):
- अनाजी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने तुर्की आक्रमणकारियों को हराया।
- चाहमान प्रशस्ति में उनके कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है:
- तुर्क अभियान: उन्होंने अजमेर के पास तुर्कों को हराया।
- मालवा विजय: मालवा के शासक नरवर्मन को हराकर उनके क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया।
- सिंधु-सरस्वती अभियान: चाहमान सेना ने सिंधु और सरस्वती क्षेत्रों में अपनी पहुँच बढ़ाई।
- हरितानक अभियान: हरितानक (आधुनिक हरियाणा) में अपने प्रभुत्व को स्थापित किया।
- वारण अभियान: उन्होंने बुलंदशहर (वारण) में डोड राजपूतों को हराया।
- चालुक्यों के साथ संबंध: सपादलक्ष के दक्षिण-पश्चिम में गुजरात के चालुक्य राज्य थे, जहाँ उस समय जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल जैसे शक्तिशाली राजा शासन कर रहे
| युद्ध | वर्ष | विरोधी | परिणाम | प्रभाव |
| अर्णोराज V/S जयसिंह | 1134 CE | जयसिम्हा सिद्धराज | अर्णोराज विजयी | जयसिम्हा ने अपनी बेटी कंचनदेवी का विवाह अर्णोराज से किया। |
| अर्णोराज V/S कुमारपाल | 1145 CE | कुमारपाल | कुमारपाल विजयी | अर्णोराज ने अपनी बेटी जल्हना का विवाह कुमारपाल से कर दिया। |
अर्णोराज की सांस्कृतिक और वास्तुशिल्पीय योगदान:
- पुष्कर वराह मंदिर : अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया, जो हिंदू संस्कृति और वास्तुकला के प्रति उनकी संरक्षण भावना को दर्शाता है।
- आनासागर झील : उन्होंने अजमेर में इंदु नदी के पानी को मोड़कर आनासागर झील का निर्माण कराया, जो तुर्क अभियान से पहले हुआ था
- जैन धर्म का समर्थन : अर्णोराज ने जैन धर्म के खतरगच्छ संप्रदाय के अनुयायियों को भूमि प्रदान की। उनके संरक्षण मे देवबोध और धर्मघोष जैसे जैन विद्वान पनपे और उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ
विग्रहराज IV (1158-1163 ईस्वी):
विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है, चौहान वंश का एक प्रमुख शासक था, जो अपनी सैन्य विजय, सांस्कृतिक संरक्षण और प्रशासनिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। उनके शासनकाल को “सपादलक्ष चौहानों का स्वर्ण युग” कहा जाता है। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने उन्हें एक सेनापति, विजेता, साहित्य का संरक्षक, कवि और निर्माता बताया। प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:
सैन्य अभियानों:
- उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार हिमालय से लेकर विंध्याचल तक किया, जो आर्यावर्त क्षेत्र को कवर करता है, जैसा कि दिल्ली-टोपरा स्तंभ लेख में उल्लेखित है।
- चालुक्य शासक कुमारपाल को हराकर पाली, नागौर, और जालौर पर कब्जा किया, जिससे राजस्थान पर उनकी पकड़ मजबूत हुई।
- दिल्ली अभियान में उन्होंने तोमर वंश को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया।
- उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा की। सोमदेव की “ललित विग्रहराज नाटक” और प्रबंध कोश में उन्हें “तुर्क विजेता” कहा गया है।
- दिल्ली-टोपरा अभिलेख में उल्लेख है कि उन्होंने बार-बार मलेच्छों (मुस्लिम आक्रमणकारियों) को हराया।
सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान:
- विग्रहराज IV एक विद्वान-राजा और कला तथा साहित्य के संरक्षक थे।
- उन्होंने स्वयं संस्कृत नाटक “हरिकेली” की रचना की।
- उनका दरबार साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। विद्वान जयनाक भट्ट ने उन्हें “कवि बंधु” की उपाधि दी।
- उनके दरबार के कवियों में सोमदेव शामिल थे, जिन्होंने “ललित विग्रहराज नाटक” लिखा, जो विग्रहराज की प्रेम कहानी का वर्णन करता है।
- इतिहासकार किलहॉर्न ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि “वे उन दुर्लभ हिंदू राजाओं में से एक थे जो कालिदास और भवभूति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे।”
वास्तुशिल्पीय योगदान:
- उन्होंने सरस्वती कंठाभरण विद्यालय (अजमेर) का निर्माण किया, जो हिंदू वास्तुकला की चरम सीमा को दर्शाता है। बाद में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा “अढ़ाई दिन का झोपड़ा” में बदल दिया गया।
- मंदिर परिसर में एक विष्णु मंदिर था, जो पवित्र हिंदू मूर्तियों से सजाया गया था।
- उन्होंने बीसलपुर (टोंक) में बीसलसागर बांध का निर्माण कराया, जिससे सिंचाई और जल प्रबंधन में सुधार हुआ।
- कई पहाड़ी किलों को मजबूत किया और अपनी विजय के स्मरण में विजय स्मारक बनाए।
धार्मिक नीतियाँ और समावेशिता:
- विग्रहराज IV, यद्यपि शैव थे, लेकिन उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन किया और जैन धर्म का समर्थन किया।
- उन्होंने जैन विहारों का निर्माण कराया और जैन उत्सवों में भाग लिया।
- जैन संत धर्मघोष सूरी की सलाह पर उन्होंने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया।
पृथ्वीराज III (1178-1192 ईस्वी):

पृथ्वीराज चौहान, अजमेर के चौहान वंश के सबसे प्रमुख शासक माने जाते हैं। उनका जन्म 1166 ईस्वी में अन्हिलापत (गुजरात) में हुआ था। उनके शासनकाल में चौहान वंश ने न केवल अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार किया, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके दरबार में कई विद्वान और कवि थे, जिससे उनका शासन इतिहास और साहित्य में स्मरणीय बना।
दरबारी विद्वान:
- चंदबरदाई: उनका वास्तविक नाम ‘पृथ्विभट्ट’ था। वे पृथ्वीराज के राजकवि, मित्र और विश्वासी थे। चंद बरदाई ने ‘पृथ्वीराज रासो’ की रचना की, जिसे उनके पुत्र जल्हण ने पूरा किया।
- जयानक: एक कश्मीरी कवि जिन्होंने ‘पृथ्वीराज विजय’ लिखा, जो अजमेर के चौहानों के शासन का विवरण देता है।
- अन्य: अशाधर, जनार्दन, विद्यापति गौड़, और वागीश्वर।
राजनीतिक चुनौतियाँ :
- नागार्जुन का दमन: युवावस्था में सिंहासन पर बैठने के बाद, पृथ्वीराज को अपने संबंधी नागार्जुन से विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसने स्वयं को सही उत्तराधिकारी घोषित किया। 1178 ईस्वी में, पृथ्वीराज ने गुरुग्राम में हुए युद्ध में उसे हराया।
- भंडानक समुदाय: सतलज क्षेत्र से भंडानक समुदाय ने गुरुग्राम, हिसार और आस-पास के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। 1182 ईस्वी में, पृथ्वीराज ने उनके विद्रोह को दबाकर अपने उत्तर-पश्चिमी सीमा को सुरक्षित किया।
- चंदेलों के साथ संघर्ष: महोबा के चंदेल शासक परमर्दिदेव ने पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण किया। 1182 ईस्वी में, पृथ्वीराज ने महोबा के युद्ध में चंदेलों को हराया।
- चौहान-चालुक्य संघर्ष (1184-87 ईस्वी):
संघर्ष के कारण:- भीम – II द्वारा सोमेश्वर की हत्या ।
- आबू की राजकुमारी इछिणी देवी का पृथ्वीराज से विवाह, जो थीं।
- 1184 ईस्वी में, पृथ्वीराज ने नागौर के युद्ध में भीम द्वितीय को हराया।
- 1187 ईस्वी में, जगदेव प्रतिहार की मध्यस्थता से शांति स्थापित हुई।
- क्षेत्रीय विस्तार की महत्वाकांक्षा।
- चौहान-गहड़वाल प्रतिद्वंद्विता : यह प्रतिद्वंद्विता तब शुरू हुई जब विग्रहराज IV ने दिल्ली पर नियंत्रण पाने के लिए विजयचंद गहड़वाल को हराया। यह पृथ्वीराज की ‘दिग्विजय नीति’ और जयचंद गहड़वाल की बेटी संयोगिता के अपहरण के कारण और अधिक तीव्र हो गई।
पृथ्वीराज Vs मो. गौरी
तराइन के युद्ध 1191 & 1192
तराइन के युद्ध, जिन्हें ताराोरी की लड़ाइयाँ भी कहा जाता है, 1191 और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान III (अजमेर के) और गौरी साम्राज्य के शासक मुहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई दो युद्धों की एक श्रृंखला थी।
मुहम्मद गौरी – मुहम्मद गज़नी ने गज़नी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गज़नी थी। उनकी मृत्यु के बाद, गज़नी में ओगुज़ तुर्कों का शासन था। गौरी ने तुर्कों को हराया और गौरी साम्राज्य की नींव रखी। गज़नी में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद, मुहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण का ध्यान केंद्रित किया।
- 1175 में – गौरी ने मुल्तान पर कब्जा किया और संपूर्ण सिंध पर कब्जा कर लिया।
- 1178 में – कयादरा की युद्ध में गुजरात के भीमदेव सोलंकी-II से पराजित हुए।
- 1186 में – उन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया, और खुर्शीद मलिक को हराकर मलिक साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। गौरी फिर गज़नी लौटे और अपने भाई की मदद करने के बाद, 1191 में भारत लौटे।
पहला तराइन के युद्ध (1191)
- 1191 में, गौरी खैबर दर्रे से भारत की ओर बढ़े और भठिंडा का किला कब्जा कर लिया।
- उत्तर भारत के हिंदू राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में एक संघ बना लिया।
- पृथ्वीराज की सेना ने अपने प्रिंस गोविंद ताई के नेतृत्व में भठिंडा की ओर मार्च किया और ताराैन में गौरी से उनका सामना हुआ।
- गोविंद ताई से व्यक्तिगत युद्ध में गौरी घायल हो गए और उनकी सेना ने पलायन किया, जिससे पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुई।
- वैकल्पिक रूप से यह भी कहा गया है कि गौरी की सेना ने आत्मसमर्पण किया और मुहम्मद को बंदी बना लिया। मुहम्मद गौरी ने दया की भीख मांगी और पृथ्वीराज ने उसे माफ कर दिया।
- पहले युद्ध के बाद: गौरी गज़नी लौटे और पराजय का बदला लेने के लिए तैयारियां शुरू कीं। जब वह लाहौर पहुंचे, तो उन्होंने पृथ्वीराज के पास दूत भेजा, ताकि पृथ्वीराज समर्पण कर दे, लेकिन चौहान शासक ने इससे मना कर दिया।
दूसरी तराइन की युद्ध (1192)
- 1192 में, गौरी ने पृथ्वीराज को फिर से चुनौती दी और तराइन में युद्ध लडा गया।
- दोनों ने अपनी सेनाओं की शक्ति बढ़ाई, लेकिन गौरी ने अपनी रणनीति बदल दी, क्योंकि वह राजपूतों के कुशल योद्धाओं के साथ खुले युद्ध में नहीं भिड़ना चाहता था।
- गौरी ने अपनी विशाल सेना को पाँच हिस्सों में बाँट लिया और चार इकाइयाँ राजपूतों के flanks और rear पर हमले के लिए भेजीं।
- राजपूतों के हमले की उम्मीद करते हुए, गौरी ने अपनी पाँचवी इकाई को तेजी से पीछे हटने का आदेश दिया। जैसा कि गौरी ने अनुमान लगाया था, राजपूतों ने भागते हुए गौरी टुकड़ी पर हमला किया। गौरी ने फिर 12,000 की नई घुड़सवार सेना भेजी और उन्होंने राजपूतों के हमले को पीछे हटा दिया।
गौरी ने दूसरी तराइन की युद्ध जीत ली।
पृथ्वीराज चौहान की हार के कारण
- According to ‘Minhaj-us-Siraj’ “Ghori’s army was well organized and Prithviraj’s army was completely disorganized.
- Lack of central leadership due to the feudal army.
- Lack of strategic foresight and diplomacy.
- Allowing Ghori enough time to prepare for the second battle.
- Use of elephants in the army, which were less effective against Ghori’s cavalry.
- Betrayal by ministers Someshwara and Pratapasimha.
पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में मत
- ‘प्रथ्वीराज रासो’: पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था, जहाँ उन्होंने अपनी ‘शब्द भेदी बाण’ (ध्वनि द्वारा मार्गदर्शित तीर) कौशल का उपयोग करके मुहम्मद गौरी को मार डाला।
- इसामी के अनुसार: पृथ्वीराज ने गौरी साम्राज्य की अधीनता में अजमेर पर शासन करना जारी रखा था, लेकिन बाद में मुहम्मद गौरी ने उसे मार डाला।
- मिन्हाज-उस-सिराज: इस संस्करण के अनुसार, मुहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध के दौरान युद्धभूमि में ही मार डाला।
तराइन की लड़ाइयों के परिणाम
- तराइन के युद्ध और चंदावर के युद्ध ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी।
- हांसी, सिरसा, समाना, अजमेर और दिल्ली जैसे प्रमुख क्षेत्र मुस्लिम शासन के तहत आए।
- राजपूतों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दबा दिया गया; पृथ्वीराज चौहान के बाद, कोई राजपूत शासक दिल्ली को पुनः प्राप्त नहीं कर सका।
- भारत और मध्य एशिया के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए।
- भारतीय संस्कृति पर प्रभाव
- सकारात्मक
- पारसी कला और वास्तुकला की शैलियों का प्रसार।
- हिंदू-मुस्लिम मिश्रित संस्कृति का विकास, जो वास्तुकला और चित्रकला में दिखाई दिया।
- भक्ति और सूफी आंदोलनों का उदय।
- व्यापार, शहरीकरण और शिल्प का विस्तार, जिसने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इरफ़ान हबीब ने इसे “नई शहरी क्रांति” के रूप में संदर्भित किया।
- नकारात्मक
- हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का पतन (जैसा कि वी.ए. स्मिथ और आर.सी. मजुमदार ने उल्लेख किया है)
- कला, साहित्य और वास्तुकला का नुकसान, जैसे कि बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का विध्वंश।
पृथ्वीराज चौहान का कला और साहित्य में योगदान
- इतिहासकार डॉ. दाशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान को “सक्षम और रहस्यमय शासक” के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने कला, संस्कृति और समावेशिता को बढ़ावा दिया।
- विद्वानों और कलाकारों के संरक्षक: उनका दरबार प्रसिद्ध विद्वानों से सजा था, जैसे कि चंदबरदाई, जिन्होंने ‘प्रथ्वीराज रासो’ लिखा, और जयनक, जिन्होंने ‘पृथ्वीराज विजय’ लिखा।
- शिक्षा को बढ़ावा दिया: शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके संस्थानों से स्पष्ट है, जैसे कि सरस्वती कांठाभरण, जिसमें 85 विषयों में शिक्षा दी जाती थी, और अन्य कई स्कूलों ने उनके संरक्षण में फल-फूल किया।
- साहित्यिक योगदान: उनके शासन के दौरान जैन विद्वानों जैसे कि जिनदत्त सूरी, जिन वल्लभ, और जिनपति सूरी ने धार्मिक और सांस्कृतिक साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उन्होंने संस्कृत, अपभ्रंश और क्षेत्रीय बोलियों में ग्रंथ रचे।
- वास्तुकला में योगदान: उन्होंने दिल्ली में राय पिथोरा किला और तरागढ़ किले का निर्माण किया, ताकि अपनी राजधानी की रक्षा कर सकें। अजमेर में, उन्होंने मंदिरों और महलों का निर्माण करके शहर का विस्तार किया, जिससे उसकी भव्यता बढ़ी।
- सभी धर्मों का समर्थन: पृथ्वीराज चौहान को उनके धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और सभी धर्मों के प्रति सम्मान के लिए जाना जाता था। जैन विद्वानों जैसे जिनदत्त सूरी, जिन वल्लभ, और जिनपति सूरी ने महत्वपूर्ण कार्यों की रचना की, जैसे कि उपदेशरसायण-रस, चर्चरी, कलास्वरूप कुलक, और प्रभोध वदस्थल।
गोविंदराज IV (1192 ई.)
- हरिराज द्वारा मुस्लिम अधीनता स्वीकार करने के कारण निर्वासित;
- रणथम्भौर के चौहान शाखा की स्थापना की।
रणथंभौर के चौहान
रणथंभौर के चहामना वंश की नींव गोविंदराज ने रखी, जो शाकंभरी चौहान परिवार के सदस्य थे (जो अजमेर के चौहान थे)। गोविंदराज, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, जिन्हें 1192 ई. में गौरी शासक मुहम्मद गोरी ने हराकर मार डाला। इस पर, घोरिद शासक मुहम्मद गोरी ने गोविंदराज को अजमेर में अपना उपाधीपति नियुक्त किया। हालांकि, पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने गोविंदराज को उखाड़कर अजमेर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और गोविंदराज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाकर नया राज्य स्थापित किया।
हम्मीर देव (1286 – 1301 ई.) :
हम्मीर देव के शासनकाल में दिल्ली में बलबन की मृत्यु के बाद, चार वर्षों तक नेतृत्व का अभाव रहा, जिससे उन्हें शक्ति संकलित करने का अवसर मिला। इस समय, मालवा और गुजरात कमजोर हो गए थे और चित्तौड़ के शासक समरसिंह के विस्तारवादी उद्देश्यों में रुचि नहीं थी। हम्मीर देव ने इसका फायदा उठाया और रणथंभौर का प्रभाव बढ़ाने के लिए आक्रामक विस्तार नीति अपनाई।
1286 में बलबन की मृत्यु के बाद, दिल्ली को लगभग चार वर्षों तक नेतृत्व शून्यता का सामना करना पड़ा, जिससे हम्मीर को सत्ता मजबूत करने की अनुमति मिली। मालवा और गुजरात सहित पड़ोसी राज्यों का पतन हो रहा था, जबकि चित्तौड़ के शासक समरसिंह में विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का अभाव था। हम्मीर ने इस अवसर का उपयोग अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किया।
राजनीतिक चुनौतियाँ और विजय:
हम्मीर देव ने रणथंभौर के प्रभाव को मजबूत करने के लिए आक्रामक विस्तार नीति अपनाई। उसने पूरे उत्तर-पश्चिमी राजपूत शासकों पर विजय प्राप्त की। प्रारंभ में, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में रणथंभौर पर हमला किया, बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन पर कब्ज़ा करने के बाद हम्मीर से संघर्ष किया।
- जलालुद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष: 1290 में, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया लेकिन वह सफल नहीं हो सका, हालांकि वह झाँईन किले पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। फिर 1299 में उसने फिर से रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन उसे फिर से पराजय मिली।
- आलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष:
- कारण :
- कर का भुगतान न करना: हम्मीर ने दिल्ली सल्तनत को कर देना बंद कर दिया।
- मंगोल विद्रोहियों को आश्रय देना: हम्मीर ने अलाउद्दीन के खिलाफ विद्रोह करने वाले मंगोल नेताओं मुहम्मद शाह और केब्रू को शरण प्रदान की।
- रणथंभौर पर विजय प्राप्त करना अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण था और उनके दक्षिणी अभियान को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य किया।
- कारण :
रणथंभौर की लड़ाई:
- 1299 ई. में अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर को वश में करने के लिए उलुग खान और नुसरत खान को भेजा। उन्होंने झाईन किले पर कब्जा करके शुरुआत की, लेकिन हम्मीर की सेना ने उन्हें बनास नदी के पास हरा दिया, जहां नुसरत खान मारा गया।
- जवाब में, अलाउद्दीन ने 1301 ई. में व्यक्तिगत रूप से रणथंभौर की विशाल घेराबंदी का नेतृत्व किया।
- घेराबंदी लगभग एक वर्ष तक चली, जिससे किले में भयंकर अकाल पड़ा। विश्वासघात का प्रयोग करते हुए, अलाउद्दीन ने हम्मीर के सेनापतियों (रतिपाल, रणमल और सरगुन शाह) को दलबदल करने के लिए मना लिया।
- भुखमरी ने रक्षकों को कमजोर कर दिया, और अब आमने सामने की लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं था। अंततः राजपूत योद्धाओं ने हम्मीर देव के नेतृत्व में अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए केसरिया किया एवं क़िले की महिलाओं ने रानी रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर किया।
- 11 जुलाई, 1301 को रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गया।
व्यक्तित्व का मूल्यांकन :
- हम्मीर एक बहुआयामी शासक था, जिसे उसकी वीरता, अटूट सिद्धांतों और असाधारण नेतृत्व के लिए जाना जाता था, लेकिन कभी-कभी प्रशासनिक गलत निर्णयों के लिए भी उसकी आलोचना की जाती थी, जैसे भीम सिंह की मौत के लिए धर्मसिंह को जिम्मेदार ठहराना और बाद में उसे अंधा कर देना। उन्हें बेजोड़ उदारता और आतिथ्य के साथ हिंदू मूल्यों और परंपराओं के कट्टर रक्षक के रूप में याद किया जाता है, जिसका उदाहरण महत्वपूर्ण जोखिमों के बावजूद मंगोल शरणार्थियों की रक्षा करने का उनका निर्णय है। उनकी सैन्य क्षमता उनके द्वारा लड़े गए 17 युद्धों से स्पष्ट होती है, जिनमें से उन्होंने 16 में जीत हासिल की। हम्मीर हठ में चन्द्रशेखर ने हम्मीर के दृढ़ संकल्प को अमर कर दिया:
“सिंह सुवन, सत्पुरुष वचन, कदली फलत एके बार
तिरिया तेल, हम्मीर हठ, चढ़े न दूजी बार।”
- यह कविता हम्मीर के समझौता न करने वाले स्वभाव पर प्रकाश डालती है, जो उनकी विरासत की एक परिभाषित विशेषता बन गई।
सांस्कृतिक और कला योगदान:
- हम्मीर देव कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उनके दरबार में राघव देव और बिजादित्य जैसे प्रसिद्ध विद्वान थे।
- उन्होंने “कोटी-यज्ञ” का आयोजन किया, जिसमें मुख्य पुजारी के रूप में विश्वस्वरूप को नियुक्त किया।
- इसके अलावा, उन्होंने अपने पिता जयत्र सिंह की याद में 32 पिल्लरों वाला छतरी बनवाया, जो उनके 32 वर्षों के शासनकाल का प्रतीक था।
- उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर पद्मला तालाब भी बनवाया और रणथंभौर में एक स्वर्णमयी मंडप ‘पुष्यक’ का निर्माण किया। उनके द्वारा लिखित “श्रृंगार हार” संगीत पर एक महाकाव्य ग्रंथ है।
जालौर के चौहान
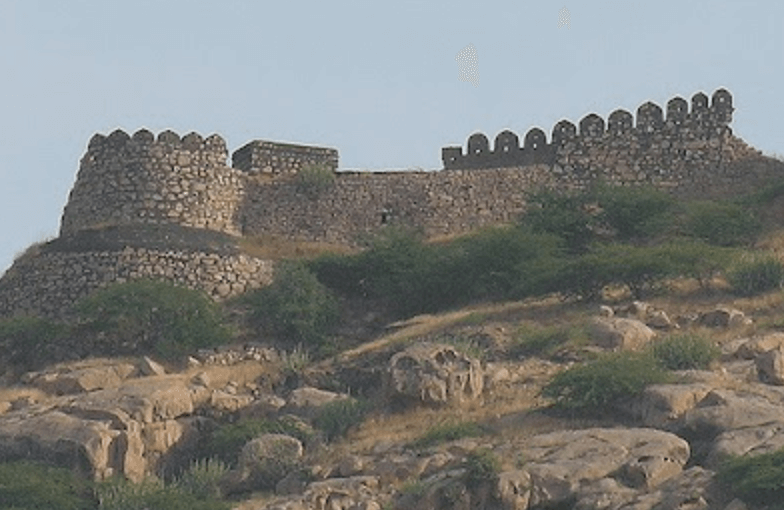
जालौर में 8वीं शताबदी में प्रतिहार राजा वत्सराज का शासन था। 12वीं शताबदी के अंत तक, यहाँ परमारों का शासन था। इतिहासकारों का मानना है कि जालौर किला परमार शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। 1238 ई. के एक शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि परमार राजा बिरल की रानी मालुदेवी ने सिंधु के राजा को हराया और स्वर्ण की विजय प्राप्त की।
प्रमुख शासक:
कीर्तिपाल चौहान (1160-1182 ई.)
- वह नाडोल के राजा अल्हण के छोटे बेटे थे।
- 1181 ई. में परमारों को हराकर चौहान साम्राज्य की नींव रखी।
- उदयसिंह (1204-1257 ई.) चौहानों का शासन जारी रखा और राज्य का विस्तार किया।
- चाचिग देव (1257-1282 ई.)
- सामंतसिंह (1282-1305 ई.)
कन्हड देव (1291-1311 ई.)
- यह जालौर के चौहानों के अंतिम और सबसे गौरवमयी शासक थे।
- कान्हड देव के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया।
- कारण:
- अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाए।
- कान्हडदेव ने राजकीय सेना को जलोर में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के दौरान उन्हें आक्रमण कर दिया।
- कन्हड देव के पुत्र वीरम देव और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा के बीच प्रेम संबंध भी आक्रमण का कारण बना, जैसा कि ‘कन्हड दे प्रबंध’ में उल्लेखित है।
- 1308: सिवाना का युद्ध
- अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने सिवाना किले को घेर लिया। किले का बचाव करने वाले लोगों ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, लेकिन किला अंततः गिर गया।
- सिवाना का पहला साका:
- जौहर – रानी मैंणा देवी के नेतृत्व में।
- केसरिया – सातल देव के नेतृत्व में।
- 1310-1314: जालौर का युद्ध
अलाउद्दीन खिलजी ने 50,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ जलोर पर आक्रमण किया। कन्हड देव ने 5,000 सैनिकों के साथ जालौर का बचाव किया और 3-4 वर्षों तक प्रतिरोध किया, लेकिन किला अंततः गिर गया। - एक विश्वासघाती दहिया सरदार ने अलाउद्दीन खिलजी से रिश्वत लेकर किले का पीछे का द्वार खोल दिया, जिससे तुर्क सैनिकों को किले में प्रवेश का मार्ग मिल गया।
- जालौर का पहला और अंतिम साका:
- जौहर – रानी जैतल देवी के नेतृत्व में।
- केसरिया – कन्हड देव के नेतृत्व में।
- परिणाम:
- अलाउद्दीन खिलजी ने जलोर को लूटा और नागरिकों को गुलाम बना लिया।
- कान्हड देव के छोटे भाई मल देव सोनगरा ही जीवित बच पाए और उन्हें सुलतान ने पुरस्कार दिया, और चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया।
- जालौर किला सुल्तान के अधीन रहा, जब तक कि सल्तनत का पतन नहीं हुआ।
अन्य शासक:
- 15वीं शताबदी में राठौड़ राजा राव मलदेव ने जालौर किले पर शासन किया।
- अकबर के शासनकाल में, अब्दुल रहीम खानख़ाना ने इसे ग़ज़नी खान से अनंतकाल तक लिया।
- सम्राट जहांगीर ने किले की दीवारों का निर्माण कराया।
- औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह स्थायी रूप से जोधपुर राज्य का हिस्सा बन गया।
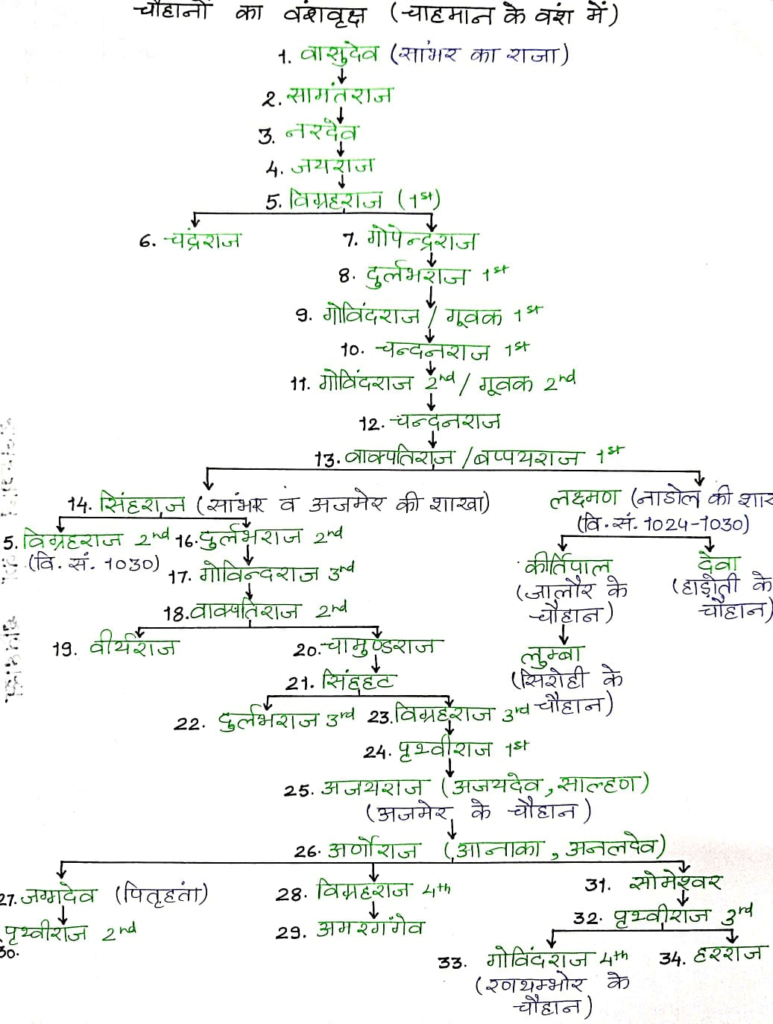
मेवाड़ का वंश

मेवाड़ राज्य वर्तमान में चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों को शामिल करता है। यह क्षेत्र पहले मेदपाट/शिवि/प्रागवाट के नाम से जाना जाता था और भगवान शिव (एकलिंगनाथ) को मेधपाटेश्वर (मेदपाट के भगवान) कहा जाता है। समय के साथ मेधपाट का नाम मेवाड़ में परिवर्तित हो गया।
मेवाड़ के राजपूत वंश की स्थापना करने वाले शासक गूहिलोत वंश से थे। स्थापना संबंधी कथाएँ बताती हैं कि यह वंश कश्मीर से उत्पन्न हुआ था और छठी शताबदी में गुजरात में प्रवासित हुआ। सातवीं शताबदी में ये लोग फिर से मेवाड़ की मैदानी क्षेत्रों में, विशेष रूप से मगड़ा क्षेत्र में आए, जो इस वंश के पहले प्रमुख नेताओं के नाम पर नामित किया गया था।
चित्तौड़गढ़ के गुहिल
गुहिल (566-586 ई.)
- गुहिल को गूहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। वे वल्लभी (गुजरात) के राजा शिलादित्य VI के वंशज थे।
- गूहिल की मां पुष्पावती जब तीर्थयात्रा पर थीं, तब वल्लभी पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया गया था। गूहिल बच गए और उनकी मां ने गुहिल वंश की स्थापना की।
बप्पा रावल (586-606 CE)
- उन्हें कालभोज भी कहा जाता है।
- अपने गुरु महर्षि हरित ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने मान मोरी को हराया और मेवाड़ में गुहिल वंश के शासन की नींव रखी।
- अरबों को परास्त करने के लिए नागभट्ट और जयसिंह के साथ त्रिकोणीय संधि बनाई।
राजस्थान का युद्ध: 738 ई.
- यह युद्धों का समूह था जिसमें गुर्जर-हिंदू संधि ने अरबी आक्रमणकारियों को हराया।
- गुर्जर-हिंदू संधि – नागभट्ट-1 (गुर्जर-प्रतिहार), बप्पा रावल (गुहिल), जयसिंह वर्मन (राष्ट्रकूट)।
- 7वीं शताब्दी के अंत तक, इस्लाम और अरबों ने ईरान और अफगानिस्तान में अपना विस्तार किया था। मुहम्मद इब्न कासिम के तहत अरबों ने 730 ई. में हिंदुस्तान में आक्रमण किया और राजस्थान, मालवा, और गुजरात में लूटपाट की।
- 738 ई. में उनकी हार ने अरबों को कमजोर कर दिया और उनकी आगे की कोशिशों को नाकाम कर दिया, जिससे हिंदुस्तान को 200 साल तक अरबों के आक्रमणों से सुरक्षित रखा।
वास्तुकला विकास
- सहस्रबाहु मंदिर (महामारु शैली), एकलिंगजी मंदिर कैलाशपुरी (उदयपुर)
खुमाण II (828–853 ई.)
- खुमान II ने 24 मुस्लिम हमलों को परास्त किया।
अल्लट/अल्लू रावल (943-953 ई.)
- रावल अल्लट, जिन्हें आल्लू रावल भी कहा जाता है, मेवाड़ के एक प्रमुख शासक थे जिनके शासनकाल में समृद्धि, धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक विकास हुआ। उन्होंने खुद को एक सक्षम प्रशासक, निर्माणकर्ता और व्यापार और वाणिज्य के प्रमोटर के रूप में स्थापित किया।
उपलब्धियाँ
- विवाह संधि – हरियादेवी से विवाह, जो हुण वंश की राजकुमारी थीं, जिसने उनके रणनीतिक कूटनीतिक गठबंधन को दर्शाया।
- प्रशासनिक और वाणिज्यिक सुधार – आहड़ (आटपुर) को एक समृद्ध प्रशासनिक, धार्मिक और वाणिज्यिक केंद्र में परिवर्तित किया और नागदा के बाद इसे अपनी दूसरी राजधानी बना दी।
- धार्मिक संरक्षण – उनके दरबार में विद्वानों और धार्मिक बहसों का स्वागत किया गया, जैसा कि जैन संत प्रद्युम्न सूरी द्वारा एक बहस में दिगंबर संतों को हराया गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि मेवाड़ में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था।
- सांस्कृतिक विकास – विष्णु के वराह रूप में सारणेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने जगत के अंबिका माता मंदिर का भी निर्माण किया, जिसे ‘खजुराहो ऑफ मेवाड़’ भी कहा जाता है।
क्षेम सिंह (1168-1172 ई.)
- क्षेम सिंह के दो बेटे थे: सामंत सिंह और कुमार सिंह।
- सामंत सिंह (1172 – 1179) ने पृथ्विबाई, जो पृथ्वीराज III चौहान की बहन थीं, से विवाह किया।
- सामंत सिंह के समय में, कीर्तिपाल चौहान (नदोल शाखा) ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और इसे कब्जा कर लिया, जिससे सामंत सिंह को भागना पड़ा।
- सामंत सिंह ने अपनी राज्य की स्थापना वागड़ क्षेत्र में की और वटभद्रक (बारोड़ा) को अपनी राजधानी बनाया।
- 1192 ई. में सामंत सिंह ने तराइन के दूसरे युद्ध में मुहम्मद गोरी से लड़ते हुए शहादत प्राप्त की।
- कुमार सिंह (1179 – 1191) ने बाद में किर्तिपाल चौहान को हराया और चित्तौड़गढ़ को पुनः प्राप्त किया।
जयतसिंह/जैत्र सिंह (1213-1253 ई.)
- चिरवा शिलालेख के अनुसार, जैत्रा सिंह ने गुजरात के चालुक्य शासक त्रिभुवन को कोटड़ा में हराया।
- शिलालेख में यह भी जानकारी दी गई है कि सुल्तान इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, भूताला का युद्ध (1227 ई.) में नागदा की राजधानी को सुल्तान ने नष्ट कर दिया और बाद में रावल जैत्र सिंह से पराजित हो गए।
- इस घटना के बाद, उन्होंने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ में स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया।
- डॉ. दशरथ शर्मा के अनुसार, जैत्र का शासनकाल मेवाड़ के प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है।
तेज सिंह (1261–1267 ई.)
- तेज सिंह के शासनकाल में, दिल्ली के सुलतान बलबन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया लेकिन वह सफल नहीं हो सके।
- रानी जैतल दे ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया।
- 1260 ई. में, आहर (उदयपुर) में, मेवाड़ चित्रकला शैली का पहला चित्रित पांडुलिपि ‘श्रावक प्रातिक्रमन सूत्र’ कमलचंद्र द्वारा तैयार किया गया।
रतन सिंह (1302-1303 ई.)
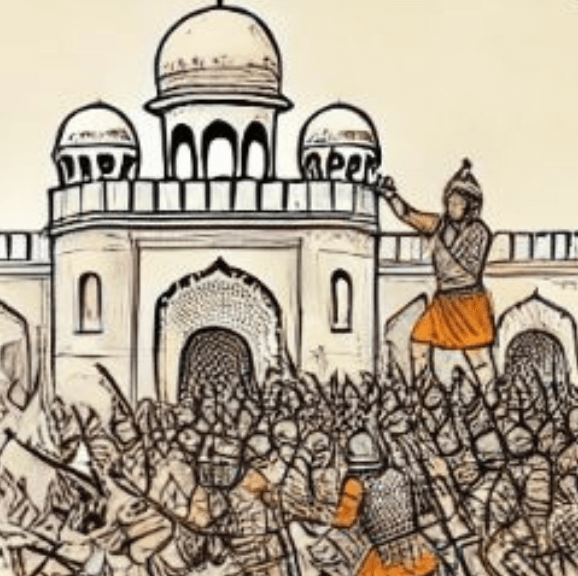
- गुहिल वंश के अंतिम शासक।
- 1303 – चित्तौड़ का पहला जौहर
- 1303 ई. में, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया, जो कि रानी पद्मिनी की सुंदरता के प्रति उनकी सनक के कारण हुआ।
- धोखाधड़ी का उपयोग करते हुए खिलजी ने राणा को पकड़ लिया और उनकी रिहाई के बदले पद्मिनी को मांगा।
- पद्मिनी ने एक योजना बनाई, जिसमें 700 सशस्त्र सैनिकों को पालकी में छिपाकर राणा को छुड़ाने भेजा। हालांकि पहले यह सफल रहा, खिलजी ने उनका पीछा किया और किले के गेट पर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राणा की मृत्यु हो गई।
- अलाउद्दीन खिलजी ने 26 अगस्त 1303 को किले पर कब्जा कर लिया। आत्मसमर्पण करने से इंकार करते हुए, रानी पद्मिनी और क़िले की अन्य महिलाओं ने जौहर किया।
- मेवाड़ का प्रशासन बाद में मालदेव, जो कि जालौर के शासक थे, को सौंपा गया।
चित्तौड़गढ़ पर खिलजी के आक्रमण के कारण:

- खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं – अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत अधिक से अधिक क्षेत्रों को जीतने का लक्ष्य रखा।
- रतनसिंह द्वारा शाही सेना से कर वसूलना – गुजरात पर जाने वाली खिलजी की सेना से मेवाड़ के शासक रतनसिंह द्वारा कर वसूलने को खिलजी ने अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ माना।
- चित्तौड़गढ़ किले की रणनीतिक स्थिति – किला मजबूत पहाड़ी पर स्थित था। विशाल दीवारें और पर्याप्त खाद्य व पानी के भंडारण ने इसे लंबे समय तक घेराबंदी झेलने योग्य बनाया।
- गुजरात और मालवा के बीच चित्तौड़गढ़ का स्थान – चित्तौड़गढ़ का भौगोलिक स्थान इसे सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बनाता था।
- मेवाड़ की बढ़ती ताकत और प्रभाव – मेवाड़ का प्रभाव क्षेत्र और सैन्य शक्ति लगातार बढ़ रही थी, जो खिलजी के लिए खतरा थी।
- रानी पद्मिनी की दंतकथा – रानी पद्मिनी की सुंदरता की दंतकथाएं खिलजी को चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के लिए प्रेरित करने वाले एक कारण के रूप में मानी जाती हैं।
- मेवाड़ की आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि (चांदी और जस्ता की प्रचुरता जो शस्त्रागार बनाने के लिए उपयोग होती थी)
मेवाड़ के सिसौदिया
राणा हम्मीर (1326-1364 ई.)
- 1303 ई. में अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ पर घेराबंदी के बाद गुहिल वंश लगभग समाप्त हो गया।
- खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर “खिज्राबाद” रखा और अपने बेटे खिज्र खान को किले का प्रशासक नियुक्त किया।
- बाद में खिलजी ने किले का नियंत्रण सोनागरा चौहान शासक मालदेव (मेड़ता के शासक) को सौंप दिया, लेकिन मालदेव इसे बनाए रखने में असफल रहे।
- मालदेव ने अपनी विधवा बेटी सोनगरी का विवाह राणा हम्मीर से किया।
- 1316 ई. में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई, जिससे क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं।
- 1326 ई. में हम्मीर सिसोदिया ने चित्तौड़ को पुनः प्राप्त किया और गुहिल वंश का शासन पुनः स्थापित किया।
- इस विजय के साथ ही मेवाड़ के शासकों को “सिसोदिया” कहा जाने लगा।
राणा लाखा (1382-1421 ई.)
- मंडोर के राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के उत्तराधिकारी चुंडा से करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गलतफहमी के कारण हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा से हो गया।
- चुंडा ने मेवाड़ के भावी शासक (राणा मोकल) के लिए अपना उत्तराधिकार त्याग दिया जिससे मेवाड़ के इतिहास में उसे “भीष्म” के रूप में जाना जाने लगा।
- चुंडा को उत्तराधिकार त्यागने पर निम्नलिखित विशेषाधिकार दिए गए:
- उनके वंशजों को “चुंडावत” कहा गया।
- उनके प्रतीक “भाला” को सभी अनुदानों में राजकुमार के हस्ताक्षर में जोड़ा गया।
- चुंडावतों को हरावल (विशिष्ट सैन्य बल) में सेवा देने का अवसर दिया गया।
- मेवाड़ के 16 प्रमुख क्षेत्रों में से चार, जिनमें सलूम्बर शामिल है, चुंडावतों को सौंपे गए।
- सलूम्बर के शासक को “रावत” की उपाधि दी गई और वे राजकीय कार्यों में सहायता करते थे।
- राजधानी के राजा की अनुपस्थिति में रावत सलूम्बर राजधानी का प्रबंधन करते थे।
- सभी शाही फरमानों पर रावत के हस्ताक्षर आवश्यक थे।
आर्थिक विकास:
- जावर में चांदी की खानों की खुदाई ने मेवाड़ की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- उत्तर-पश्चिम व्यापार मार्ग पर स्थित देलवाड़ा एक प्रमुख व्यापार और वाणिज्य केंद्र बन गया।
- महाराणा लाखा ने स्वयं व्यापारियों को मेवाड़ में बसने के लिए प्रोत्साहित किया।
- उनके शासनकाल में बंजारा छीतर ने गिरवा घाटी में प्रसिद्ध पिछोला झील का निर्माण किया।
वास्तुकला और सांस्कृतिक योगदान:
- झोटिंग भट्ट और धनेश्वर जैसे कवि उनके दरबार में थे।
- उन्होंने चित्तौड़, केलवाड़ा और लाखावली में जलाशयों का निर्माण करवाया।
मिट्टी के किले की कहानी
महाराणा लाखा ने बूंदी के तारागढ़ किले पर कब्जा करने तक भोजन न करने की कसम खाई थी। जब उनके सरदारों ने बताया कि किले पर जल्दी कब्ज़ा करना संभव नहीं है, तो राणा की प्रतिज्ञा के लिए एक नकली “मिट्टी का किला” बनाया गया। इसकी रक्षा के लिए, एक हाड़ा राजपूत, कुंभकरण को 300 लोगों के साथ नियुक्त किया गया था और कहा गया था कि जब लाखा हमला करेगा तो वह आत्मसमर्पण कर देगा। हालाँकि, कुम्भकरण ने अपने राजपूत सम्मान के प्रति सच्चे रहते हुए, मिट्टी के किले की जमकर रक्षा की। जब लाखा ने आक्रमण किया तो कुम्भकरण ने वीरगति प्राप्त करने से पहले लाखा के कई सैनिकों को मार डाला।
राणा मोकल सिंह (1421-1433 ई.)
- चूंकि मोकल नाबालिग थे, इसलिए चुंडा ने राज्य के मामलों को संभाला।
- चुंडा और राजमाता हंसा बाई के बीच मतभेद हो गए, इसलिए हंसा बाई ने राव रणमल से मेवाड़ में हस्तक्षेप करने के लिए कहा।
- राव रणमल का आगमन मेवाड़ के शाही परिवार को काफी प्रभावित कर गया, लेकिन बाद में रणमल के इरादों को समझा गया।
- रानी ने चुंडा को वापस बुलाया, जिन्होंने आकर मोकल सिंह की रक्षा की।
- मोकल के तीन पुत्र थे: राणा कुम्भा और दो अन्य पुत्र, साथ ही एक पुत्री लाल बाई।
राणा कुम्भा (1433-1468 ई.)
- महाराणा कुम्भा मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे, जो अपने सैन्य कौशल, विद्वता, वास्तु उपलब्धियों और सांस्कृतिक योगदान के लिए प्रसिद्ध थे।
- उनका जन्म 1417 ई. में महाराणा मोकल और महारानी सोभाग्य देवी के घर देवगढ़, मदरिया में हुआ था।
- 1433 ई. में उन्होंने मेवाड़ का सिंहासन ग्रहण किया और इसे एक शक्तिशाली राज्य में बदल दिया।
कुम्भा के सामने प्रारंभिक चुनौतियाँ:
- यह संबंध क्षेत्रीय और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए बार-बार संघर्ष से चिह्नित थे, जो कई युद्धों में परिणत हुए।
- मेवाड़-मालवा संघर्ष: यह संबंध क्षेत्रीय और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए बार-बार संघर्ष से चिह्नित थे, जो कई युद्धों में परिणत हुए।
- मेवाड़-गुजरात संबंध: नागौर में उत्तराधिकार विवादों के कारण मेवाड़-गुजरात संबंध खराब हो गए। 1456 ई. में कुम्भा ने शम्स खान को नागौर का शासक बनने में मदद की। हालांकि, शम्स खान ने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से गठबंधन किया, जिससे कुम्भा ने संयुक्त सेना पर हमला किया और उन्हें हराया।
- चम्पानेर की संधि (1456 ई.): यह संधि मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच कुम्भा के खिलाफ की गई थी। इस संधि का उद्देश्य विजय के बाद मेवाड़ को विभाजित करना था, जिसमें दक्षिणी क्षेत्र गुजरात और केंद्रीय भाग मालवा को मिलना था। संयुक्त सेनाओं ने 1457 ई. में मेवाड़ पर हमला किया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं हुई।
| युद्ध | वर्ष | परिणाम |
| सारंगपुर का युद्ध | 1437 ई. | कुम्भा की जीत; विजयस्तम्भ के निर्माण से इसेस्मरणीय बनाया गया। |
| कुंभलगढ़ पर हमला | 1442-43 ई. | अनिर्णायक परिणाम। |
| गागरोन परहमला | 1444 ई. | महमूद खिलजी की जीत;अचल सिंह कुम्भा के सामंतबने। |
| मंडलगढ़ परहमले | 1446 ई. (दो हमले) और 1456 ई. | तीनों हमले अनिर्णायक रहे। |
| अजमेर परहमला | 1455 ई. | मेवाड़ के गवर्नर गजाधरसिंह को हराने के बाद इसेथोड़े समय के लिए मालवा नेनियंत्रित किया। |
कुम्भा और उनकी उपलब्धियाँ:
सैन्य और रणनीतिक कौशल:
- महाराणा कुम्भा ने एक ऐसा राज्य विरासत में पाया जो आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा था। हालांकि, उनके असाधारण सैन्य और रणनीतिक कौशल ने इन प्रतिकूलताओं को पार करने में मदद की।
- शासक के रूप में उनका पहला कार्य अपने पिता, महाराणा मोकल की हत्या का बदला लेना था। उन्होंने मेवाड़ में रणमल राठौड़ के प्रभाव को समाप्त किया और बाद में उन्हें खत्म कर दिया।
- “आवल-बावल संधि” के माध्यम से, जिसे हंसा बाई ने मध्यस्थता की, शांति स्थापित की गई।
- उन्होंने मालवा, गुजरात और नागौर के आक्रमणों से मेवाड़ की रक्षा की और उसकी संप्रभुता सुनिश्चित की। शुरुआत में चित्तौड़ तक सीमित, मेवाड़ का विस्तार उनके नेतृत्व में अबू, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, पोकरण, फलोदी और कांठल तक हुआ।
आवल-बावल संधि- 1453 : सीमा विवादों को सुलझाने और संबंधों को मजबूत करने के लिए मेवाड़ के राणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के बीच आंवल-बावल की संधि (1453 ई.) पर हस्ताक्षर किए गए थे। हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई इस संधि ने सोजत को केंद्रीय संदर्भ बिंदु बनाते हुए मारवाड़ और मेवाड़ के बीच सीमा स्थापित की। सीमा का निर्धारण क्षेत्र के पेड़ों के आधार पर किया गया था: खेजड़ी के पेड़ वाले क्षेत्र मारवाड़ के थे, जबकि आम के पेड़ वाले क्षेत्र मेवाड़ का हिस्सा थे। संधि में राव जोधा की बेटी, श्रृंगार देवी का कुंभा के बेटे, रायमल से विवाह भी शामिल था, जिससे गठबंधन और मजबूत हुआ।
वास्तुकला विरासत:
महाराणा कुम्भा, जिन्हें “राजस्थानी वास्तुकला के पिता” के रूप में जाना जाता है, ने मेवाड़ की वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेवाड़ के 82 किलों में से, उन्होंने 32 का निर्माण किया, जिनमें मुख्य वास्तुकार ‘शिल्पाचार्य’ मंडन और जैता थे।
- मेवाड़ की सीमाओं पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए कुम्भा ने आबू में अचलगढ़ और वसंतगढ़ किलों का निर्माण किया।
- गोड़वाड़ के पास की सीमाओं के लिए, कुम्भलगढ़ का शक्तिशाली किला और किले को घेरते हुए 36 किमी लंबी किले की दीवार का निर्माण किया गया। मेरों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मचान किले का निर्माण किया गया।
- उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले का भी पुनर्निर्माण किया, पूर्व दिशा के प्रवेश द्वार को बदला और पश्चिम दिशा में किले में प्रवेश के लिए 7 द्वारों का निर्माण किया।
- मंदिर वास्तुकला – कुम्भा के शासन में मेवाड़ की वास्तुकला ने मील के पत्थर प्राप्त किए, जिसमें चित्तौड़गढ़ किले में कुम्भ स्वामी मंदिर और शृंगार चवरी, अचलगढ़ में कुम्भ श्याम मंदिर, श्री एकलिंगनाथजी मंदिर का पुनर्निर्माण, नागदा में श्वेताम्बर जैन मंदिर और विष्णु मंदिर, कुम्भलगढ़ में मामादेव मंदिर और यज्ञवेदि, आबू में शांतिनाथ मंदिर, खतरगच्छ मंदिर, रणकपुर में चौमुखा मंदिर आदि शामिल हैं।
- मंदिरों और किलों के साथ-साथ कई तालाब और बावड़ियों का भी निर्माण किया गया। मालवा पर अपनी महाकाव्य जीत को याद करने के लिए, कुम्भा ने नौ मंजिला कीर्ति स्तम्भ या विजय स्तम्भ के निर्माण का आदेश दिया, जिसे ‘देवता मूर्ति कोष’ या मूर्तियों के संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है।
सांस्कृतिक संरक्षण :
- महाराणा कुम्भा केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान और कला व संस्कृति के प्रेमी भी थे।
- साहित्य : उन्होंने संगीत राज, सूड प्रबंध, और मेवाड़ी बोली में गीत गोविंद पर टीका जैसी उल्लेखनीय रचनाएं कीं। उनका दरबार प्रसिद्ध विद्वानों जैसे कान्हड़ व्यास (एकलिंग महात्म्य के लेखक), कवि मेहा (तीर्थमाला के लेखक), और अत्रि और महेश भट्ट (कीर्ति स्तम्भ प्रशस्ति के रचयिता) से सुसज्जित था।
- संगीत : उनकी रचनाएँ (संगीतराज, संगीत रत्नाकर, वाध्य प्रबंधक) और “कुम्भ मल्हार” की प्रस्तुति ने भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा को समृद्ध किया। उन्हें ‘अभिनव भरताचार्य’ और ‘वीणा वादन प्रवीण’ के रूप में जाना जाता है।
- नृत्य : उनकी पुस्तक नृत्य रत्न कोश अभिनय में विभिन्न मुद्राओं का विवरण प्रदान करती है, जो उनके नृत्य ज्ञान को वैध ठहराती है।
- चित्रकला : उन्हें राजस्थानी चित्रकला का पिता कहा जाता है। महाराणा कुम्भा के संरक्षण में, पंडित भीष्मचंद द्वारा ‘रसिकाष्टक’ और गोगुंदा में पंडित रमिश द्वारा ‘गीता गोविंद आख्यिका’ जैसी चित्रित ग्रंथों की रचना हुई। इस काल में, ‘सुपास नह चरियाँ’ ग्रंथ को चित्रित किया गया। चित्रकला से संबंधित विस्तृत जानकारी ‘राजवल्लभ मंडन’ से भी प्राप्त होती है जिसमें महलों और मंदिरों में सुंदर चित्र बनाने के निर्देश दिए गए थे। महाराणा कुम्भा के काल में, देलवाड़ा चित्रकला का केंद्र था।
आर्थिक विकास :
- कुम्भा के शासनकाल में मेवाड़ की अर्थव्यवस्था फली-फूली, जिसका समर्थन देलवाड़ा, आहड़, और नागदा जैसे व्यापारिक केंद्रों से हुआ।
- जावर में खनन गतिविधियों ने आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया।
- उनके सिक्के, मुख्य रूप से तांबे में, मेवाड़ की आर्थिक स्थिरता को दर्शाते हैं।
राणा सांगा / संग्राम सिंह (1508-1528)

- शासक बनने से पहले, राणा सांगा ने अपने भाइयों, पृथ्वीराज और जयमल के साथ संघर्ष के दौरान अपनी एक आंख खो दी और कुछ समय के लिए श्रीनगर (अजमेर) में करमचंद पवार के निवास पर निर्वासन में रहे।
- खतौली और बाडी का युद्ध (1518) – उनके नेतृत्व में, मेवाड़ की सीमाएं उनके सैन्य रणनीतियों और दूरदर्शिता के कारण मजबूत और विस्तारित हुईं। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने मेवाड़ के बढ़ते प्रभाव को सहन नहीं कर सका और उसके विस्तार को चुनौती दी। 1517 में, सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खतौली (बूंदी) के युद्ध में और 1518 में बाड़ी (धौलपुर) का युद्ध में हराया।
- गागरोन का युद्ध (1519) – राणा सांगा ने मेड़ता के राठौड़ों के साथ राव वीरमदेव के नेतृत्व में चित्तौड़ से एक बड़ी सेना के साथ सुल्तान महमूद खिलजी II के खिलाफ अग्रसर हुए, जो आसफ खान के नेतृत्व में गुजरात के सहायक सैनिकों के साथ थे। राजपूतों के उग्र आक्रमण के सामने सुल्तान की सेना टिक नहीं सकी और पूरी तरह से पराजित हो गई। राणा सांगा ने सुल्तान के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उसे उसका राज्य वापस कर दिया।
बाबर-सांगा संबंध :
- संघर्ष के कारण–
- बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी में सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि सांगा ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, जबकि आगरा पर हमले का वादा किया था, लेकिन यह आरोप असंभव प्रतीत होता है क्योंकि सांगा ने पहले ही दिल्ली के सुल्तान को दो बार हरा दिया था।
- उनकी महत्वाकांक्षाएं टकराई थीं, क्योंकि बाबर पूरे भारत को जीतना चाहता था, जिसके लिए उसे सांगा को हराना जरूरी था, जो एक प्रमुख “हिंदूपत” थे।
- राजपूत-अफगान गठबंधन बाबर के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा था, क्योंकि अफगान नेता हसन खान मेवाती और महमूद लोदी (इब्राहिम लोदी के भाई) पानीपत की हार के बाद सांगा के साथ शरण ली थी।
- सांगा ने पानीपत के बाद की अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सल्तनत क्षेत्रों जैसे खंडार किला (सवाई माधोपुर) और आसपास के 200 गांवों पर कब्जा कर लिया।
- बयाना का युद्ध – सांगा ने फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध में एक बड़ी जीत हासिल की, जहां बाबर के किले के संरक्षक मेहंदी ख्वाजा को हराया गया।
- खानवा का युद्ध (1527) – यह युद्ध 17 मार्च 1527 को खानवा गांव के पास लड़ी गई थी, जिसमें पहले मुगल सम्राट बाबर की आक्रमणकारी सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना के बीच हुई थी। बाबर की श्रेष्ठ नेतृत्व क्षमता, तोपखाने, और संगठित कौशल निर्णायक साबित हुए और राणा सांगा पराजित हो गए। इस जीत ने भारत में मुगल वंश के शासन को मजबूत किया।
- खानवा के युद्ध में सांगा की हार के कारण–
- बयाना में जीत के बाद, सांगा ने युद्ध करने में देरी की, जिससे बाबर को तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया।
- राजपूतों की पारंपरिक युद्ध रणनीति और हथियार बाबर के तोपखाने और तुर्क शैली की युद्ध तकनीकों के सामने कम प्रभावी साबित हुए।
- सांगा की चोट और युद्ध क्षेत्र से उनकी वापसी ने राजपूत सेनाओं का मनोबल गिरा दिया।
- राजपूत नेतृत्व में एकता की कमी, क्योंकि सेना विभिन्न सरदारों के द्वारा चलाई जा रही थी, जिससे समन्वय प्रभावित हुआ।
- रायसेन के सलहदी तंवर और नागौर के ख़ानजादा का युद्ध के अंतिम चरण में बाबर से मिल जाना।
राणा की व्यक्तित्व की समीक्षा–
राणा सांगा को भारत के अंतिम महान हिंदू शासक के रूप में याद किया जाता है, जिनके नेतृत्व ने सभी राजपूत गुटों को विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट किया। अपने देश की रक्षा में उनके वीर प्रयासों ने उन्हें शारीरिक रूप से विकलांग कर दिया—उन्होंने एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो दिया, और उनके शरीर पर 80 तलवारों के घाव थे। बाबर ने उन्हें एक डरावना शासक बताया। उनकी आर्थिक स्थिरता एवं उदारता उनके शासन के दौरान जारी भूमि अनुदानों जो कि कुंभलगढ़ के नीलकंठ (मामादेव) मंदिर और डोवनी तांबे की पट्टिका के अभिलेखों से ज्ञात होती है। इसके अलावा, उन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए, जिन्हें संग्राम साही सिक्कों के नाम से जाना जाता है, जो उनके शासनकाल के दौरान लोकप्रिय हो गए। यदि उनके उत्तराधिकारी उतने ही सक्षम होते, तो मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित नहीं हो सकता था। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने उन्हें “एक सैनिक का अवशेष” कहा, जो उनके शारीरिक घावों को देखते हुए था, जिससे उनकी वीरता को और भी मजबूत किया गया। राणा सांगा का निस्वार्थता और अपने देश के प्रति समर्पण तब स्पष्ट हुआ जब, महमूद खिलजी को पकड़ने की खुशी में, उन्होंने चित्तौड़गढ़ के पूरे राज्य को कवि चारण हरिदास को दे दिया, हालांकि हरिदास ने केवल 12 गांवों को इनाम के रूप में चुना। राणा सांगा का नाम बलिदान, साहस और त्याग के प्रतीक के रूप में अमर है।
विक्रमादित्य सिंह (1531–1536)
- उनके शासनकाल के दौरान, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1534 में चित्तौड़ पर हमला किया, और उदय सिंह को सुरक्षा के लिए बूंदी भेजा गया।
- राणा सांगा की पत्नी कर्णावती ने हुमायूँ को राखी भेजी। लेकिन हुमायूँ देर से आया – चित्तौड़ का दूसरा जौहर (1535)
- केसरिया – देवालिया ठाकुर बाघ सिंह
- जौहर – रानी कर्मवती
- बहादुर शाह 1526 में गुजरात के सुल्तान बने और 1531 में मालवा और 1532 में रायसेन पर कब्जा करके अपना शासन विस्तार किया। फिर उन्होंने चित्तौड़ किले की घेराबंदी की। रानी कर्णावती ने मदद के लिए हुमायूँ से अपील की और उन्हें राखी भेजी। हुमायूँ ने स्वीकार कर लिया लेकिन समय पर नहीं पहुंच सके। युवा उदय सिंह की रक्षा के लिए उन्हें बूंदी भेजा गया। 8 मार्च 1535 को, रानी कर्णावती और 13,000 महिलाओं ने जौहर किया, जबकि राजपूत सेना ने बहादुर शाह की सेना के खिलाफ अंतिम साका लड़ा। यह चित्तौड़ के तीन ऐतिहासिक जौहरों में से दूसरा था।
उदय सिंह द्वितीय (1540–1572)
- 1540 में, मेवाड़ के सामंतों द्वारा कुंभलगढ़ में उन्हें महाराणा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। उसी वर्ष (9 मई 1540) महाराणा प्रताप का जन्म हुआ।
- 1562 में, उन्होंने मालवा के बाज बहादुर को शरण दी। इस बहाने, अकबर ने अक्टूबर 1563 में मेवाड़ पर हमला किया। उदय सिंह गोगुन्दा की तरफ़ चल गये हुए।
- राव जयमल और पत्ता – वीरता के साथ लड़े – यहाँ तक कि अकबर भी प्रभावित हुआ – फतेहपुर सीकरी में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई।
- जौहर – चित्तौड़ का तीसरा जौहर (1567)
- केसरिया – जयमल-फत्ता के नेतृत्व में
- जौहर – रानी फूल कंवर के नेतृत्व में
- 1556-66 के बीच, मुगलों का ध्यान मारवाड़ पर केंद्रित रहा, जिससे मेवाड़ के उदय सिंह द्वितीय ने शक्ति को मजबूत किया। 1562 में, जयमल को अकबर ने मेड़ता से बाहर कर दिया जिसे मेवाड़ में शरण दी गई, जहाँ उन्हें बदनौर की जागीर दी गई। अकबर द्वारा पराजित बाज बहादुर ने भी मेवाड़ में शरण मांगी, जिससे सम्राट नाराज हो गया। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी की, जिससे उदय सिंह को भागना पड़ा और जयमल को प्रभार छोड़ना पड़ा। 58 दिनों की घेराबंदी के बाद, राजपूतों ने केसरिया किया और वीरता से लड़े लेकिन अंततः मुगल सेना द्वारा मारे गए।
- उदयपुर शहर की स्थापना की। यह आगे चलकर मेवाड़ की राजधानी बन गई।

महाराणा प्रताप (9 मई 1540 – 29 जनवरी 1597)
हल्दीघाटी का युद्ध – 1576
- हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तकनीकी रूप से मुगलों ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन यह व्यर्थ था क्योंकि वे प्रताप को पकड़ने में विफल रहे, जो युद्ध जारी रख सके और अधिकांश खोए हुए क्षेत्रों को वापस लेने में सक्षम रहे। कर्नल टॉड ने इसे ग्रीस की प्रसिद्ध ‘थर्मोपल्ली का युद्ध’ से तुलना की और इसे ‘मेवाड़ की ‘थर्मोपल्ली कहा।
- पृष्ठभूमि – 1567 की चित्तौड़ की घेराबंदी में हारने के बाद, उदय सिंह राजपीपली के जंगलों में चले गए। 1572 में उनकी मृत्यु के बाद, एक संक्षिप्त उत्तराधिकार संघर्ष के बाद, महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। अकबर ने प्रताप को मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए कई दूत भेजे, जिनमें जलाल खान कुरची, मान सिंह, राजा भगवंत दास, और टोडरमल शामिल थे। जब कूटनीति विफल हो गई, तो युद्ध अनिवार्य हो गया।
- युद्ध – अकबर ने मुगल सेनाओं का नेतृत्व करने के लिए राजा मान सिंह को नियुक्त किया, जिन्होंने मंडलगढ़ में अपना बेस स्थापित किया। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी के पास युद्ध शुरू हुआ, जो गोगुन्दा से 23 किमी उत्तर में है। महाराणा प्रताप की सेना, जिसमें हकीम खान सूर, भीम सिंह डोडिया, रामदास राठौर (जयमल के पुत्र), और झाला कबीले के बीदा माणा शामिल थे, ने बड़ी मुगल सेना का सामना किया। अपनी वीरता के बावजूद, प्रताप की सेना हार गई। प्रताप कोलियारि चले गए, जो गोगुन्दा के पश्चिम में एक पहाड़ी नगर था, और अपनी प्रतिरोध जारी रखा।
- परिणाम – मुगलों ने गोगुन्दा, कुंभलगढ़ और उदयपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में स्वतंत्र रहने के लिए दृढ़ थे। 1579 तक, मुगलों का ध्यान कहीं और केंद्रित हो गया था, जिससे प्रताप ने अपने पश्चिमी क्षेत्रों का अधिकांश हिस्सा वापस ले लिया। हालाँकि, चित्तौड़ मुगल नियंत्रण में रहा। शाहबाज खान के अभियानों – हल्दीघाटी के बाद, अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए तीन बार (1577-79 ईस्वी) शाहबाज खान को भेजा। कुंभलगढ़ पर कब्जा करने के बावजूद, वह असफल रहा। 1580 ईस्वी में, अब्दुल रहीम खान-ए-खाना ने भी कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे।
दिवेर का युद्ध –
- 1582 – 1582 में दशहरा (विजयदशमी) के दौरान, महाराणा प्रताप ने दिवेर पर हमला किया, जिससे मेवाड़ को महत्वपूर्ण जीत मिली।
- पृष्ठभूमि – हल्दीघाटी के युद्ध के बाद, महाराणा प्रताप के पास केवल 7,000 सैनिक बचे थे। उन्होंने एक नई युद्ध नीति अपनाई, जिससे मुगल सेनाओं को मेवाड़ में बसने से रोका जा सके। अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए छह बड़े सैन्य अभियान भेजे, लेकिन सभी विफल रहे।
- युद्ध – मेवाड़ की सेना को दो समूहों में विभाजित किया गया था: एक महाराणा प्रताप के नेतृत्व में और दूसरा कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में। निर्णायक युद्ध में, मुगलों को हराया गया, और उनके सैनिक भाग गए। लगभग 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इस जीत ने मेवाड़ में सभी 36 मुगल चौकियों को बंद कर दिया। कर्नल टॉड ने हल्दीघाटी से दिवेर तक महाराणा प्रताप के युद्ध की तुलना प्रसिद्ध ग्रीक युद्धों से की, हल्दीघाटी को “मेवाड़ की थर्मोपल्ली” और दिवेर को “मेवाड़ की मैराथन” कहा, प्रताप के वीरता और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की।
- परिणाम – महाराणा प्रताप ने एक निर्णायक विजय प्राप्त की, जिससे मेवाड़ में मुगल प्रभाव स्थायी रूप से समाप्त हो गया। उन्होंने लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया, केवल चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़कर। चावंड मेवाड़ की नई राजधानी बन गई, जिसने कला और संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित किया।
प्रताप की नई युद्ध नीति रक्षात्मक रणनीति
- रक्षात्मक रणनीति: मुगल नियंत्रण को रोकने और मेवाड़ के संसाधनों की रक्षा करने का लक्ष्य था।
- पहाड़ के किले: दुश्मन की घुसपैठ को रोकने या उनके प्रवेश पर नुकसान पहुँचाने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों को सुदृढ़ किया गया।
- भीलों का समर्थन: भील जासूस और संदेशवाहक के रूप में कार्य करते थे।
- सुरक्षित संसाधन: खजाना, हथियार, और भोजन पहाड़ी गुफाओं में संग्रहीत किए गए।
- गुरिल्ला युद्ध: हल्दीघाटी के बाद हिट-एंड-रन रणनीति का इस्तेमाल किया।
- दुश्मन के संसाधनों का विनाश: विनाश की नीति के साथ मुगलों को परेशान किया।
- चावंड में राजधानी: चावंड, एक सुरक्षित, कठिन पहुँच वाले स्थान पर स्थानांतरित की गई।
महाराणा प्रताप: एक बहुआयामी व्यक्तित्व –
महाराणा प्रताप, जिन्हें मेवाड़ केसरी और हिंदु सूरज के रूप में पूजा जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों में से एक हैं। उन्होंने अपने लोगों के कल्याण और गर्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अपराजेय साहस और दृढ़ता के लिए जाने जाने वाले महाराणा प्रताप न केवल एक अद्वितीय योद्धा थे, बल्कि कला, संस्कृति और वास्तुकला के संरक्षक भी थे। इन क्षेत्रों में उनके योगदान निम्नलिखित हैं: सैन्य कौशल: महाराणा प्रताप की सैन्य प्रतिभा उनके गुरिल्ला युद्ध कौशल, किलेबंदी, और रक्षा रणनीतियों में स्पष्ट थी। उनकी सेना अकबर की सेना की तुलना में छोटी और कम सुसज्जित होने के बावजूद, प्रताप ने अरावली पहाड़ियों के भूगोल का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, वर्षों तक मेवाड़ की स्वतंत्रता बनाए रखी। उनके अतुलनीय साहस और असाधारण नेतृत्व कौशल ने उन्हें कर्नल टॉड से ‘राजस्थान के लियोनिडास’ की उपाधि दिलाई।
- साहित्य और बौद्धिक योगदान: उनके दरबार में पंडित चक्रपाणि मिश्र (चार प्रमुख कार्य: विश्ववल्लभ, मुहूर्त माला, व्यवहारदर्शन, और राज्याभिषेक पद्धति), जैन मुनि हेमरत्न सूरी (गोरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई, महिपाल चौपाई) और चारण कवि दुरसा आढ़ा ने विरुद्ध छतहरी की रचना की। माला सांदू और रामसा सांदू जैसे कवियों ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- वास्तुकला विकास: मंदिरों और किलेबंदी का निर्माण। बडारण में हरिहर मंदिर और चावंड का चावंडा देवी मंदिर उनकी धार्मिक वास्तुकला के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। 1585 में लूणा चांवडिया को हराने के बाद, प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया, जो नगर नियोजन के एकशीतिपद वास्तु सिद्धांतों का पालन करता था (बस्तियों के केंद्र में खुले आंगन)।
- कला और सांस्कृतिक विकास: महाराणा प्रताप के शासनकाल को सांस्कृतिक दृढ़ता और रचनात्मक संरक्षण के लिए जाना जाता था। उन्होंने चावंड शैली की पेंटिंग की शुरुआत की, जिसमें प्रसिद्ध चित्रकार निसारुद्दीन ने छह राग और छत्तीस रागिनी चित्रों का निर्माण किया।
अमर सिंह प्रथम (1597-1620)
- महाराणा प्रताप के निधन के बाद, अकबर और जहांगीर को अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का एक और मौका मिला और उन्होंने क्रमशः 1599, 1605 और 1613 ईस्वी में (पांच बार) उदयपुर पर हमला किया। महाराणा अमर सिंह ने उंटाला के युद्ध में जहांगीर की सेना को पराजित किया।
दूसरा दिवेर का युद्ध – 1606 –
- राणा अमर सिंह ने सुल्तान खान को हराया और मार डाला। मुगल राजकुमार मोहम्मद परवेज अपने कमांडर आसिफ खान के साथ युद्धक्षेत्र से भाग गए।
- युद्ध- जहांगीर ने राजकुमार परवेज और आसिफ खान को 80,000 घुड़सवार सेना के साथ भेजा। मुगल सेना का नेतृत्व सुल्तान खान कर रहे थे। अमर सिंह ने बहादुरी से लड़ते हुए सुल्तान खान को मार गिराया। मुगल सेना शर्मनाक रूप से पराजित हुई और अजमेर की ओर भाग गई।
- परिणाम- दिवेर में मुगलों की हार के बावजूद जहांगीर डटा रहा। 1608 में, उसने महाबत खान को एक और सेना के साथ भेजा। जबकि मुगलों ने विजय का दावा किया, वे जमीन की वास्तविकता को महत्वपूर्ण रूप से बदलने में असफल रहे। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद, अमर सिंह ने 17 प्रमुख युद्ध लड़े। जहांगीर ने बाद में राजकुमार खुर्रम (शाहजहां) के अधीन एक और बड़ी सेना भेजी। अमर सिंह और उनके पुत्र करण सिंह, अपने साहसी प्रयासों के बावजूद, मुगलों की प्रबल शक्ति का सामना नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप मेवाड़ में भारी जन और संपत्ति की हानि हुई। अंततः 1615 ईस्वी में, अमर सिंह ने जहांगीर की तरफ़ से आए शाहजहां के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए।
Amar Singh I (1597-1620)
- After the demise of Maharana Pratap, Akbar and Jahangir got another chance to fulfil his ambition and attacked Udaipur in 1599, 1605 AD and 1613 AD (five times) respectively. Maharana Amar Singh defeated Jahangir’s army in the battle of Untala.
मुगल-मेवाड़ संधि 5 फरवरी, 1615
- राणा कभी भी मुगल शाही दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। हालांकि, राणा के सबसे बड़े पुत्र, कुंवर करण, दरबार में शामिल होंगे और उन्हें पांच हजार (मंसब) का पद मिलेगा।
- राणा को मुगल सेवा में सूचीबद्ध किया जाएगा, लेकिन उनकी दरबार में उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।
- राणा एक हजार घुड़सवार मुगल सेवा में प्रदान करेंगे।
- चित्तौड़ किले को राणा को लौटाया जाएगा लेकिन उसे मरम्मत करने की अनुमति नहीं होगी।
- राणा को वैवाहिक गठबंधन स्थापित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
राज सिंह प्रथम (1652-1680)
- मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार संकट के दौरान, राजकुमार औरंगजेब ने राजकुमार दारा शिकोह के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल की।
- महाराणा राज सिंह ने दारा के सहायता के आह्वान का जवाब देने से चतुराई से इनकार कर दिया और अपने राज्य को मजबूत करने में बुद्धिमानी दिखाई। मुगलों के साथ युद्ध में तटस्थ रहने के परिणामस्वरूप मेवाड़ के लिए व्यापक क्षेत्रीय लाभ हुए।
- औरंगजेब के सम्राट बनने के बाद, उसकी हिंदू विरोधी नीतियाँ इतनी कठोर हो गईं कि महाराणा इसका विरोध किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने अपने पिता की तरह चित्तौड़ किले की मरम्मत करके मुगलों के साथ संधि का उल्लंघन जारी रखा।
- 1660 ईस्वी में, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की घटना से औरंगजेब नाराज हो गया। 1669 ईस्वी में, कट्टर औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों और शैक्षिक संस्थानों को नष्ट करने का आदेश दिया और जजिया पुनः लागू किया, जिसका महाराणा ने खुलेआम विरोध किया। हालांकि, जब महाराणा ने जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह को शरण दी, तो औरंगजेब ने अंततः 1679 ईस्वी में मेवाड़ पर हमला किया।
चारुमती की घटना
1658 में, किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की मृत्यु के बाद, मानसिंह शासक बने। औरंगजेब ने मानसिंह की बहन चारुमती से विवाह करने की इच्छा जताई। हालांकि, चारुमती औरंगजेब से विवाह करने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने राज सिंह को लिखा, “एक हंस बगुलों के बीच नहीं रह सकता। मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती; कृपया मेरे धर्म की रक्षा करें और मुझसे विवाह करें।”
उनकी विनती के जवाब में, राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया। जब औरंगजेब को यह पता चला, तो उसने देओली के रावत हरि सिंह के माध्यम से यह खबर पाई, और उसने ग्यासपुर और बासावर को उदयपुर से अलग कर दिया और उन्हें हरि सिंह को उपहार स्वरूप दिया। इस घटना ने औरंगजेब और राज सिंह के बीच शत्रुता के बीज बो दिए।
हाड़ी रानी की कहानी
हाड़ी रानी, जिनका असली नाम सहल कंवर था, बूंदी के सामंत संग्राम सिंह की पुत्री थीं। उन्होंने सलूम्बर के राव रतन सिंह चुंडावत से विवाह किया। विवाह के एक दिन बाद ही, महाराणा राज सिंह ने रतन सिंह को औरंगजेब के खिलाफ देवासुरी दर्रे के युद्ध में भाग लेने के लिए बुलाया। युद्ध की तैयारी करते हुए, रतन सिंह, अपनी नवविवाहित पत्नी के लिए तड़पते हुए, एक सेवक को उनके पास भेजा, जिससे उन्होंने एक स्मृति चिह्न की मांग की। हाड़ी रानी ने साहसिकता का अनूठा प्रदर्शन करते हुए, अपनी कटी हुई सिर को एक प्रेम-स्मृति के रूप में भेजा। रतन सिंह, उनकी बहादुरी से प्रेरित होकर, वीरता से लड़े लेकिन युद्ध में मारे गए। इस अद्वितीय बलिदान को मेघराज ‘मुकुल’ की कविता “सैनानी” में अमर कर दिया गया है, जो हाड़ी रानी की वीरता को सम्मानित करती है:
“चुंडावत मांगी सैनानी, सिर काट दे दीयो क्षत्राणी”
राज सिंह: एक उदार शासक –
राज सिंह ने अपने प्रजा में सैन्य और नैतिक गुणों को बढ़ावा देने के लिए विजय कटकटु का खिताब अर्जित किया। उनके शासनकाल ने कल्याण और सांस्कृतिक प्रगति के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाया।
वास्तुकला में योगदान –
उनकी पत्नी, रामरसदे, ने उदयपुर में जया बावड़ी (त्रिमुखी बावड़ी) का निर्माण किया। सूखे की समस्याओं का समाधान करने के लिए, राजा सिंह ने गोमती नदी को बांध कर राजसमंद झील का निर्माण किया। इसके उत्तरी तट पर, राज प्रशस्ति स्थापित की गई। यह 25 काले संगमरमर की पट्टियों पर उकेरी गई है, जो मेवाड़ के इतिहास का दस्तावेज है, जिसमें 1615 की मुगल-मेवाड़ संधि और शासकों की तकनीकी कुशलताएँ शामिल हैं। सिंचाई से जुड़े कार्यों के कारण उन्हें राजस्थान का ‘हाइड्रोलिक शासक’ कहा जाता है।
धार्मिक संरक्षण
- 1669-70 में, राजा सिंह ने मथुरा से श्रीनाथजी और द्वारकाधीश की मूर्तियों को बचाया, जो औरंगजेब के उत्पीड़न के तहत खतरे में थे। उन्होंने श्रीनाथजी को सीहाड़ (आधुनिक नाथद्वारा) और द्वारकाधीश को कांकरोली (राजसमंद) में स्थापित किया। उन्होंने उदयपुर के अंबिका माता मंदिर को पुनर्जीवित किया। उन्होंने हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर का विरोध भी किया।
शहरी विकास
- राज सिंह ने राजसमंद झील के पास राजनगर शहर की स्थापना की और सर्वऋतु विलास और जनासागर जैसी संरचनाओं का निर्माण किया।
साहित्यिक विकास
- उन्होंने संस्कृत, हिंदी, और राजस्थानी विद्वानों को संरक्षण दिया, जिनमें प्रमुख हैं रणछोड़ भट्ट और सदाशिव।
- उनका शासन सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचे और धार्मिक संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाला था, जिससे मेवाड़ के इतिहास में एक स्थायी विरासत बनी।
अमर सिंह द्वितीय (1698–1710) –
- महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान शाहजादा मुअज्ज़म का समर्थन किया और उनके सम्राट बहादुर शाह प्रथम के रूप में सिंहासन पर बैठने के बाद भी उनसे सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे।
- महाराणा ने जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय और जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह को उनके राज्यों की पुनः प्राप्ति में सहायता प्रदान की तथा मुगलों की उन रणनीतियों का विरोध किया, जिनके माध्यम से वे इन शासकों को उनकी ही भूमि से दूर रखना चाहते थे।
- मेवाड़ सेना, सांवलदास के नेतृत्व में, महाराणा द्वारा जयपुर और जोधपुर की सहायता के लिए भेजी गई थी ताकि वे मुगल सत्ता के विरुद्ध संघर्ष कर सकें।
देबारी संधि, 1707
- यह संधि देबारी, उदयपुर में आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बीच संपन्न हुई।
- इसका मुख्य उद्देश्य सवाई जय सिंह को आमेर के सिंहासन पर पुनः स्थापित करना था।
- संधि के एक भाग के रूप में, जय सिंह का विवाह मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवरी से तय हुआ, जिसमें यह शर्त रखी गई कि उनका पुत्र आमेर का अगला शासक बनेगा।
महाराणा जगत सिंह
- उनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना हुरड़ा सम्मेलन थी।
हुरड़ा सम्मेलन
- स्थान – भीलवाड़ा
- समय – 17 जुलाई 1734 ई.
- अध्यक्ष – जगत सिंह द्वितीय (मेवाड़)
- आयोजक/नेता – सवाई जय सिंह (आमेर)
- उद्देश्य – मराठों के आक्रमणों के विरुद्ध राजपूत शासकों को एकजुट करना।
- इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि सभी राजा एक-दूसरे की सहायता करेंगे और वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद रामपुर (कोटा) में एकत्र होकर मराठों के विरुद्ध युद्ध करेंगे।
- परिणाम – यह व्यक्तिगत मतभेदों के कारण असफल रहा, लेकिन खानवा के युद्ध के बाद पहली बार राजपूतों ने विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संगठित होने का प्रयास किया। इस सम्मेलन के कारण मराठों के आक्रमण राजस्थान पर और बढ़ गए।
महाराणा भीम सिंह (1778 – 1828 ई.)
- उनके शासनकाल में मेवाड़ की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बिगड़ गई थी, जिसका सबसे शर्मनाक परिणाम कृष्णा कुमारी विवाद था।
कृष्णा कुमारी विवाद
कृष्णा कुमारी विवाद मेवाड़ की अत्यंत दुःखद घटनाओं में से एक है। कृष्णा कुमारी, महाराणा भीम सिंह की 16 वर्षीय पुत्री, प्रारंभ में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह से विवाह के लिए वचनबद्ध थी। हालांकि, विवाह से पहले ही महाराजा की मृत्यु हो गई और विवाह का प्रस्ताव जयपुर के महाराजा जगत सिंह को दे दिया गया।
इस बदलाव से जोधपुर के नए शासक महाराजा मान सिंह क्रोधित हो गए और उन्होंने इस निर्णय का विरोध किया। मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध परबतसर के निकट हुआ, जिसमें मान सिंह ने पिंडारी नेता अमीर खान को बुलाया, जिसने सभी पक्षों को लूटा। इसके बाद, अमीर खान ने महाराणा भीम सिंह को धमकी दी कि वे या तो कृष्णा कुमारी का विवाह महाराजा मान सिंह से करा दें या उसे मार दें। दबाव में आकर, महाराणा ने अनिच्छा से यह आदेश दिया कि कृष्णा कुमारी को मार दिया जाए। दौलत सिंह, जिन्हें यह कार्य सौंपा गया, ने इसे हत्या मानते हुए आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद यह कार्य महाराणा के पुत्र जवान दास को सौंपा गया, जिन्होंने भी भावनात्मक रूप से झिझक दिखाई।
अंततः, कृष्णा कुमारी को विष पिलाया गया, और जब कई बार विष देने के बावजूद वह नहीं मरी, तो उसे जबरन अफीम खिलाकर मार दिया गया।
- गिंगोली का युद्ध (1807) – गिंगोली (परबतसर) का युद्ध जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के मान सिंह के बीच हुआ था। इस युद्ध का कारण मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर संघर्ष था।
- परिणाम – इस युद्ध में जगत सिंह द्वितीय ने विजय प्राप्त की।
- ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि (1818) – 1818 में, महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे मेवाड़ अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी नियंत्रण में आ गया।
महाराणा स्वरूप सिंह (1842-1861 CE)
- वे 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ के महाराणा थे।
- उन्होंने ‘स्वरूप शाही’ सिक्के जारी किए ताकि नकली मुद्रा के कारण व्यापार में आई बाधा को दूर किया जा सके।
- उन्होंने अपने शासनकाल में बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुए विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण कराया।
- समाज सुधार कार्य
- 1844 में बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया।
- 1853 में डाकन प्रथा को समाप्त किया।
- 15 अगस्त 1861 को सती प्रथा पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगाया।
- समाधि प्रथा को समाप्त कर मानव जीवन की रक्षा सुनिश्चित की।
बामनी डाक प्रणाली
मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल के दौरान पेश किया गया। इस प्रणाली के तहत, ब्राह्मण समुदाय के सदस्यों को वार्षिक अनुबंध के आधार पर डाक जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं। ब्राह्मणों को चुनने का कारण यह था, कि समाज में उनका सम्मान किया जाता था और उन्हें पवित्र माना जाता था। उन्हें नुकसान पहुँचाना या लूटना पाप माना जाता था। बाद में इस व्यवस्था को आम जनता के लिए भी लागू कर दिया गया।
महाराणा शंभु सिंह (1861–1874 ई.)
- महाराणा स्वरूप सिंह के दत्तक पुत्र थे।
- उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा हेतु विद्यालय स्थापित किया।
- सती प्रथा को समाप्त करने के लिए विशेष उपाय लागू किए।
सज्जन सिंह (1874-1884 ई.)
बागोर के महाराज शक्ति सिंह के पुत्र महाराजा सज्जन सिंह को महाराणा शंभू सिंह ने गोद लिया था। वह एक दूरदर्शी शासक था जो अपने लोगों के कल्याण और अपने राज्य की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध था। उनके शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देखा गया:
- प्रशासनिक सुधार :
- उन्होंने शैलकांतर सम्बन्धिनी सभा का गठन किया, जिसका नेतृत्व स्वयं किया और परगनों के लिए बजट प्रणाली शुरू की।
- महेंद्रराज सभा की स्थापना की, जिसने न्यायिक और राजस्व मामलों में निर्णय लेने का कार्य किया।
- मेवाड़ पुलिस बल की स्थापना कर अपराधों को नियंत्रित किया।
- उन्होंने मेवाड़ की पहली जनगणना कराई, जिससे प्रशासनिक योजना में सुधार हुआ।
- समाज कल्याण :
- सड़कों का सुधार, लाइटें लगवाना, वृक्षारोपण और स्वच्छता विभाग की स्थापना।
- अतिक्रमण रोकने के लिए नगर नियोजन कानून लागू किए।
- सज्जन निवास बाग (गुलाब बाग) और उदयपुर का पहला चिड़ियाघर बनवाया।
- जल संसाधन विभाग की स्थापना की, झीलों की मरम्मत करवाई और उदयसागर व राजसमंद से नहरें बनवाईं।
- चित्तौड़-उदयपुर रेलवे योजना बनाई, जिसे महाराणा फतेह सिंह ने पूरा किया।
- सज्जन अस्पताल और वॉल्टर जनाना अस्पताल की स्थापना की।
- गौशाला, अनाथालय और मानसिक चिकित्सालय की स्थापना की।
- भूमि सुधार:
- भूमि राजस्व निपटान प्रणाली लागू की, जिसमें सटीक माप और आवंटन की प्रक्रिया अपनाई गई।
- इस कार्य के लिए विंगेट महोदय को नियुक्त किया गया।
- शैक्षिक एवं साहित्यिक कार्य :
- राज्य में नौ विद्यालय खोले और भूमि राजस्व का एक भाग शिक्षा के लिए आवंटित किया।
- अपने गुरु जनी बिहारीलाल से प्रेरित होकर मेवाड़ के पहले इतिहास विभाग की स्थापना की, जिसके प्रमुख कविराज श्यामलदास बने।
- साहित्यक रचना :
- उनके दरबार में उजाल फतेहकरण और बारहठ किशन सिंह जैसे विद्वानों और कवियों को संरक्षण मिला।
- उन्होंने सज्जन यंत्रालय मुद्रणालय की स्थापना की, जिसमें सज्जन कीर्ति सुधारक पत्रिका प्रकाशित होती थी।
- सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय की स्थापना की, जिससे ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण किया गया।
फ़तेह सिंह (1884-1930 ई.)
- भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्ज़न ने 1 जनवरी 1903 को लंदन में सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के अवसर पर दिल्ली में एक राजकीय दरबार का आयोजन किया।
- इस अवसर पर महाराणा फतेह सिंह को भी दिल्ली जाकर वायसराय के दरबार में उपस्थित होना था।
- प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहठ ने इसे मेवाड़ की गरिमा एवं शौर्य के विरुद्ध समझा एवं डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखे और महाराणा को भेजे। ये सोरठे ‘चेतावनी रा चूंगटिया’ नाम से प्रसिद्ध हुए।
- महाराणा ने बारहठ के सोरठे पढ़ने के बाद, दिल्ली पहुंचने के बावजूद भी दरबार में भाग नहीं लिया।
- कल्याणकारी कार्य :
- 1889 ई. में, वॉल्टर कृत राजपूत हितकारनी सभा की स्थापना की जिसका प्रमुख उद्देश्य राजपूत समुदाय में सामाजिक सुधार करना था।
- भू राजस्व बंदोबस्त का कार्य जो महाराणा सज्जन सिंह के समय शुरू हुआ था महाराणा फतेह सिंह के शासन में पूरा हुआ।
- राज्य में सड़कें और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाया गया तथा टेलीग्राफ सेवाएँ शुरू की गईं
- मेवाड़ रिसाला की स्थापना जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मेवाड़ लांसर्स में परिवर्तित किया गया ।
- 1889 में देवली झील पर कनॉट बांध का निर्माण करवाया जिससे झील का विस्तार हुआ और इसे बाद में फतेह सागर झील नाम दिया गया
महाराणा भूपाल सिंह 1930–1947 ई
- उनके शासनकाल में बिजौलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण जैसी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं।
- उन्होंने 18 अप्रैल 1948 को अपने राज्य का राजस्थान संघ में विलय कर दिया
- प्रमुख कार्य :
- उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि ली और राणा प्रताप हिंदी विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ कृषि महाविद्यालय महाराणा भूपाल नोबल्स स्कूल और कॉलेज की स्थापना की।
- उनके शासनकाल में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया एवं भूपाल सागर बांध का निर्माण करवाया गया। उन्होंने गन्ने की खेती को प्रोत्साहित किया और चित्तौड़गढ़ के निकट एक चीनी मिल स्थापित की। उन्हीं के समय में एक विशेष खनन विभाग की स्थापना की गई।
- एक पर्यावरणविद् के रूप में उन्होंने अरावली में दीर्घकालिक वनीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया
कछवाहा राजवंश
टी.एच. हेंडले के अनुसार कछवाहा वंश के बारे में माना जाता है कि प्रारंभिक काल में उन्होंने वर्तमान बिहार में सोन नदी के किनारे रोहतास (रहाटस) में निवास किया। वे यह भी उल्लेख करते हैं कि उनके प्रमुख सत्ता केंद्र वर्तमान मध्य प्रदेश में थे, जिनमें कुतवार, ग्वालियर, डुबखंड, सिंहपानिया और नरवर (नलपुरा) शामिल हैं। इस दूसरी पश्चिमी दिशा में मध्य प्रदेश की ओर प्रव्रजन की शुरुआत राजा नल के नेतृत्व में मानी जाती है, जिन्हें नरवर का पौराणिक संस्थापक कहा जाता है।
रूडोल्फ होर्नले (1905) के अनुसार कछवाहा वंश गुर्जर-प्रतिहारों से संबंधित है। वे बताते हैं कि कन्नौज के मध्य 10वीं शताब्दी के शासकों की वंशावली और ग्वालियर के आठ कछवाहा शासकों की वंशावली (महिपाल के सास-बाहू शिलालेख के आधार पर) में समानता पाई जाती है।
इतिहासकारों के अनुसार, कच्छपघात वंश की उत्पत्ति चंदेलों और परमारों की तरह क्षेत्र की पूर्ववर्ती शक्तियों के जागीरदारों के रूप में हुई थी। उनके अनुसार 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज (हर्ष के साम्राज्य के विघटन के बाद क्षेत्रीय सत्ता का केंद्र) के पतन के बाद ही कच्छपघाट राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश के चंबल घाटी में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। पुरातात्विक प्रमाण भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। मध्य प्रदेश में खोजे गए कच्छपघात काल के सिक्के, जो गुप्तकालीन ढंग से ढाले गए थे, और गोपाक्षेत्र शिलालेख इस दृष्टिकोण को प्रमाणित करते हैं।
दौसा के कछवाहा शासक
मध्ययुगीन काल के दौरान, 10वीं शताब्दी ईस्वी में चौहानों और बड़गुर्जरों ने इस भूमि पर शासन किया था। दौसा शहर तब प्रसिद्ध हुआ जब यह ढूंढाड़ की पहली राजधानी बन गया। 1006 ई. में कच्छवाहा राजपूत राजा दुल्हे राय ने इस क्षेत्र को गुर्जर-प्रतिहारों और मीणा के नियंत्रण से छीन लिया था। दूल्हे राय द्वारा बसाए गए इस यह दौसा से ही बाद में आमेर एवं जयपुर राजवंश की उत्पत्ति होती है।
धोला राय, दौसा के राजा (1006-1036)
- 1006 ई. में राजा धोला राय का विवाह अजमेर के राजा रल्हण सिंह चौहान की पुत्री से हुआ, जिसके साथ ढूँढाड़ क्षेत्र उन्हें दहेज के रूप में प्राप्त हुआ।
- राजा धोला राय ने बड़ गुर्जर राजपूतों को ढूँढाड़ से निष्कासित किया और मीणाओं से गठबंधन किया। उन्होंने मीणाओं को उनकी पारंपरिक रीति-रिवाजों को बनाए रखने का आश्वासन दिया, उन्हें जागीरें प्रदान कीं और किलेदार के रूप में नियुक्त किया।
राजा कोकिल देव (1036 से 1038)
- राजा कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को पराजित किया, खोह, झोटवाड़ा और गेटोर को अपने राज्य में मिलाया, और इसे अपनी राजधानी बनाया।
- उन्होंने यादवों से मेड़ और बैराठ को भी जीत लिया।
- आमेर कछवाहा वंश की राजधानी बना रहा, जब तक कि जयपुर की स्थापना नहीं हुई।
- प्रारंभिक काल में कछवाहा वंश चौहानों और बाद में गुहिल वंश के अधीन था। मुगल साम्राज्य के साथ गठबंधन स्थापित करने के बाद राजस्थान में उनकी प्रमुखता काफी बढ़ गई
आमेर के कछवाहा शासक (1036 -1727)

पृथ्वीराज (1503-1527)
- पृथ्वीराज के शासनकाल में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने आमेर पर आक्रमण कर उसे मेवाड़ का अधीनस्थ राज्य बना लिया। खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज सांगा के साथ लड़े। वह गलता के रामानुज संप्रदाय के संत कृष्ण दास पयहारी के भक्त थे।
- टॉड का राजस्थान किताब के अनुसार मलेसीजी और पृथ्वीराज के बीच के काल में राज्य में आंतरिक अशांति थी जिसे पृथ्वीराज ने अपने राज्य को 12 भागों में विभाजित करके शांत किया। उन्होंने इन 12 भागों को अपने 12 पुत्रों में बाँट दिया, जिसे ‘12 कोटड़ी’ के रूप में जाना जाता है।
राजा भारमल (1548 – 1574)
- भारमल पहले राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल आधिपत्य को स्वीकार किया और अपनी बेटी हरका बाई की शादी सम्राट अकबर से करके वैवाहिक गठबंधन स्थापित किया।
- हरका बाई, जिन्हें जोधा बाई और मरियम-उज़-ज़मानी के नाम से भी जाना जाता है, प्रिंस सलीम (बाद में सम्राट जहांगीर) की मां थीं।
- भगवंत दास, ये आमेर के अगले राजा हुए इन्होंने अपनी बेटी मान बाई की शादी राजकुमार सलीम (जहांगीर) से करके मुगलों के साथ संबंध मजबूत किए। उनके पुत्र राजकुमार खुसरो थे।
मिर्ज़ा राजा मान सिंह प्रथम (1589 – 1614)
- वह आमेर के प्रमुख शासकों में से एक हैं, उन्हें युद्ध, प्रशासन, साहित्य, वास्तुकला और धार्मिक सद्भाव में उनके असाधारण योगदान के लिए याद किया जाता है। उनके अपने शासनकाल के 75 वर्षों में से 55 वर्ष युद्ध लड़ने में व्यतीत हुए। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर के अधीन कार्य किया। बेहतर समझ के लिए, उनके शासनकाल को तीन अलग-अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है:
- प्रारंभिक काल/ कुंवर मानसिंह (1562-1574 ई.) :
- अकबर के शासनकाल में राजा मान सिंह ने सबसे पहले अपनी सैन्य क्षमताओं को साबित किया। रणथंभौर अभियान में रणथंभौर के शासक सुरजन हाड़ा को सफलतापूर्वक अपने अधीन कर उन्हें मुगल अधीन बना लिया।
- उन्होंने शाही सेनाओं का नेतृत्व किया, सरनाल की लड़ाई लडा और डूंगरपुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया।
- मध्य काल / भँवर मानसिंह (1574-1589 ई.) :
- अकबर ने मान सिंह को शाही सेना का सेनापति नियुक्त किया। उन्होंने प्रसिद्ध हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ मुगल सेना का नेतृत्व किया।
- बाद में उन्होंने काबुल में मिर्ज़ा हकीम को अपने अधीन कर लिया, जिसके बाद अकबर ने उन्हें काबुल का सूबेदार (गवर्नर) बना दिया।
- अकबर ने उसे सूबेदार का कार्यभार भी सौंपा बिहार का, और उसे मंदसौर की जागीर के साथ 5000 का मनसब (रैंक) प्रदान किया गया।
- बाद का काल / राजा मानसिंह (1589-1614 ई.) :
- राजा मान सिंह ने ओडिशा में विद्रोहों को कुचल दिया और क्षेत्र में शांति स्थापित की। इसके बाद, उन्हें बंगाल का सूबेदार बनाया गया।
- उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान काबुल, बंगाल और बिहार का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया।
- अकबर ने उनकी वफादारी और प्रशासनिक क्षमताओं को पहचानते हुए उनके मनसब को बढ़ाकर 7000 कर दिया। हालाँकि, जहाँगीर के साथ उनके संबंध उतने सौहार्दपूर्ण नहीं थे।
सांस्कृतिक योगदान
- साहित्य विकास : वह न केवल युद्ध और रणनीति में कुशल थे बल्कि साहित्य एवं कला के संरक्षक भी थे। उनकी संस्कृत सीखने में गहरी रुचि थी। उनका दरबार साहित्यिक प्रतिभा का केंद्र था जिसमे कई साहित्यिक कृतियों की रचना हुई।
- मानचरित्र रासौ – नरोत्तम द्वारा
- मान सिंह कीर्ति मुक्तावली – जगन्नाथ द्वारा
- मान प्रकाश और मानचरित्र – मुरारीदास द्वारा
- राग मंजरी और राग माला – पुंडरीक विट्ठल द्वारा
- स्थापत्य विरासत: उनके वास्तुशिल्प प्रयास राजपूत और मुगल शैलियों का एक अनूठा मिश्रण दर्शाते हैं। आमेर के शाही महल में दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास जैसे मुगल-प्रेरित वास्तुकला के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। उनके मंदिरों की वास्तुकला हिंदू, जैन और मुगल शैलियों यानी जगत शिरोमणि मंदिर, शिला देवी मंदिर आदि का मिश्रण दर्शाती है।
- धार्मिक विचार : राजा मान सिंह, एक कट्टर हिंदू, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे। हालाँकि उन्होंने अकबर के दीन-ए-इलाही की सदस्यता नहीं ली और मुंगेर के संत शाह दौलत के अनुरोध के बावजूद इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने मस्जिदों के लिए भी उतना ही सम्मान दिखाया जितना उन्होंने मंदिरों के लिए दिखाया। आमेर श्मशान घाट में उनकी कब्रगाह सार्वभौमिक भाईचारे का प्रतीक है, जिसमें बुद्ध और महावीर के साथ हिंदू देवताओं के चित्रण हैं।
व्यक्तित्व का मूल्यांकन :
- राजा मान सिंह का व्यक्तित्व वीरता, कूटनीति, सांस्कृतिक परिष्कार और धार्मिक सहिष्णुता का समन्वित रूप था। एक साहसी योद्धा के रूप में, उन्होंने मुग़ल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और काबुल, बंगाल, ओडिशा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध उनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण अकबर ने उन पर गहरा विश्वास रखा और उन्हें ‘फ़रज़ंद’ (पुत्र) तथा ‘मिर्ज़ा राजा’ जैसी प्रतिष्ठित उपाधियाँ प्रदान कीं, जो उनकी निष्ठा और रणनीतिक कुशलता का प्रमाण हैं। सैन्य पराक्रम के अतिरिक्त, मान सिंह ने प्रशासनिक दक्षता का भी परिचय दिया और काबुल व बंगाल जैसे प्रांतों में शांति और स्थायित्व स्थापित किया। उनकी शासन शैली समावेशी थी, जिसमें सभी समुदायों के प्रति सम्मानभाव निहित था, जो उनकी एकता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यद्यपि उन्होंने अकबर के दीन-ए-इलाही मत को स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक स्थलों का सम्मान किया। वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण तथा स्थानीय धार्मिक संरचनाओं को संरक्षण प्रदान करना उनकी धर्मनिरपेक्ष नीतियों का परिचायक है। राजा मान सिंह की वास्तुकला और संस्कृति में गहरी रुचि थी, जिसे उनके संरक्षण से निर्मित भव्य कृतियों से देखा जा सकता है। उनके संरक्षण में निर्मित आमेर किला एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें दीवान-ए-आम और दीवान-ए-ख़ास जैसे भाग मुग़ल एवं राजपूत स्थापत्य शैली के उत्कृष्ट समन्वय को दर्शाते हैं। कला और साहित्य के प्रति उनके प्रोत्साहन ने विद्वानों और कलाकारों को उनके दरबार की ओर आकर्षित किया, जिससे एक समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण निर्मित हुआ।
- निस्कर्षत:, वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल राजनेता भी थे, जिन्होंने गठबंधनों, सांस्कृतिक समावेशन और कुशल शासन की महत्ता को भली-भांति समझा।
मिर्ज़ा राजा जय सिंह प्रथम (1621 – 1667)
- राजा जय सिंह प्रथम (आमतौर पर मिर्जा राजा जय सिंह के रूप में जाना जाता है) ने तीन मुगल सम्राटों: जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की, और अपने सैन्य और प्रशासनिक कौशल के माध्यम से उनका विश्वास अर्जित किया। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि को सफलतापूर्वक संपन्न कराना उनकी राजनैतिक कुशलता का प्रमाण है।
- कला एवं सांस्कृतिक विकास : जय सिंह को वास्तुकला से विशेष प्रेम था, जो आमेर किला, जयगढ़ किला, औरंगाबाद में जयसिंहपुरा तथा अन्य स्थापत्य संरचनाओं के निर्माण में स्पष्ट रूप से झलकता है। ये संरचनाएँ उत्तर-मुग़ल कालीन राजपूत वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वे कला एवं साहित्य के महान संरक्षक थे तथा बहुभाषी विद्वानों को महत्व देते थे। उनके दरबार में बिहारी लाल जैसे प्रतिष्ठित हिंदी कवि उपस्थित थे, जिन्होंने ‘बिहारी सतसई’ की रचना की। कुलपति मिश्रा ने 52 ग्रंथों की रचना की, जबकि राम कवि ने ‘जय सिंह चरित्र’ की रचना की। दक्षिण भारत में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने भूमि बंदोबस्त और राजस्व प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे वहाँ की शासन व्यवस्था पर स्थायी प्रभाव पड़ा।
- जय सिंह की विरासत उनकी बौद्धिक गहराई, सांस्कृतिक संरक्षण और मार्शल और प्रशासनिक जिम्मेदारी को संतुलित करने की क्षमता को दर्शाती है
जयपुर के कछवाहा शासक (1727-1947)
मिर्जा राजा सवाई जय सिंह द्वितीय (1699 – 1743)
- सवाई जयसिंह द्वितीय को उसकी उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता के लिए औरंगज़ेब द्वारा ‘सवाई’ की उपाधि प्रदान की गई।
- 1707 के मुगल उत्तराधिकार युद्ध के दौरान उन्होंने राजकुमार आज़म का समर्थन किया, लेकिन बहादुर शाह प्रथम की जीत हुई । जीत के बाद बहादुर शाह प्रथम ने जय सिंह को पदच्युत कर दिया गया, और उनके भाई विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया गया, तथा इस क्षेत्र का नाम बदलकर इस्लामाबाद रखा दिया, जिसे बाद में मोमिनाबाद कर दिया गया। हालाँकि, जय सिंह ने कुशल कूटनीति का परिचय देते हुए देबारी संधि (1708) के माध्यम से मेवाड़ के महाराणा पर दबाव बनाकर पुनः आमेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।
- मुग़ल बादशाह मराठाओं के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अक्सर जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त करते थे।
राजनीतिक अभियान:
- भरतपुर उत्तराधिकार में हस्तक्षेप (1722) – राजा मोहकम सिंह के खिलाफ बदन सिंह का समर्थन किया, अंततः बदन सिंह को भरतपुर के शासक के रूप में स्थापित किया।
- बूंदी से संबंध – उन्होंने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाड़ा के दत्तक पुत्र दलेल सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया, जबकि उम्मेद सिंह इस पद के दावेदार थे। इस दौरान मराठों ने बूंदी की राजनीति में हस्तक्षेप किया।
- मराठों के साथ संबंध:
- 1715: पीलसुद के युद्ध में भाग लिया
- 1733: मंदसौर का युद्ध
- 1735: रामपुरा का युद्ध
- उन्होंने राजपूत सरदारों को मराठों के विरुद्ध संगठित करने के लिए भीलवाड़ा में हुरड़ा सम्मेलन आयोजित किया, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ।
सवाई जयसिंह की मराठा नीति
प्रारंभ में, जय सिंह द्वितीय ने अपने पहले कार्यकाल में मालवा के सूबेदार के रूप में मराठों का कड़ा विरोध किया, लेकिन 1729 में पुनः इस पद पर नियुक्त होने के बाद उन्होंने महसूस किया कि मुग़ल साम्राज्य मराठों के विस्तार को रोकने में अक्षम हो चुका है। इसके बाद उन्होंने वैकल्पिक रणनीतियों की खोज की और 1732 में महाराणा संग्राम सिंह (मेवाड़) के साथ गठबंधन किया। इस संधि के तहत 48,000 सैनिकों की एक संयुक्त सेना गठित करने और मालवा के राजस्व को साझा करने की योजना बनाई गई। हालाँकि, यह गठबंधन मूर्त रूप ले पाता, इससे पहले ही मराठों ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। मुग़लों से कोई सहायता न मिलने के कारण, जय सिंह को मराठों के साथ समझौता करना पड़ा, जिसके तहत उन्हें ₹6 लाख की धनराशि का भुगतान करना पड़ा और मालवा के 58 परगनों का राजस्व अधिकार मराठों को सौंपना पड़ा।
- 1715: पीलसुद के युद्ध में भाग लिया
- 1733: मंदसौर का युद्ध
- 1735: रामपुरा का युद्ध
- उन्होंने राजपूत सरदारों को मराठों के विरुद्ध संगठित करने के लिए भीलवाड़ा में हुरड़ा सम्मेलन आयोजित किया, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ।
- 1741 में उन्होंने पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर की संधि की, जो मराठों के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु थी। इस समझौते के तहत मुग़ल एवं मराठाओ के मध्य अधिकार सीमा तय की गई।
मराठों का राजस्थान में प्रवेश
मराठों का राजस्थान में प्रवेश राजपूत राज्यों के आंतरिक संघर्षों के कारण हुआ, जिनमें तीन प्रमुख विवाद केंद्र बूँदी, जयपुर और जोधपुर थे। बूँदी के शासक महाराव बुद्ध सिंह, जो सवाई जय सिंह द्वितीय के बहनोई थे, प्रारंभ में उनके साथ अच्छे संबंध रखते थे, लेकिन बाद में उनके रिश्तों में दरार आ गई। इसका प्रमुख कारण यह था कि बुध सिंह ने अपनी कच्छवाहा रानी से दूरी बना ली और उनके पुत्र भवानी सिंह को अपना उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। इस स्थिति को देखते हुए, जय सिंह ने उन्हें सत्ता से हटाने का निर्णय लिया। 1730 में, जब बुध सिंह बूँदी से बाहर थे, जय सिंह ने बूँदी किले पर अधिकार कर लिया और हाड़ा सलीम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को शासक घोषित कर दिया। इस सत्ता परिवर्तन को और दृढ़ करने के लिए 1732 में जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्ण कुमारी का विवाह दलेल सिंह से करवा दिया। हालांकि, इस कदम से अप्रत्यक्ष रूप से मराठों के लिए राजपूत राजनीति में हस्तक्षेप का मार्ग खुल गया।
1734 – मराठों का राजस्थान पर प्रथम आक्रमण :
सत्ता से हटाए जाने के बाद बुद्ध सिंह ने बूँदी पर पुनः अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन पंचोला के युद्ध में पराजित हो गए। 1739 में उनकी मृत्यु के बाद बूँदी में अस्थिरता और बढ़ गई। इस बीच, कच्छवाहा रानी (जो जय सिंह की बहन थीं) ने चूंडावत रानी से उत्पन्न बुद्ध सिंह के पुत्र उम्मेद सिंह का समर्थन किया और मराठों से सहायता प्राप्त करने के लिए दलेल सिंह के बड़े भाई प्रताप सिंह के माध्यम से पहल की।
18 अप्रैल 1734 को मराठों ने मल्हार राव होल्कर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में बूँदी पर आक्रमण किया, जिसके लिए उन्हें ₹6 लाख की पेशगी दी गई थी। चार दिन तक चले इस संघर्ष के बाद 22 अप्रैल 1734 को बूँदी मराठों के नियंत्रण में आ गया। यह घटना राजस्थान में मराठों के पहले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का प्रतीक बनी।
सवाई जय सिंह के सामाजिक सुधार
- सती प्रथा का उन्मूलन: जय सिंह ने विधवा-दाह प्रतिगामी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया और इसे चुनौती देने वाले पहले राजपूत शासक बने।
- विधवा पुनर्विवाह हेतु सहायता: उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी और इसे लागू करने का प्रयास किया, जिससे विधवाओं को सम्मान और जीवन में दूसरा अवसर मिला।
- अंतर-जातीय विवाहों को बढ़ावा: समाज में विभाजन को कम करने और एकता को बढ़ाने के लिए उन्होंने अंतर-जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया।
- लोक-कल्याणकारी योजनाएँ: उन्होंने जनहित के लिए कुएँ, धर्मशालाएँ, अनाथालय और सदाव्रत (भोजन दान केंद्र) स्थापित किए।
- धार्मिक संप्रदायों का नियमन: उन्होंने संन्यासियों को धन-संपत्ति संचय करने, हथियार रखने या महिलाओं से संबंध रखने पर रोक लगाई और उन्हें अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया।
- ब्राह्मण वर्ग में एकता: उन्होंने छह ब्राह्मण उप-जातियों (छन्यात) को एकजुट करने के लिए सामूहिक भोजन की परंपरा को बढ़ावा दिया, जिससे सामाजिक सौहार्द्र को बल मिला
- महिला कल्याण: विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे उन्हें आजीविका में बेहतर समर्थन मिला।
धार्मिक सुधार
- जजिया और तीर्थयात्रा करों का उन्मूलन: मुगल सम्राट मुहम्मद शाह को जजिया (1720) और गया (1728) और इलाहाबाद (1733) में तीर्थयात्रा कर समाप्त करने के लिए राजी किया, जिससे हिंदुओं को काफी लाभ हुआ।
- हिंदू परंपराओं का संरक्षण: उन्होंने राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जैसे प्राचीन अनुष्ठानों को पुनर्जीवित किया, जिससे भारतीय परंपराओं को बनाए रखा गया।
- धार्मिक सद्भाव: भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करके, धर्मों के बीच एकता को बढ़ावा देकर विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता की वकालत की गई।
- संस्कृत का प्रचार-प्रसार: वैष्णव संप्रदाय के निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण संस्कृत सीखने को प्रोत्साहित किया और धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान का प्रचार करने के लिए विद्वानों का समर्थन किया।
वास्तुकला में योगदान
- नियोजित शहर: जय सिंह ने 1727 में जयपुर की स्थापना की, जिसे वास्तुशास्त्री विद्याधर भट्टाचार्य ने शिल्पशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर योजनाबद्ध रूप से निर्मित किया। शहर को नौ चौकियों (ब्लॉक्स) में विभाजित किया गया, जहाँ विभिन्न व्यवसायों के लिए स्थान निर्धारित किए गए। 2020 में जयपुर को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया।
- किलेबंदी और महल: उन्होंने जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला और सिटी पैलेस (जिसमें चंद्र महल सबसे भव्य भाग है) का निर्माण किया। इन स्थापत्यकृतियों में मुगल और राजपूत शैली का समावेश देखा जा सकता है।
- जल वास्तुकला: उन्होंने जल महल का निर्माण आरंभ करवाया, जिसे बाद में प्रताप सिंह ने पूरा किया।
- धार्मिक वास्तुकला: उन्होंने गोविंद देव जी मंदिर, मथुरा और गोवर्धन में मंदिर, तथा सिरह ड्योढ़ी बाजार में कल्कि मंदिर का निर्माण करवाया।
कला और साहित्य का विकास
- चित्रकला का संवर्धन: उन्होंने ‘सुरतखाना’ नामक चित्रकला विभाग की स्थापना की, जिससे कलात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा मिला और कारीगरों को रोजगार मिला।
- साहित्यिक योगदान: स्वयं एक विद्वान होने के नाते, उन्होंने 1701 में “जय सिंह कारिका” की रचना की और ज्योतिष तथा खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति का समर्थन किया। उन्होंने जयपुर में वेधशालाओं का निर्माण कराया।
- धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि: उन्होंने जयपुर में भगवान कल्कि की एक प्रतिमा की स्थापना करवाई, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक सोच को दर्शाती है।
- विद्वानों दरबारी: उनके दरबार में पुंडरीक रत्नाकर, पंडित जगन्नाथ, केवलराम, नयन चंद्र मुखर्जी और मुहम्मद मेहरी जैसे प्रसिद्ध विद्वान सम्मिलित थे।
नियोजित शहर – जयपुर

- संस्थापक: जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को की थी।
- प्राचीन नाम: जयनगर।
- वास्तुकार: इसे बंगाली ब्राह्मण वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने डिज़ाइन किया था।
- डिज़ाइन संरचना: इसे चोपड़ पैटर्न पर बनाया गया, जिसमें 9 चौक (चौकड़ी) और 7 द्वार थे।
- प्रेरणा स्रोत: इस शहर का मॉडल कैंटन (चीन) और बगदाद (इराक) की तर्ज़ पर तैयार किया गया था।
- ज्योतिषीय परामर्श: पुर्तगाली ज्योतिषी ज़ेवियर डी सिल्वा ने इसके निर्माण योजना में सहायता की थी।
- स्थापना समारोह: जयपुर की आधारशिला गंगा पोल पर जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी।
- आधुनिक नगर नियोजन: जयपुर भारत का पहला योजनाबद्ध नगर है, जिसे सुव्यवस्थित शहरी योजना सिद्धांतों के अनुसार विकसित किया गया।
सवाई जय सिंह और खगोल विज्ञान
रुचि और अध्ययन: सवाई जय सिंह को बचपन से ही गणित और खगोल विज्ञान में गहरी रुचि थी। जगन्नाथ सम्राट उनके खगोल विज्ञान के गुरु थे। अपने ज्ञान को परिष्कृत करने के लिए, उन्होंने अपने विद्वानों को यूरोप और इस्लामिक देशों की खगोल प्रणालियों का अध्ययन करने भेजा और विदेशी विशेषज्ञों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। उन्होंने पारंपरिक अरबी और संस्कृत पंचांगों में दर्ज खगोलीय पिंडों की स्थितियों और आकाश में उनकी वास्तविक स्थिति के बीच विसंगतियों का विश्लेषण किया।
चुनौतियाँ: जय सिंह ने पाया कि खगोलीय अवलोकनों में प्रयुक्त पीतल के उपकरणों में मापन की अशुद्धि और घिसने-टूटने जैसी गंभीर सीमाएँ थीं।समाधान: इन समस्याओं के समाधान के लिए, जय सिंह ने पत्थर और चूने से बने बड़े और स्थिर उपकरणों का उपयोग शुरू किया, जिससे अधिक सटीक माप संभव हुआ। पहला वेधशाला, जिसे आज जंतर मंतर कहा जाता है, दिल्ली में बनाई गई। सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र और राम यंत्र जैसे उपकरणों का निर्माण किया गया ताकि खगोलीय गणनाओं की सटीकता बढ़ाई जा सके। जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी वेधशालाएँ स्थापित की गईं ताकि आँकड़ों को सत्यापित किया जा सके।
जयपुर वेधशाला:

- निर्माण : 1728
- यह जय सिंह की वेधशालाओं में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण वेधशाला है।
- इसमें 10 पत्थर और चूने के उपकरण तथा 4 धातु के उपकरण हैं।
- सम्राट यंत्र (दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी) इसका मुख्य आकर्षण है, जो समय को अत्यधिक सटीकता से माप सकता है।
- जुलाई 2010 में यूनेस्को ने जयपुर वेधशाला को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया।
सवाई जयसिंह के व्यक्तित्व का मूल्यांकन
सवाई जय सिंह द्वितीय एक दूरदर्शी और व्यावहारिक शासक थे, जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और कला, विज्ञान तथा जनकल्याण में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। औरंगजेब ने उनकी वाकपटुता से प्रभावित होकर उन्हें “सवाई” की उपाधि प्रदान की। उन्होंने 1727 में जयपुर की स्थापना की, जो वैदिक सिद्धांतों पर आधारित भारत का पहला योजनाबद्ध नगर था। राजनीतिक रूप से दक्ष, उन्होंने भरतपुर के उत्तराधिकार विवाद (1722) और बूंदी के राजनीतिक संकट (1730) में हस्तक्षेप कर अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। प्रारंभ में उन्होंने मराठाओं का सैन्य रूप से विरोध किया, लेकिन बाद में 1732 में मेवाड़ के साथ संधि कर कूटनीतिक नीति अपनाई, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता बनी रही।
सवाई जय सिंह कला और संस्कृति के संरक्षक थे। उन्होंने सुरतखाना चित्रकला विभाग की स्थापना कर कलाकारों को प्रोत्साहित किया और अपने दरबार को विद्वानों से सुशोभित किया। स्थापत्य कला एवं चित्रकला के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामाजिक कल्याण की दिशा में भी उनका शासन उल्लेखनीय रहा। उन्होंने कई लोक-कल्याणकारी योजनाएँ लागू कीं, जिससे जनता की समृद्धि सुनिश्चित हुई। वह स्वयं एक विद्वान और खगोलशास्त्री थे। उन्होंने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में वेधशालाएँ स्थापित कर अपनी वैज्ञानिक दृष्टि को मूर्त रूप दिया। सवाई जय सिंह की अनुकूलनशीलता और राजस्थान के राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास में उनके योगदान ने उन्हें एक असाधारण शासक बना दिया। उनकी शासन शैली प्रगतिशीलता और नवाचार की स्थायी विरासत को दर्शाती है।
सवाई ईश्वर सिंह (1743 – 1750)
- सवाई माधोसिंह जी के द्वारा किया देबारी समझौता (1708 ई.) जयपुर के लिए घातक साबित होता है, इसी समझौते के कारण सवाई ईश्वरी जी एवं माधोसिंह जी का अधिकांश समय शासन के उत्तराधिकार के युद्ध में निकल जाता है।
- यही उत्तराधिकार का युद्ध जयपुर में मराठों के हस्तक्षेप का कारण बनती है।
- उत्तराधिकार विवाद: मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुमारी का विवाह जय सिंह के साथ इस शर्त पर तय हुआ कि उसका पुत्र आमेर का भावी शासक होगा। माधो सिंह चंद्रकुमारी के पुत्र थे।
- जय सिंह की मृत्यु के बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र ईश्वरी सिंह शासक बना। हालाँकि, उपरोक्त शर्त के कारण, माधो सिंह खुद को आमेर का असली शासक मानते थे, जिसके कारण दोनों के बीच सिंहासन को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। ईश्वरी सिंह जय सिंह द्वितीय की मारवाड़ी रानी सूरज कुंवरी के पुत्र थे।
- राजमहल का युद्ध (1747)
- बनास नदी के तट पर हुआ यह युद्ध माधो सिंह हार गए। ईश्वर सिंह ने इसरलाट/सरगासूली (सात मंजिला अष्टकोणीय संरचना) का निर्माण कराया।
- बगरू का युद्ध (1748)
- माधो सिंह विजयी हुए।
- ईश्वर सिंह ने संधि के तहत माधो सिंह को 20 लाख रुपये, 3 जागीरें तथा मराठा सरदार मल्हार राव होल्कर को 2 जागीरें देने का वचन दिया।
- 1750 में मराठा दबाव में आकर, ईश्वर सिंह ने अपनी दो पत्नियों के साथ इसरलाट/सरगासूली से कूदकर आत्महत्या कर ली।
सवाई माधो सिंह प्रथम (1750 – 1768)
- मुग़ल सम्राट द्वारा रणथंभौर का किला पुरस्कार में दिया गया था
- 1765 में सवाई माधोपुर शहर के संस्थापक।
- शेख शादी के गुलिस्तां का संस्कृत में अनुवाद करवाया।
- कछवाहा साम्राज्य को मराठों से मुक्त कराया
- कान्कोड़ का युद्ध (1759) :- मुगल सम्राट अहमद शाह ने 1754 में रणथंभौर को माधो सिंह को दे दिया, लेकिन मराठा भी रणथंभौर पर कब्जा करना चाहते थे। परिणामस्वरूप, 1759 में मल्हार राव होल्कर की सेना और माधो सिंह के बीच कान्कोड़ (टोंक) का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना की हार हुई।
- भटवाड़ा का युद्ध (1761) :- माधोसिंह ने रणथम्भौर के अधीन पुराने क्षेत्र पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। इससे क्रोधित होकर कोटा के शत्रुसाल ने झाला जालिम सिंह को भेजा। जालिम सिंह ने 2 दिसंबर 1761 को भटवाड़ा के युद्ध में माधव सिंह की सेना को हराया।
- माचेड़ी के सामंत ने जयपुर के कछवाहा वंश से अलग होकर अलवर में एक स्वतंत्र कछवाहा राज्य की स्थापना की।
सवाई प्रताप सिंह (1778 -1803)
- तुंगा का युद्ध (28 जुलाई 1787)
- महादजी सिंधिया और महाराजा प्रताप सिंह के बीच हुआ, जिसमें सिंधिया पराजित हुआ।
- हार के बाद सिंधिया ने कहा, “अगर मैं बच गया, तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूँगा।“
- पाटन का युद्ध (जून 1790)
- जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह और जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने मराठों के खिलाफ संयुक्त रूप से युद्ध किया, लेकिन पराजित हुए।
- मालपुरा का युद्ध (1800)
- इस संघर्ष में दौलत राव सिंधिया के नेतृत्व में मराठों ने जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह और जोधपुर के महाराजा भीम सिंह की संयुक्त सेना को हराया।
कला एवं सांस्कृतिक विकास :
- कविता और साहित्य
- प्रताप सिंह स्वयं एक कवि थे, जिन्होंने ब्रजनिधि नाम से रचनाएँ कीं। उनकी कृतियाँ प्रीतिलता, स्नेह संग्राम, फग रंग, प्रेम प्रकाश, और रंग चौपड़ा थीं। उनकी रचनाएँ ब्रजनिधि ग्रंथावली में संकलित हैं और ढूँढाड़ी तथा ब्रज भाषा में लिखी गई हैं।
- संगीत और संगीत सम्मेलन
- वे संगीत के संरक्षक थे और उनके गुरु उस्ताद चांद खां ने स्वर सागर की रचना की। उन्होंने जयपुर में संगीत सम्मेलनों का आयोजन किया, जिनकी अध्यक्षता देव ऋषि बृजपाल भट्ट ने की, और राधा गोविंद संगीत सार की रचना हुई।
- लोक रंगमंच
- उनके शासनकाल में तमाशा लोक नाट्य को बढ़ावा मिला और उन्होंने महाराष्ट्र से बंशीधर भट्ट को आमंत्रित कर इस कला को समृद्ध किया।
- चित्रकारी और कला
- उनके शासनकाल में जयपुर चित्रकला का स्वर्ण युग था। चित्रों में प्रमुख विषय राग-रागिनी, दुर्गा सप्तशती, रामायण, राधा-कृष्ण लीला, और बारहमासा थे। दरबारी चित्रकार लालचंद अपने युद्ध और पशु चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे।
- वास्तुकला
- शैली – हिंदू राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण।
- उन्होंने हवा महल और जल महल का निर्माण करवाया।

- वास्तुकार – लाल चंद
- पाँच मंजिला संरचना, 953 खिड़कियाँ और 365 झरोखे हैं
- विशेषता – समतल भूमि पर बिना नींव के निर्मित।
- भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखता है (कर्नल टॉड)
- इसके विभिन्न तल शरद प्रताप मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर हैं।
सवाई जय सिंह तृतीय (1819 -1835)
- गिंगोली का युद्ध (1807): यह युद्ध जयपुर (जगत सिंह) और जोधपुर (मान सिंह) के बीच कृष्ण कुमारी विवाद पर लड़ा गया।
- 1818 में सहायक संधि: मराठों और पिंडारियों से राज्य की रक्षा के लिए जगत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की और राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों को सौंप दी।
सवाई राम सिंह द्वितीय (1835 -1880)
- सवाई राम सिंह द्वितीय के शासन की शुरुआत में प्रशासन मेजर जॉन लुडलो द्वारा संभाला गया, जिन्होंने सती प्रथा, दासता, बाल विवाह और दहेज जैसी सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगाई।
- 1857 की क्रांति के दौरान, उन्होंने ब्रिटिशों का समर्थन किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सितार-ए-हिंद की उपाधि और कोटपुतली जागीर प्रदान की गई।
उनकी उपलब्धियां :
- समाज सुधार
- इनके शासन काल में सती प्रथा, दास, बाल विवाह और दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया।
- वास्तुकला और सांस्कृतिक योगदान
- लॉर्ड नॉर्थब्रुक (1875) और प्रिंस अल्बर्ट (1876) की यात्राओं की स्मृति में अल्बर्ट हॉल और राम निवास गार्डन का निर्माण कराया गया।
- उन्होंने 1857 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट और उत्तर भारत का पहला थिएटर, रामप्रकाश थिएटर स्थापित किया।
- 1868 में, जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया गया, जिससे इसे गुलाबी नगरी के रूप में जाना जाने लगा।
- उन्होंने रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया।
- शैक्षिक विकास
- उन्होंने महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, और महाराजा पुस्तकालय (1844) की स्थापना की।
सवाई मान सिंह द्वितीय (1922-1947)
- वे 30 मार्च 1949 को राजस्थान के पहले राजप्रमुख बने और 1 नवंबर 1956 तक इस पद पर रहे।
- 1962 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और 1965 में भारत के स्पेन में राजदूत बने।
- उन्होंने मिर्ज़ा इस्माइल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
- इन्होंने कई महत्वपूर्ण संस्थान जैसे सवाई मान सिंह अस्पताल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, एसएमएस स्कूल, और एसएमएस स्टेडियम की स्थापना की।
- उन्होंने अपनी पत्नी गायत्री देवी के लिए मोती डूंगरी पर अंग्रेजी स्थापत्य शैली में तख्त-ए-शाही महल बनवाया। उन्होंने जयपुर में सिटी पैलेस संग्रहालय की स्थापना की।
बूंदी का हाड़ा
प्राचीन काल में बूंदी क्षेत्र में विभिन्न स्थानीय जनजातियाँ निवास करती थीं, जिनमें से अधिकांश मीणा जनजाति से संबंधित थीं। बूंदी का नाम एक पूर्व मीणा जनजाति के मुखिया बूंदा मीणा के नाम पर रखा गया माना जाता है। पहले इसे “बूंदा-का-नाल” कहा जाता था, जहाँ “नाल” का अर्थ संकीर्ण रास्ते होता है। बाद में, इस क्षेत्र को राव देवा हाड़ा ने 1342 में जयता मीणा से जीतकर हाड़ा वंश की एक रियासत के रूप में स्थापित किया और आसपास के क्षेत्र को हाड़ौती (महान हाड़ा राजपूतों की भूमि) नाम दिया।
बूंदी के शासक
- राव देवा हाड़ा (1342-43)
- 1342 में जेता मीणा से बूंदी जीतकर हाड़ा वंश की नींव रखी।
- राव राजा रतन सिंह (1608 से 1632)
- रतन सिंह और उनके पुत्र माधो सिंह ने जहांगीर के शासनकाल में विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की।
- जहांगीर ने हाड़ौती को दो भागों में बाँटकर कोटा को एक अलग राज्य के रूप में माधो सिंह को सौंप दिया।
- शाहजहाँ ने कोटा की जागीर को माधो सिंह को आधिकारिक रूप से प्रदान किया।
- राव राजा रतन सिंह (1608 से 1632)
- रतन सिंह और उनके बेटे माधो सिंह – जहांगीर शासनकाल के दौरान विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध लड़े और जीत हासिल की।
- जहांगीर ने हाड़ौती को बूंदी और कोटा में विभाजित कर कोटा को माधो सिंह को अलग राज्य दे दिया
- शाहजहाँ ने माधो सिंह को कोटा देने की पुष्टि की।
- राव राजा छत्तर साल सिंह (1632 से 1658)
- मुगल राजकुमार दारा शिकोह (सम्राट शाहजहाँ का पुत्र) ने छत्तर सिंह को दिल्ली का गवर्नर नियुक्त किया।
- बाद में, वे शाहजहाँ के उत्तराधिकारी औरंगजेब के खिलाफ युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।
- बूंदी चित्रकला राव छत्रसाल के समय फली-फूली थी। इन्होंने प्रसिद्ध भित्ति चित्र रंगमहल का निर्माण कराया था
- राव राजा भाऊ सिंह (1658-1682)
- औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध लड़ा और राजा आत्माराम को पराजित किया।
- औरंगजेब, भाऊ सिंह की वीरता से प्रभावित हुआ और उनसे मेल-मिलाप कर उन्हें औरंगाबाद का गवर्नर नियुक्त किया।
- राव राजा बुद्ध सिंह (1696-1735)
- औरंगजेब की मृत्यु के बाद बुद्ध सिंह ने बहादुर शाह प्रथम का समर्थन किया, जबकि कोटा के राम सिंह ने राजकुमार आज़म का साथ दिया।
- इस कारण से बूंदी और कोटा के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई।
भरतपुर के जाट शासक
17वीं शताब्दी के अंत में, जाट सरदार बैजा और उनके पुत्र राजाराम (गाँव सिनसिनी के ज़मींदार) ने मुग़ल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर अपने क्षेत्र का विस्तार किया। भगवान राम के भाई लक्ष्मण को भरतपुर के पूर्व शाही परिवार का कुलदेवता माना जाता है। राज्य के हथियारों, मुहरों और प्रतीकों पर ‘लक्ष्मण’ नाम अंकित किया जाता था।
चूड़ामन (1695–1721)
- 18वीं शताब्दी में बदन सिंह और चूड़ामन के नेतृत्व में भरतपुर में जाट शक्ति का विस्तार हुआ।
- 1707 के आसपास, चूड़ामन ने थून किला बनवाकर अपना राज्य स्थापित किया।
- मुग़ल सम्राट फ़र्रुख़सियर ने चूड़ामन को “राव बहादुर” की उपाधि दी।
- हालांकि, 1721 में मुगलों ने जाट सरदार चूड़ामन की हत्या करवा दी।
बदन सिंह (1722–1756)
महाराजा सूरज मल (1756–1767)
- महाराजा सूरज मल एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और अपराजेय शासक थे।
- जयपुर राज्य में ईश्वर सिंह की गद्दी को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- कुंभेर की विजय (1754): मराठा नेता होल्कर के हमले को सफलतापूर्वक विफल किया।
- अब्दाली के खिलाफ संघर्ष: नजीब-उद-दौला की योजना को नाकाम किया, जिससे भारत को अब्दाली के प्रभाव में इस्लामी राज्य बनने से बचाया।
- आगरा किले पर अधिकार (12 जून 1761): सूरज मल ने आगरा किले पर कब्ज़ा कर लिया।
- उनकी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक सूझबूझ और प्रशासनिक क्षमता के कारण उन्हें “जाट जाति का प्लेटो” (जाटों का अफलातून) कहा गया।
- बूंदी के दरबारी कवि सूर्यमल ने उनकी वीरता पर कविता लिखी
“नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर
जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर”
- डीग के जलमहल उनके शासनकाल की उत्कृष्ट स्थापत्य कला का प्रमाण हैं।
- ये महल विशाल आंगनों, मुग़ल शैली के सुंदर बागों और फव्वारों से सुसज्जित हैं।
- इनमें मुग़ल और राजपूत स्थापत्य शैलियों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है।

- लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया।
- 1733 ई. में भरतपुर में निर्मित यह किला अपने पूरे इतिहास में अजेय रहा।
- इसकी सुरक्षा को 100 फुट चौड़ी और 60 फुट गहरी खाई के साथ-साथ चिनाई और मिट्टी के निर्माण के संयोजन वाली दोहरी परत वाली दीवार द्वारा मजबूत किया गया था।

महाराजा जवाहर सिंह (1767-1768)
- जवाहर सिंह के समय में जाट शक्ति का पतन प्रारम्भ हो गया।
- उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली के लाल किले से 8 धातु के दरवाजे लाकर भरतपुर किले में रखवाये।
- मराठों, रोहिल्लाओं और राजपूतों से लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ा।
महाराजा रणजीत सिंह (1776–1805)
- 1803 ई. में अंग्रेजों के साथ संधि पर हस्ताक्षर किये।
- 1805 में, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में, लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर आक्रमण किया, क्योंकि रणजीत सिंह ने इंदौर के जसवंत राव होल्कर को शरण दी थी।
- चार महीने की घेराबंदी के बाद भी लॉर्ड लेक किला जीतने में असफल रहा, जिससे यह किला “लोहगढ़” (अजेय गढ़) कहलाया।
- 4 मई 1805 को रणजीत सिंह को शांति संधि करनी पड़ी और नई संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
महाराजा रणधीर सिंह (1805–1823)
- रणधीर सिंह ने 1818 ई. में अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किये।
महाराजा बृजेन्द्र सिंह (1929–1947)
- राजस्थान का पहला एकीकृत राज्य “मत्स्य संघ” बना, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल हुए और भारतीय संघ का हिस्सा बने।
FAQ (Previous year questions)
राव मालदेव राठौड़, मारवाड़ के एक शक्तिशाली शासक, ने अपनी रणनीतिक सूझबूझ से हुमायूं और शेरशाह सूरी जैसे समकालीन शासकों के साथ चतुराईपूर्ण संबंध बनाए। ये संबंध न तो सीधे-सादे थे और न ही भावनाओं पर आधारित, बल्कि उस दौर के अस्थिर राजनीतिक माहौल में मारवाड़ की संप्रभुता को बचाने के लिए यथार्थवादी नीतियों (Realpolitik) से प्रेरित थे।
हुमायूं से संबंध – सतर्कता के साथ गठबंधन:
1541 में शेरशाह से हारकर भाग रहे हुमायूं को मारवाड़ के राव मालदेव ने 20,000 सैनिकों के साथ सैन्य और राजनीतिक सहायता दी।
यह मदद केवल सहानुभूति नहीं थी, बल्कि मालदेव ने इसे हुमायूं को सत्ता में लौटाकर एक शक्तिशाली सहयोगी पाने और मारवाड़ की प्रतिष्ठा को राणा सांगा की तरह ऊँचा उठाने के अवसर के रूप में देखा।
लेकिन 1542 में हुमायूं की देरी और शेरशाह की उत्तरी भारत में मज़बूत स्थिति के कारण यह गठबंधन असफल रहा।
जोखिम को भाँपकर मालदेव ने समर्थन वापस ले लिया—कुछ इतिहासकार इसे विश्वासघात कहते हैं, पर यह वास्तव में एक रणनीतिक कदम था।
शेरशाह से संबंध – तनाव एवं रणनीतिक टकराव:
मारवाड़ में राव मालदेव की बढ़ती ताकत शेरशाह के पश्चिमी विस्तार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई।
हालाँकि मालदेव शुरू में तटस्थ रहे, लेकिन शेरशाह ने उन्हें खतरे के रूप में देखा और 1544 में मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी, जिसके परिणामस्वरूप सैमल (गिरी-सुमेल) का युद्ध हुआ।
शेरशाह ने मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाई और मालदेव के शिविर में भ्रम फैलाने के लिए जाली पत्र भेजे। इस कारण मालदेव को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उनके सेनानायकों जैता और कूंपा ने अद्भुत वीरता दिखाई।
उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर शेरशाह ने कहा, “मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता”
